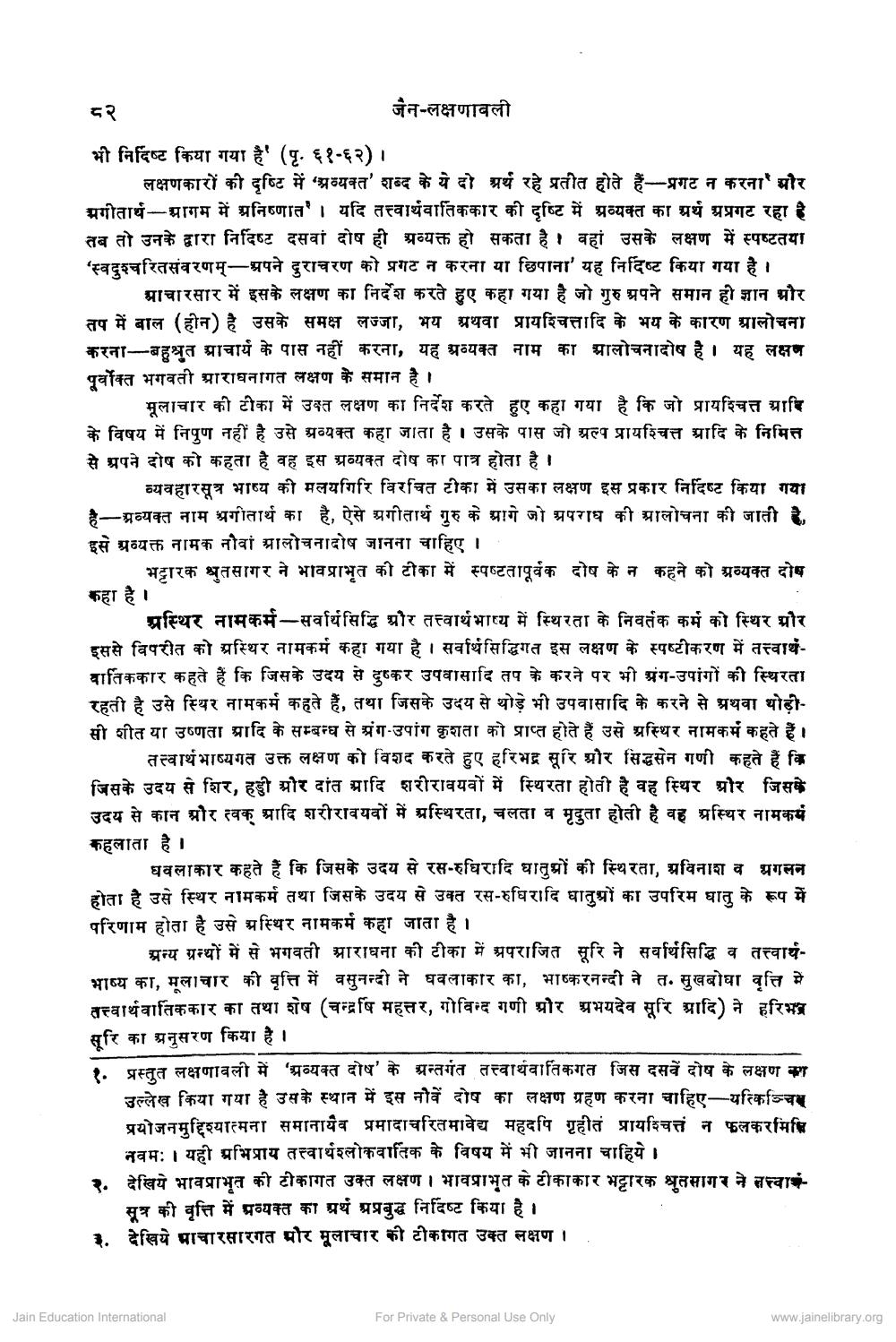________________
८२
भी निर्दिष्ट किया गया है' (पृ. ६१-६२) ।
लक्षणकारों की दृष्टि में 'अव्यक्त' शब्द के ये दो अर्थ रहे प्रतीत होते हैं-प्रगट न करना मौर गीतार्थ - आगम में अनिष्णात' । यदि तत्त्वार्थवार्तिककार की दृष्टि में अव्यक्त का अर्थ अप्रगट रहा है तब तो उनके द्वारा निर्दिष्ट दसवां दोष ही अव्यक्त हो सकता है। वहां उसके लक्षण में स्पष्टतया 'स्वदुश्चरितसंवरणम् - अपने दुराचरण को प्रगट न करना या छिपाना' यह निर्दिष्ट किया गया है । आचारसार में इसके लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है जो गुरु अपने समान हो ज्ञान भौर तप में बाल (हीन) है उसके समक्ष लज्जा, भय अथवा प्रायश्चित्तादि के भय के कारण प्रालोचना करना - बहुश्रुत आचार्य के पास नहीं करना, यह अव्यक्त नाम का आलोचनादोष है । यह लक्षण पूर्वोक्त भगवती श्राराधनागत लक्षण के समान है ।
जैन - लक्षणावली
मूलाचार की टीका में उक्त लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो प्रायश्चित्त ग्रादि के विषय में निपुण नहीं है उसे अव्यक्त कहा जाता है । उसके पास जो अल्प प्रायश्चित्त प्रादि के निमित्त से अपने दोष को कहता है वह इस अव्यक्त दोष का पात्र होता है ।
व्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीका में उसका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया - अव्यक्त नाम अगीतार्थ का है, ऐसे प्रगीतार्थ गुरु के आगे जो अपराध की आलोचना की जाती है, इसे अव्यक्त नामक नौवां मालोचनादोष जानना चाहिए ।
भट्टारक श्रुतसागर ने भावप्राभृत की टीका में स्पष्टतापूर्वक दोष के न कहने को अव्यक्त दोष कहा 1
अस्थिर नामकर्म - सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थ भाष्य में स्थिरता के निवर्तक कर्म को स्थिर र इससे विपरीत को अस्थिर नामकर्म कहा गया है । सर्वार्थसिद्धिगत इस लक्षण के स्पष्टीकरण में तत्त्वार्थवार्तिककार कहते हैं कि जिसके उदय से दुष्कर उपवासादि तप के करने पर भी अंग- उपांगों की स्थिरता रहती है उसे स्थिर नामकर्म कहते तथा जिसके उदय से थोड़े भी उपवासादि के करने से अथवा थोड़ीसी शीत या उष्णता आदि के सम्बन्ध से अंग- उपांग कृशता को प्राप्त होते हैं उसे अस्थिर नामकर्म कहते हैं । तत्त्वार्थभाष्यगत उक्त लक्षण को विशद करते हुए हरिभद्र सूरि औौर सिद्धसेन गणी कहते हैं कि जिसके उदय से शिर, हड्डी और दांत आदि शरीरावयवों में स्थिरता होती है वह स्थिर और जिसके उदय से कान और त्वक् श्रादि शरीरावयवों में अस्थिरता, चलता व मृदुता होती है वह अस्थिर नामकर्म कहलाता है ।
धवलाकार कहते हैं कि जिसके उदय से रस- रुधिरादि धातुनों की स्थिरता, अविनाश व प्रगलन होता है उसे स्थिर नामकर्म तथा जिसके उदय से उक्त रस- रुधिरादि धातुनों का उपरिम धातु के रूप में परिणाम होता है उसे अस्थिर नामकर्म कहा जाता है ।
अन्य ग्रन्थों में से भगवती आराधना की टीका में अपराजित सूरि ने सर्वार्थसिद्धि व तत्त्वार्थभाष्य का, मूलाचार की वृत्ति में वसुनन्दी ने घवलाकार का, भाष्करनन्दी ने त. सुखबोघा वृत्ति में तत्त्वार्थवार्तिककार का तथा शेष ( चन्द्रर्षि महत्तर, गोविन्द गणी और अभयदेव सूरि आदि) ने हरिभन सूरि का अनुसरण किया है।
१. प्रस्तुत लक्षणावली में 'अव्यक्त दोष' के अन्तर्गत तत्त्वार्थवार्तिकगत जिस दसवें दोष के लक्षण का उल्लेख किया गया है उसके स्थान में इस नौवें दोष का लक्षण ग्रहण करना चाहिए— यत्किञ्चिद प्रयोजनमुद्दिश्यात्मना समानायैव प्रमादाचरितमावेद्य महदपि गृहीतं प्रायश्चित्तं न फलकरमिति नवमः । यही अभिप्राय तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक के विषय में भी जानना चाहिये ।
२. देखिये भावप्राभृत की टीकागत उक्त लक्षण । भावप्राभूत के टीकाकार भट्टारक श्रुतसागर ने तत्त्वार्थसूत्र की वृत्ति में प्रव्यक्त का अर्थ अप्रबुद्ध निर्दिष्ट किया है ।
३. देखिये प्राचारसारगत धौर मूलाचार की टीकागत उक्त लक्षण ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org