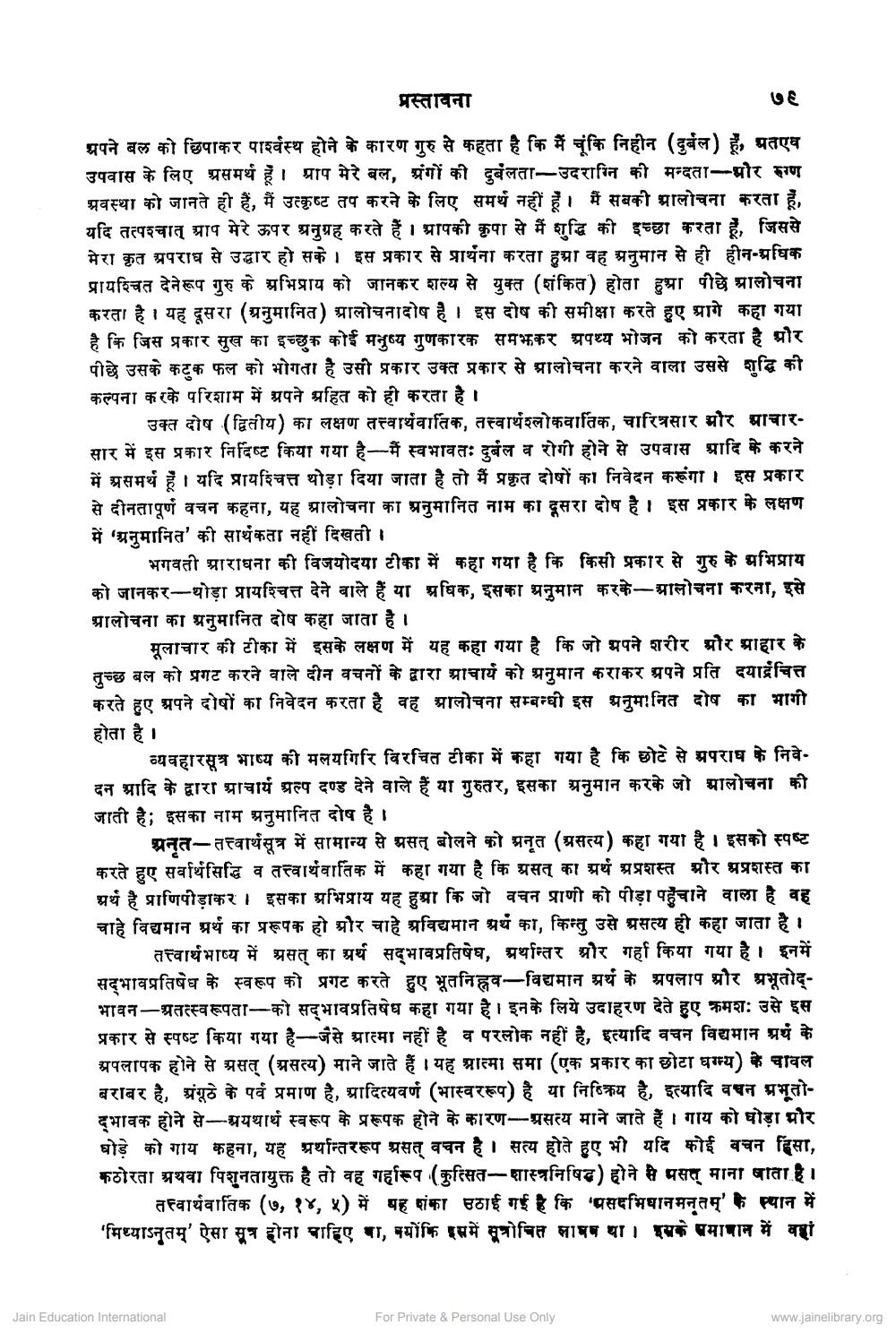________________
प्रस्तावना
अपने बल को छिपाकर पार्श्वस्थ होने के कारण गुरु से कहता है कि मैं चूंकि निहीन (दुर्बल) हूँ, प्रतएव उपवास के लिए असमर्थ हूँ। प्राप मेरे बल, अंगों की दुर्बलता-उदराग्नि की मन्दता-पौर रुग्ण अवस्था को जानते ही हैं, मैं उत्कृष्ट तप करने के लिए समर्थ नहीं है। मैं सबकी मालोचना करता है, यदि तत्पश्चात् आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं । आपकी कृपा से मैं शुद्धि की इच्छा करता हूँ, जिससे मेरा कृत अपराध से उद्धार हो सके। इस प्रकार से प्रार्थना करता हा वह अनुमान से ही हीन-अधिक प्रायश्चित देनेरूप गुरु के अभिप्राय को जानकर शल्य से युक्त (शंकित) होता हुआ पीछे पालोचना करता है । यह दूसरा (अनुमानित) पालोचनादोष है । इस दोष की समीक्षा करते हुए आगे कहा गया है कि जिस प्रकार सुख का इच्छुक कोई मनुष्य गुणकारक समझकर अपथ्य भोजन को करता है और पीछे उसके कटुक फल को भोगता है उसी प्रकार उक्त प्रकार से पालोचना करने वाला उससे शुद्धि की कल्पना करके परिशाम में अपने अहित को ही करता है।
उक्त दोष (द्वितीय) का लक्षण तत्त्वार्थवार्तिक, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, चारित्रसार मौर प्राचारसार में इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है-मैं स्वभावतः दुर्बल व रोगी होने से उपवास प्रादि के करने में असमर्थ हैं। यदि प्रायश्चित्त थोड़ा दिया जाता है तो मैं प्रकृत दोषों का निवेदन करूंगा। इस प्रकार से दीनतापूर्ण वचन कहना, यह आलोचना का अनुमानित नाम का दूसरा दोष है। इस प्रकार के लक्षण में 'अनुमानित' की सार्थकता नहीं दिखती।
भगवती पाराधना की विजयोदया टीका में कहा गया है कि किसी प्रकार से गुरु के अभिप्राय को जानकर-थोड़ा प्रायश्चित्त देने वाले हैं या अधिक, इसका अनुमान करके-पालोचना करना, इसे पालोचना का अनुमानित दोष कहा जाता है।
मूलाचार की टीका में इसके लक्षण में यह कहा गया है कि जो अपने शरीर और माहार के तुच्छ बल को प्रगट करने वाले दीन वचनों के द्वारा प्राचार्य को अनुमान कराकर अपने प्रति दयाचित्त करते हुए अपने दोषों का निवेदन करता है वह आलोचना सम्बन्धी इस अनुमानित दोष का भागी होता है।
__व्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीका में कहा गया है कि छोटे से अपराध के निवे. दन आदि के द्वारा प्राचार्य अल्प दण्ड देने वाले हैं या गुरुतर, इसका अनुमान करके जो मालोचना की जाती है। इसका नाम अनुमानित दोष है ।
अनृत-तत्त्वार्थसूत्र में सामान्य से असत् बोलने को अनृत (असत्य) कहा गया है । इसको स्पष्ट करते हुए सर्वार्थसिद्धि व तत्त्वार्थवार्तिक में कहा गया है कि असत् का अर्थ अप्रशस्त और अप्रशस्त का अर्थ है प्राणिपीड़ाकर । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो वचन प्राणी को पीड़ा पहुंचाने वाला है वह चाहे विद्यमान अर्थ का प्ररूपक हो और चाहे अविद्यमान अर्थ का, किन्तु उसे असत्य ही कहा जा
तत्त्वार्थभाष्य में असत् का अर्थ सद्भावप्रतिषेध, अर्थान्तर और गर्दा किया गया है। इनमें सदभावप्रतिषेध के स्वरूप को प्रगट करते हुए भूतनिह्नव-विद्यमान अर्थ के अपलाप और अभूतो भावन-अतत्स्वरूपता-को सद्भावप्रतिषेध कहा गया है। इनके लिये उदाहरण देते हुए क्रमशः उसे इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है-जैसे प्रात्मा नहीं है व परलोक नहीं है, इत्यादि वचन विद्यमान अर्थ के अपलापक होने से असत् (असत्य) माने जाते हैं । यह प्रात्मा समा (एक प्रकार का छोटा घम्य) के चावल बराबर है, अंगूठे के पर्व प्रमाण है, आदित्यवर्ण (भास्वररूप) है या निष्क्रिय है, इत्यादि वचन प्रभूतो
द्भावक होने से-अयथार्थ स्वरूप के प्ररूपक होने के कारण-असत्य माने जाते हैं। गाय को घोड़ा भोर घोड़े को गाय कहना, यह अर्थान्तररूप असत् वचन है। सत्य होते हुए भी यदि कोई वचन हिंसा, कठोरता अथवा पिशुनतायुक्त है तो वह गह रूप (कुत्सित-शास्त्रनिषिद्ध) होने से प्रसत् माना जाता है।
तत्वार्थवार्तिक (७, १४, ५) में यह शंका उठाई गई है कि 'प्रसदभिधानमनतम्' के स्थान में 'मिथ्याऽनृतम्' ऐसा सूत्र होना चाहिए था, क्योंकि इसमें सूत्रोचित भाषण था। इसके पमाधान में वहां
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org