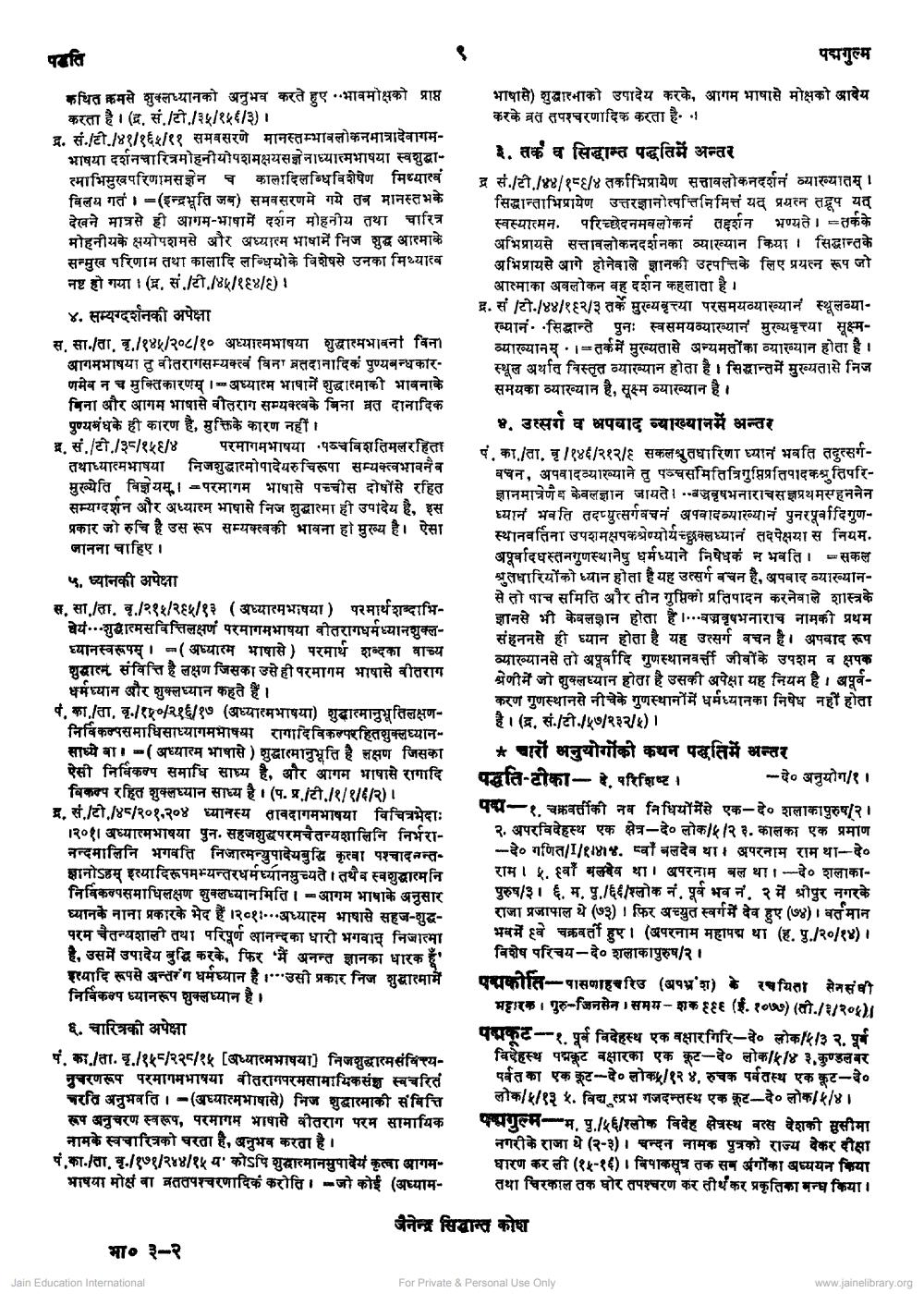________________
पद्धति
कथित कमसे शुभ्यानको अनुभव करते हुए अनमोलको प्राप्त करता है। (द्र.सं./टी./२७/९५/२ प्र.सं./टी./४१/१६२/९१ समवसरणे मानस्तन्यावसीकन मात्रादेवामभाषया दर्शनचारित्रमोहनी यो पक्षमक्षयज्ञेन ध्यारमभाषया स्वशुद्धा त्माभिमुखपरिणामस ज्ञेन च कालादिलब्धिविशेषेण मिध्यात्वं विलय गतं । - ( इन्द्रभूति जब) समवसरणमे गये तब मानस्तभके देखने मात्र से ही आगम-भाषा में दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीयके क्षयोपशमसे और अध्यात्म भाषामें निज शुद्ध आत्माके सन्मुख परिणाम तथा कालादि लब्धियोके विशेषसे उनका मिथ्यात्व नष्ट हो गया (प्र.सं./टी./२५/९६४/६
४. सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा
स. सा./ता.वृ./१४५/२०८/१० अध्यात्मभाषया शुद्धात्मभावना विना आगमभाषया तु वीतरागसम्यक्त्वं विना बतदानादिकं पुण्यबन्धकारणमेव न च मुक्तिकारणम् । अध्यात्म भाषामें शुद्धात्माकी भावनाके बिना और आगम भाषासे वीतराग सम्यक्त्वके बिना व्रत दानादिक पुण्यगंधके ही कारण है, मुसिके कारण नहीं। प्र. सं./टी./३८ / १५६/४
तथाध्यात्मभाषया
परमागमभाषया पञ्चविशतिमलरहिता निजशुद्धात्मोपावरुचिता सम्यवधानमेव मुस्येति विज्ञेयम्। परमागम भाषासे पच्चीस दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन और अध्यात्म भाषासे निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार जो रुचि है उस रूप सम्यक्त्वकी भावना हो मुख्य है। ऐसा जानना चाहिए।
५. ध्यानकी अपेक्षा
स. सा./ता.वृ./२१५/२१२/१३ (अध्यात्म भाषा) परमार्थशब्दाभि चेयं... शुद्धात्मस वित्तिलक्षणं परमागमभाषया वीतरागधर्मध्यानशुक्लध्यानस्वरूपम् । (अध्यात्म भाषासे) परमार्थ शब्दका वाच्य शुद्धा संवित्ति है लक्षण जिसका उसे ही परमागम भाषासे वीतराग धर्मध्यान और शुक्लध्यान कहते हैं। पं.का./ता.वृ./१२०/२१६/१० (अध्यात्मभाषा शुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिर्विकल्पसमाधिसाध्यागमभाषया रागादिविकल्परहितसुध्यानसाध्ये वा । - ( अध्यात्म भाषासे) शुद्धात्मानुभूति है लक्षण जिसका ऐसी निर्मिक समाधि साध्य है, और आगम भाषासे रागादि विकल्परहित शुक्लध्यान साध्य है (प. प्र./टी./१/१२/१/२) प्र. सं./टी./ ४८/२०१,२०४ ध्यानस्य तावदागमभाषया विचित्रभेदाः २०१। बध्यात्मभावया पुन. सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि निर्भरानन्दमाशिनि भगवति निजात्मन्यपादेयमुद्धि कृत्वा परचाद ज्ञानोऽहम् इत्यादिरूपमयन्तरधर्मानमुच्यते। तथैवमनि निर्विकल्पसमाधिलक्षण शुक्लध्यानमिति । - आगम भाषाके अनुसार ध्यानके नाना प्रकारके भेद हैं । २०१३... अध्यात्म भाषासे सहज-शुद्धपरम चैतन्यशाली तथा परिपूर्ण आनन्दका धारी भगवान् निजात्मा है, उसमें उपादेय बुद्धि करके, फिर 'मैं अनन्त ज्ञानका धारक हूँ' इत्यादि रूपसे अन्तरंग धर्मध्यान है। उसी प्रकार निज शुद्धात्मामे निर्विकल्प ध्यानरूप शुक्लध्यान है।
६. चारित्रको अपेक्षा
पं.का./ता.वृ./१०/२२०/१५ ध्यात्मभाषया निद्वारमसंवि नुचरणरूप परमागमभाषया वीतरागपरमसामायिकसंज्ञ स्वचरितं चरति अनुमति - (अध्यात्मभाषासे) निज शुद्धात्माकी संविति रूप अनुचरण स्वरूप, परमागम भाषासे वीतराग परम सामायिक नामके स्वचारित्रको चरता है, अनुभव करता है । पं.का./ता.वृ./१०२/२४४/१५ कोऽपि शुद्धात्मानमुपादेय कृत्या आगमभाषया मोक्षं वा व्रततपश्चरणादिकं करोति । -जो कोई (अध्याम
भा० ३-२
Jain Education International
पद्मगुल्म
भाषा सुद्धाराको उपादेय करके आगम भाषासे मोक्षको आय करके व्रत तपश्चरणादिक करता है ।
३. सर्क व सिद्धान्त पद्धति अन्तर
सं./टी./४४/११/४ तर्काभिप्रायेण सचावलोकनदर्शनं व्याख्यासम् । सिद्धान्ताभिप्रायेण उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं यत् प्रयत्न तद्रूप यत् स्वस्यात्मन. परिच्छेदनमलो हर्शन भव्यते = तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकनदर्शनका व्याख्यान किया । सिद्धान्तके अभिप्राय से जागे होनेवाले ज्ञानकी उत्पत्ति के लिए प्रयत्न रूप जो आत्माका अवलोकन वह दर्शन कहलाता है ।
३. सं/टी./४४/१६२/३ तर्फे मुख्य कृष्णा परसमयव्याख्यानं स्थूलव्या ख्यानं सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्याख्यानं मुख्यवृत्त्या सूक्ष्मव्याख्यानम् । तर्क में मुख्यतासे अन्यमतों का व्याख्यान होता है । स्थूल अर्थात विस्तृत व्याख्यान होता है। सिद्धान्त में मुख्यता से निज समयका व्याख्यान है, सूक्ष्म व्याख्यान है ।
४. उपसर्ग व अपवाद व्याख्यानमें अन्तर पं.का./ता.वृ/१४६/२१२/१ सकलश्रुतधारिणा ध्यानं भवति तदुत्सर्गवचन, अपवादव्याख्याने तु पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकश्रुतिपरिज्ञानमात्रेणेव केवलज्ञान जायते। नाराचसपथ महननेन ध्यानं भवति तदप्पुत्सर्गवचनं मायव्याख्यानं पुनरपूर्वादिगुणस्थानवर्तिना उपशमक्षपग्योयध्यानं सवपेक्षया से नियम. अपूर्वादधस्तनगुणस्थानेषु धर्मध्याने निषेधकं न भवति ।
सकल
तधारियोंको ध्यान होता है यह उत्सर्ग बचन है, अपवाद व्याख्यानसे सो पाच समिति और तीन गुप्तिको प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र के ज्ञानसे भी केवलज्ञान होता है।... वज्रवृषभनाराच नामको प्रथम संहननसे ही ध्यान होता है यह उत्सर्ग वचन है । अपवाद रूप व्याख्यान से तो अपूर्वादि गुणस्थानवर्त्ती जीवोंके उपशम व क्षपक श्रेणी में जो शुक्लध्यान होता है उसकी अपेक्षा यह नियम है। अपूर्वकरण गुणस्थानसे नीचेके गुणस्थानों में धर्मध्यानका निषेध नहीं होता है (द्र.सं./टी./५०/२३२/६) ।
* चारों अनुयोगोंकी कथन पद्धतिमें अन्तर पद्धति टीका है परिशिष्ट - दे० अनुयोग / १ । पद्म- १. चर्तीकी नव निधियों एक-दे० कापुरुष २ २. अपरविदेहस्थ एक क्षेत्र-दे० लोक / ५ /२३. कालका एक प्रमाण - दे० गणित / I / १२४१४. प्वाँ बलदेव था । अपरनाम राम था- दे० राम । ५. व मलदेव था। अपरनाम बल था । दे० शलाकापुरुष / ३६. म. पू. /६६ / श्लोक नं. पूर्व भवनं २ में धोपुर नगरके राजा प्रजापाल थे (७३) । फिर अच्युत स्वर्ग में देव हुए (७४) । वर्तमान भव हवे चक्रवर्ती हुए। (अपरनाम महापद्म था (ह. पु. / २०/१४) । विशेष परिचय- दे० शलाकापुरुष / २ ।
पद्मकीर्ति-पासणाहचरिउ (अपभ्रंश) के रचयिता सेनसंधी भट्टारक। गुरु- जिनसेन । समय- शक १६६ (ई. १०७७) (ती./३/२०५) | पद्मकूट -- १. पूर्व विदेहस्थ एक वक्षारगिरि-वे० लोक /५/३२. पूर्व विदेहस्थ पद्मकूट महारका एक कूट-दे० लोक/५/४२ कुण्डलबर पर्व का एक कूट- दे० / १२४, रुपक पदस्थ एक कूट-३० लोक/२/१३५. विद्याभ गजदन्तस्थ एक कूट० लोक /२/४ | पद्मगुल्म-म. पु. / ५६ / श्लोक विदेह क्षेत्रस्थ वरस देशकी सीमा नगरीके राजा थे (२-३) । चन्दन नामक पुत्रको राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली (१५-१६) । विपाकसूत्र तक सब अंगोंका अध्ययन किया तथा चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर तीर्थ कर प्रकृतिका बन्ध किया ।
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
-
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org