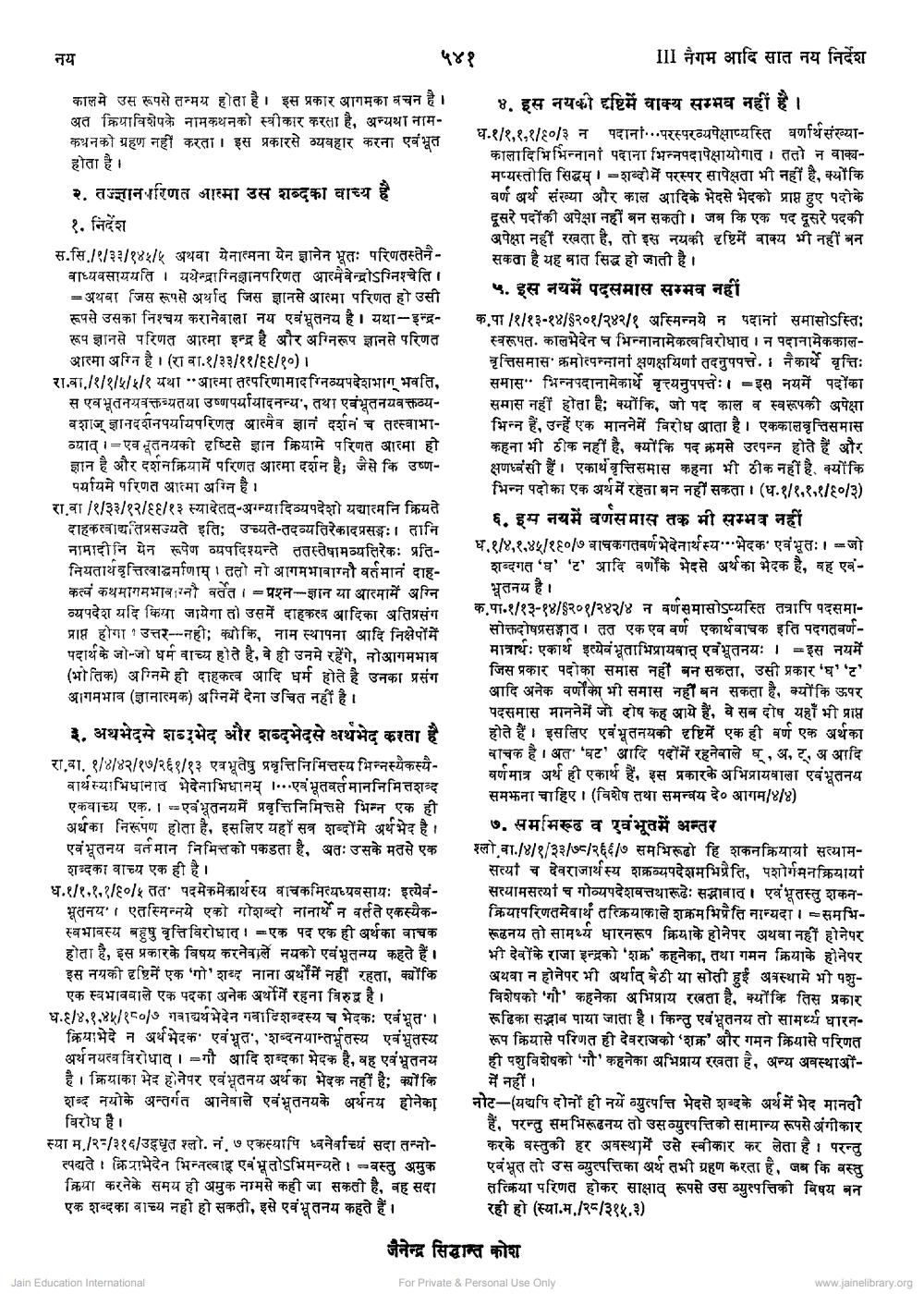________________
नय
५४१
III नैगम आदि सात नय निर्देश
कालमे उस रूपसे तन्मय होता है। इस प्रकार आगमका वचन है। ४. इस नयको दृष्टिमें वाक्य सम्भव नहीं है। अत क्रियाविशेपके नामकथनको स्वीकार करता है, अन्यथा नामकथन को ग्रहण नहीं करता। इस प्रकारसे व्यवहार करना एवंभूत
घ.१/१,१,१/१०/३ न पदाना...परस्परव्यपेक्षाप्यस्ति वर्थिसंख्या
कालादिभिभिन्नानां पदाना भिन्नपदापेक्षायोगात । ततो न वाक्यहोता है।
मप्यस्तोति सिद्धम् । = शब्दो में परस्पर सापेक्षता भी नहीं है, क्योंकि २. तज्ज्ञानारिणत आत्मा उस शब्दका वाच्य है
वर्ण अर्थ संख्या और काल आदिके भेदसे भेदको प्राप्त हुए पदोके १. निर्देश
दूसरे पदोंकी अपेक्षा नहीं बन सकती। जब कि एक पद दूसरे पदकी
अपेक्षा नहीं रखता है, तो इस नयकी दृष्टिमें बाक्य भी नहीं बन स.सि./९/३३/१४५/५ अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः परिणतस्तेनै
सकता है यह बात सिद्ध हो जाती है। वाध्यवसाययति । यथेन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्मैवेन्द्रोऽग्निश्चेति । = अथवा जिस रूपसे अर्थात जिस ज्ञानसे आत्मा परिणत हो उसी
५. इस नयमें पदसमास सम्भव नहीं रूपसे उसका निश्चय करानेवाला नय एवंभूतनय है। यथा-इन्द्र- क.पा १/१३-१४/६२०१/२४२/१ अस्मिन्नये न पदानां समासोऽस्ति: रूप ज्ञानसे परिणत आत्मा इन्द्र है और अग्निरूप ज्ञानसे परिणत स्वरूपत. कालभेदेन च भिन्मानामेकत्वविरोधात । न पदानामेककालआत्मा अग्नि है । (रावा.१/३३/११/१६/१०)।।
वृत्तिसमास' क्रमोत्पन्नानां क्षणक्षयिणां तदनुपपत्ते. । नैकार्थे वृत्तिः रा.वा./१/२/५/१/१ यथा “आत्मा तत्परिणामादग्निव्यपदेशभाग भवति, समास" भिन्नपदानामेकार्थे वृत्त्यनुपपत्तेः। =इस नयमें पदोंका
स एवभूतनयवक्तव्यतया उष्णपर्यायादनन्या, तथा एवंभूतनयवक्तव्य- समास नहीं होता है; क्योंकि, जो पद काल व स्वरूपकी अपेक्षा वशाज् ज्ञानदर्शनपर्यायपरिणत आत्मैव ज्ञानं दर्शनं च तत्स्वाभा- भिन्न हैं, उन्हें एक माननेमें विरोध आता है। एककालवृत्तिसमास व्यात् ।- एव भूतनयको दृष्टिसे ज्ञान क्रियामे परिणत आत्मा हो कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पद क्रमसे उत्पन्न होते हैं और ज्ञान है और दर्शनक्रियामें परिणत आत्मा दर्शन है। जैसे कि उष्ण- क्षणध्वंसी हैं। एकार्थ वृत्तिसमास कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पर्यायमे परिणत आत्मा अग्नि है।
भिन्न पदोका एक अर्थ में रहता बन नहीं सकता। (ध.१/१,१.१/80/३) रा.वा /१/३३/१२/६६/१३ स्यादेतत्-अग्न्यादिव्यपदेशो यद्यात्मनि क्रियते
६. इस नयमें वर्णसमास तक भी सम्भव नहीं दाहकत्वाद्यतिप्रसज्यते इति; उच्यते-तदव्यतिरेकादप्रसङ्गः। तानि नामादीनि येन रूपेण व्यपदिश्यन्ते ततस्तेषामव्यतिरेकः प्रति
घ.१/४,१,४५/१६०/७ बाचकगतवर्णभेदेनार्थस्य भेदक एवंभूतः। - जो नियतार्थवृत्तित्वाद्धर्माणाम् । ततो नो आगमभावाग्नौ वर्तमानं दाह
शब्दगत 'घ' 'ट' आदि वर्गों के भेदसे अर्थका भेदक है, वह एवंकत्वं कथमागमभावाग्नौ वर्तेत । = प्रश्न-ज्ञान या आत्मामें अग्नि
भूतनय है। व्यपदेश यदि किया जायेगा तो उसमें दाहकत्व आदिका अतिप्रसंग
क.पा.१/१३-१४/६२०९/२४२/४ न वर्णसमासोऽप्यस्ति तत्रापि पदसमाप्राप्त होगा । उत्तर--नही; क्यो कि, नाम स्थापना आदि निक्षेपों में
सोक्तदोषप्रसङ्गात । तत एक एव वर्ण एकार्थवाचक इति पदगतवर्णपदार्थ के जो-जो धर्म वाच्य होते है, वे ही उनमे रहेंगे, नोआगमभाव
मात्रार्थः एकार्थ इत्येवंभूताभिप्रायवात् एवंभूतनयः । = इस नयमें (भोतिक) अग्निमे ही दाहकत्व आदि धर्म होते है उनका प्रसंग
जिस प्रकार पदोका समास नहीं बन सकता, उसी प्रकार 'घ' 'ट' आगमभाव (ज्ञानात्मक) अग्निमें देना उचित नहीं है।
आदि अनेक वर्णों का भी समास नहीं बन सकता है, क्योंकि ऊपर
पदसमास मानने में जो दोष कह आये हैं, वे सब दोष यहाँ भी प्राप्त ३. अथभेदसे शब्दभेद और शब्दभेदसे अर्थभेद करता है होते हैं। इसलिए एवंभूतनयकी दृष्टि में एक ही वर्ण एक अर्थका
वाचक है । अत'घट' आदि पदोंमें रहनेवाले छ, अ., अ आदि रा.वा. १/४/४२/१७/२६१/१३ एवभूतेषु प्रवृत्तिनिमित्तस्य भिन्नस्यैकस्यै
वर्णमात्र अर्थ ही एकार्थ हैं, इस प्रकारके अभिप्रायवाला एवंभूतनय वार्थ स्याभिधानात भेदेनाभिधानम् ।...एवं भूतवर्तमाननिमित्तशब्द
समझना चाहिए। (विशेष तथा समन्वय दे० आगम/४/४) एकवाच्य एक.। -एवंभूतनयमें प्रवृत्तिनिमित्तसे भिन्न एक ही अर्थका निरूपण होता है, इसलिए यहाँ सत्र शब्दोंमे अर्थभेद है।
७. सममिरूढ व एवंभूतमें अन्तर एवं भूतनय वर्तमान निमित्तको पकडता है, अतः उसके मतसे एक __ श्लो वा./४/१/३३/७८/२६६/७ समभिरूढो हि शकनक्रियायां सत्यामशब्दका वाच्य एक ही है।
सत्यां च देवराजार्थस्य शक्रव्यपदेशमभिप्रैति, पशोर्गमनक्रियायां ध.१/१,१,२/१०/५ ततः पदमेकमेकार्थस्य वाचकमित्यध्यवसायः इत्येवं- सत्यामसत्यां च गोव्यपदेशवत्तथारूढेः सद्भावात् । एवं भूतस्तु शकनभूतनयः । एतस्मिन्नये एको गोशब्दो नानार्थे न वर्तते एकस्यैक- क्रियापरिणतमेवार्थ तरिक्रयाकाले शक्रमभिप्रैति नान्यदा। -समभिस्वभावस्य बहुषु वृत्तिविरोधात् । = एक पद एक ही अर्थका वाचक रूढनय तो सामर्थ्य धारनरूप क्रियाके होनेपर अथवा नहीं होनेपर होता है, इस प्रकारके विषय करनेवाले नयको एवंभूतनय कहते हैं। भी देवोंके राजा इन्द्रको 'शक' कहनेका, तथा गमन क्रियाके होनेपर इस नयकी दृष्टि में एक 'गो' शब्द नाना अर्थों में नहीं रहता, क्योंकि अथवा न होनेपर भी अर्थात् बैठी या सोती हुई अवस्थामे भी पशुएक स्वभाववाले एक पदका अनेक अर्थोमें रहना विरुद्ध है।
विशेषको 'गौ' कहनेका अभिप्राय रखता है, क्योंकि तिस प्रकार ध.६/४,१,४५/१८०/७ गवाद्यर्थभेदेन गवादिशब्दस्य च भेदकः एवंभूतः। रूढिका सद्भाव पाया जाता है। किन्तु एवंभूतनय तो सामर्थ्य धारनक्रियाभेदे न अर्थ भेदक' एवंभूत', 'शब्दनयान्तर्भूतस्य एवंभूतस्य रूप क्रियासे परिणत ही देवराजको 'शक' और गमन क्रियासे परिणत अर्थनयत्व विरोधात् । - गौ आदि शब्दका भेदक है, वह एवंभूतनय ही पशुविशेषको 'गौ' कहनेका अभिप्राय रखता है, अन्य अवस्थाओंहै। क्रियाका भेद होनेपर एवंभूतनय अर्थका भेदक नहीं है; क्यों कि में नहीं। शब्द नयोके अन्तर्गत आनेवाले एवंभूतनयके अर्थनय होनेका नोट-(यद्यपि दोनों ही नये व्युत्पत्ति भेदसे शब्दके अर्थ में भेद मानती विरोध है।
हैं, परन्तु समभिरूढनय तो उस व्युत्पत्तिको सामान्य रूपसे अंगीकार स्या म./२/३१६/उद्धृत श्लो. नं.७ एकस्यापि ध्वनेर्वाच्यं सदा तन्नो- करके वस्तुकी हर अवस्थामें उसे स्वीकार कर लेता है। परन्तु त्पद्यते। क्रिपाभेदेन भिन्नत्वाद् एवंभूतोऽभिमन्यते। -वस्तु अमुक एवंभूत तो उस व्युत्पत्तिका अर्थ तभी ग्रहण करता है, जब कि वस्तु क्रिया करनेके समय ही अमुक नामसे कही जा सकती है, वह सदा तक्रिया परिणत होकर साक्षात् रूपसे उस व्युत्पत्तिको विषय बन एक शब्दका बाच्य नही हो सकती, इसे एवंभूतनय कहते हैं।
रही हो (स्या.म./२८/३१५.३)
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org