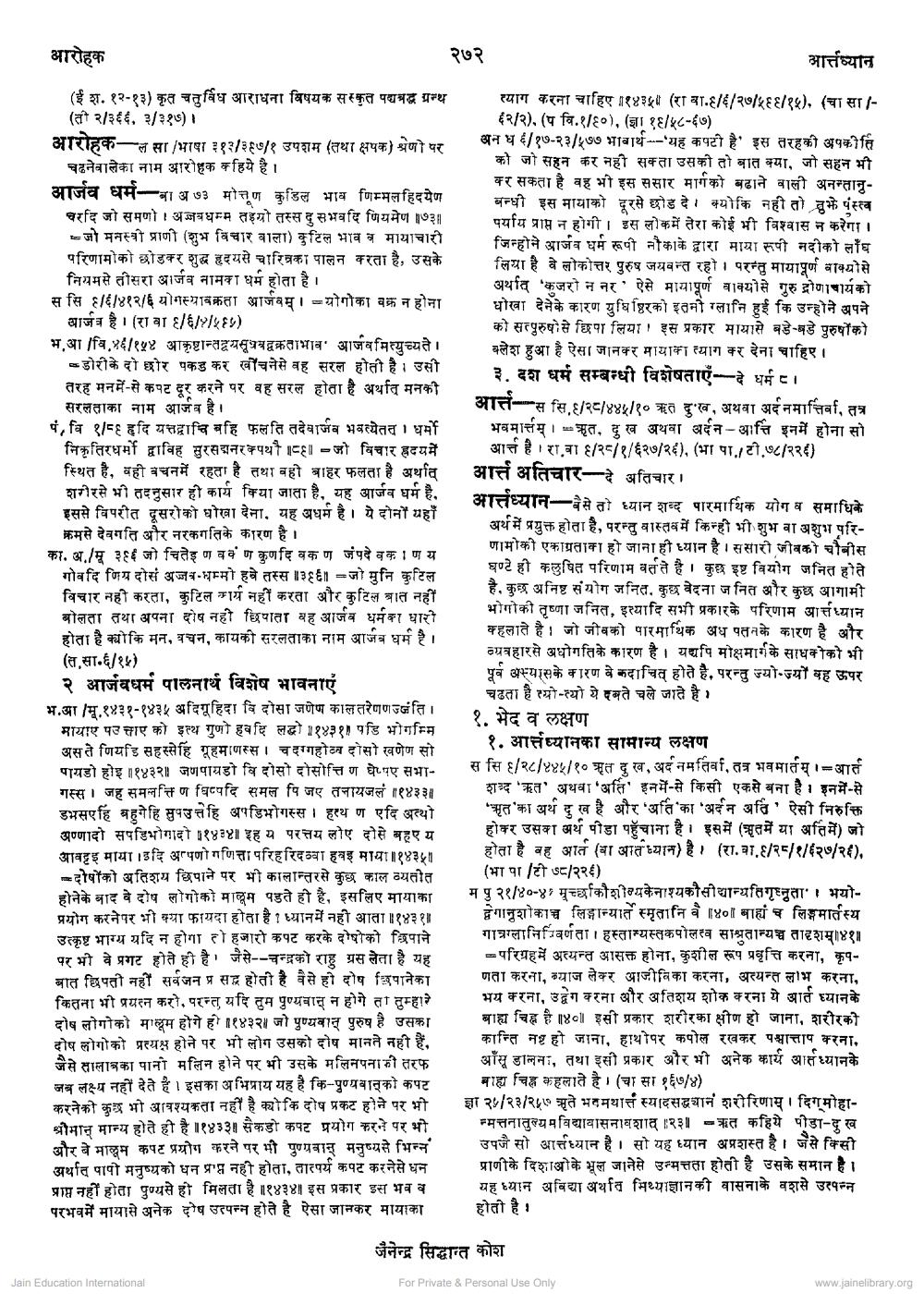________________
आरोहक
२७२
आर्तध्यान
(ई श. १२-१३) कृत चतुर्विध आराधना विषयक सस्कृत पद्यश्रद्ध ग्रन्थ (ती २/३६६, ३/३१७)। आरोहक-लसा/भाषा ३१३/३६७/१ उपशम (तथा क्षपक) श्रेणो पर
चढनेवालेका नाम आरोहक कहिये है। आर्जव धर्म-बा अ७३ मोत्तण कुडिल भाव णिम्मल हिदयेण चरदि जो समणो । अजवधम्म तइयो तस्स दु सभवदि णियमेण ॥७३॥ - जो मनस्वी प्राणी (शुभ विचार वाला) कुटिल भाव व मायाचारी परिणामोको छोडकर शुद्ध हृदयसे चारित्रका पालन करता है, उसके नियमसे तीसरा आर्जव नामका धर्म होता है। स सि ६/६/४१२/६ योगस्यावक्रता आर्जवम् । = योगोका वक्र न होना
बार्जव है । (रा वा ६/६/१/५४५) भ,आ /वि.४६/१५४ आकृष्टान्तद्वयसूधवद्वक्रताभाव' आजवमित्युच्यते।
- डोरीके दो छोर पकड कर खींचनेसे वह सरल होती है। उसी तरह मन में से कपट दूर करने पर वह सरल होता है अर्थात मनकी
सरलताका नाम आजव है। पं, वि १/हृदि यत्तद्वाचि बहि फलति तदेवार्जव भवत्येतत । धर्मों निकृतिरधर्मो द्वाविह सुरसानरपिथौ।-जो विचार हृदयमें स्थित है, वही वचनमें रहता है तथा वही बाहर फलता है अर्थात् शरीरसे भी तदनुसार ही कार्य किया जाता है, यह आर्जव धर्म है, इससे विपरीत दूसरोको धोखा देना. यह अधर्म है। ये दोनों यहाँ क्रमसे देवगति और नरकगतिके कारण है। का. अ./मू ३६६ जो चितेइ ण वण कुणदि वक ण जंपदे व क । ण य गोवदि णिय दोसं अजब-धम्मो हवे तस्स ॥३६६ =जो मुनि कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता और कुटिल बात नहीं बोलता तथा अपना दोष नही छिपाता वह आर्जव धर्मका धारी होता है क्योकि मन, वचन, कायकी सरलताका नाम आर्जब धर्म है। (त.सा.६/१५)
२ आर्जवधर्म पालनार्थ विशेष भावनाएं भ.आ /मू.१४३१-१४३५ अदिगूहिदा वि दोसा जणेण काल तरेणणजंति। मायाए पउत्ताए को इत्थ गुणो हव दि लो।१४३१॥ पडि भोगम्मि असते णियइि सहस्से हिं गृहमाणस्स। च दग्गहोठव दोसो खणेण सो पायडो होइ ॥१४३२॥ जणपायडो वि दोसो दोसोत्ति ण घेपए सभागस्स। जह समन्नक्तिण घिपदि समल पि जए तनायजलं ॥१४३३॥ डभसएहि बहुगेहि सुपउत्तं हि अपडिभोगस्स । हस्थ ण एदि अत्थो अण्णादो सपडिभोगादो ॥१४३४॥ इह य परत्तय लोए दोसे बहए य आवदृइ माया । इदि अपणो गणित्ता परिहरिदव्वा हवइ माया॥१४३५॥ गळ दोषोंको अतिशय छिपाने पर भी कालान्तरसे कुछ काल व्यतीत होने के बाद वे दोष लोगोको मालूम पडते ही है, इसलिए मायाका प्रयोग करने पर भी क्या फायदा होता है ? ध्यान में नहीं आता ॥१४३१॥ उत्कृष्ट भाग्य यदि न होगा तो हजारो कपट करके दोषोको छिपाने पर भी वे प्रगट होते ही है। जैसे--चन्द्रको राहु ग्रस लेता है यह बात छिपती नहीं सर्वजन प्रसद्ध होती है वैसे ही दोष पिानेका कितना भी प्रयत्न करो, परन्त यदि तुम पुण्यवान् न होगे तो तुम्हारे दोष लोगोको मालूम होगे हो ॥१४३२॥ जो पुण्यवान् पुरुष है उसका दोष लोगो को प्रत्यक्ष होने पर भी लोग उसको दोष मानते नही हैं, जैसे तालाब का पानी मलिन होने पर भी उसके मलिनपना की तरफ जब लक्ष्य नहीं देते है। इसका अभिप्राय यह है कि-पुण्यवानको कपट करनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है क्योकि दोष प्रकट होने पर भी श्रीमान् मान्य होते ही है ॥१४३३॥ सैकडो कपट प्रयोग करने पर भी और बे मालूम कपट प्रयोग करने पर भी पुण्यवान् मनुष्य से भिन्न अर्थात पापी मनुष्यको धन प्राप्त नहीं होता, तात्पर्य कपट करनेसे धन प्राप्त नहीं होता पुण्यसे ही मिलता है ॥१४३४॥ इस प्रकार इस भव व परभवमें मायासे अनेक दोष उत्पन्न होते है ऐसा जानकर मायाका
त्याग करना चाहिए ॥१४३५॥ (रावा.६/६/२७/५६४/१५), (चा सा/६२/२).(प वि.१/१०), (ज्ञा १४/५८-६७) अन ध4/१७-२३/५७७ भावार्थ---'यह कपटी है। इस तरह की अपकीति
को जो सहन कर नही सक्ता उसकी तो बात क्या, जो सहन भी कर सकता है वह भी इस ससार मार्ग को बढ़ाने वाली अनन्तानबन्धी इस मायाको दूरसे छोड दे। क्योकि नही तो तुझे पस्त्व पर्याय प्राप्त न होगी। इस लोकमें तेरा कोई भी विश्वास न करेगा। जिन्होने आर्जव धर्म रूपी नौकाके द्वारा माया रूपी नदीको लाँघ लिया है वे लोकोत्तर पुरुष जयवन्त रहो। परन्तु मायापूर्ण बाक्योसे अर्थात 'कुजरो न नर' ऐसे माया पूर्ण वाक्योसे गुरु द्रोणाचार्यको धोखा देने के कारण युधिष्ठिरको इतनी ग्लानि हुई कि उन्होने अपने को सत्पुरुषोसे छिपा लिया। इस प्रकार मायासे बड़े-बडे पुरुषों को क्लेश हुआ है ऐसा जानकर मायाका त्याग कर देना चाहिए।
३. दश धर्म सम्बन्धी विशेषताएँ-दे धर्म । आत्तस सि.६/२८/४४५/१० ऋत दुख, अथवा अर्द नमात्तिर्वा, तत्र भवमातम् । = ऋत, दु ख अथवा अर्दन-आत्ति इनमें होना सो आर्त है । रा.वा ६/२८/१/६२७/२६), (भा पा./टी.७८/२२६) आर्त अतिचार-दे अतिचार। आत्तंध्यान-वैसे तो ध्यान शब्द पारमार्थिक योग व समाधिके अर्थ में प्रयुक्त होता है, परन्तु वास्तव में किन्ही भी शुभ वा अशुभ परिणामोकी एकाग्रताका हो जाना ही ध्यान है । ससारी जीवको चौबीस घण्टे ही कलुषित परिणाम वर्तते है। कुछ इष्ट वियोग जनित होते है, कुछ अनिष्ट संयोग जनित. कुछ वेदना ज नित और कुछ आगामी भोगोकी तृष्णा जनित, इत्यादि सभी प्रकारके परिणाम आर्सध्यान कहलाते है। जो जीवको पारमार्थिक अध पतनके कारण है और व्यवहारसे अधोगति के कारण है। यद्यपि मोक्षमार्ग के साधकोको भी पूर्व अभ्यासके कारण वे कदाचित् होते है, परन्तु ज्योज्यों वह ऊपर चढता है त्यो-त्यो ये दबते चले जाते है। १. भेद व लक्षण
१. आतध्यानका सामान्य लक्षण स सि ६/२८/१४५/१० ऋत दुरव, अर्द नमतिर्वा, तत्र भवमार्तम् ।- आर्त
शब्द 'ऋत' अथवा 'अति' इनमें से किसी एकसे बना है। इनमें से 'मृत'का अर्थ दुख है और 'अति का 'अर्दन अति' ऐसी निरुक्ति होकर उसका अर्थ पीडा पहुंचाना है। इसमें (ऋतमें या अतिमें) जो होता है वह आर्त (वा आत ध्यान) है। (रा.वा.६/२८/१/६२७/२६), (भा पा /टी ७८/२२६) म पु २१/४०-४१ मुकौशीग्यकेनाश्यकौसीद्यान्यतिगृध्नुता'। भयो
द्वेगानुशोकाच्च लिङ्गान्यात स्मृतानि वै ॥४०॥ बाह्यं च लिङ्गमार्तस्थ गात्रग्लानिरिवर्णता । हस्ताग्यस्तकपोलत्व साश्रुतान्यच्च तादृशम्॥४१॥ -परिग्रह में अत्यन्त आसक्त होना, कुशील रूप प्रवृत्ति करना, कृपणता करना, व्याज लेकर आजीविका करना, अत्यन्त लाभ करना, भय करना, उद्वेग करना और अतिशय शोक करना ये आर्त ध्यानके बाह्य चिह्न है ॥४०॥ इसी प्रकार शरीरका क्षीण हो जाना, शरीरको कान्ति नष्ट हो जाना, हाथोपर कपोल रखकर पश्चात्ताप करना, आँसू डालना, तथा इसी प्रकार और भी अनेक कार्य आर्त ध्यानके बाह्य चिह्न कहलाते है । (चा सा १६७/४) ज्ञा २४/२३/२५५७ ऋते भवमथात्तं स्यादसद्धयानं शरीरिणाम् । दिगमोहान्मत्तनातुल्य मविद्यावासनावशात् ।२३। -ऋत कहिये पीडा-दुख उपजै सो आर्तध्यान है। सो यह ध्यान अप्रशस्त है। जैसे क्सिी प्राणीके दिशाओके भूल जानेसे उन्मत्तता होती है उसके समान है। यह ध्यान अविद्या अर्थात मिथ्याज्ञान की वासनाके वशसे उत्पन्न होती है।
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org