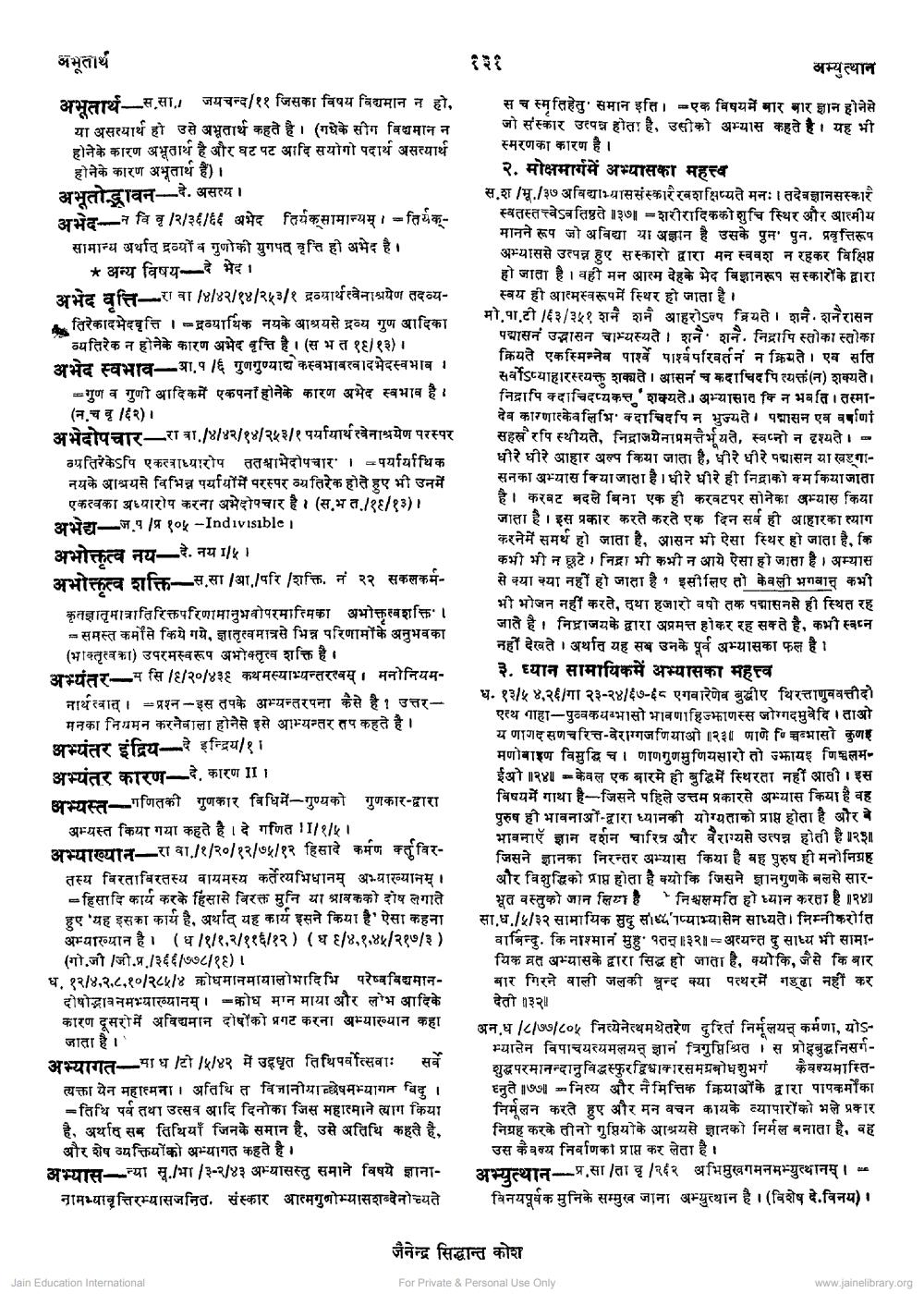________________
अभूतार्थ
अभ्युत्थान अभूतार्थ—स.सा., जयचन्द/११ जिसका विषय विद्यमान न हो,
स च स्मतिहेतु समान इति। -एक विषय में मार मार ज्ञान होनेसे या असत्यार्थ हो उसे अभूतार्थ कहते है। (गधेके सोग विद्यमान न
जो संस्कार उत्पन्न होता है, उसीको अभ्यास कहते है। यह भी होने के कारण अभूतार्थ है और घट पट आदि सयोगो पदार्थ असत्यार्थ स्मरणका कारण है। होनेके कारण अभूतार्थ हैं)।
२. मोक्षमार्गमें अभ्यासका महत्त्व अभूतोद्भावन-दे. असत्य ।
स.श/मू./३७ अविद्याभ्याससंस्काररवशक्षिप्यते मनः। तदेवज्ञानसस्कार अभेद-न वि व /२/३६/६६ अभेद तिर्यक्सामान्यम् । -तिर्यक
स्वतस्तत्त्वेऽवतिष्ठते ॥३७॥ - शरीरादिकको शुचि स्थिर और आत्मीय
मानने रूप जो अविद्या या अज्ञान है उसके पुन' पुन, प्रवृत्तिरूप सामान्य अर्थात् द्रव्यों व गुणोकी युगपत् वृत्ति ही अभेद है।
अभ्याससे उत्पन्न हुए सस्कारो द्वारा मन स्ववश न रहकर विक्षिप्त * अन्य विषय-दे भेद ।
हो जाता है। वही मन आत्म देहके भेद विज्ञानरूप सस्कारों के द्वारा अभेद वत्ति-रा वा /४/४२/१४/२५३/१ द्रव्यार्थत्वेनाश्रयेण तदव्य- स्वय ही आत्मस्वरूपमें स्थिर हो जाता है। तिरेकादभेदवृत्ति । -द्रव्याथिक नयके आश्रयसे द्रव्य गुण आदिका
मो.पा.टी /६३/३५१ शनै शनै आहरोऽल्प वियते । शनैः शनैरासन व्यतिरेक न होनेके कारण अभेद वृत्ति है । (स भ त १६/१३) ।
पद्मासनं उद्भासन चाभ्यस्यते। शनैः शन. निद्रापि स्तोका स्तोका
क्रियते एकस्मिन्नेव पावें पार्श्व परिवर्तनं न क्रियते। एव सति अभेद स्वभाव-आ.५/६ गुणगुण्याद्य कस्वभावरवादभेदस्वभाव ।
सर्वोऽप्याहारस्त्यक्तु शक्यते । आसनं च कदाचिदपि त्यक्त(न) शक्यते। -गुण व गुणी आदि कमें एकपना होनेके कारण अभेद स्वभाव है।
निद्रापि कदाचिदप्यकत्त शक्यते। अभ्यासात कि न भवति । तस्मा(न.च वृ/६२)।
देव कारणास्केवलिभिः कदाचिदपि न भुज्यते। पद्मासन एव वर्षाणां अभेदोपचार-रावा./४/४२/१४/२५३/१ पर्यायार्थ त्वेनाश्रयेण परस्पर सहस्ररपि स्थीयते, निद्राजयेनाप्रमत्तै यते, स्वप्नो न दृश्यते। - व्यतिरेकेऽपि एकत्वाध्यारोप ततश्चाभेदोपचार' । = पर्याथिक
धीरे धीरे आहार अल्प किया जाता है, धीरे धीरे पद्मासन या खगानयके आश्रयसे विभिन्न पर्यायोंमें परस्पर व्यतिरेक होते हुए भी उनमें
सन का अभ्यास क्यिा जाता है। धीरे धीरे ही निद्राको कम किया जाता एकत्वका अध्यारोप करना अभेदोपचार है। (स.भ त./११/१३)।
है। करवट बदले बिना एक ही करवटपर सोनेका अभ्यास किया अभेद्य-ज.प/प्र १०५ -Indivisiblet
जाता है । इस प्रकार करते करते एक दिन सर्व ही आहारका त्याग
करने में समर्थ हो जाता है, आसन भी ऐसा स्थिर हो जाता है, कि अभोक्तृत्व नय-दे. नय 1/५ ।
कभी भी न छूटे। निद्रा भी कभी न आये ऐसा हो जाता है। अम्यास अभोक्तत्व शक्ति-स.सा /आ./परि /शक्ति. नं २२ सकलकर्म
से क्या क्या नहीं हो जाता है। इसीलिए तो केवली भगवान कभी कृतज्ञातृमात्रातिरिक्तपरिणामानुभवोपरमात्मिका अभोक्तत्वशक्ति।
भी भोजन नहीं करते, तथा हजारो वषो तक पद्मासनसे ही स्थित रह का समस्त कर्मों से किये गये, ज्ञातृत्वमात्रसे भिन्न परिणामों के अनुभवका
जाते है। निद्राजयके द्वारा अप्रमत्त होकर रह सकते है, कभी स्वप्न (भक्तृित्वका) उपरमस्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति है।
नहीं देखते । अर्थात यह सब उनके पूर्व अभ्यासका फल है। अभ्यंतर-मसि /8/२०/४३६ कथमस्याभ्यन्तरत्वम् । मनोनियम- ३. ध्यान सामायिकमें अभ्यासका महत्त्व नार्थत्वात् । - प्रश्न-इस तपके अभ्यन्तरपना कैसे है। उत्तर
ध. १३/५४,२६/गा २३-२४/६७-६८ एगवारेणेव बुद्धीए थिरत्ताणुववत्तीदो मनका नियमन करनेवाला होनेसे इसे आभ्यन्तर तप कहते है ।
एत्थ गाहा-पुवकयम्भासो भावणाहिज्माणस्स जोग्गदमुवेदि । ताओ
य णागद सणचरित्त-वेराग्गजणियाओ ॥२३॥ णाणे चिन्भासो कुणाह अभ्यंतर इंद्रिय-दे इन्द्रिय/१॥
मणोबाइण विसुद्धि च । णाणगुणमणियसारो तो जमायइ णिश्चलमअभ्यंतर कारण-दे. कारण II |
ईओ ॥२४॥ = केवल एक बारमे ही बुद्धिमें स्थिरता नहीं आती। इस अभ्यस्त-गणितकी गुणकार विधिमें-गुण्यको गुणकार-द्वारा विषयमें गाथा है-जिसने पहिले उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया है वह
पुरुष ही भावनाओं द्वारा ध्यानकी योग्यताको प्राप्त होता है और वे अभ्यस्त किया गया कहते है । दे गणित 11/१/५।।
भावनाएँ ज्ञान दर्शन चारित्र और वैराग्यसे उत्पन्न होती है ॥२३॥ अभ्याख्यान-रावा./१/२०/१२/७५/१२ हिसादे कर्मण कर्तृविर
जिसने ज्ञानका निरन्तर अभ्यास किया है वह पुरुष ही मनोनिग्रह तस्य विरताविरतस्य वायमस्य कर्तेत्यभिधानम् अभ्याख्यानम् । और विशुद्धिको प्राप्त होता है क्योकि जिसने ज्ञानगुणके बलसे सार-हिसादि कार्य करके हिंसासे विरक्त मुनि या श्रावकको दोष लगाते भूत वस्तुको जान लिया है निश्चल मति हो ध्यान करता है ॥२४॥ हुए 'यह इसका कार्य है, अर्थात् यह कार्य इसने किया है' ऐसा कहना सा.ध./५/३२ सामायिक सुदु साध्य प्याभ्यासेन साध्यते। निम्नीकरोति अभ्याख्यान है। (ध /१/१,२/११६/१२) (ध६/४,१,४५/२१७/३) वाबिन्दु. कि नाश्मानं मुह पतन् । ३२॥ - अत्यन्त दु साध्य भी सामा(गो.जी /जी.प्र./३६६/७७८/१६)।
यिक व्रत अभ्यासके द्वारा सिद्ध हो जाता है, क्यो कि, जैसे कि बार ध, १२/४,२,८,१०/२८५/४ क्रोधमानमायालोभादिभि परेष्वविद्यमान- बार गिरने वाली जलकी बन्द क्या पत्थरमें गड्ढा नहीं कर दोषोद्भावनमभ्याख्यानम्। -क्रोध मान माया और लोभ आदिके
देती ॥३२॥ कारण दूसरोमें अविद्यमान दोषोंको प्रगट करना अभ्याख्यान कहा
अन.ध /८/०७/८०५ नित्येनेत्थमथेतरेण दुरितं निर्मूलयन् कर्मणा, योsजाता है।
भ्यालेन विपाचयत्यमलयन् ज्ञानं त्रिगुप्तिश्रित । स प्रोद्बुद्धनिसर्गअभ्यागत-मा ध /टो /५/४२ में उद्धृत तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे
शुद्ध परमानन्दानुविद्धस्फुरद्विश्वाकारसमग्रबोधशुभगं कैवल्यमास्तित्यक्ता येन महात्मना। अतिथि त विजानीया छेषमभ्यागत विदुः । ध्नुते ॥७७॥ नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं के द्वारा पापकर्मों का -तिथि पर्व तथा उत्सव आदि दिनोका जिस महात्माने त्याग किया निर्मूलन करते हुए और मन वचन कायके व्यापारों को भले प्रकार है, अर्थात सब तिथियाँ जिनके समान है, उसे अतिथि कहते है, निग्रह करके तीनो गुप्तियोके आश्रयसे ज्ञानको निर्मल बनाता है, वह और शेष व्यक्तियोंको अभ्यागत कहते है।
उस कैवल्य निर्वाणको प्राप्त कर लेता है। अभ्यास-न्या सू./भा /३-२/४३ अभ्यासस्तु समाने विषये ज्ञाना
अभ्युत्थान-प्र.सा/ता वृ/२६२ अभिमुखगमनमभ्युत्थानम् । - नामभ्यावृत्तिरभ्यासजनित. संस्कार आत्मगुणोभ्यासशब्देनोच्यते विनयपूर्वक मुनिके सम्मुख जाना अभ्युत्थान है । (विशेष दे.विनय)।
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org