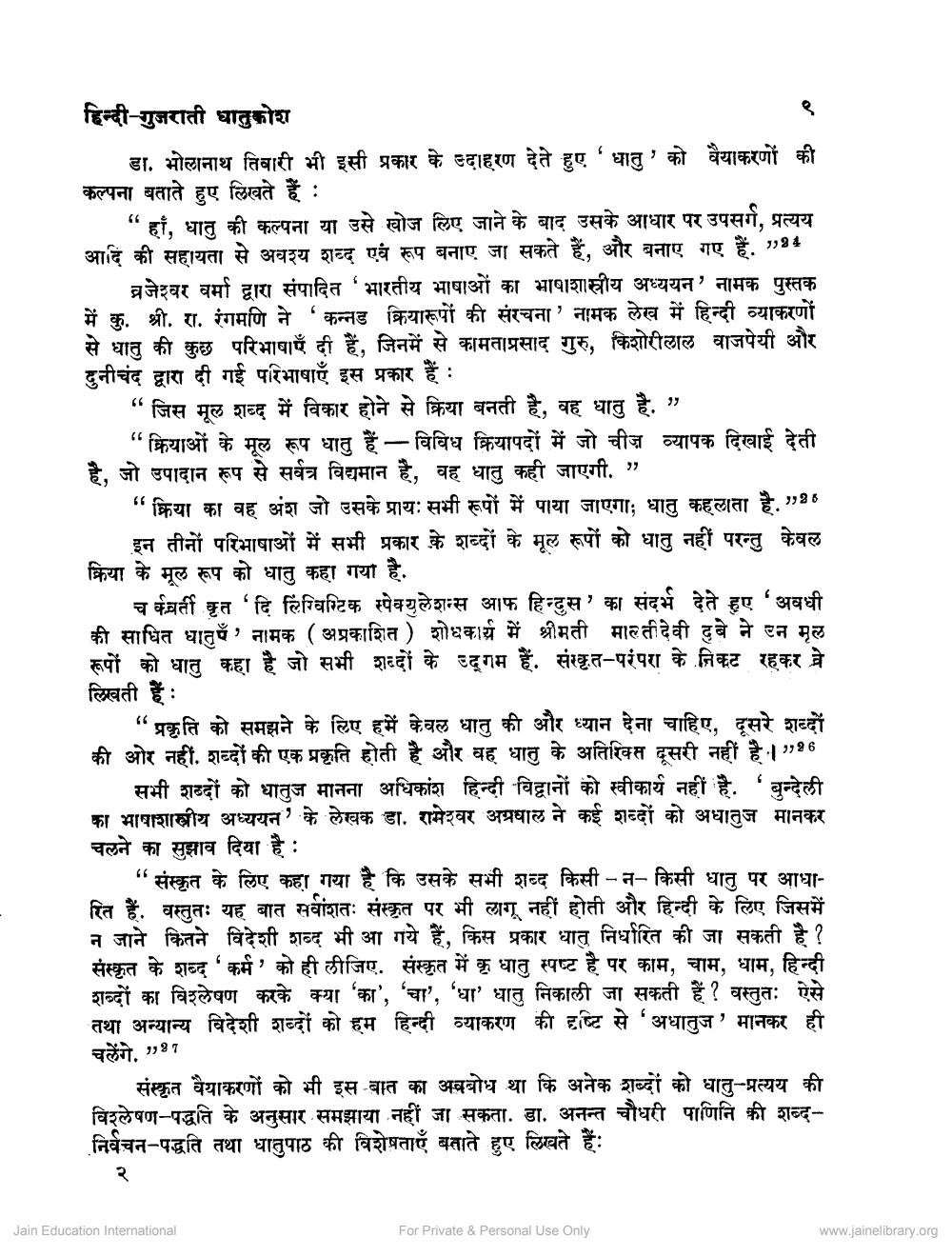________________
हिन्दी-गुजराती धातुकोश
___ डा. भोलानाथ तिवारी भी इसी प्रकार के उदाहरण देते हुए 'धातु' को वैयाकरणों की कल्पना बताते हुए लिखते हैं : __ " हाँ, धातु की कल्पना या उसे खोज लिए जाने के बाद उसके आधार पर उपसर्ग, प्रत्यय आदि की सहायता से अवश्य शब्द एवं रूप बनाए जा सकते हैं, और बनाए गए हैं. "34
ब्रजेश्वर वर्मा द्वारा संपादित 'भारतीय भाषाओं का भाषाशास्त्रीय अध्ययन' नामक पुस्तक में कु. श्री. रा. रंगमणि ने 'कन्नड क्रियारूपों की संरचना' नामक लेख में हिन्दी व्याकरणों से धातु की कुछ परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें से कामताप्रसाद गुरु, किशोरीलाल वाजपेयी और दुनीचंद द्वारा दी गई परिभाषाएँ इस प्रकार हैं :
" जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, वह धातु है." __ "क्रियाओं के मूल रूप धातु हैं - विविध क्रियापदों में जो चीज़ व्यापक दिखाई देती है, जो उपादान रूप से सर्वत्र विद्यमान है, वह धातु कही जाएगी. ” ।
"क्रिया का वह अंश जो उसके प्रायः सभी रूपों में पाया जाएगा; धातु कहलाता है."36
इन तीनों परिभाषाओं में सभी प्रकार के शब्दों के मूल रूपों को धातु नहीं परन्तु केवल क्रिया के मूल रूप को धातु कहा गया है.
च वर्ती कृत 'दि लिंग्विस्टिक स्पेक्युलेशन्स आफ हिन्दुस' का संदर्भ देते हुए 'अवधी की साधित धातुएँ' नामक (अप्रकाशित) शोधकार्य में श्रीमती मालती देवी दुबे ने उन मल रूपों को धातु कहा है जो सभी शब्दों के उद्गम हैं. संस्कृत-परंपरा के निकट रहकर वे लिखती हैं:
___ "प्रकृति को समझने के लिए हमें केवल धातु की और ध्यान देना चाहिए, दूसरे शब्दों की ओर नहीं. शब्दों की एक प्रकृति होती है और वह धातु के अतिरिक्स दूसरी नहीं है।"26
सभी शब्दों को धातुज मानना अधिकांश हिन्दी विद्वानों को स्वीकार्य नहीं है. 'बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन' के लेखक डा. रामेश्वर अग्रवाल ने कई शब्दों को अधातुज मानकर चलने का सुझाव दिया है :
"संस्कृत के लिए कहा गया है कि उसके सभी शब्द किसी-न-किसी धातु पर आधारित हैं. वस्तुतः यह बात सर्वांशतः संस्कृत पर भी लागू नहीं होती और हिन्दी के लिए जिसमें न जाने कितने विदेशी शब्द भी आ गये हैं. किस प्रकार धात निर्धारित की जा सकती है? संस्कृत के शब्द 'कर्म' को ही लीजिए. संस्कृत में कृ धातु स्पष्ट है पर काम, चाम, धाम, हिन्दी शब्दों का विश्लेषण करके क्या 'का', 'चा', 'धा' धातु निकाली जा सकती हैं ? वस्तुतः ऐसे तथा अन्यान्य विदेशी शब्दों को हम हिन्दी व्याकरण की दृष्टि से 'अधातुज' मानकर ही चलेंगे."
संस्कृत वैयाकरणों को भी इस बात का अवबोध था कि अनेक शब्दों को धातु-प्रत्यय की विश्लेषण-पद्धति के अनुसार समझाया नहीं जा सकता. डा. अनन्त चौधरी पाणिनि की शब्दनिर्वचन-पद्धति तथा धातुपाठ की विशेषताएँ बताते हुए लिखते हैं:
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org