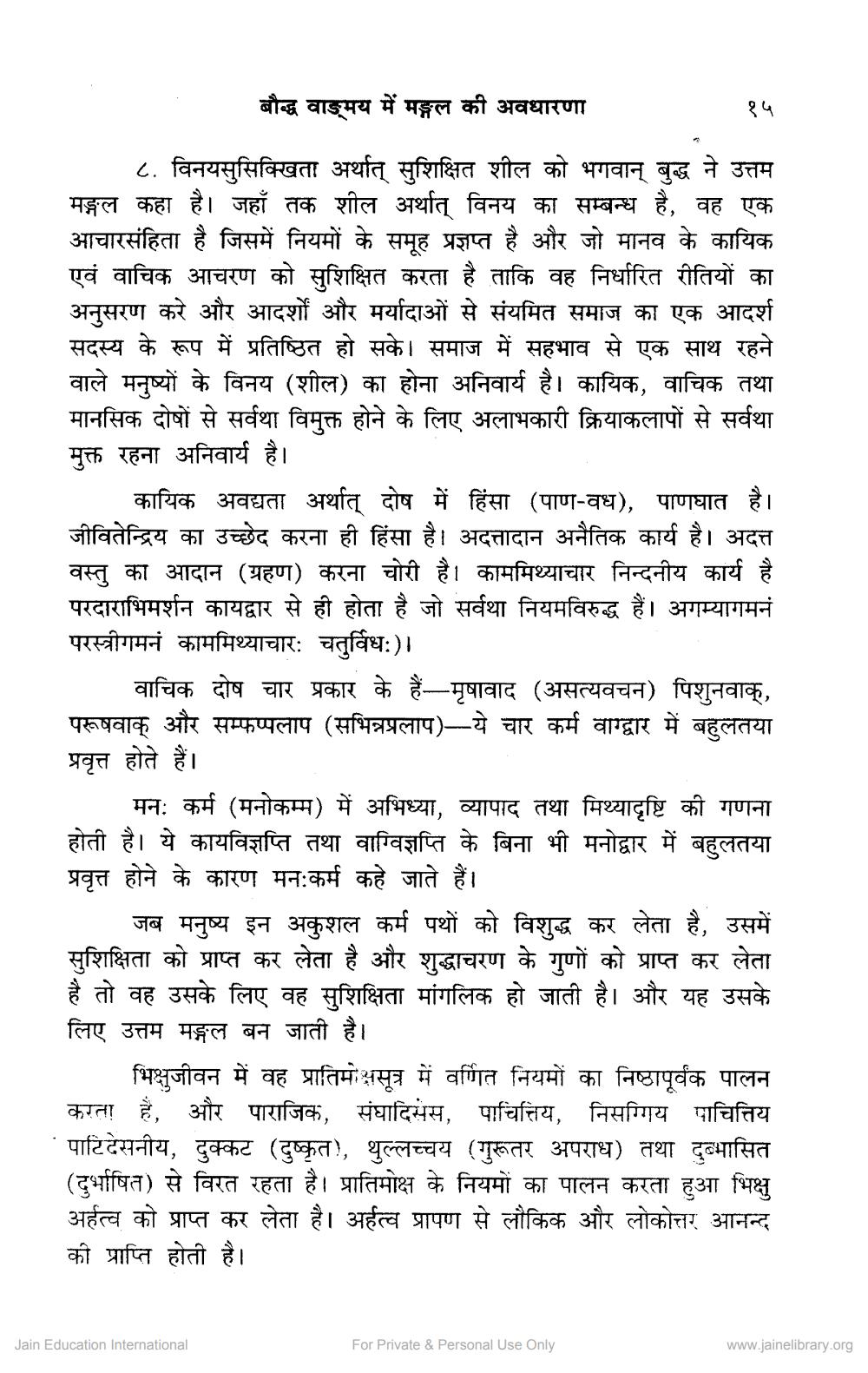________________
बौद्ध वाङ्मय में मङ्गल की अवधारणा
१५
८. विनयसुसिक्खिता अर्थात् सुशिक्षित शील को भगवान् बुद्ध ने उत्तम मङ्गल कहा है। जहाँ तक शील अर्थात् विनय का सम्बन्ध है, वह एक आचारसंहिता है जिसमें नियमों के समूह प्रज्ञप्त है और जो मानव के कायिक एवं वाचिक आचरण को सुशिक्षित करता है ताकि वह निर्धारित रीतियों का अनुसरण करे और आदर्शों और मर्यादाओं से संयमित समाज का एक आदर्श सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। समाज में सहभाव से एक साथ रहने वाले मनुष्यों के विनय (शील) का होना अनिवार्य है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक दोषों से सर्वथा विमुक्त होने के लिए अलाभकारी क्रियाकलापों से सर्वथा मुक्त रहना अनिवार्य है।
कायिक अवधता अर्थात् दोष में हिंसा (पाण-वध), पाणघात है। जीवितेन्द्रिय का उच्छेद करना ही हिंसा है। अदत्तादान अनैतिक कार्य है। अदत्त वस्तु का आदान (ग्रहण) करना चोरी है। काममिथ्याचार निन्दनीय कार्य है परदाराभिमर्शन कायद्वार से ही होता है जो सर्वथा नियमविरुद्ध हैं। अगम्यागमनं परस्त्रीगमनं काममिथ्याचार: चतुर्विधः)।
वाचिक दोष चार प्रकार के हैं—मृषावाद (असत्यवचन) पिशुनवाक्, परूषवाक् और सम्फप्पलाप (सभिन्नप्रलाप)-ये चार कर्म वाग्द्वार में बहुलतया प्रवृत्त होते हैं।
___ मनः कर्म (मनोकम्म) में अभिध्या, व्यापाद तथा मिथ्यादृष्टि की गणना होती है। ये कायविज्ञप्ति तथा वाग्विज्ञप्ति के बिना भी मनोद्वार में बहुलतया प्रवृत्त होने के कारण मन:कर्म कहे जाते हैं।
जब मनुष्य इन अकुशल कर्म पथों को विशुद्ध कर लेता है, उसमें सुशिक्षिता को प्राप्त कर लेता है और शुद्धाचरण के गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वह उसके लिए वह सुशिक्षिता मांगलिक हो जाती है। और यह उसके लिए उत्तम मङ्गल बन जाती है।
भिक्षुजीवन में वह प्रातिम सूत्र में वर्णित नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, और पाराजिक, संघादिसंस, पाचित्तिय, निसग्गिय पाचित्तिय पाटिदेसनीय, दुक्कट (दुष्कृत), थुल्लच्चय (गुरूतर अपराध) तथा दुब्भासित (दुर्भाषित) से विरत रहता है। प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन करता हुआ भिक्षु अर्हत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्हत्व प्रापण से लौकिक और लोकोत्तर आनन्द की प्राप्ति होती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org