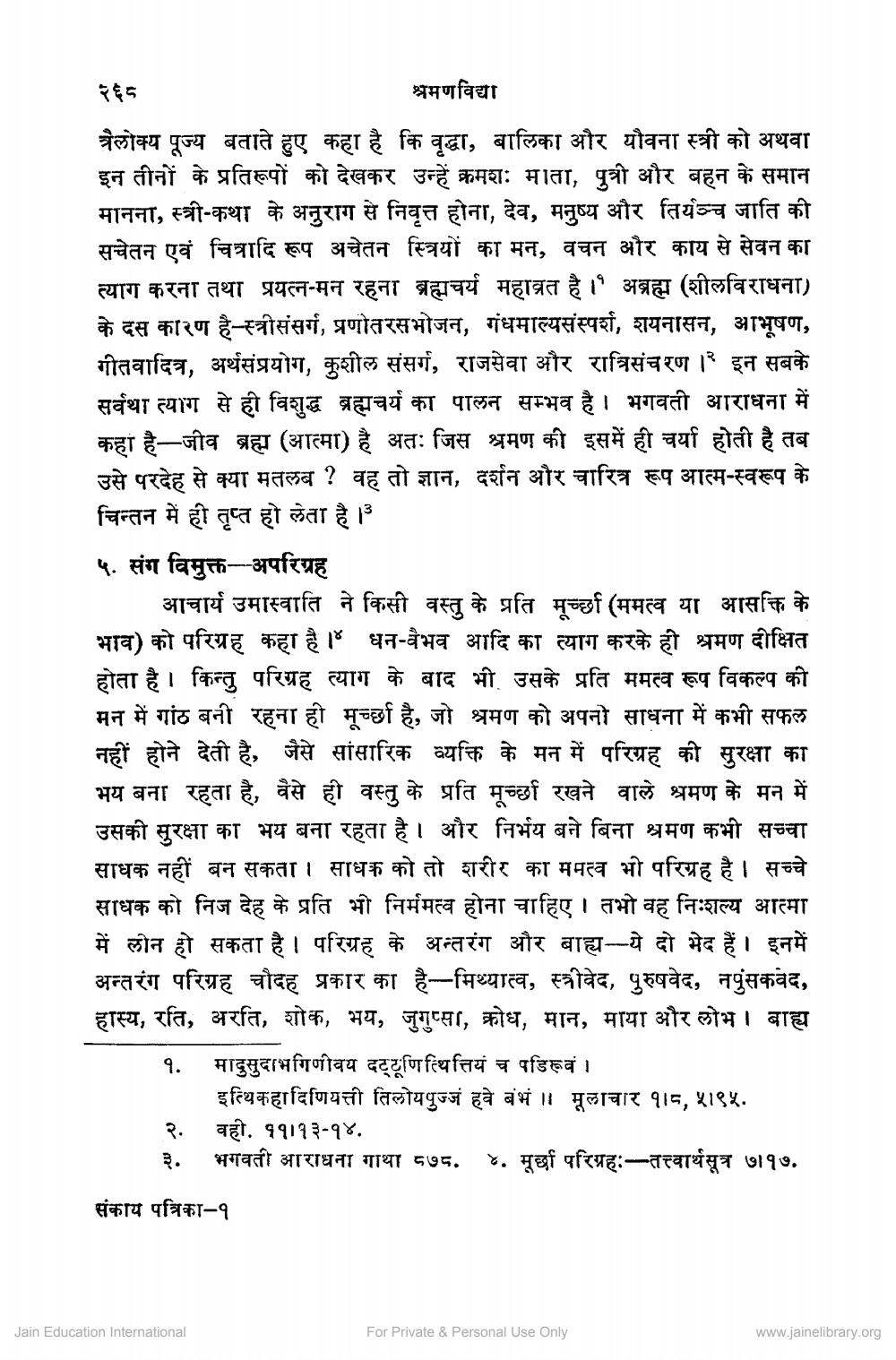________________
२६८
श्रमण विद्या
त्रैलोक्य पूज्य बताते हुए कहा है कि वृद्धा, बालिका और यौवना स्त्री को अथवा इन तीनों के प्रतिरूपों को देखकर उन्हें क्रमशः माता, पुत्री और बहन के समान मानना, स्त्री-कथा के अनुराग से निवृत्त होना, देव, मनुष्य और तिर्यञ्च जाति की सचेतन एवं चित्रादि रूप अचेतन स्त्रियों का मन, वचन और काय से सेवन का त्याग करना तथा प्रयत्न-मन रहना ब्रह्मचर्य महाव्रत है।' अब्रह्म (शीलविराधना) के दस कारण है-स्त्रीसंसर्ग, प्रणोतरसभोजन, गंधमाल्यसंस्पर्श, शयनासन, आभूषण, गीतवादित्र, अर्थसंप्रयोग, कुशील संसर्ग, राजसेवा और रात्रिसंचरण । इन सबके सर्वथा त्याग से ही विशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन सम्भव है। भगवती आराधना में कहा है-जीव ब्रह्म (आत्मा) है अतः जिस श्रमण की इसमें ही चर्या होती है तब उसे परदेह से क्या मतलब ? वह तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप आत्म-स्वरूप के चिन्तन में ही तृप्त हो लेता है। ५. संग विमुक्त-अपरिग्रह
आचार्य उमास्वाति ने किसी वस्तु के प्रति मूर्छा (ममत्व या आसक्ति के भाव) को परिग्रह कहा है। धन-वैभव आदि का त्याग करके ही श्रमण दीक्षित होता है। किन्तु परिग्रह त्याग के बाद भी उसके प्रति ममत्व रूप विकल्प की मन में गांठ बनी रहना ही मूर्छा है, जो श्रमण को अपनो साधना में कभी सफल नहीं होने देती है, जैसे सांसारिक व्यक्ति के मन में परिग्रह की सुरक्षा का भय बना रहता है, वैसे ही वस्तु के प्रति मूर्छा रखने वाले श्रमण के मन में उसकी सुरक्षा का भय बना रहता है। और निर्भय बने बिना श्रमण कभी सच्चा साधक नहीं बन सकता। साधक को तो शरीर का ममत्व भी परिग्रह है। सच्चे साधक को निज देह के प्रति भी निर्ममत्व होना चाहिए। तभी वह निःशल्य आत्मा में लीन हो सकता है। परिग्रह के अन्तरंग और बाह्य-ये दो भेद हैं। इनमें अन्तरंग परिग्रह चौदह प्रकार का है-मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया और लोभ । बाह्य १. मादुसुदाभगिणीवय दटूणि स्थित्तियं च पडिरूवं ।
इत्थिकहादिणियत्ती तिलोयपुज्ज हवे बंभं ॥ मूलाचार १८, २९५. २. वही. ११।१३-१४. ३. भगवती आराधना गाथा ८७८. ४. मूर्छा परिग्रहः-तत्त्वार्थसूत्र ७.१७.
संकाय पत्रिका-१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org