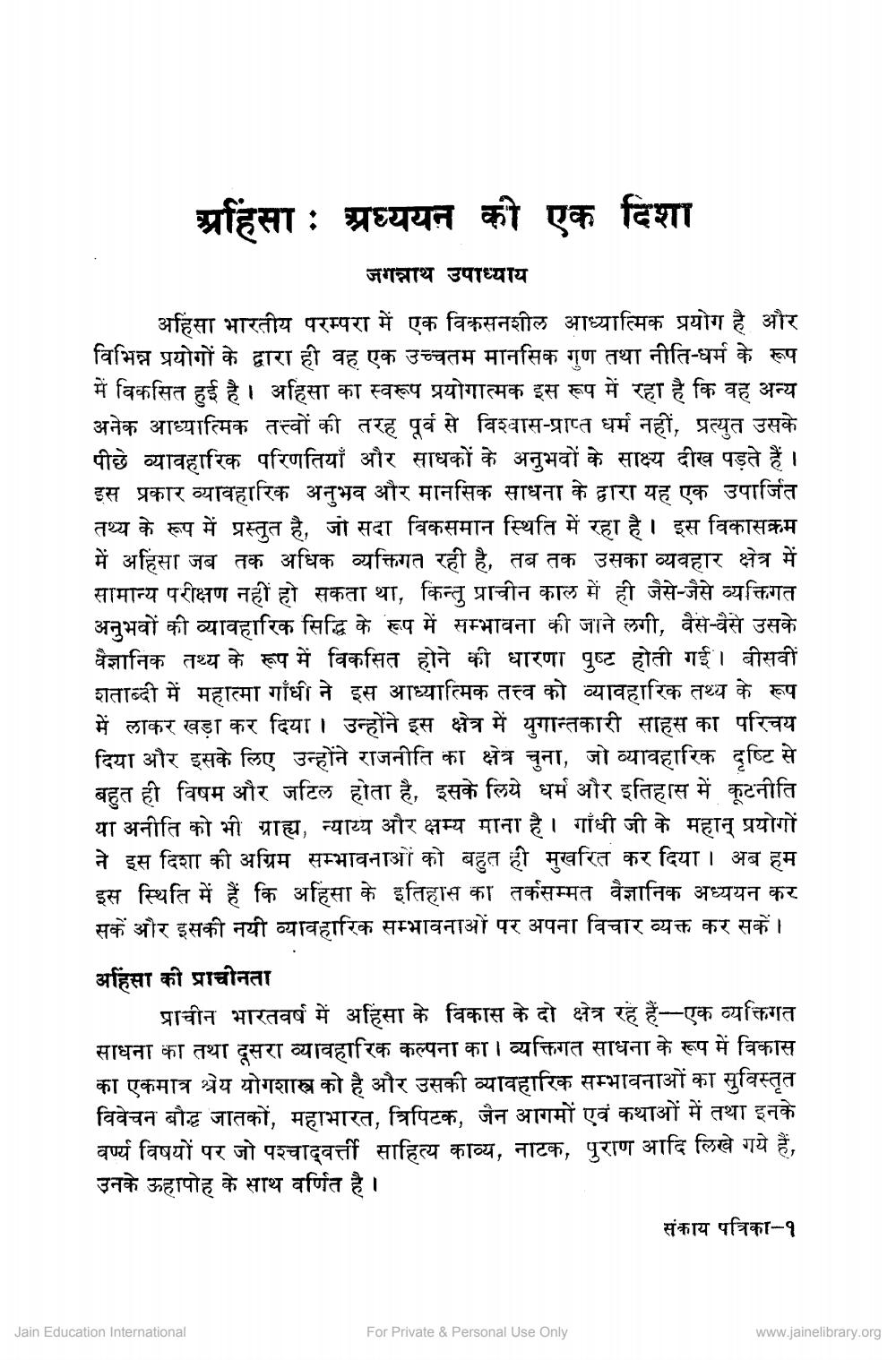________________
अहिंसा : अध्ययन की एक दिशा
जगन्नाथ उपाध्याय अहिंसा भारतीय परम्परा में एक विकसनशील आध्यात्मिक प्रयोग है और विभिन्न प्रयोगों के द्वारा ही वह एक उच्चतम मानसिक गुण तथा नीति-धर्म के रूप में विकसित हुई है। अहिंसा का स्वरूप प्रयोगात्मक इस रूप में रहा है कि वह अन्य अनेक आध्यात्मिक तत्त्वों की तरह पूर्व से विश्वास-प्राप्त धर्म नहीं, प्रत्युत उसके पीछे व्यावहारिक परिणतियाँ और साधकों के अनुभवों के साक्ष्य दीख पड़ते हैं। इस प्रकार व्यावहारिक अनुभव और मानसिक साधना के द्वारा यह एक उपार्जित तथ्य के रूप में प्रस्तुत है, जो सदा विकसमान स्थिति में रहा है। इस विकासक्रम में अहिंसा जब तक अधिक व्यक्तिगत रही है, तब तक उसका व्यवहार क्षेत्र में सामान्य परीक्षण नहीं हो सकता था, किन्तु प्राचीन काल में ही जैसे-जैसे व्यक्तिगत अनुभवों की व्यावहारिक सिद्धि के रूप में सम्भावना की जाने लगी, वैसे-वैसे उसके वैज्ञानिक तथ्य के रूप में विकसित होने की धारणा पुष्ट होती गई। बीसवीं शताब्दी में महात्मा गाँधी ने इस आध्यात्मिक तत्त्व को व्यावहारिक तथ्य के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में युगान्तकारी साहस का परिचय दिया और इसके लिए उन्होंने राजनीति का क्षेत्र चुना, जो व्यावहारिक दृष्टि से बहुत ही विषम और जटिल होता है, इसके लिये धर्म और इतिहास में कूटनीति या अनीति को भी ग्राह्य, न्याय्य और क्षम्य माना है। गाँधी जी के महान् प्रयोगों ने इस दिशा की अग्रिम सम्भावनाओं को बहुत ही मुखरित कर दिया। अब हम इस स्थिति में हैं कि अहिंसा के इतिहास का तर्कसम्मत वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें और इसकी नयी व्यावहारिक सम्भावनाओं पर अपना विचार व्यक्त कर सकें। अहिंसा की प्राचीनता
प्राचीन भारतवर्ष में अहिंसा के विकास के दो क्षेत्र रह हैं-एक व्यक्तिगत साधना का तथा दूसरा व्यावहारिक कल्पना का। व्यक्तिगत साधना के रूप में विकास का एकमात्र श्रेय योगशास्त्र को है और उसकी व्यावहारिक सम्भावनाओं का सुविस्तृत विवेचन बौद्ध जातकों, महाभारत, त्रिपिटक, जैन आगमों एवं कथाओं में तथा इनके वर्ण्य विषयों पर जो पश्चाद्वर्ती साहित्य काव्य, नाटक, पुराण आदि लिखे गये हैं, उनके ऊहापोह के साथ वर्णित है।
संकाय पत्रिका-१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org