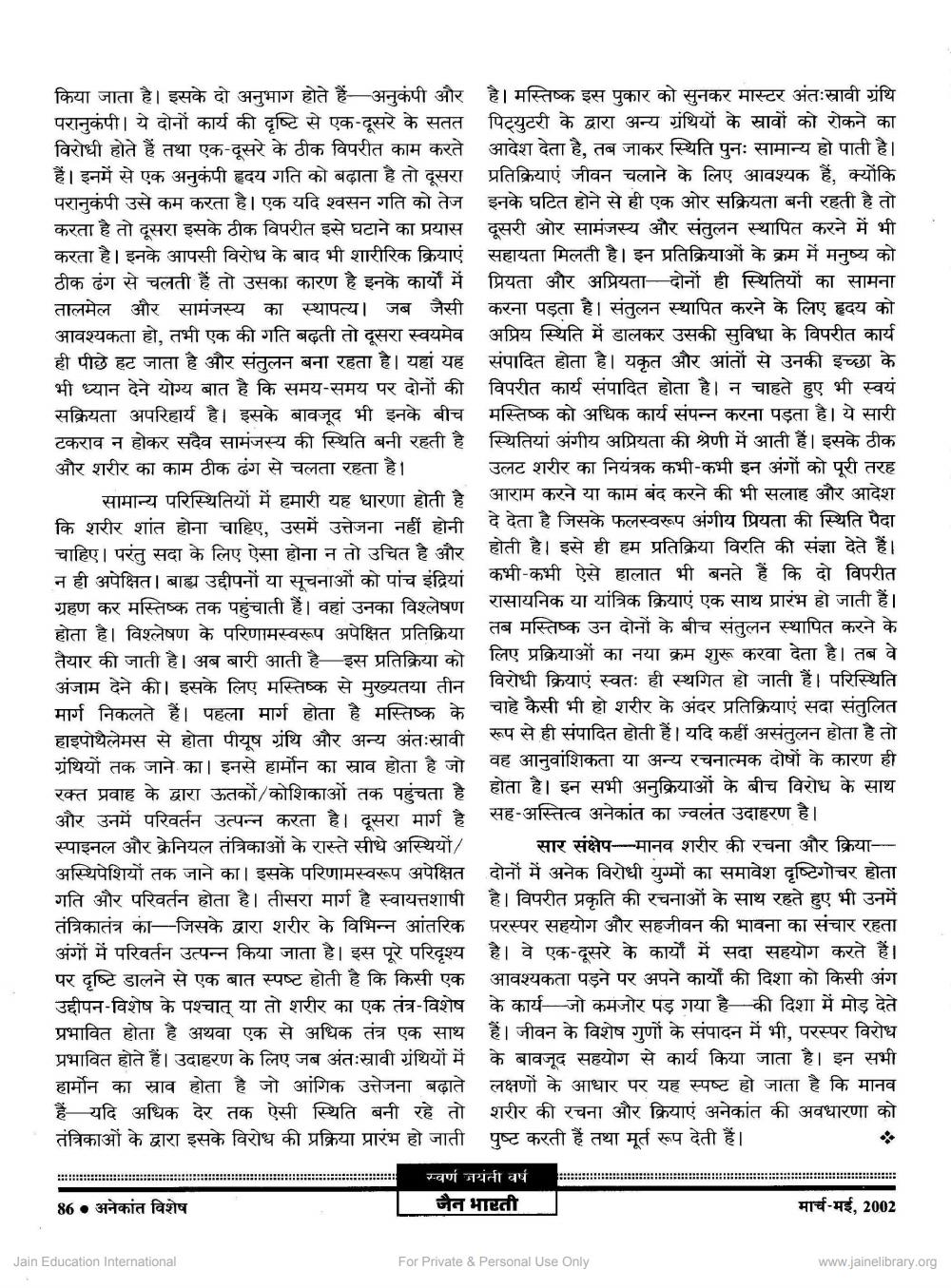________________
किया जाता है। इसके दो अनुभाग होते हैं अनुकंपी और है। मस्तिष्क इस पुकार को सुनकर मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि परानुकंपी। ये दोनों कार्य की दृष्टि से एक-दूसरे के सतत पिट्युटरी के द्वारा अन्य ग्रंथियों के स्रावों को रोकने का विरोधी होते हैं तथा एक-दूसरे के ठीक विपरीत काम करते आदेश देता है, तब जाकर स्थिति पुनः सामान्य हो पाती है। हैं। इनमें से एक अनुकंपी हृदय गति को बढ़ाता है तो दूसरा प्रतिक्रियाएं जीवन चलाने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि परानुकंपी उसे कम करता है। एक यदि श्वसन गति को तेज इनके घटित होने से ही एक ओर सक्रियता बनी रहती है तो करता है तो दूसरा इसके ठीक विपरीत इसे घटाने का प्रयास दूसरी ओर सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने में भी करता है। इनके आपसी विरोध के बाद भी शारीरिक क्रियाएं सहायता मिलती है। इन प्रतिक्रियाओं के क्रम में मनुष्य को ठीक ढंग से चलती हैं तो उसका कारण है इनके कार्यों में प्रियता और अप्रियता दोनों ही स्थितियों का सामना तालमेल और सामंजस्य का स्थापत्य। जब जैसी करना पड़ता है। संतुलन स्थापित करने के लिए हृदय को आवश्यकता हो, तभी एक की गति बढ़ती तो दूसरा स्वयमेव अप्रिय स्थिति में डालकर उसकी सुविधा के विपरीत कार्य ही पीछे हट जाता है और संतुलन बना रहता है। यहां यह संपादित होता है। यकृत और आंतों से उनकी इच्छा के भी ध्यान देने योग्य बात है कि समय-समय पर दोनों की विपरीत कार्य संपादित होता है। न चाहते हुए भी स्वयं सक्रियता अपरिहार्य है। इसके बावजूद भी इनके बीच मस्तिष्क को अधिक कार्य संपन्न करना पड़ता है। ये सारी टकराव न होकर सदैव सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है स्थितियां अंगीय अप्रियता की श्रेणी में आती हैं। इसके ठीक और शरीर का काम ठीक ढंग से चलता रहता है। उलट शरीर का नियंत्रक कभी-कभी इन अंगों को पूरी तरह
सामान्य परिस्थितियों में हमारी यह धारणा होती है आराम करने या काम बंद करने की भी सलाह और आदेश कि शरीर शांत होना चाहिए. उसमें उत्तेजना नहीं होनी दे देता है जिसके फलस्वरूप अंगीय प्रियता की स्थिति पैदा चाहिए। परंत सदा के लिए ऐसा होना न तो उचित है और होती है। इसे ही हम प्रतिक्रिया विरति की संज्ञा देते हैं। न ही अपेक्षित। बाह्य उद्दीपनों या सूचनाओं को पांच इंद्रियां कभी-कभी ऐसे हालात भी बनते हैं कि दो विपरीत ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। वहां उनका विश्लेषण रासायनिक या यांत्रिक क्रियाएं एक साथ प्रारंभ हो जाती हैं। होता है। विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपेक्षित प्रतिक्रिया तब मस्तिष्क उन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के तैयार की जाती है। अब बारी आती है। इस प्रतिक्रिया को लिए प्रक्रियाओं का नया क्रम शुरू करवा देता है। तब वे अंजाम देने की। इसके लिए मस्तिष्क से मख्यतया तीन विरोधी क्रियाएं स्वतः ही स्थगित हो जाती हैं। परिस्थिति मार्ग निकलते हैं। पहला मार्ग होता है मस्तिष्क के चाहे कैसी भी हो शरीर के अंदर प्रतिक्रियाएं सदा संतुलित हाइपोथैलेमस से होता पीयूष ग्रंथि और अन्य अंतःस्रावी रूप से ही संपादित होती हैं। यदि कहीं असंतुलन होता है तो ग्रंथियों तक जाने का। इनसे हार्मोन का स्राव होता है जो वह आनुवांशिकता या अन्य रचनात्मक दोषों के कारण ही रक्त प्रवाह के द्वारा ऊतकों/कोशिकाओं तक पहुंचता है होता है। इन सभी अनुक्रियाओं के बीच विरोध के साथ
और उनमें परिवर्तन उत्पन्न करता है। दूसरा मार्ग है सह-अस्तित्व अनेकांत का ज्वलंत उदाहरण है। स्पाइनल और क्रेनियल तंत्रिकाओं के रास्ते सीधे अस्थियों/ सार संक्षेप-मानव शरीर की रचना और क्रिया-- अस्थिपेशियों तक जाने का। इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित दोनों में अनेक विरोधी युग्मों का समावेश दृष्टिगोचर होता गति और परिवर्तन होता है। तीसरा मार्ग है स्वायत्तशाषी है। विपरीत प्रकृति की रचनाओं के साथ रहते हुए भी उनमें तंत्रिकातंत्र का जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न आंतरिक परस्पर सहयोग और सहजीवन की भावना का संचार रहता अंगों में परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है। इस पूरे परिदृश्य है। वे एक-दूसरे के कार्यों में सदा सहयोग करते हैं। पर दृष्टि डालने से एक बात स्पष्ट होती है कि किसी एक आवश्यकता पड़ने पर अपने कार्यों की दिशा को किसी अंग उद्दीपन-विशेष के पश्चात् या तो शरीर का एक तंत्र-विशेष के कार्य जो कमजोर पड़ गया है की दिशा में मोड़ देते प्रभावित होता है अथवा एक से अधिक तंत्र एक साथ हैं। जीवन के विशेष गुणों के संपादन में भी, परस्पर विरोध प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए जब अंतःस्रावी ग्रंथियों में के बावजूद सहयोग से कार्य किया जाता है। इन सभी हार्मोन का स्राव होता है जो आंगिक उत्तेजना बढ़ाते लक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव हैं यदि अधिक देर तक ऐसी स्थिति बनी रहे तो शरीर की रचना और क्रियाएं अनेकांत की अवधारणा को तंत्रिकाओं के द्वारा इसके विरोध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती पुष्ट करती हैं तथा मूर्त रूप देती हैं।
.........
2011
स्वर्ण जयंती वर्ष जैन भारती
86. अनेकांत विशेष
|
मार्च-मई, 2002
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org