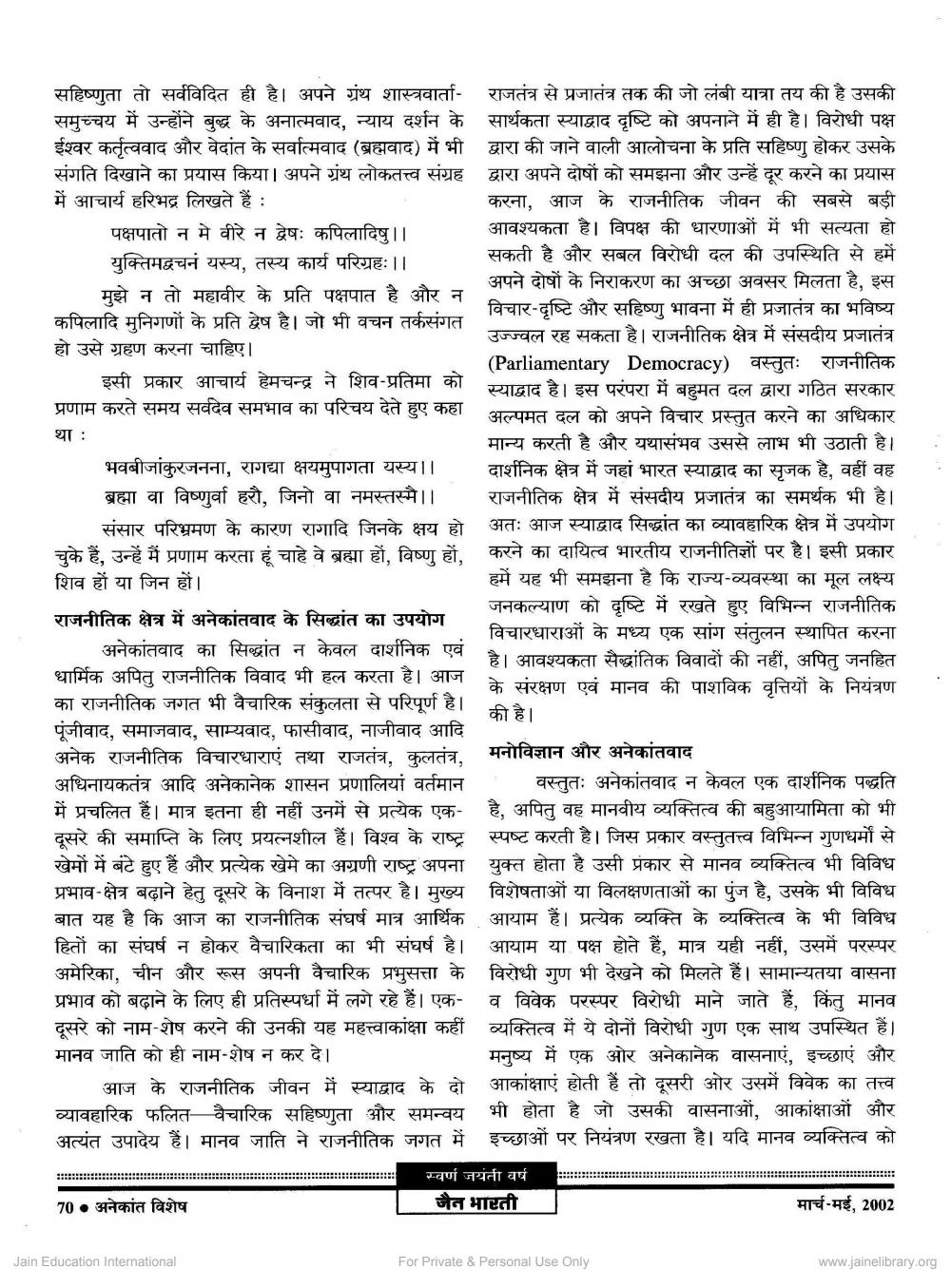________________
सहिष्णुता तो सर्वविदित ही है अपने ग्रंथ शास्त्रवार्ता समुच्चय में उन्होंने बुद्ध के अनात्मवाद, न्याय दर्शन के ईश्वर कर्तृत्ववाद और वेदांत के सर्वात्मवाद (ब्रह्मवाद) में भी संगति दिखाने का प्रयास किया। अपने ग्रंथ लोकतत्त्व संग्रह में आचार्य हरिभद्र लिखते हैं।
:
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । । युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रहः ।।
मुझे न तो महावीर के प्रति पक्षपात है और न कपिलादि मुनिगणों के प्रति द्वेष है। जो भी वचन तर्कसंगत हो उसे ग्रहण करना चाहिए।
-
इसी प्रकार आचार्य हेमचन्द्र ने शिव प्रतिमा को प्रणाम करते समय सर्वदेव समभाव का परिचय देते हुए कहा था :
भवबीजांकुरजनना, रागद्या क्षयमुपागता यस्य । । ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरौ, जिनो वा नमस्तस्मै ।। संसार परिभ्रमण के कारण रागादि जिनके क्षय हो चुके हैं, उन्हें में प्रणाम करता हूं चाहे वे ब्रह्मा हो, विष्णु हों, शिव हों या जिन हों।
राजनीतिक क्षेत्र में अनेकांतवाद के सिद्धांत का उपयोग
अनेकांतवाद का सिद्धांत न केवल दार्शनिक एवं धार्मिक अपितु राजनीतिक विवाद भी हल करता है। आज का राजनीतिक जगत भी वैचारिक संकुलता से परिपूर्ण है। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद, नाजीवाद आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराएं तथा राजतंत्र, कुलतंत्र, अधिनायकतंत्र आदि अनेकानेक शासन प्रणालियां वर्तमान में प्रचलित हैं। मात्र इतना ही नहीं उनमें से प्रत्येक एक दूसरे की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। विश्व के राष्ट्र खेमों में बंटे हुए हैं और प्रत्येक खेमे का अग्रणी राष्ट्र अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने हेतु दूसरे के विनाश में तत्पर है। मुख्य बात यह है कि आज का राजनीतिक संघर्ष मात्र आर्थिक हितों का संघर्ष न होकर वैचारिकता का भी संघर्ष है। अमेरिका, चीन और रूस अपनी वैचारिक प्रभुसत्ता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही प्रतिस्पर्धा में लगे रहे हैं। एकदूसरे को नाम शेष करने की उनकी यह महत्त्वाकांक्षा कहीं - मानव जाति को ही नाम शेष न कर दे।
आज के राजनीतिक जीवन में स्याद्वाद के दो व्यावहारिक फलित वैचारिक सहिष्णुता और समन्वय अत्यंत उपादेय हैं मानव जाति ने राजनीतिक जगत में
70 • अनेकांत विशेष
Jain Education International
राजतंत्र से प्रजातंत्र तक की जो लंबी यात्रा तय की है उसकी सार्थकता स्याद्वाद दृष्टि को अपनाने में ही है। विरोधी पक्ष द्वारा की जाने वाली आलोचना के प्रति सहिष्णु होकर उसके द्वारा अपने दोषों को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, आज के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विपक्ष की धारणाओं में भी सत्यता हो सकती है और सबल विरोधी दल की उपस्थिति से हमें अपने दोषों के निराकरण का अच्छा अवसर मिलता है, इस विचार दृष्टि और सहिष्णु भावना में ही प्रजातंत्र का भविष्य उज्ज्वल रह सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में संसदीय प्रजातंत्र (Parliamentary Democracy) वस्तुतः राजनीतिक स्याद्वाद है। इस परंपरा में बहुमत दल द्वारा गठित सरकार अल्पमत दल को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार मान्य करती है और यथासंभव उससे लाभ भी उठाती है। दार्शनिक क्षेत्र में जहां भारत स्याद्वाद का सृजक है, वहीं वह राजनीतिक क्षेत्र में संसदीय प्रजातंत्र का समर्थक भी है। अतः आज स्याद्वाद सिद्धांत का व्यावहारिक क्षेत्र में उपयोग करने का दायित्व भारतीय राजनीतिज्ञों पर है। इसी प्रकार हमें यह भी समझना है कि राज्य व्यवस्था का मूल लक्ष्य जनकल्याण को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के मध्य एक सांग संतुलन स्थापित करना है आवश्यकता सैद्धांतिक विवादों की नहीं, अपितु जनहित । के संरक्षण एवं मानव की पाशविक वृत्तियों के नियंत्रण की है।
मनोविज्ञान और अनेकांतवाद
वस्तुतः अनेकांतवाद न केवल एक दार्शनिक पद्धति है, अपितु वह मानवीय व्यक्तित्व की बहुआयामिता को भी स्पष्ट करती है । जिस प्रकार वस्तुतत्त्व विभिन्न गुणधर्मों से युक्त होता है उसी प्रकार से मानव व्यक्तित्व भी विविध विशेषताओं या विलक्षणताओं का पुंज है, उसके भी विविध आयाम हैं। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के भी विविध आयाम या पक्ष होते हैं. मात्र यही नहीं, उसमें परस्पर विरोधी गुण भी देखने को मिलते हैं। सामान्यतया वासना व विवेक परस्पर विरोधी माने जाते हैं, किंतु मानव व्यक्तित्व में ये दोनों विरोधी गुण एक साथ उपस्थित हैं। मनुष्य में एक ओर अनेकानेक वासनाएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं तो दूसरी ओर उसमें विवेक का तत्त्व भी होता है जो उसकी वासनाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। यदि मानव व्यक्तित्व को
स्वर्ण जयंती वर्ष
जैन भारती
For Private & Personal Use Only
मार्च मई, 2002
www.jainelibrary.org