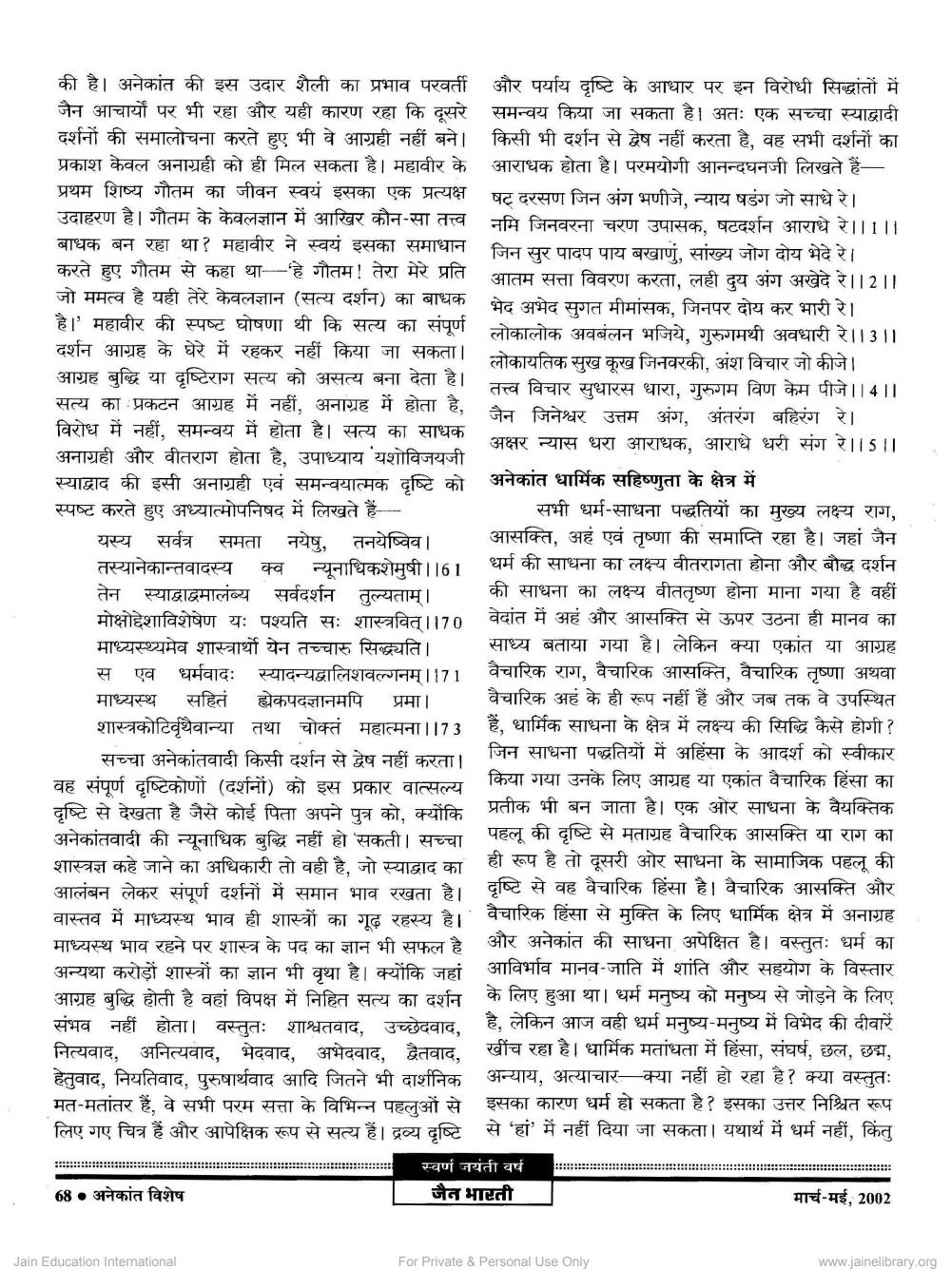________________
की है। अनेकांत की इस उदार शैली का प्रभाव परवर्ती और पर्याय दृष्टि के आधार पर इन विरोधी सिद्धांतों में जैन आचार्यों पर भी रहा और यही कारण रहा कि दूसरे समन्वय किया जा सकता है। अतः एक सच्चा स्याद्वादी दर्शनों की समालोचना करते हुए भी वे आग्रही नहीं बने। किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं करता है, वह सभी दर्शनों का प्रकाश केवल अनाग्रही को ही मिल सकता है। महावीर के आराधक होता है। परमयोगी आनन्दघनजी लिखते हैंप्रथम शिष्य गौतम का जीवन स्वयं इसका एक प्रत्यक्ष षट दरसण जिन अंग भणीजे. न्याय षडंग जो साधे रे। उदाहरण है। गौतम के केवलज्ञान में आखिर कौन-सा तत्त्व नमि जिनवरना चरण उपासक, षटदर्शन आराधे रे।।।।। बाधक बन रहा था? महावीर ने स्वयं इसका समाधान जिन सर पादप पाय बखाणं. सांख्य जोग दोय भेदे रे। करते हुए गौतम से कहा था-'हे गौतम! तेरा मेरे प्रति
आतम सत्ता विवरण करता, लही दुय अंग अखेदे रे।। 2 ।। जो ममत्व है यही तेरे केवलज्ञान (सत्य दर्शन) का बाधक भेद अभेद सगत मीमांसक, जिनपर दोय कर भारी रे। है।' महावीर की स्पष्ट घोषणा थी कि सत्य का संपूर्ण नोमालो गलत प्रजिरो गाम्याथी अवधारी ।।1।। दर्शन आग्रह के घेरे में रहकर नहीं किया जा सकता।
लोकायतिक सुख कूख जिनवरकी, अंश विचार जो कीजे। आग्रह बुद्धि या दृष्टिराग सत्य को असत्य बना देता है।
तत्त्व विचार सुधारस धारा, गुरुगम विण केम पीजे।।4।। सत्य का प्रकटन आग्रह में नहीं, अनाग्रह में होता है,
जैन जिनेश्वर उत्तम अंग, अंतरंग बहिरंग रे। विरोध में नहीं, समन्वय में होता है। सत्य का साधक
अक्षर न्यास धरा आराधक, आराधे धरी संग रे।। 5 ।। अनाग्रही और वीतराग होता है, उपाध्याय यशोविजयजी स्याद्वाद की इसी अनाग्रही एवं समन्वयात्मक दृष्टि को अनेकांत धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में स्पष्ट करते हुए अध्यात्मोपनिषद में लिखते हैं
सभी धर्म-साधना पद्धतियों का मुख्य लक्ष्य राग, यस्य सर्वत्र समता नयेषु, तनयेष्विव।
आसक्ति, अहं एवं तृष्णा की समाप्ति रहा है। जहां जैन तस्यानेकान्तवादस्य क्व न्यूनाधिकशेमुषी।।61
धर्म की साधना का लक्ष्य वीतरागता होना और बौद्ध दर्शन तेन स्याद्वाद्वमालंब्य सर्वदर्शन तुल्यताम्।
की साधना का लक्ष्य वीततृष्ण होना माना गया है वहीं मोक्षोद्देशाविशेषेण यः पश्यति सः शास्त्रवित्।।70 वेदांत में अहं और आसक्ति से ऊपर उठना ही मानव का माध्यस्थ्यमेव शास्त्रार्थो येन तच्चारु सिद्ध्यति।
साध्य बताया गया है। लेकिन क्या एकांत या आग्रह स एव धर्मवादः स्यादन्यद्वालिशवल्गनम्।171 वैचारिक राग, वैचारिक आसक्ति, वैचारिक तृष्णा अथवा माध्यस्थ सहितं ह्येकपदज्ञानमपि प्रमा। वैचारिक अहं के ही रूप नहीं हैं और जब तक वे उपस्थित शास्त्रकोटिवृथैवान्या तथा चोक्तं महात्मना।।73
हैं, धार्मिक साधना के क्षेत्र में लक्ष्य की सिद्धि कैसे होगी? सच्चा अनेकांतवादी किसी दर्शन से द्वेष नहीं करता।
जिन साधना पद्धतियों में अहिंसा के आदर्श को स्वीकार वह संपूर्ण दृष्टिकोणों (दर्शनों) को इस प्रकार वात्सल्य
किया गया उनके लिए आग्रह या एकांत वैचारिक हिंसा का दृष्टि से देखता है जैसे कोई पिता अपने पुत्र को, क्योंकि
प्रतीक भी बन जाता है। एक ओर साधना के वैयक्तिक अनेकांतवादी की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं हो सकती। सच्चा
पहलू की दृष्टि से मताग्रह वैचारिक आसक्ति या राग का
ही रूप है तो दूसरी ओर साधना के सामाजिक पहलू की आलंबन लेकर संपर्ण दर्शनों में समान भाव रखता है। दृष्टि से वह वैचारिक हिसा है। वैचारिक आसक्ति और वास्तव में माध्यस्थ भाव ही शास्त्रों का गूढ रहस्य है। वैचारिक हिंसा से मुक्ति के लिए धार्मिक क्षेत्र में अनाग्रह माध्यस्थ भाव रहने पर शास्त्र के पद का ज्ञान भी सफल है और अनेकांत की साधना अपेक्षित है। वस्तुतः धर्म का अन्यथा करोड़ों शास्त्रों का ज्ञान भी वृथा है। क्योंकि जहां
आविर्भाव मानव-जाति में शांति और सहयोग के विस्तार आग्रह बुद्धि होती है वहां विपक्ष में निहित सत्य का दर्शन के लिए हुआ था। धर्म मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए संभव नहीं होता। वस्तुतः शाश्वतवाद, उच्छेदवाद, है, लेकिन आज वही धर्म मनुष्य-मनुष्य में विभेद की दीवारें नित्यवाद, अनित्यवाद, भेदवाद, अभेदवाद. द्वैतवाद. खींच रहा है। धार्मिक मतांधता में हिंसा, संघर्ष, छल, छद्म, हेतवाद, नियतिवाद, पुरुषार्थवाद आदि जितने भी दार्शनिक अन्याय, अत्याचार क्या नहीं हो रहा है? क्या वस्तुतः मत-मतांतर हैं, वे सभी परम सत्ता के विभिन्न पहलओं से इसका कारण धर्म हो सकता है? इसका उत्तर निश्चित रूप लिए गए चित्र हैं और आपेक्षिक रूप से सत्य हैं। द्रव्य दृष्टि से 'हां' में नहीं दिया जा सकता। यथार्थ में धर्म नहीं, किंतु 1 11111111111111111 स्वर्ण जयंती वर्ष
1111111111111111111
1 68. अनेकांत विशेष
जैन भारती
मार्च-मई, 2002
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org