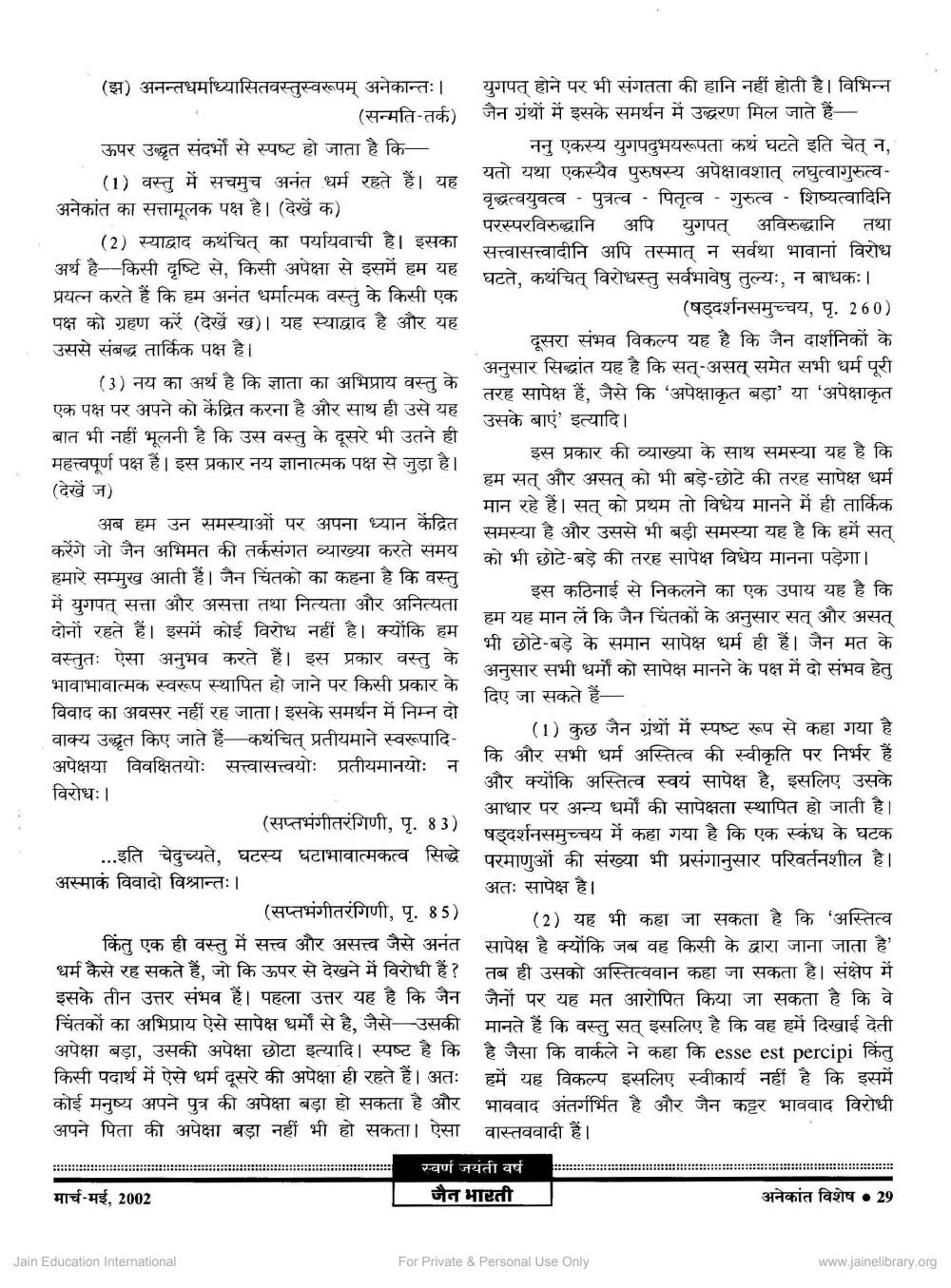________________
(झ) अनन्तधर्माध्यासितवस्तुस्वरूपम् अनेकान्तः। युगपत् होने पर भी संगतता की हानि नहीं होती है। विभिन्न
(सन्मति-तर्क) जैन ग्रंथों में इसके समर्थन में उद्धरण मिल जाते हैंऊपर उद्धत संदर्भो से स्पष्ट हो जाता है कि
ननु एकस्य युगपदुभयरूपता कथं घटते इति चेत् न, (1) वस्तु में सचमुच अनंत धर्म रहते हैं। यह यतो यथा एकस्यैव पुरुषस्य अपेक्षावशात् लघुत्वागुरुत्वअनेकांत का सत्तामूलक पक्ष है। (देखें क)
वृद्धत्वयुवत्व - पुत्रत्व - पितृत्व - गुरुत्व - शिष्यत्वादिनि
परस्परविरुद्धानि अपि युगपत् अविरुद्धानि तथा (2) स्याद्वाद कथंचित् का पर्यायवाची है। इसका
सत्त्वासत्त्वादीनि अपि तस्मात् न सर्वथा भावानां विरोध अर्थ है-किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से इसमें हम यह
घटते, कथंचित् विरोधस्तु सर्वभावेषु तुल्यः, न बाधकः। प्रयत्न करते हैं कि हम अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक
(षड्दर्शनसमुच्चय, पृ. 260) पक्ष को ग्रहण करें (देखें ख)। यह स्याद्वाद है और यह उससे संबद्ध तार्किक पक्ष है।
दूसरा संभव विकल्प यह है कि जैन दार्शनिकों के
अनुसार सिद्धांत यह है कि सत्-असत् समेत सभी धर्म पूरी (3) नय का अर्थ है कि ज्ञाता का अभिप्राय वस्तु के
तरह सापेक्ष हैं, जैसे कि 'अपेक्षाकृत बड़ा' या 'अपेक्षाकृत एक पक्ष पर अपने को केंद्रित करना है और साथ ही उसे यह
उसके बाएं' इत्यादि। बात भी नहीं भूलनी है कि उस वस्तु के दूसरे भी उतने ही महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। इस प्रकार नय ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा है।
इस प्रकार की व्याख्या के साथ समस्या यह है कि (देखें ज)
हम सत् और असत् को भी बड़े-छोटे की तरह सापेक्ष धर्म
मान रहे हैं। सत् को प्रथम तो विधेय मानने में ही तार्किक अब हम उन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित
समस्या है और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि हमें सत् करेंगे जो जैन अभिमत की तर्कसंगत व्याख्या करते समय
को भी छोटे-बड़े की तरह सापेक्ष विधेय मानना पड़ेगा। हमारे सम्मुख आती हैं। जैन चिंतको का कहना है कि वस्तु
इस कठिनाई से निकलने का एक उपाय यह है कि में युगपत् सत्ता और असत्ता तथा नित्यता और अनित्यता
हम यह मान लें कि जैन चिंतकों के अनुसार सत् और असत् दोनों रहते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि हम
भी छोटे-बड़े के समान सापेक्ष धर्म ही हैं। जैन मत के वस्तुतः ऐसा अनुभव करते हैं। इस प्रकार वस्तु के
अनुसार सभी धर्मों को सापेक्ष मानने के पक्ष में दो संभव हेतु भावाभावात्मक स्वरूप स्थापित हो जाने पर किसी प्रकार के
दिए जा सकते हैंविवाद का अवसर नहीं रह जाता। इसके समर्थन में निम्न दो वाक्य उद्धृत किए जाते हैं कथंचित् प्रतीयमाने स्वरूपादि
(1) कुछ जैन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है अपेक्षया विवक्षितयोः सत्त्वासत्त्वयोः प्रतीयमानयोः न
कि और सभी धर्म अस्तित्व की स्वीकृति पर निर्भर हैं
और क्योंकि अस्तित्व स्वयं सापेक्ष है, इसलिए उसके विरोधः।
आधार पर अन्य धर्मों की सापेक्षता स्थापित हो जाती है। (सप्तभंगीतरंगिणी, पृ. 83)
षड्दर्शनसमुच्चय में कहा गया है कि एक स्कंध के घटक ...इति चेदुच्यते, घटस्य घटाभावात्मकत्व सिद्ध परमाणओं की संख्या भी प्रसंगानुसार परिवर्तनशील है। अस्माकं विवादो विश्रान्तः।
अतः सापेक्ष है। (सप्तभंगीतरंगिणी, पृ. 85) (2) यह भी कहा जा सकता है कि 'अस्तित्व किंतु एक ही वस्तु में सत्त्व और असत्त्व जैसे अनंत सापेक्ष है क्योंकि जब वह किसी के द्वारा जाना जाता है धर्म कैसे रह सकते हैं, जो कि ऊपर से देखने में विरोधी हैं? तब ही उसको अस्तित्ववान कहा जा सकता है। संक्षेप में इसके तीन उत्तर संभव हैं। पहला उत्तर यह है कि जैन जैनों पर यह मत आरोपित किया जा सकता है कि वे चिंतकों का अभिप्राय ऐसे सापेक्ष धर्मों से है, जैसे—उसकी मानते हैं कि वस्तु सत् इसलिए है कि वह हमें दिखाई देती अपेक्षा बड़ा, उसकी अपेक्षा छोटा इत्यादि। स्पष्ट है कि है जैसा कि वार्कले ने कहा कि esse est percipi किंतु किसी पदार्थ में ऐसे धर्म दूसरे की अपेक्षा ही रहते हैं। अतः हमें यह विकल्प इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि इसमें कोई मनुष्य अपने पुत्र की अपेक्षा बड़ा हो सकता है और भाववाद अंतर्गर्भित है और जैन कट्टर भाववाद विरोधी अपने पिता की अपेक्षा बड़ा नहीं भी हो सकता। ऐसा वास्तववादी हैं।
HAL
स्वर्ण जयंती वर्ष
::::::::
मार्च-मई, 2002
|
जैन भारती
।
अनेकांत विशेष .29
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org