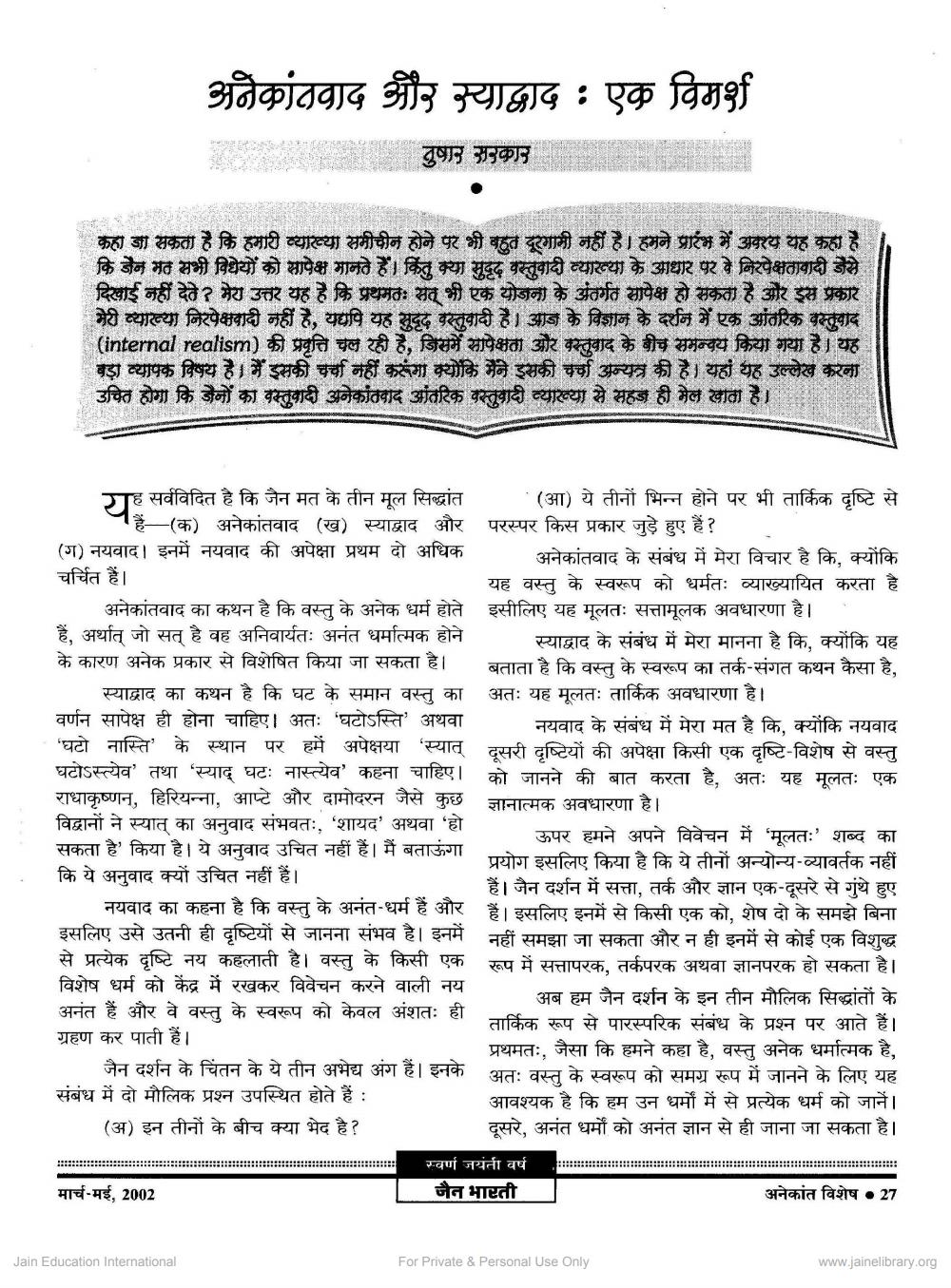________________
कहा जा सकता है कि हमारी व्याख्या समीचीन होने पर भी बहुत दूरगामी नहीं है। हमने प्रारंभ में अवश्य यह कहा है। कि जैन मत सभी विधेयों को सापेक्ष मानते हैं। किंतु क्या सुदृद वस्तुवादी व्याख्या के आधार पर वे निरपेक्षतावादी जैसे दिखाई नहीं देते ? मेरा उत्तर यह है कि प्रथमतः सत् भी एक योजना के अंतर्गत सापेक्ष हो सकता है और इस प्रकार मेरी व्याख्या निरपेक्षवादी नहीं है, यद्यपि यह सुदृद वस्तुवादी है। आज के विज्ञान के दर्शन में एक आंतरिक वस्तुवाद (internal realism) की प्रवृत्ति चल रही है, जिसमें सापेक्षता और वस्तुवाद के बीच समन्वय किया गया है। यह बड़ा व्यापक विषय है। मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसकी चर्चा अन्यत्र की है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जैनों का वस्तुवादी अनेकांतवाद आंतरिक वस्तुवादी व्याख्या से सहज ही मेल खाता है।
अनेकांतवाद और स्याद्वाद : एक विमर्श
तुषार सरकार
यह सर्वविदित है कि जैन मत के तीन मूल सिद्धांत
हैं— (क) अनेकांतवाद (ख) स्याद्वाद और (ग) नयवाद। इनमें नयवाद की अपेक्षा प्रथम दो अधिक चर्चित हैं।
अनेकांतवाद का कथन है कि वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अर्थात् जो सत् है वह अनिवार्यतः अनंत धर्मात्मक होने के कारण अनेक प्रकार से विशेषित किया जा सकता है।
।
स्याद्वाद का कथन है कि घट के समान वस्तु का वर्णन सापेक्ष ही होना चाहिए। अतः 'घटोऽस्ति' अथवा 'घटो नास्ति' के स्थान पर हमें अपेक्षया 'स्यात् घटोऽस्त्येव' तथा 'स्याद् घटः नास्त्येव' कहना चाहिए राधाकृष्णन, हिरियन्ना, आप्टे और दामोदरन जैसे कुछ विद्वानों ने स्यात् का अनुवाद संभवतः, 'शायद' अथवा 'हो सकता है' किया है। ये अनुवाद उचित नहीं हैं। मैं बताऊंगा कि ये अनुवाद क्यों उचित नहीं है।
नयवाद का कहना है कि वस्तु के अनंत धर्म हैं और इसलिए उसे उतनी ही दृष्टियों से जानना संभव है। इनमें से प्रत्येक दृष्टि नय कहलाती है। वस्तु के किसी एक विशेष धर्म को केंद्र में रखकर विवेचन करने वाली नय अनंत हैं और वे वस्तु के स्वरूप को केवल अंशतः ही ग्रहण कर पाती हैं।
जैन दर्शन के चिंतन के ये तीन अभेद्य अंग हैं। इनके संबंध में दो मौलिक प्रश्न उपस्थित होते हैं :
(अ) इन तीनों के बीच क्या भेद है?
मार्च - मई, 2002
Jain Education International
(आ) ये तीनों भिन्न होने पर भी तार्किक दृष्टि से परस्पर किस प्रकार जुड़े हुए हैं ?
अनेकांतवाद के संबंध में मेरा विचार है कि, क्योंकि यह वस्तु के स्वरूप को धर्मतः व्याख्यायित करता है इसीलिए यह मूलतः सत्तामूलक अवधारणा है।
स्याद्वाद के संबंध में मेरा मानना है कि, क्योंकि यह बताता है कि वस्तु के स्वरूप का तर्क संगत कथन कैसा है, अतः यह मूलतः तार्किक अवधारणा है।
-
नयवाद के संबंध में मेरा मत है कि, क्योंकि नयवाद दूसरी दृष्टियों की अपेक्षा किसी एक दृष्टि-विशेष से वस्तु को जानने की बात करता है, अतः यह मूलतः एक ज्ञानात्मक अवधारणा है।
ऊपर हमने अपने विवेचन में 'मूलतः ' शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि ये तीनों अन्योन्य व्यावर्तक नहीं हैं। जैन दर्शन में सत्ता, तर्क और ज्ञान एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं। इसलिए इनमें से किसी एक को, शेष दो के समझे बिना नहीं समझा जा सकता और न ही इनमें से कोई एक विशुद्ध रूप में सत्तापरक, तर्कपरक अथवा ज्ञानपरक हो सकता है।
अब हम जैन दर्शन के इन तीन मौलिक सिद्धांतों के तार्किक रूप से पारस्परिक संबंध के प्रश्न पर आते हैं। प्रथमतः, जैसा कि हमने कहा है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अतः वस्तु के स्वरूप को समग्र रूप में जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन धर्मों में से प्रत्येक धर्म को जानें। दूसरे, अनंत धर्मों को अनंत ज्ञान से ही जाना जा सकता है।
स्वर्ण जयंती वर्ष जैन भारती
For Private & Personal Use Only
अनेकांत विशेष • 27
www.jainelibrary.org