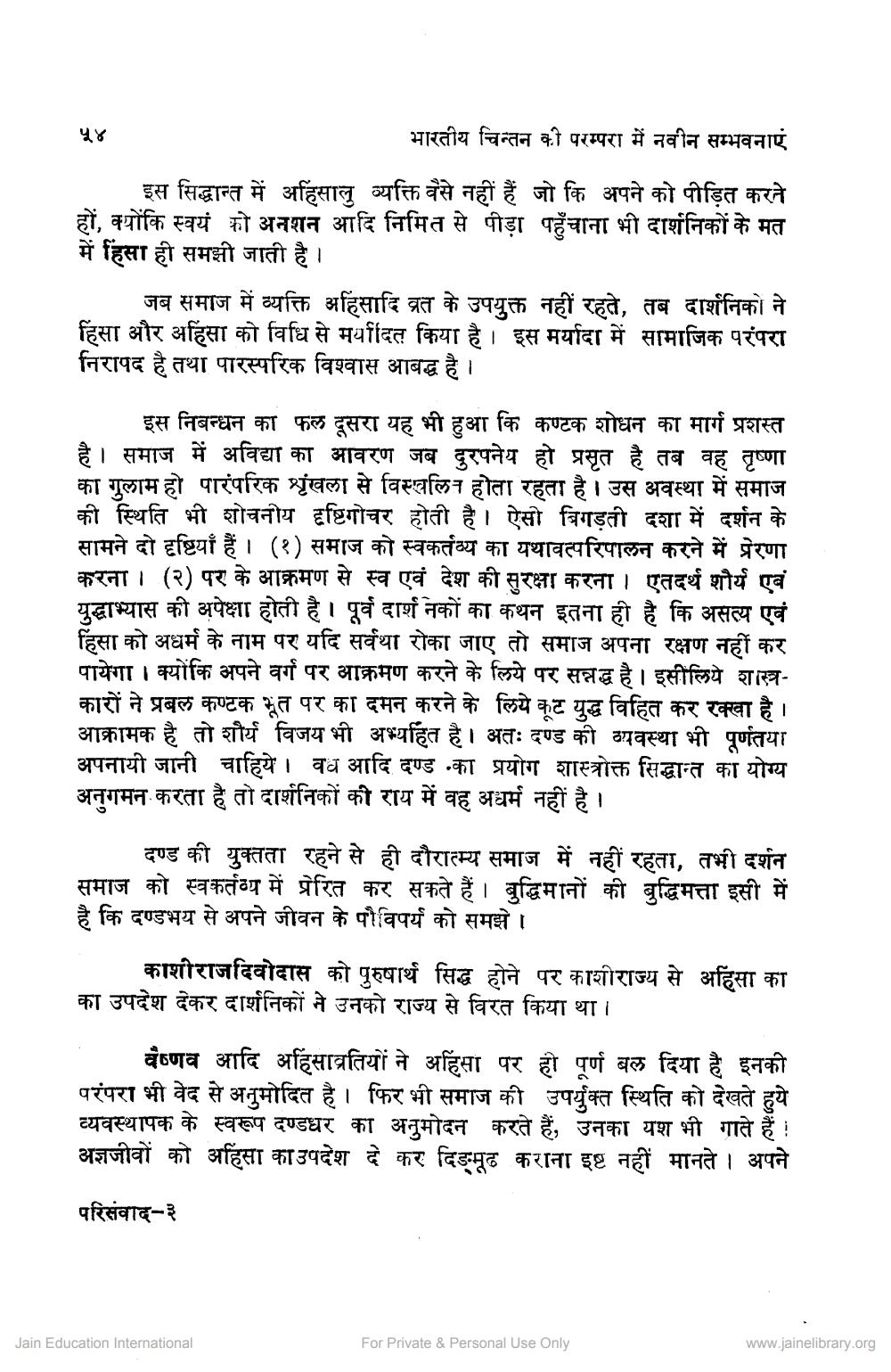________________
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भवनाएं
इस सिद्धान्त में अहिंसालु व्यक्ति वैसे नहीं हैं जो कि अपने को पीड़ित करने हों, क्योंकि स्वयं को अनशन आदि निमित से पीड़ा पहुँचाना भी दार्शनिकों के मत में हिंसा ही समझी जाती है ।
૧૪
जब समाज में व्यक्ति अहिंसादि व्रत के उपयुक्त नहीं रहते, तब दार्शनिको ने हिंसा और अहिंसा को विधि से मर्यादित किया है। इस मर्यादा में सामाजिक परंपरा निरापद है तथा पारस्परिक विश्वास आबद्ध है ।
इस निबन्धन का फल दूसरा यह भी हुआ कि कण्टक शोधन का मार्ग प्रशस्त है। समाज में अविद्या का आवरण जब दुरपनेय हो प्रसृत है तब वह तृष्णा का गुलाम हो पारंपरिक श्रृंखला से विस्खलित होता रहता है । उस अवस्था में समाज की स्थिति भी शोचनीय दृष्टिगोचर होती है । ऐसी बिगड़ती दशा में दर्शन के सामने दो दृष्टियाँ हैं । (१) समाज को स्वकर्तव्य का यथावत्परिपालन करने में प्रेरणा करना । (२) पर के आक्रमण से स्व एवं देश की सुरक्षा करना । एतदर्थ शौर्य एवं युद्धाभ्यास की अपेक्षा होती है । पूर्व दार्श नकों का कथन इतना ही है कि असत्य एवं हिंसा को अधर्म के नाम पर यदि सर्वथा रोका जाए तो समाज अपना रक्षण नहीं कर पायेगा । क्योंकि अपने वर्ग पर आक्रमण करने के लिये पर सन्नद्ध है । इसीलिये शास्त्रकारों ने प्रबल कण्टक भूत पर का दमन करने के लिये कूट युद्ध विहित कर रक्खा है । आक्रामक है तो शौर्य विजय भी अभ्यर्हित है । अतः दण्ड की व्यवस्था भी पूर्णतया अपनायी जानी चाहिये । वध आदि दण्ड का प्रयोग शास्त्रोक्त सिद्धान्त का योग्य अनुगमन करता है तो दार्शनिकों की राय में वह अधर्म नहीं है ।
I
दण्ड की युक्तता रहने से ही दौरात्म्य समाज में नहीं रहता, तभी दर्शन समाज को स्वकर्तव्य में प्रेरित कर सकते हैं । बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है कि दण्डभय से अपने जीवन के पौविपर्य को समझे ।
काशीराज दिवोदास को पुरुषार्थ सिद्ध होने पर काशीराज्य से अहिंसा का का उपदेश देकर दार्शनिकों ने उनको राज्य से विरत किया था ।
वैष्णव आदि अहिंसाव्रतियों ने अहिंसा पर ही पूर्ण बल दिया है इनकी परंपरा भी वेद से अनुमोदित है । फिर भी समाज की उपर्युक्त स्थिति को देखते हुये व्यवस्थापक के स्वरूप दण्डधर का अनुमोदन करते हैं, उनका यश भी गाते हैं ! अज्ञजीवों को अहिंसा का उपदेश दे कर दिङ्मूढ कराना इष्ट नहीं मानते । अपने
परिसंवाद - ३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org