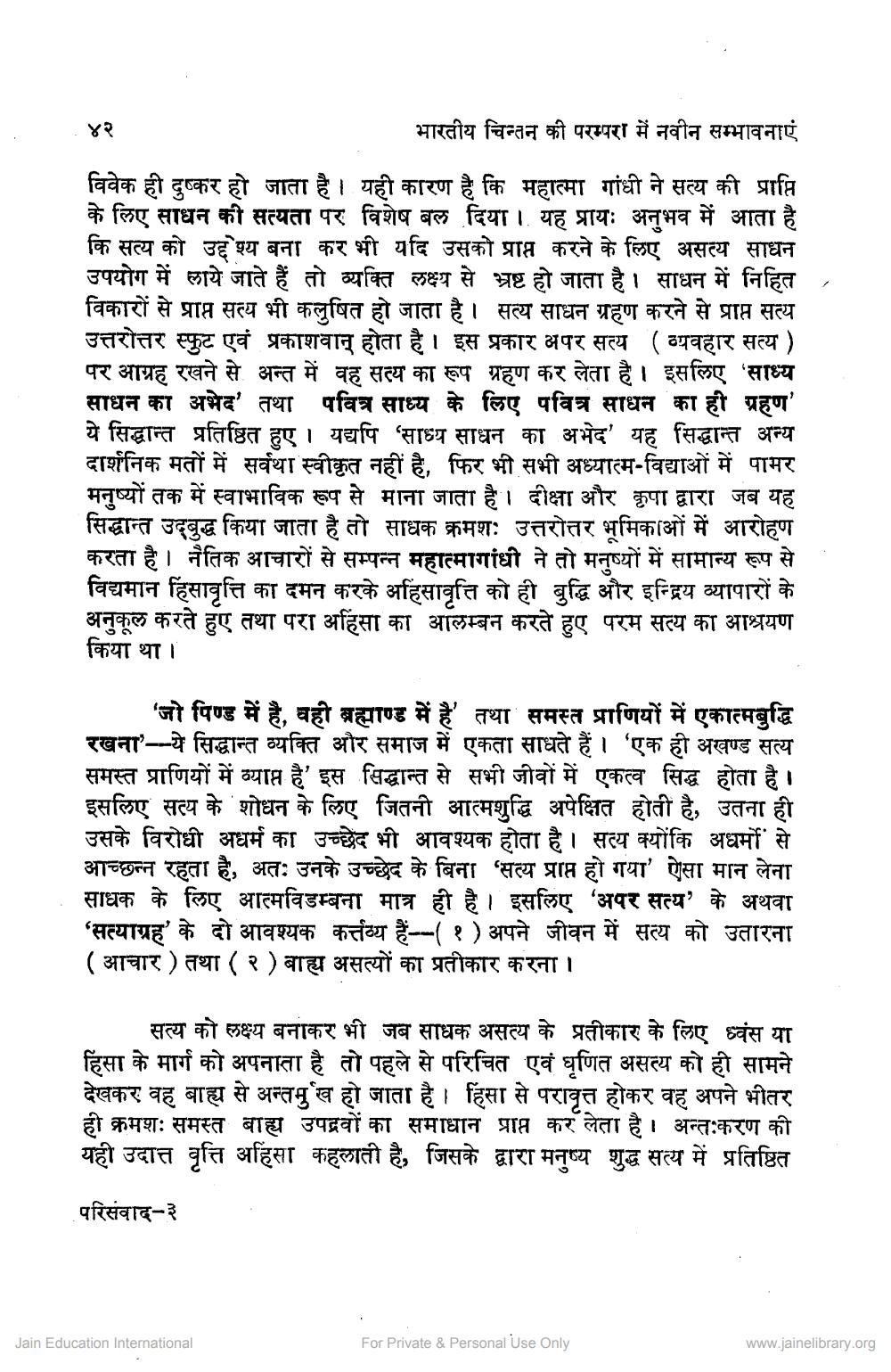________________
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएं
विवेक ही दुष्कर हो जाता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने सत्य की प्राप्ति के लिए साधन की सत्यता पर विशेष बल दिया। यह प्रायः अनुभव में आता है कि सत्य को उद्देश्य बना कर भी यदि उसको प्राप्त करने के लिए असत्य साधन उपयोग में लाये जाते हैं तो व्यक्ति लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। साधन में निहित , विकारों से प्राप्त सत्य भी कलुषित हो जाता है। सत्य साधन ग्रहण करने से प्राप्त सत्य उत्तरोत्तर स्फुट एवं प्रकाशवान् होता है। इस प्रकार अपर सत्य ( व्यवहार सत्य) पर आग्रह रखने से अन्त में वह सत्य' का रूप ग्रहण कर लेता है। इसलिए ‘साध्य साधन का अभेद' तथा पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन का ही ग्रहण' ये सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुए। यद्यपि 'साध्य साधन का अभेद' यह सिद्धान्त अन्य दार्शनिक मतों में सर्वथा स्वीकृत नहीं है, फिर भी सभी अध्यात्म-विद्याओं में पामर मनुष्यों तक में स्वाभाविक रूप से माना जाता है। दीक्षा और कृपा द्वारा जब यह सिद्धान्त उबुद्ध किया जाता है तो साधक क्रमशः उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरोहण करता है। नैतिक आचारों से सम्पन्न महात्मागांधी ने तो मनुष्यों में सामान्य रूप से विद्यमान हिंसावृत्ति का दमन करके अहिंसावृत्ति को ही बुद्धि और इन्द्रिय व्यापारों के अनुकूल करते हुए तथा परा अहिंसा का आलम्बन करते हुए परम सत्य का आश्रयण किया था।
'जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में हैं तथा समस्त प्राणियों में एकात्मबुद्धि रखना'-ये सिद्धान्त व्यक्ति और समाज में एकता साधते हैं। 'एक ही अखण्ड सत्य समस्त प्राणियों में व्याप्त है' इस सिद्धान्त से सभी जीवों में एकत्व सिद्ध होता है। इसलिए सत्य के शोधन के लिए जितनी आत्मशुद्धि अपेक्षित होती है, उतना ही उसके विरोधी अधर्म का उच्छेद भी आवश्यक होता है। सत्य क्योंकि अधर्मो से आच्छन्न रहता है, अतः उनके उच्छेद के बिना 'सत्य' प्राप्त हो गया' ऐसा मान लेना साधक के लिए आत्मविडम्बना मात्र ही है। इसलिए 'अपर सत्य' के अथवा 'सत्याग्रह' के दो आवश्यक कर्तव्य हैं--(१) अपने जीवन में सत्य को उतारना (आचार) तथा (२) बाह्य असत्यों का प्रतीकार करना।
सत्य' को लक्ष्य बनाकर भी जब साधक असत्य के प्रतीकार के लिए ध्वंस या हिंसा के मार्ग को अपनाता है तो पहले से परिचित एवं घृणित असत्य को ही सामने देखकर वह बाह्य से अन्तर्मुख हो जाता है। हिंसा से परावृत्त होकर वह अपने भीतर ही क्रमशः समस्त बाह्य उपद्रवों का समाधान प्राप्त कर लेता है। अन्तःकरण की यही उदात्त वृत्ति अहिंसा कहलाती है, जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित
परिसंवाद-३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org