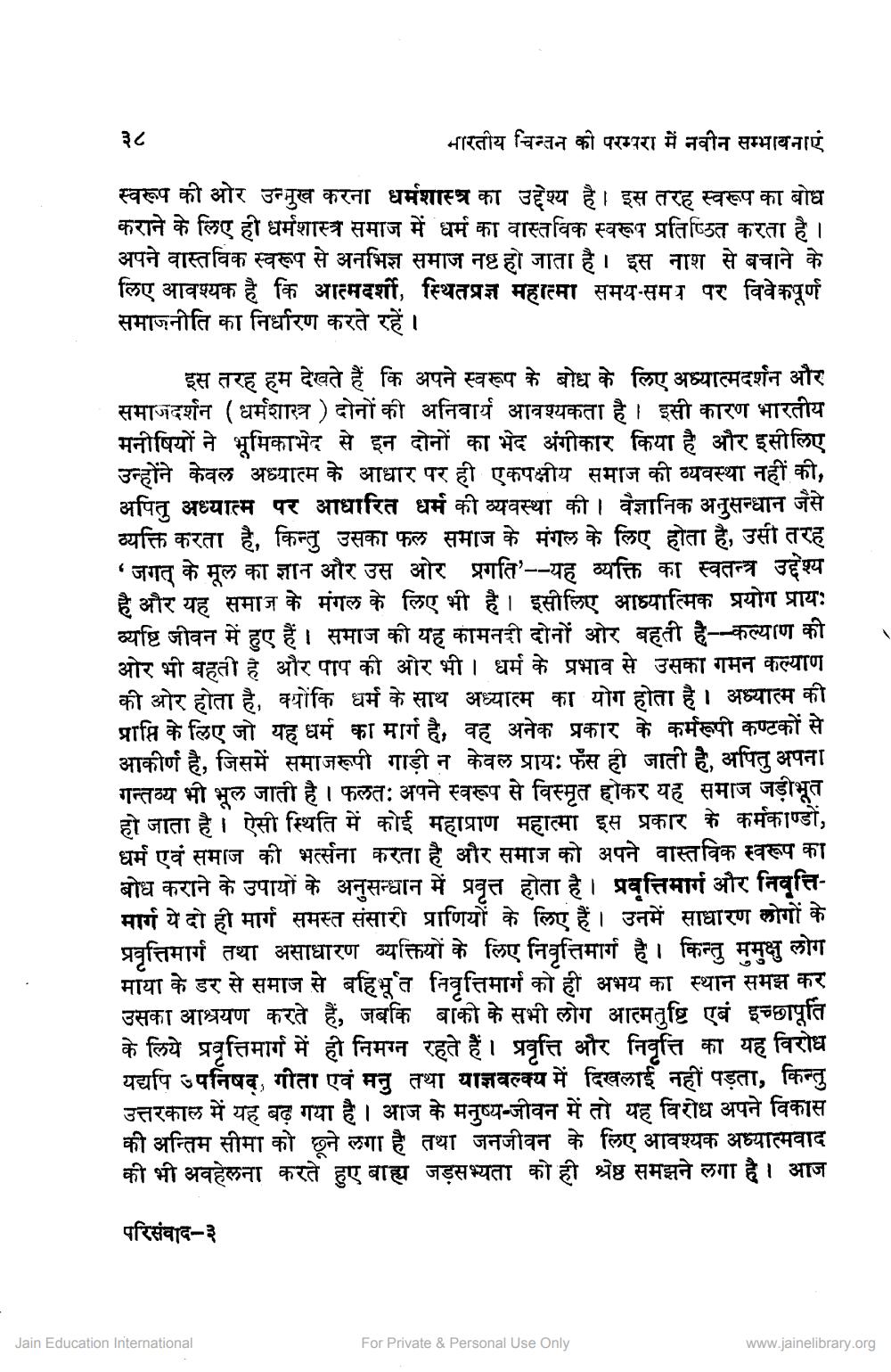________________
३८
भारतीय चिन्तन को परम्परा में नवीन सम्भावनाएं
स्वरूप की ओर उन्मुख करना धर्मशास्त्र का उद्देश्य है। इस तरह स्वरूप का बोध कराने के लिए ही धर्मशास्त्र समाज में धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रतिष्ठित करता है । अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ समाज नष्ट हो जाता है। इस नाश से बचाने के लिए आवश्यक है कि आत्मदर्शी, स्थितप्रज्ञ महात्मा समय-समय पर विवेकपूर्ण समाजनीति का निर्धारण करते रहें।
इस तरह हम देखते हैं कि अपने स्वरूप के बोध के लिए अध्यात्मदर्शन और समाजदर्शन (धर्मशास्त्र) दोनों की अनिवार्य आवश्यकता है। इसी कारण भारतीय मनीषियों ने भूमिकाभेद से इन दोनों का भेद अंगीकार किया है और इसीलिए उन्होंने केवल अध्यात्म के आधार पर ही एकपक्षीय समाज की व्यवस्था नहीं की, अपितु अध्यात्म पर आधारित धर्म की व्यवस्था की। वैज्ञानिक अनुसन्धान जैसे व्यक्ति करता है, किन्तु उसका फल समाज के मंगल के लिए होता है, उसी तरह 'जगत् के मूल का ज्ञान और उस ओर प्रगति'--यह व्यक्ति का स्वतन्त्र उद्देश्य है और यह समाज के मंगल के लिए भी है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रयोग प्रायः व्यष्टि जीवन में हुए हैं। समाज की यह कामनदी दोनों ओर बहती है--कल्याण की ओर भी बहती है और पाप की ओर भी। धर्म के प्रभाव से उसका गमन कल्याण की ओर होता है, क्योंकि धर्म के साथ अध्यात्म का योग होता है। अध्यात्म की प्राप्ति के लिए जो यह धर्म का मार्ग है, वह अनेक प्रकार के कर्मरूपी कण्टकों से आकीर्ण है, जिसमें समाजरूपी गाड़ी न केवल प्रायः फंस ही जाती है, अपितु अपना गन्तव्य भी भूल जाती है । फलतः अपने स्वरूप से विस्मृत होकर यह समाज जड़ीभूत हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई महाप्राण महात्मा इस प्रकार के कर्मकाण्डों, धर्म एवं समाज की भर्त्सना करता है और समाज को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराने के उपायों के अनुसन्धान में प्रवृत्त होता है। प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग ये दो ही मार्ग समस्त संसारी प्राणियों के लिए हैं। उनमें साधारण लोगों के प्रवृत्तिमार्ग तथा असाधारण व्यक्तियों के लिए निवृत्तिमार्ग है। किन्तु ममुक्षु लोग माया के डर से समाज से बहिभूत निवृत्तिमार्ग को ही अभय का स्थान समझ कर उसका आश्रयण करते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग आत्मतुष्टि एवं इच्छापूर्ति के लिये प्रवृत्तिमार्ग में ही निमग्न रहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह विरोध यद्यपि उपनिषद, गीता एवं मनु तथा याज्ञवल्क्य में दिखलाई नहीं पड़ता, किन्तु उत्तरकाल में यह बढ़ गया है। आज के मनुष्य-जीवन में तो यह विरोध अपने विकास की अन्तिम सीमा को छूने लगा है तथा जनजीवन के लिए आवश्यक अध्यात्मवाद की भी अवहेलना करते हुए बाह्य जड़सभ्यता को ही श्रेष्ठ समझने लगा है। आज
परिसंवाद-३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org