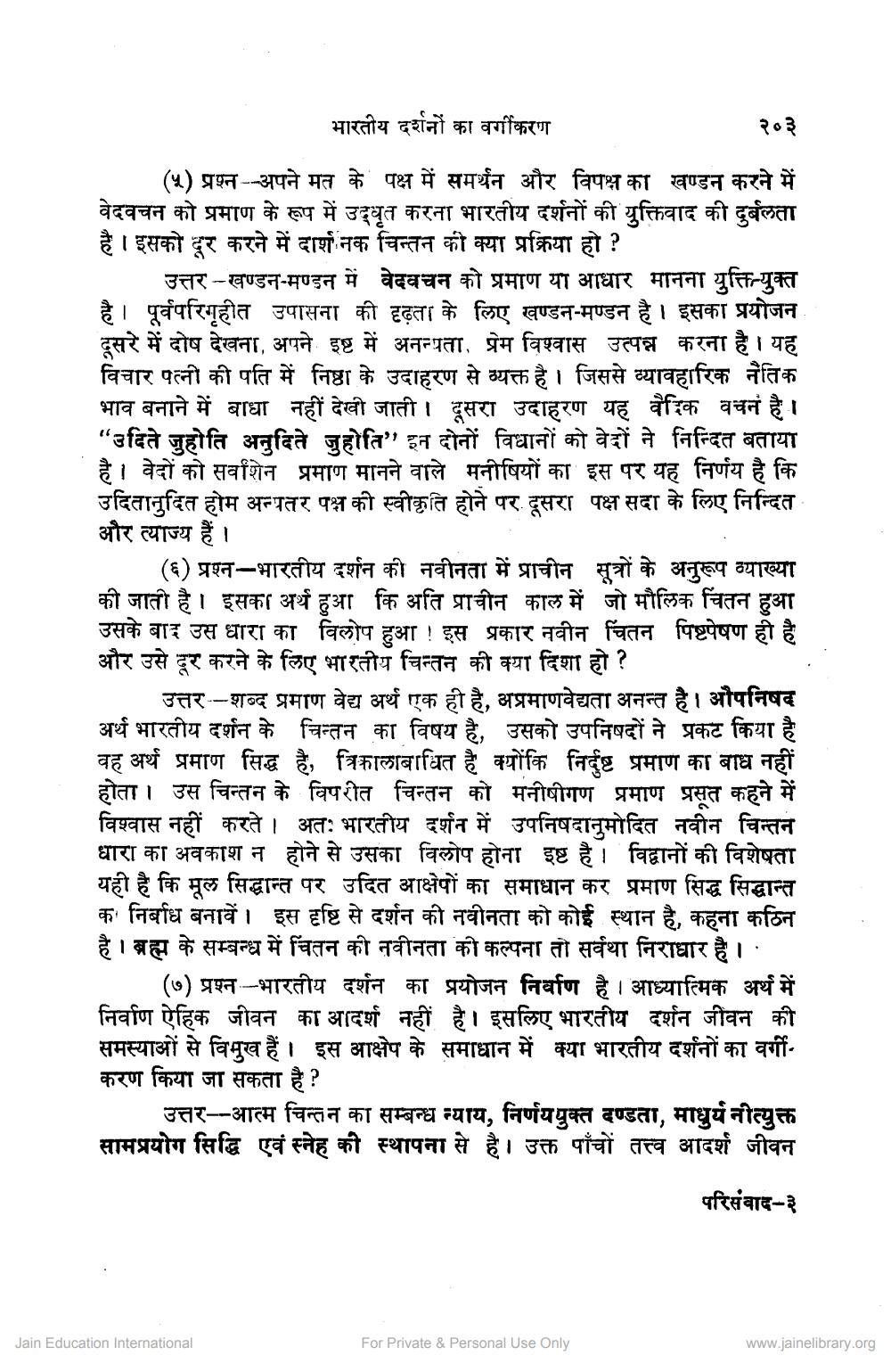________________
भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण
२०३
(५) प्रश्न--अपने मत के पक्ष में समर्थन और विपक्ष का खण्डन करने में वेदवचन को प्रमाण के रूप में उद्धृत करना भारतीय दर्शनों की युक्तिवाद की दुर्बलता है । इसको दूर करने में दार्शनक चिन्तन की क्या प्रक्रिया हो?
__उत्तर-खण्डन-मण्डन में वेदवचन को प्रमाण या आधार मानना युक्ति-युक्त है। पूर्वपरिगृहीत उपासना की दृढ़ता के लिए खण्डन-मण्डन है। इसका प्रयोजन दूसरे में दोष देखना, अपने इष्ट में अनन्यता, प्रेम विश्वास उत्पन्न करना है। यह विचार पत्नी की पति में निष्ठा के उदाहरण से व्यक्त है। जिससे व्यावहारिक नैतिक भाव बनाने में बाधा नहीं देखी जाती। दूसरा उदाहरण यह वैदिक वचनं है । "उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति" इन दोनों विधानों को वेदों ने निन्दित बताया है। वेदों को सर्वांशेन प्रमाण मानने वाले मनीषियों का इस पर यह निर्णय है कि उदितानुदित होम अन्यतर पक्ष की स्वीकृति होने पर दूसरा पक्ष सदा के लिए निन्दित और त्याज्य हैं।
(६) प्रश्न-भारतीय दर्शन की नवीनता में प्राचीन सूत्रों के अनुरूप व्याख्या की जाती है। इसका अर्थ हुआ कि अति प्राचीन काल में जो मौलिक चिंतन हुआ उसके बाद उस धारा का विलोप हुआ । इस प्रकार नवीन चिंतन पिष्टपेषण ही है और उसे दूर करने के लिए भारतीय चिन्तन की क्या दिशा हो ?
उत्तर-शब्द प्रमाण वेद्य अर्थ एक ही है, अप्रमाणवेद्यता अनन्त है। औपनिषद अर्थ भारतीय दर्शन के चिन्तन का विषय है, उसको उपनिषदों ने प्रकट किया है वह अर्थ प्रमाण सिद्ध है, त्रिकालाबाधित है क्योंकि निर्दुष्ट प्रमाण का बाध नहीं होता। उस चिन्तन के विपरीत चिन्तन को मनीषीगण प्रमाण प्रसूत कहने में विश्वास नहीं करते। अतः भारतीय दर्शन में उपनिषदानुमोदित नवीन चिन्तन धारा का अवकाश न होने से उसका विलोप होना इष्ट है। विद्वानों की विशेषता यही है कि मूल सिद्धान्त पर उदित आक्षेपों का समाधान कर प्रमाण सिद्ध सिद्धान्त का निर्बाध बनावें। इस दृष्टि से दर्शन की नवीनता को कोई स्थान है, कहना कठिन है । ब्रह्म के सम्बन्ध में चिंतन की नवीनता की कल्पना तो सर्वथा निराधार है। .
(७) प्रश्न-भारतीय दर्शन का प्रयोजन निर्वाण है। आध्यात्मिक अर्थ में निर्वाण ऐहिक जीवन का आदर्श नहीं है। इसलिए भारतीय दर्शन जीवन की समस्याओं से विमुख हैं। इस आक्षेप के समाधान में क्या भारतीय दर्शनों का वर्गी करण किया जा सकता है ? ।
उत्तर--आत्म चिन्तन का सम्बन्ध न्याय, निर्णययुक्त दण्डता, माधुर्य नीत्युक्त सामप्रयोग सिद्धि एवं स्नेह की स्थापना से है। उक्त पाँचों तत्त्व आदर्श जीवन
परिसंवाद-३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org