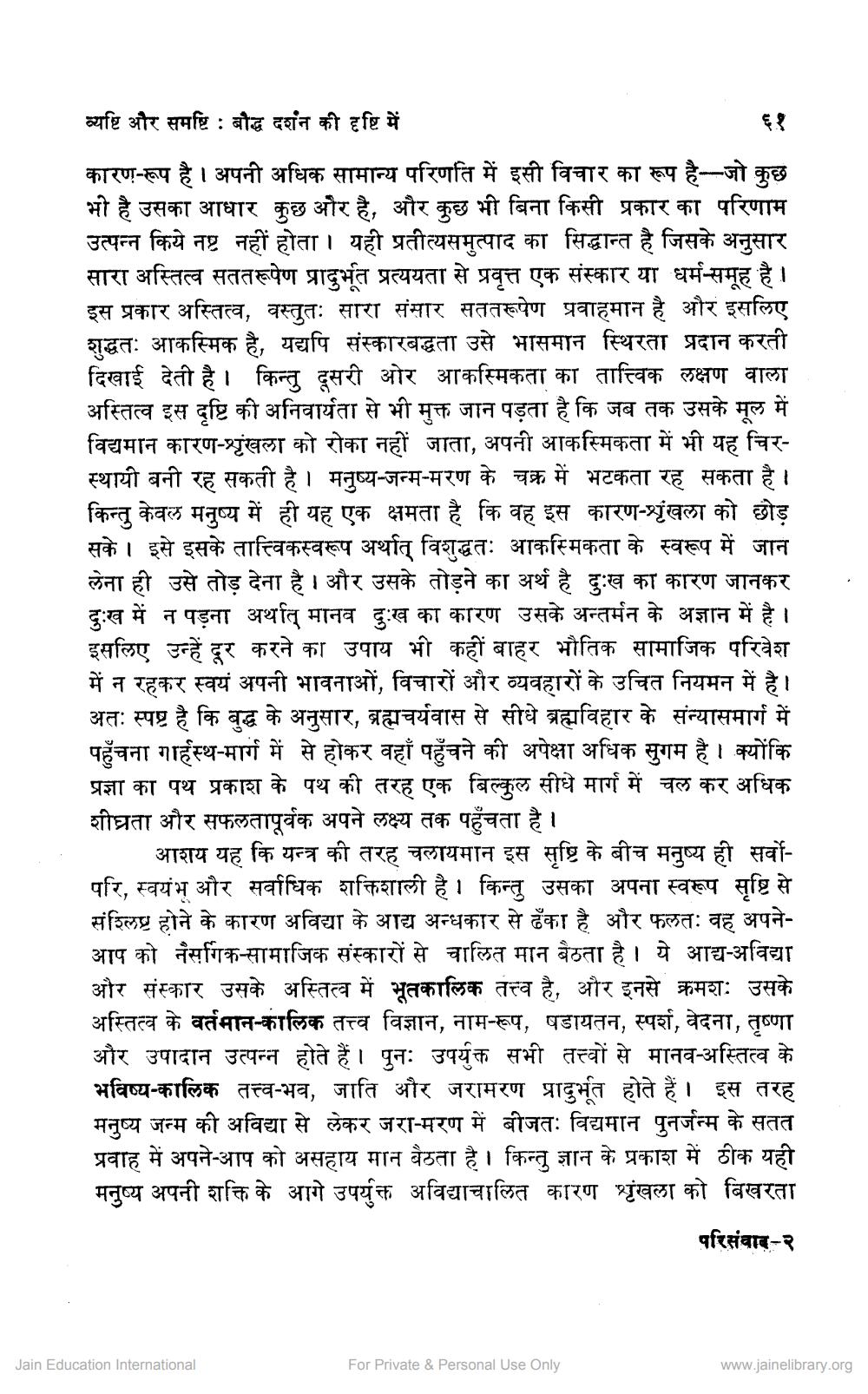________________
व्यष्टि और समष्टि : बौद्ध दर्शन की दृष्टि में
कारण-रूप है । अपनी अधिक सामान्य परिणति में इसी विचार का रूप है-जो कुछ भी है उसका आधार कुछ और है, और कुछ भी बिना किसी प्रकार का परिणाम उत्पन्न किये नष्ट नहीं होता। यही प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त है जिसके अनुसार सारा अस्तित्व सततरूपेण प्रादुर्भूत प्रत्ययता से प्रवृत्त एक संस्कार या धर्म-समूह है। इस प्रकार अस्तित्व, वस्तुतः सारा संसार सततरूपेण प्रवाहमान है और इसलिए शुद्धतः आकस्मिक है, यद्यपि संस्कारबद्धता उसे भासमान स्थिरता प्रदान करती दिखाई देती है। किन्तु दूसरी ओर आकस्मिकता का तात्त्विक लक्षण वाला अस्तित्व इस दृष्टि की अनिवार्यता से भी मुक्त जान पड़ता है कि जब तक उसके मूल में विद्यमान कारण-शृंखला को रोका नहीं जाता, अपनी आकस्मिकता में भी यह चिरस्थायी बनी रह सकती है। मनुष्य-जन्म-मरण के चक्र में भटकता रह सकता है। किन्तु केवल मनुष्य में ही यह एक क्षमता है कि वह इस कारण-शृंखला को छोड़ सके। इसे इसके तात्त्विकस्वरूप अर्थात् विशुद्धतः आकस्मिकता के स्वरूप में जान लेना ही उसे तोड़ देना है। और उसके तोड़ने का अर्थ है दुःख का कारण जानकर दुःख में न पड़ना अर्थात् मानव दुःख का कारण उसके अन्तर्मन के अज्ञान में है। इसलिए उन्हें दूर करने का उपाय भी कहीं बाहर भौतिक सामाजिक परिवेश में न रहकर स्वयं अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों के उचित नियमन में है। अतः स्पष्ट है कि बुद्ध के अनुसार, ब्रह्मचर्यवास से सीधे ब्रह्मविहार के संन्यासमार्ग में पहुँचना गार्हस्थ-मार्ग में से होकर वहाँ पहुँचने की अपेक्षा अधिक सुगम है। क्योंकि प्रज्ञा का पथ प्रकाश के पथ की तरह एक बिल्कुल सीधे मार्ग में चल कर अधिक शीघ्रता और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुँचता है।
आशय यह कि यन्त्र की तरह चलायमान इस सृष्टि के बीच मनुष्य ही सर्वोपरि, स्वयंभ और सर्वाधिक शक्तिशाली है। किन्तु उसका अपना स्वरूप सृष्टि से संश्लिष्ट होने के कारण अविद्या के आद्य अन्धकार से ढंका है और फलतः वह अपनेआप को नैसर्गिक-सामाजिक संस्कारों से चालित मान बैठता है। ये आद्य-अविद्या और संस्कार उसके अस्तित्व में भूतकालिक तत्त्व है, और इनसे क्रमशः उसके अस्तित्व के वर्तमान-कालिक तत्त्व विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा और उपादान उत्पन्न होते हैं। पुनः उपर्युक्त सभी तत्त्वों से मानव-अस्तित्व के भविष्य-कालिक तत्त्व-भव, जाति और जरामरण प्रादुर्भूत होते हैं। इस तरह मनुष्य जन्म की अविद्या से लेकर जरा-मरण में बीजतः विद्यमान पुनर्जन्म के सतत प्रवाह में अपने-आप को असहाय मान बैठता है। किन्तु ज्ञान के प्रकाश में ठीक यही मनुष्य अपनी शक्ति के आगे उपर्युक्त अविद्याचालित कारण शृंखला को बिखरता
परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org