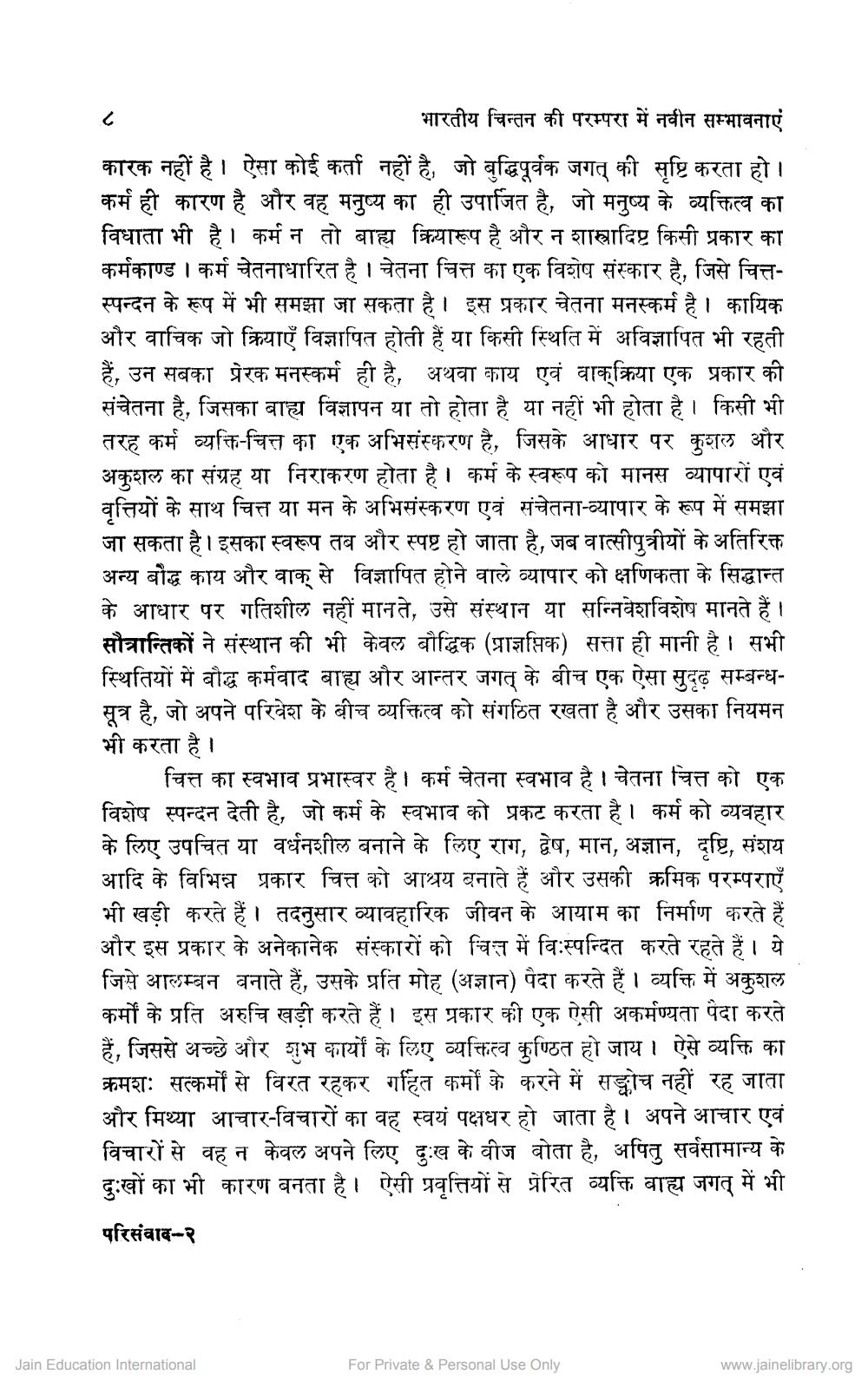________________
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएं कारक नहीं है। ऐसा कोई कर्ता नहीं है, जो बुद्धिपूर्वक जगत् की सृष्टि करता हो । कर्म ही कारण है और वह मनुष्य का ही उपार्जित है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व का विधाता भी है। कर्म न तो बाह्य क्रियारूप है और न शास्त्रादिष्ट किसी प्रकार का कर्मकाण्ड । कर्म चेतनाधारित है । चेतना चित्त का एक विशेष संस्कार है, जिसे चित्तस्पन्दन के रूप में भी समझा जा सकता है। इस प्रकार चेतना मनस्कर्म है। कायिक और वाचिक जो क्रियाएँ विज्ञापित होती हैं या किसी स्थिति में अविज्ञापित भी रहती हैं, उन सबका प्रेरक मनस्कर्म ही है, अथवा काय एवं वाक्रिया एक प्रकार की संचेतना है, जिसका बाह्य विज्ञापन या तो होता है या नहीं भी होता है। किसी भी तरह कर्म व्यक्ति-चित्त का एक अभिसंस्करण है, जिसके आधार पर कुशल और अकुशल का संग्रह या निराकरण होता है। कर्म के स्वरूप को मानस व्यापारों एवं वृत्तियों के साथ चित्त या मन के अभिसंस्करण एवं संचेतना-व्यापार के रूप में समझा जा सकता है। इसका स्वरूप तब और स्पष्ट हो जाता है, जब वात्सीपुत्रीयों के अतिरिक्त अन्य बौद्ध काय और वाक् से विज्ञापित होने वाले व्यापार को क्षणिकता के सिद्धान्त के आधार पर गतिशील नहीं मानते, उसे संस्थान या सन्निवेशविशेष मानते हैं । सौत्रान्तिकों ने संस्थान की भी केवल बौद्धिक (प्राज्ञप्तिक) सत्ता ही मानी है। सभी स्थितियों में बौद्ध कर्मवाद बाह्य और आन्तर जगत् के बीच एक ऐसा सुदृढ़ सम्बन्धसूत्र है, जो अपने परिवेश के बीच व्यक्तित्व को संगठित रखता है और उसका नियमन भी करता है।
चित्त का स्वभाव प्रभास्वर है। कर्म चेतना स्वभाव है । चेतना चित्त को एक विशेष स्पन्दन देती है, जो कर्म के स्वभाव को प्रकट करता है। कर्म को व्यवहार के लिए उपचित या वर्धनशील बनाने के लिए राग, द्वेष, मान, अज्ञान, दृष्टि, संशय आदि के विभिन्न प्रकार चित्त को आश्रय बनाते हैं और उसकी क्रमिक परम्पराएँ भी खड़ी करते हैं। तदनुसार व्यावहारिक जीवन के आयाम का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के अनेकानेक संस्कारों को चित्त में विःस्पन्दित करते रहते हैं। ये जिसे आलम्बन बनाते हैं, उसके प्रति मोह (अज्ञान) पैदा करते हैं। व्यक्ति में अकुशल कर्मों के प्रति अरुचि खड़ी करते हैं। इस प्रकार की एक ऐसी अकर्मण्यता पैदा करते हैं, जिससे अच्छे और शुभ कार्यों के लिए व्यक्तित्व कुण्ठित हो जाय। ऐसे व्यक्ति का क्रमशः सत्कर्मों से विरत रहकर गहित कर्मों के करने में सोच नहीं रह जाता
और मिथ्या आचार-विचारों का वह स्वयं पक्षधर हो जाता है। अपने आचार एवं विचारों से वह न केवल अपने लिए दुःख के वीज बोता है, अपितु सर्वसामान्य के दुःखों का भी कारण बनता है। ऐसी प्रवृत्तियों से प्रेरित व्यक्ति बाह्य जगत् में भी
परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org