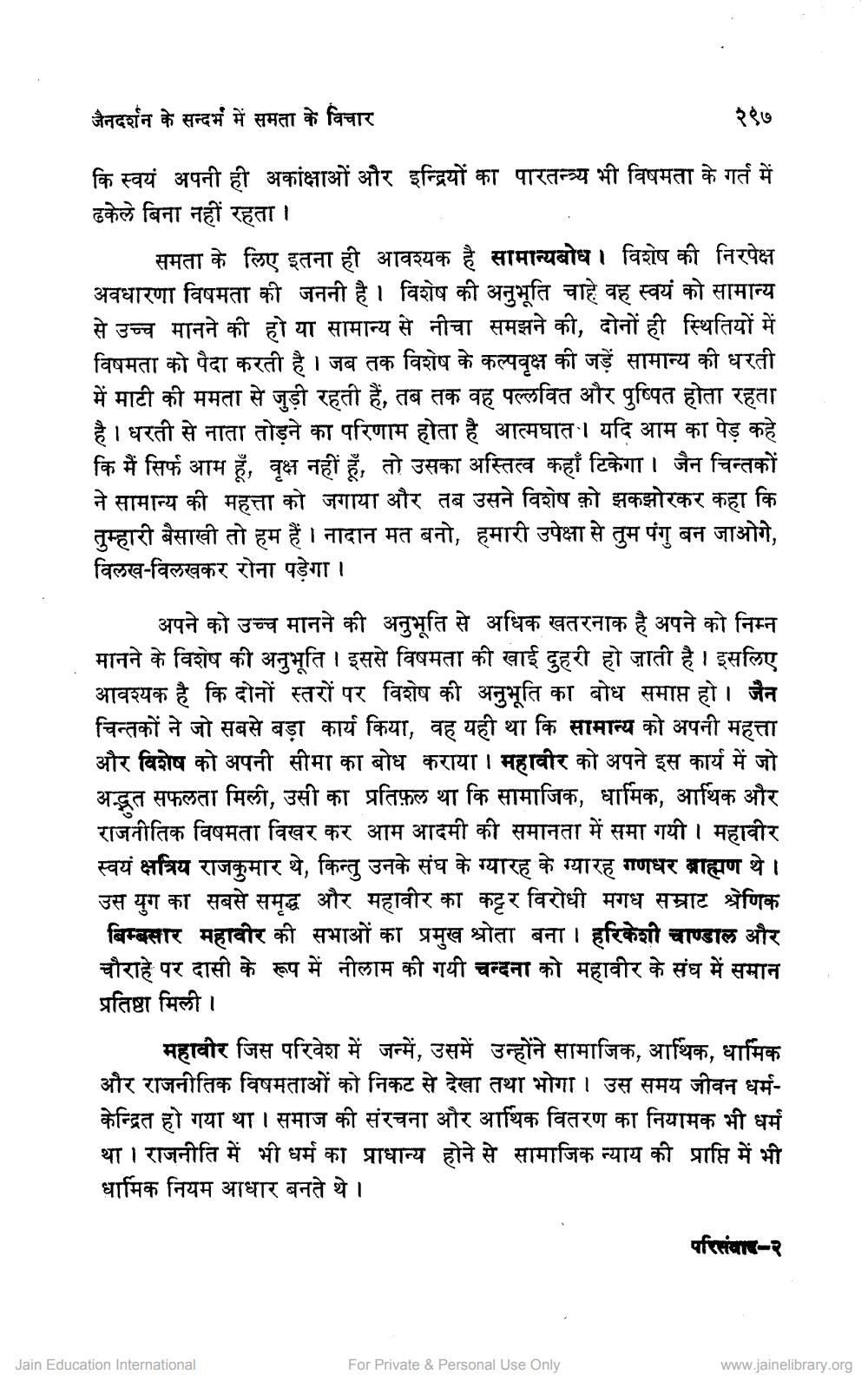________________
जैनदर्शन के सन्दर्भ में समता के विचार
२९७
कि स्वयं अपनी ही अकांक्षाओं और इन्द्रियों का पारतन्त्र्य भी विषमता के गर्त में ढके बिना नहीं रहता ।
समता के लिए इतना ही आवश्यक है सामान्यबोध । विशेष की निरपेक्ष अवधारणा विषमता की जननी है । विशेष की अनुभूति चाहे वह स्वयं को सामान्य से उच्च मानने की हो या सामान्य से नीचा समझने की, दोनों ही स्थितियों में विषमता को पैदा करती है । जब तक विशेष के कल्पवृक्ष की जड़ें सामान्य की धरती में माटी की ममता से जुड़ी रहती हैं, तब तक वह पल्लवित और पुष्पित होता रहता है । धरती से नाता तोड़ने का परिणाम होता है आत्मघात । यदि आम का पेड़ कहे कि मैं सिर्फ आम हूँ, वृक्ष नहीं हूँ, तो उसका अस्तित्व कहाँ टिकेगा । जैन चिन्तकों ने सामान्य की महत्ता को जगाया और तब उसने विशेष को झकझोरकर कहा कि तुम्हारी बैसाखी तो हम हैं । नादान मत बनो, हमारी उपेक्षा से तुम पंगु बन जाओगे, विलख - विलखकर रोना पड़ेगा ।
अपने को उच्च मानने की अनुभूति से अधिक खतरनाक है अपने को निम्न मानने के विशेष की अनुभूति । इससे विषमता की खाई दुहरी हो जाती है । इसलिए आवश्यक है कि दोनों स्तरों पर विशेष की अनुभूति का बोध समाप्त हो । जैन चिन्तकों ने जो सबसे बड़ा कार्य किया, वह यही था कि सामान्य को अपनी महत्ता और विशेष को अपनी सीमा का बोध कराया । महावीर को अपने इस कार्य में जो अद्भुत सफलता मिली, उसी का प्रतिफ़ल था कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता विखर कर आम आदमी की समानता में समा गयी । महावीर स्वयं क्षत्रिय राजकुमार थे, किन्तु उनके संघ के ग्यारह के ग्यारह गणधर ब्राह्मण थे । उस युग का सबसे समृद्ध और महावीर का कट्टर विरोधी मगध सम्राट श्रेणिक बिम्बसार महावीर की सभाओं का प्रमुख श्रोता बना । हरिकेशी चाण्डाल और चौराहे पर दासी के रूप में नीलाम की गयी चन्दना को महावीर के संघ में समान प्रतिष्ठा मिली ।
महावीर जिस परिवेश में जन्में, उसमें उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक विषमताओं को निकट से देखा तथा भोगा । उस समय जीवन धर्मकेन्द्रित हो गया था। समाज की संरचना और आर्थिक वितरण का नियामक भी धर्म था । राजनीति में भी धर्म का प्राधान्य होने से सामाजिक न्याय की प्राप्ति में भी धार्मिक नियम आधार बनते थे ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
परिसंवाद - २
www.jainelibrary.org