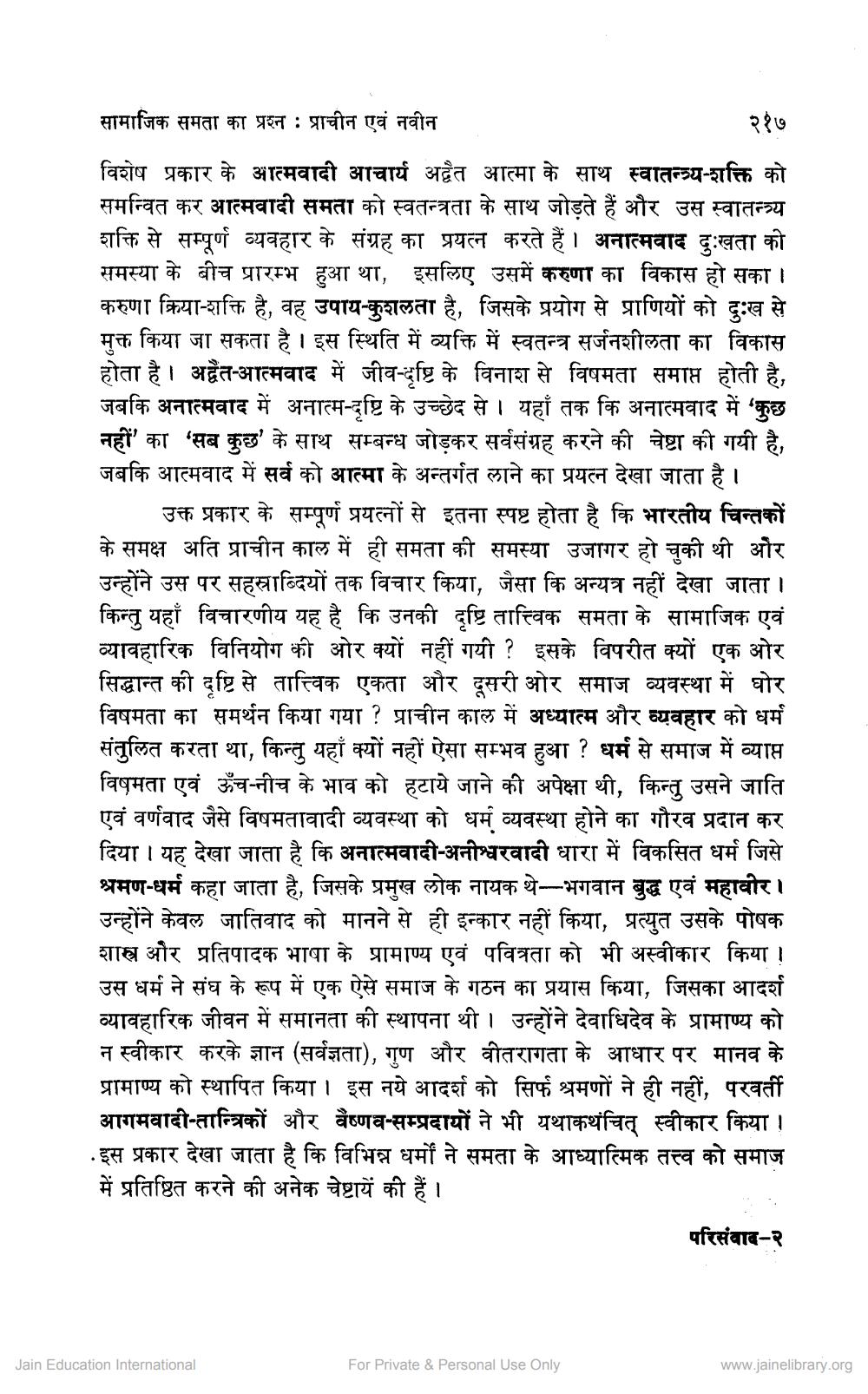________________
सामाजिक समता का प्रश्न : प्राचीन एवं नवीन
२१७ विशेष प्रकार के आत्मवादी आचार्य अद्वैत आत्मा के साथ स्वातन्त्र्य-शक्ति को समन्वित कर आत्मवादी समता को स्वतन्त्रता के साथ जोड़ते हैं और उस स्वातन्त्र्य शक्ति से सम्पूर्ण व्यवहार के संग्रह का प्रयत्न करते हैं। अनात्मवाद दुःखता को समस्या के बीच प्रारम्भ हुआ था, इसलिए उसमें करुणा का विकास हो सका। करुणा क्रिया-शक्ति है, वह उपाय-कुशलता है, जिसके प्रयोग से प्राणियों को दुःख से मुक्त किया जा सकता है । इस स्थिति में व्यक्ति में स्वतन्त्र सर्जनशीलता का विकास होता है। अद्वैत-आत्मवाद में जीव-दृष्टि के विनाश से विषमता समाप्त होती है, जबकि अनात्मवाद में अनात्म-दष्टि के उच्छेद से । यहाँ तक कि अनात्मवाद में 'कुछ नहीं' का 'सब कुछ' के साथ सम्बन्ध जोड़कर सर्वसंग्रह करने की चेष्टा की गयी है, जबकि आत्मवाद में सर्व को आत्मा के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न देखा जाता है।
__उक्त प्रकार के सम्पूर्ण प्रयत्नों से इतना स्पष्ट होता है कि भारतीय चिन्तकों के समक्ष अति प्राचीन काल में ही समता की समस्या उजागर हो चुकी थी और उन्होंने उस पर सहस्राब्दियों तक विचार किया, जैसा कि अन्यत्र नहीं देखा जाता। किन्तु यहाँ विचारणीय यह है कि उनकी दृष्टि तात्त्विक समता के सामाजिक एवं व्यावहारिक विनियोग की ओर क्यों नहीं गयी ? इसके विपरीत क्यों एक ओर सिद्धान्त की दृष्टि से तात्त्विक एकता और दूसरी ओर समाज व्यवस्था में घोर विषमता का समर्थन किया गया ? प्राचीन काल में अध्यात्म और व्यवहार को धर्म संतुलित करता था, किन्तु यहाँ क्यों नहीं ऐसा सम्भव हुआ ? धर्म से समाज में व्याप्त विषमता एवं ऊँच-नीच के भाव को हटाये जाने की अपेक्षा थी, किन्तु उसने जाति एवं वर्णवाद जैसे विषमतावादी व्यवस्था को धर्म व्यवस्था होने का गौरव प्रदान कर दिया। यह देखा जाता है कि अनात्मवादी-अनीश्वरवादी धारा में विकसित धर्म जिसे श्रमण-धर्म कहा जाता है, जिसके प्रमुख लोक नायक थे-भगवान बुद्ध एवं महावीर । उन्होंने केवल जातिवाद को मानने से ही इन्कार नहीं किया, प्रत्युत उसके पोषक शास्त्र और प्रतिपादक भाषा के प्रामाण्य एवं पवित्रता को भी अस्वीकार किया। उस धर्म ने संघ के रूप में एक ऐसे समाज के गठन का प्रयास किया, जिसका आदर्श व्यावहारिक जीवन में समानता की स्थापना थी। उन्होंने देवाधिदेव के प्रामाण्य को न स्वीकार करके ज्ञान (सर्वज्ञता), गुण और वीतरागता के आधार पर मानव के प्रामाण्य को स्थापित किया। इस नये आदर्श को सिर्फ श्रमणों ने ही नहीं, परवर्ती
आगमवादी-तान्त्रिकों और वैष्णव-सम्प्रदायों ने भी यथाकथंचित् स्वीकार किया। .इस प्रकार देखा जाता है कि विभिन्न धर्मों ने समता के आध्यात्मिक तत्त्व को समाज में प्रतिष्ठित करने की अनेक चेष्टायें की हैं।
परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org