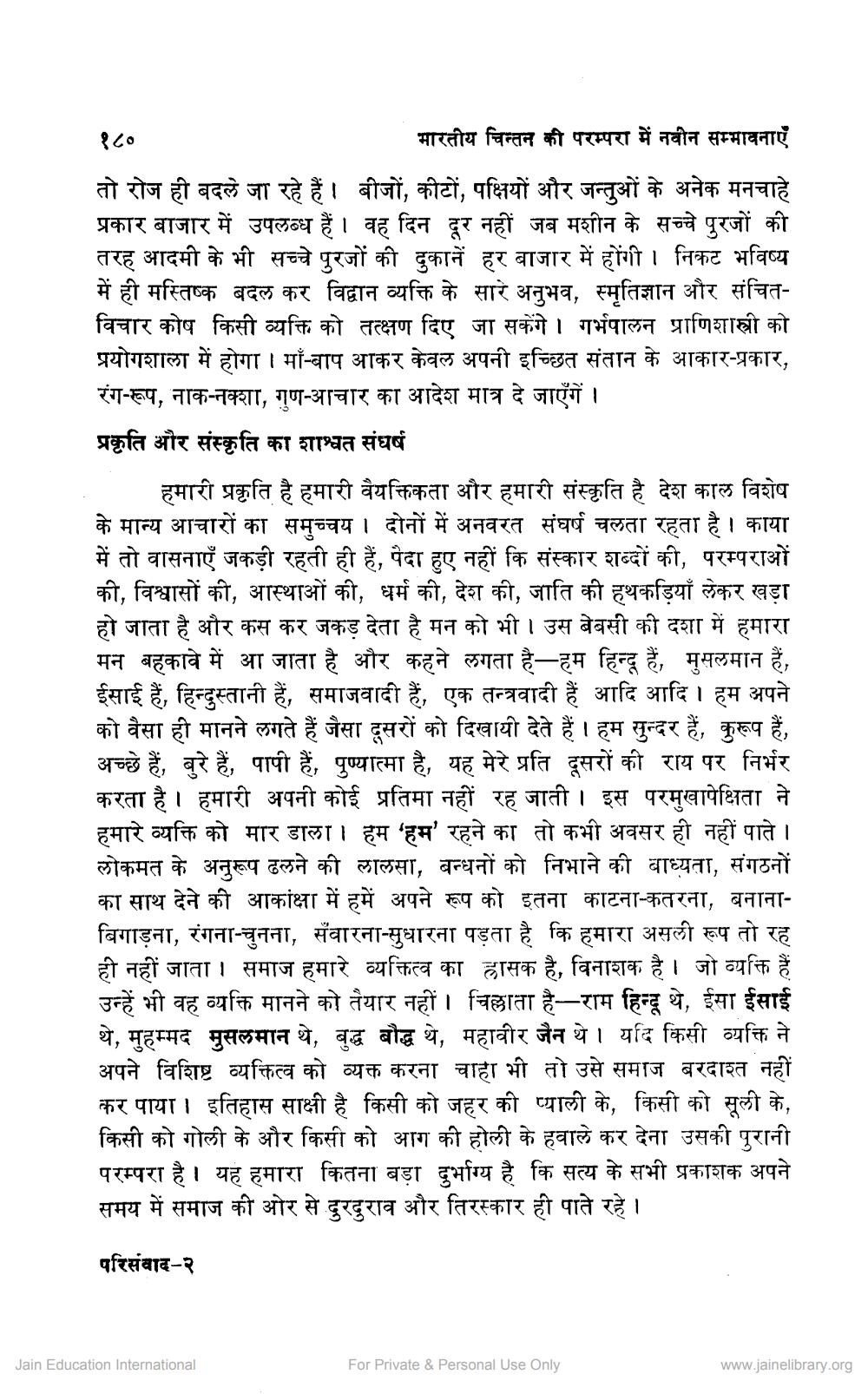________________
१८०
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएं तो रोज ही बदले जा रहे हैं। बीजों, कीटों, पक्षियों और जन्तुओं के अनेक मनचाहे प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। वह दिन दूर नहीं जब मशीन के सच्चे पुरजों की तरह आदमी के भी सच्चे पुरजों की दुकानें हर बाजार में होंगी। निकट भविष्य में ही मस्तिष्क बदल कर विद्वान व्यक्ति के सारे अनुभव, स्मृतिज्ञान और संचितविचार कोष किसी व्यक्ति को तत्क्षण दिए जा सकेंगे। गर्भपालन प्राणिशास्त्री को प्रयोगशाला में होगा। माँ-बाप आकर केवल अपनी इच्छित संतान के आकार-प्रकार, रंग-रूप, नाक-नक्शा, गुण-आचार का आदेश मात्र दे जाएँगें । प्रकृति और संस्कृति का शाश्वत संघर्ष
हमारी प्रकृति है हमारी वैयक्तिकता और हमारी संस्कृति है देश काल विशेष के मान्य आचारों का समुच्चय । दोनों में अनवरत संघर्ष चलता रहता है। काया में तो वासनाएँ जकड़ी रहती ही हैं, पैदा हुए नहीं कि संस्कार शब्दों की, परम्पराओं की, विश्वासों की, आस्थाओं की, धर्म की, देश की, जाति की हथकड़ियाँ लेकर खड़ा हो जाता है और कस कर जकड़ देता है मन को भी। उस बेबसी की दशा में हमारा मन बहकावे में आ जाता है और कहने लगता है-हम हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, हिन्दुस्तानी हैं, समाजवादी हैं, एक तन्त्रवादी हैं आदि आदि। हम अपने को वैसा ही मानने लगते हैं जैसा दूसरों को दिखायी देते हैं । हम सुन्दर हैं, कुरूप हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा है, यह मेरे प्रति दूसरों की राय पर निर्भर करता है। हमारी अपनी कोई प्रतिमा नहीं रह जाती। इस परमुखापेक्षिता ने हमारे व्यक्ति को मार डाला। हम 'हम' रहने का तो कभी अवसर ही नहीं पाते । लोकमत के अनुरूप ढलने की लालसा, बन्धनों को निभाने की बाध्यता, संगठनों का साथ देने की आकांक्षा में हमें अपने रूप को इतना काटना-कतरना, बनानाबिगाड़ना, रंगना-चुनना, सँवारना-सुधारना पड़ता है कि हमारा असली रूप तो रह ही नहीं जाता। समाज हमारे व्यक्तित्व का ह्रासक है, विनाशक है। जो व्यक्ति हैं उन्हें भी वह व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। चिल्लाता है-राम हिन्दू थे, ईसा ईसाई थे, मुहम्मद मुसलमान थे, बुद्ध बौद्ध थे, महावीर जैन थे। यदि किसी व्यक्ति ने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को व्यक्त करना चाहा भी तो उसे समाज बरदाश्त नहीं कर पाया। इतिहास साक्षी है किसी को जहर की प्याली के, किसी को सूली के, किसी को गोली के और किसी को आग की होली के हवाले कर देना उसकी पुरानी परम्परा है। यह हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्य के सभी प्रकाशक अपने समय में समाज की ओर से दुरदुराव और तिरस्कार ही पाते रहे ।
परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org