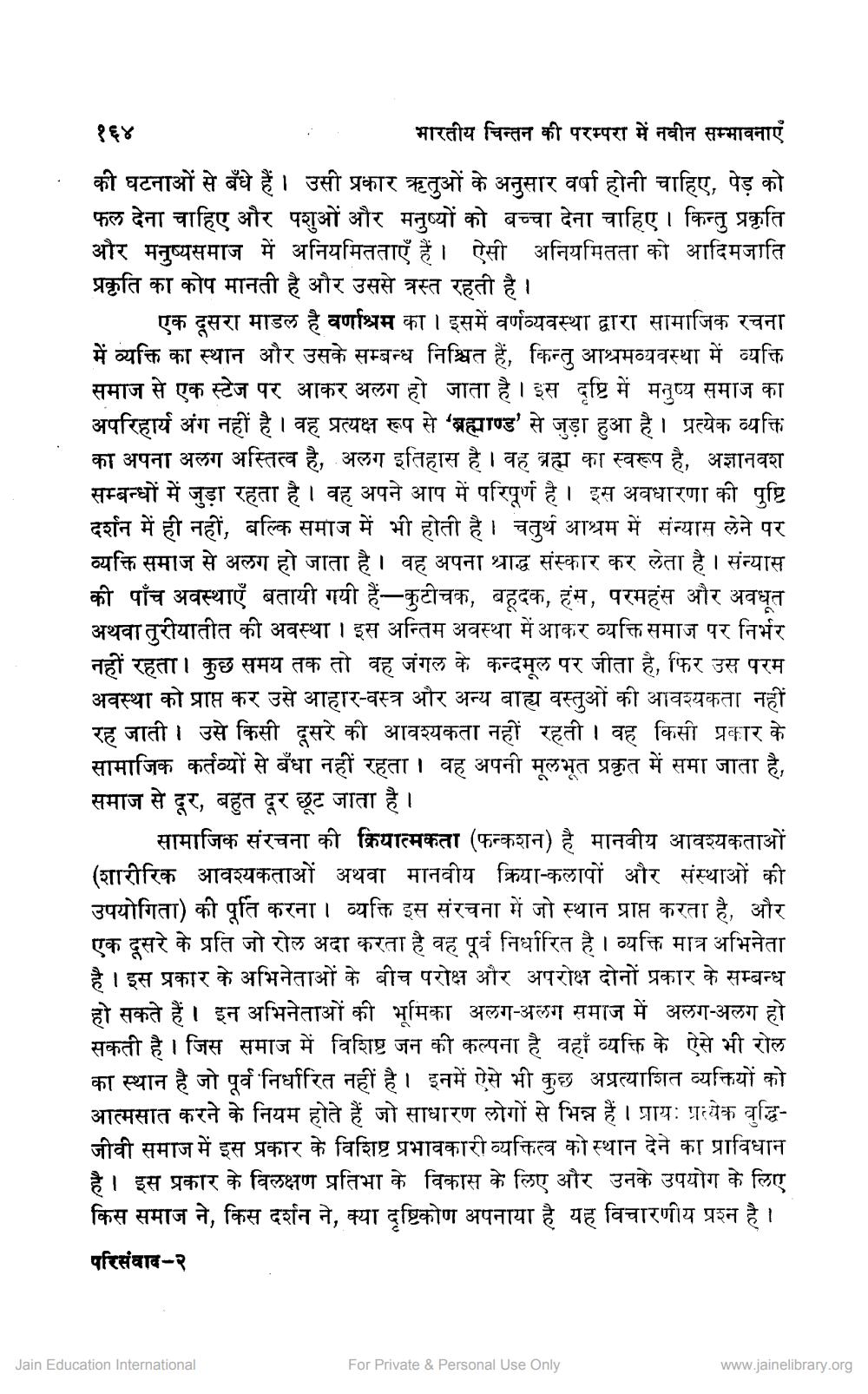________________
१६४
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएँ
की घटनाओं से बँधे हैं । उसी प्रकार ऋतुओं के अनुसार वर्षा होनी चाहिए, पेड़ को फल देना चाहिए और पशुओं और मनुष्यों को बच्चा देना चाहिए । किन्तु प्रकृति और मनुष्यसमाज में अनियमितताएँ हैं । ऐसी अनियमितता को आदिमजाति प्रकृति का कोप मानती है और उससे त्रस्त रहती है ।
एक दूसरा माडल है वर्णाश्रम का । इसमें वर्णव्यवस्था द्वारा सामाजिक रचना में व्यक्ति का स्थान और उसके सम्बन्ध निश्चित हैं, किन्तु आश्रमव्यवस्था में व्यक्ति समाज से एक स्टेज पर आकर अलग हो जाता है । इस दृष्टि में मनुष्य समाज का अपरिहार्य अंग नहीं है । वह प्रत्यक्ष रूप से 'ब्रह्माण्ड' से जुड़ा हुआ है । प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व है, अलग इतिहास है । वह ब्रह्म का स्वरूप है, अज्ञानवश सम्बन्धों में जुड़ा रहता है । वह अपने आप में परिपूर्ण है । इस अवधारणा की पुष्टि दर्शन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी होती है । चतुर्थ आश्रम में संन्यास लेने पर व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है । वह अपना श्राद्ध संस्कार कर लेता है । संन्यास की पाँच अवस्थाएँ बतायी गयी हैं- कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस और अवधूत अथवा तुरीयातीत की अवस्था | इस अन्तिम अवस्था में आकर व्यक्ति समाज पर निर्भर नहीं रहता। कुछ समय तक तो वह जंगल के कन्दमूल पर जीता है, फिर उस परम अवस्था को प्राप्त कर उसे आहार-वस्त्र और अन्य बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती । वह किसी प्रकार के सामाजिक कर्तव्यों से बँधा नहीं रहता । वह अपनी मूलभूत प्रकृत में समा जाता है, समाज से दूर, बहुत दूर छूट जाता है ।
सामाजिक संरचना की क्रियात्मकता (फन्कशन ) है मानवीय आवश्यकताओं (शारीरिक आवश्यकताओं अथवा मानवीय क्रिया-कलापों और संस्थाओं की उपयोगिता ) की पूर्ति करना । व्यक्ति इस संरचना में जो स्थान प्राप्त करता है, और एक दूसरे के प्रति जो रोल अदा करता है वह पूर्व निर्धारित है । व्यक्ति मात्र अभिनेता है । इस प्रकार के अभिनेताओं के बीच परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं । इन अभिनेताओं की भूमिका अलग-अलग समाज में अलग-अलग हो सकती है । जिस समाज में विशिष्ट जन की कल्पना है वहाँ व्यक्ति के ऐसे भी रोल स्थान है जो पूर्व निर्धारित नहीं है । इनमें ऐसे भी कुछ अप्रत्याशित व्यक्तियों को आत्मसात करने के नियम होते हैं जो साधारण लोगों से भिन्न हैं । प्रायः प्रत्येक बुद्धिजीवी समाज में इस प्रकार के विशिष्ट प्रभावकारी व्यक्तित्व को स्थान देने का प्राविधान है । इस प्रकार के विलक्षण प्रतिभा के विकास के लिए और उनके उपयोग के लिए किस समाज ने, किस दर्शन ने, क्या दृष्टिकोण अपनाया है यह विचारणीय प्रश्न है ।
परिसंवाद - २
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org