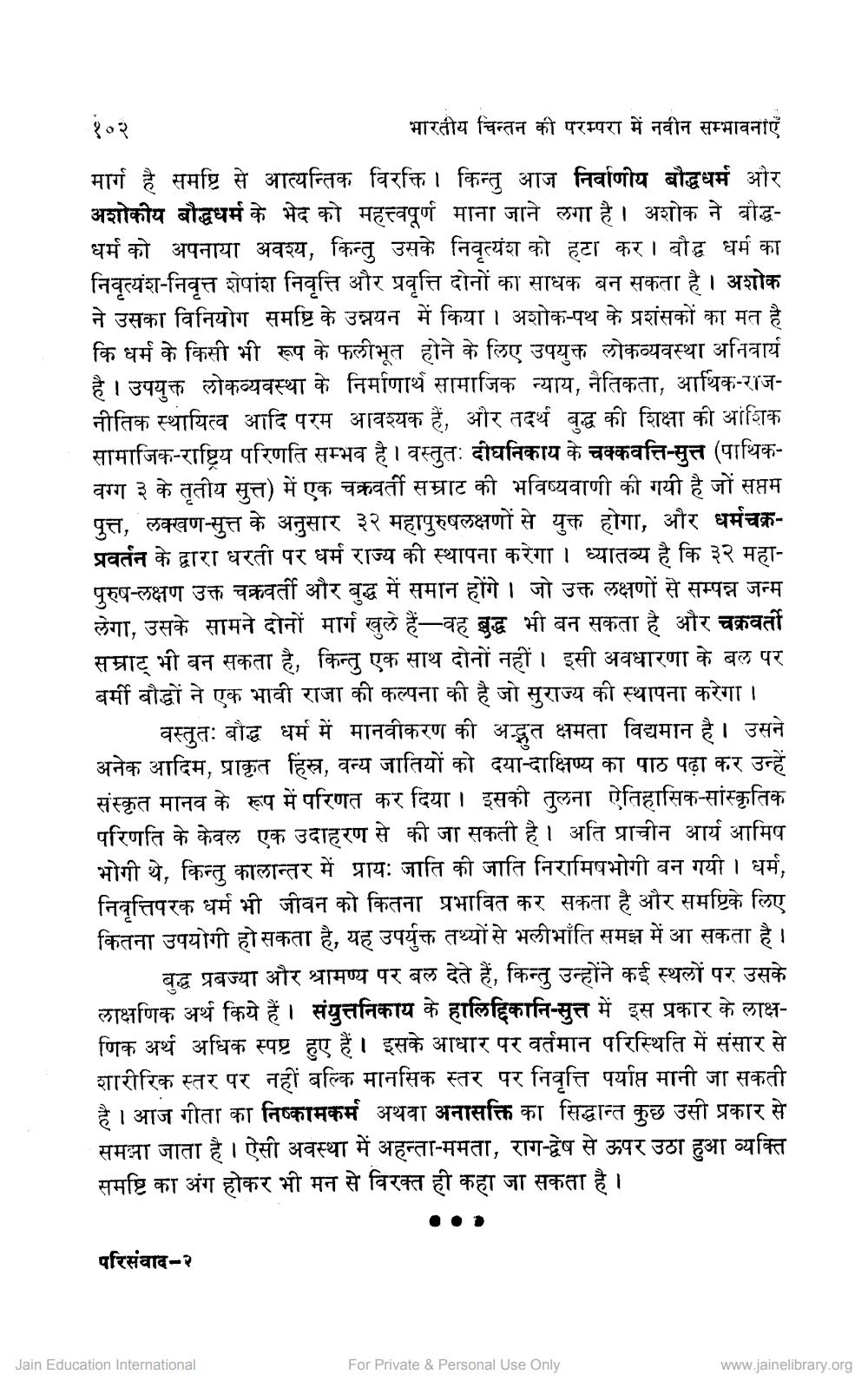________________
१०२
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएँ मार्ग है समष्टि से आत्यन्तिक विरक्ति। किन्तु आज निर्वाणीय बौद्धधर्म और अशोकीय बौद्धधर्म के भेद को महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है। अशोक ने बौद्धधर्म को अपनाया अवश्य, किन्तु उसके निवृत्यंश को हटा कर । बौद्ध धर्म का निवृत्यंश-निवृत्त शेषांश निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का साधक बन सकता है। अशोक ने उसका विनियोग समष्टि के उन्नयन में किया। अशोक-पथ के प्रशंसकों का मत है कि धर्म के किसी भी रूप के फलीभूत होने के लिए उपयुक्त लोकव्यवस्था अनिवार्य है। उपयुक्त लोकव्यवस्था के निर्माणार्थ सामाजिक न्याय, नैतिकता, आर्थिक-राजनीतिक स्थायित्व आदि परम आवश्यक हैं, और तदर्थ बुद्ध की शिक्षा की आंशिक सामाजिक-राष्ट्रिय परिणति सम्भव है। वस्तुतः दीघनिकाय के चक्कवत्ति-सुत्त (पाथिकवग्ग ३ के तृतीय सुत्त) में एक चक्रवर्ती सम्राट की भविष्यवाणी की गयी है जो सप्तम पुत्त, लक्खण-सुत्त के अनुसार ३२ महापुरुषलक्षणों से युक्त होगा, और धर्मचक्रप्रवर्तन के द्वारा धरती पर धर्म राज्य की स्थापना करेगा। ध्यातव्य है कि ३२ महापुरुष-लक्षण उक्त चक्रवर्ती और बुद्ध में समान होंगे। जो उक्त लक्षणों से सम्पन्न जन्म लेगा, उसके सामने दोनों मार्ग खुले हैं—वह बुद्ध भी बन सकता है और चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता है, किन्तु एक साथ दोनों नहीं। इसी अवधारणा के बल पर बर्मी बौद्धों ने एक भावी राजा की कल्पना की है जो सुराज्य की स्थापना करेगा।
वस्तुतः बौद्ध धर्म में मानवीकरण की अद्भत क्षमता विद्यमान है। उसने अनेक आदिम, प्राकृत हिंस्र, वन्य जातियों को दया दाक्षिण्य का पाठ पढ़ा कर उन्हें संस्कृत मानव के रूप में परिणत कर दिया। इसकी तुलना ऐतिहासिक-सांस्कृतिक परिणति के केवल एक उदाहरण से की जा सकती है। अति प्राचीन आर्य आमिष भोगी थे, किन्तु कालान्तर में प्रायः जाति की जाति निरामिषभोगी बन गयी। धर्म, निवृत्तिपरक धर्म भी जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है और समष्टिके लिए कितना उपयोगी हो सकता है, यह उपर्युक्त तथ्यों से भलीभाँति समझ में आ सकता है।
बुद्ध प्रबज्या और श्रामण्य पर बल देते हैं, किन्तु उन्होंने कई स्थलों पर उसके लाक्षणिक अर्थ किये हैं। संयुत्तनिकाय के हालिद्दिकानि-सुत्त में इस प्रकार के लाक्षणिक अर्थ अधिक स्पष्ट हुए हैं। इसके आधार पर वर्तमान परिस्थिति में संसार से शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर निवृत्ति पर्याप्त मानी जा सकती है। आज गीता का निष्कामकर्म अथवा अनासक्ति का सिद्धान्त कुछ उसी प्रकार से समझा जाता है। ऐसी अवस्था में अहन्ता-ममता, राग-द्वेष से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति समष्टि का अंग होकर भी मन से विरक्त ही कहा जा सकता है।
परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org