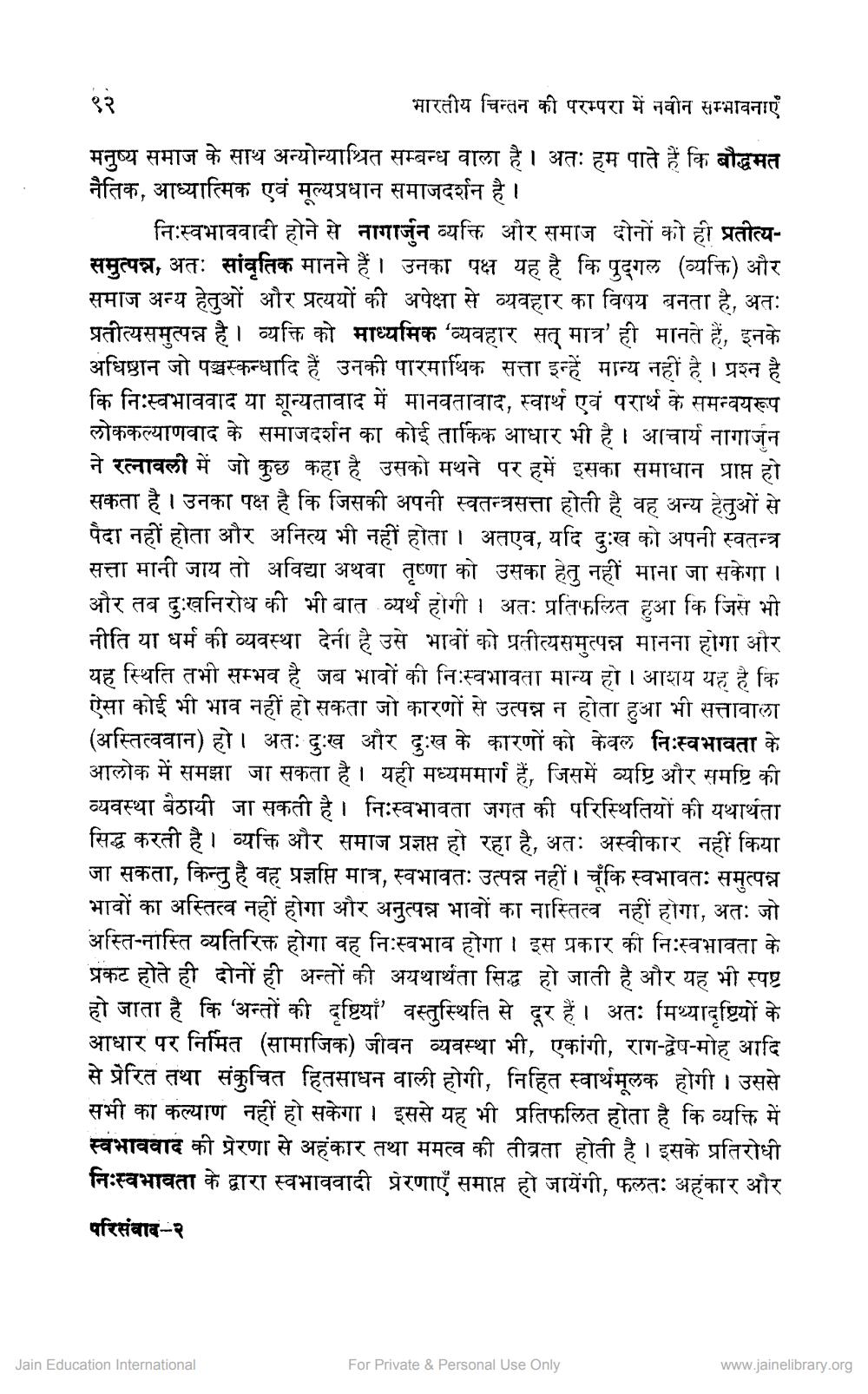________________
९२
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएँ
मनुष्य समाज के साथ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध वाला है । अतः हम पाते हैं कि बौद्धमत नैतिक, आध्यात्मिक एवं मूल्यप्रधान समाजदर्शन है ।
निःस्वभाववादी होने से नागार्जुन व्यक्ति और समाज दोनों को ही प्रतीत्यसमुत्पन्न, अतः सांवृतिक मानने हैं । उनका पक्ष यह है कि पुद्गल (व्यक्ति) और समाज अन्य हेतुओं और प्रत्ययों की अपेक्षा से व्यवहार का विषय बनता है, अतः प्रतीत्यसमुत्पन्न है । व्यक्ति को माध्यमिक 'व्यवहार सत् मात्र' ही मानते हैं, इनके अधिष्ठान जो पञ्चस्कन्धादि हैं उनकी पारमार्थिक सत्ता इन्हें मान्य नहीं है । प्रश्न है कि निःस्वभाववाद या शून्यतावाद में मानवतावाद, स्वार्थ एवं परार्थ के समन्वयरूप लोककल्याणवाद के समाजदर्शन का कोई तार्किक आधार भी है । आचार्य नागार्जुन ने रत्नावली में जो कुछ कहा है उसको मथने पर हमें इसका समाधान प्राप्त हो सकता है । उनका पक्ष है कि जिसकी अपनी स्वतन्त्रसत्ता होती है वह अन्य हेतुओं से पैदा नहीं होता और अनित्य भी नहीं होता । अतएव, यदि दुःख को अपनी स्वतन्त्र सत्ता मानी जाय तो अविद्या अथवा तृष्णा को उसका हेतु नहीं माना जा सकेगा । और तब दुःखनिरोध की भी बात व्यर्थ होगी । अतः प्रतिफलित हुआ कि जिसे भी नीति या धर्म की व्यवस्था देनी है उसे भावों को प्रतीत्यसमुत्पन्न मानना होगा और यह स्थिति तभी सम्भव है जब भावों की निःस्वभावता मान्य हो । आशय यह है कि ऐसा कोई भी भाव नहीं हो सकता जो कारणों से उत्पन्न न होता हुआ भी सत्तावाला ( अस्तित्ववान ) हो । अतः दुःख और दुःख के कारणों को केवल निःस्वभावता के आलोक में समझा जा सकता है । यही मध्यममार्ग हैं, जिसमें व्यष्टि और समष्टि की व्यवस्था बैठायी जा सकती है । निःस्वभावता जगत की परिस्थितियों की यथार्थता सिद्ध करती है । व्यक्ति और समाज प्रज्ञप्त हो रहा है, अतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किन्तु है वह प्रज्ञप्ति मात्र, स्वभावतः उत्पन्न नहीं । चूँकि स्वभावतः समुत्पन्न भावों का अस्तित्व नहीं होगा और अनुत्पन्न भावों का नास्तित्व नहीं होगा, अतः जो अस्ति नास्ति व्यतिरिक्त होगा वह निःस्वभाव होगा। इस प्रकार की नि:स्वभावता के प्रकट होते ही दोनों ही अन्तों की अयथार्थता सिद्ध हो जाती है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 'अन्तों की दृष्टियाँ' वस्तुस्थिति से दूर हैं । अतः मिथ्यादृष्टियों के आधार पर निर्मित (सामाजिक) जीवन व्यवस्था भी, एकांगी, राग-द्वेष - मोह आदि से प्रेरित तथा संकुचित हितसाधन वाली होगी, निहित स्वार्थमूलक होगी । उससे सभी का कल्याण नहीं हो सकेगा । इससे यह भी प्रतिफलित होता है कि व्यक्ति में स्वभाववाद की प्रेरणा से अहंकार तथा ममत्व की तीव्रता होती है । इसके प्रतिरोधी निःस्वभावता के द्वारा स्वभाववादी प्रेरणाएँ समाप्त हो जायेंगी, फलतः अहंकार और
परिसंवाद - २
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org