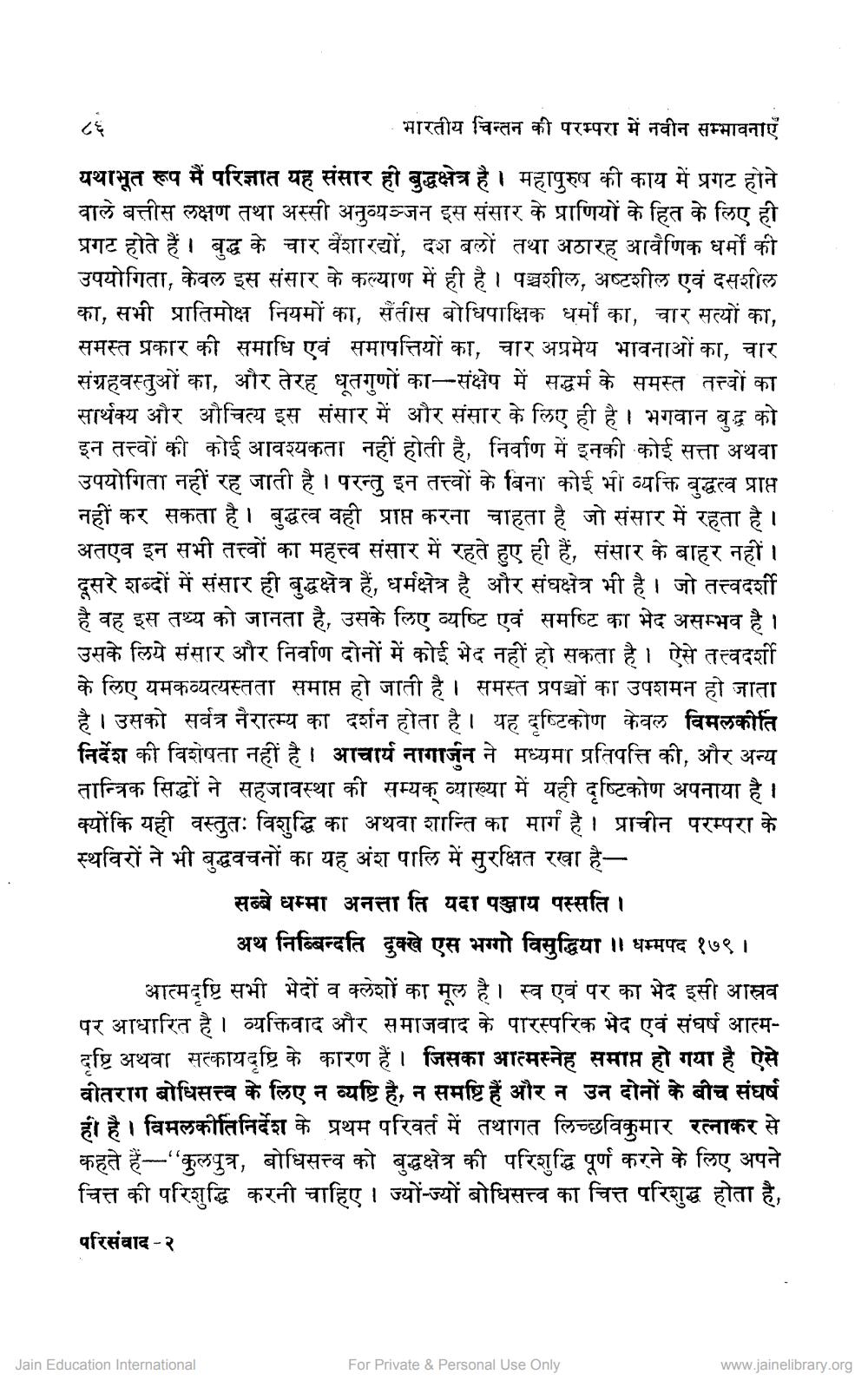________________
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएँ यथाभूत रूप में परिज्ञात यह संसार ही बुद्धक्षेत्र है। महापुरुष की काय में प्रगट होने वाले बत्तीस लक्षण तथा अस्सी अनुव्यञ्जन इस संसार के प्राणियों के हित के लिए ही प्रगट होते हैं। बुद्ध के चार वैशारद्यों, दश बलों तथा अठारह आवैणिक धर्मों की उपयोगिता, केवल इस संसार के कल्याण में ही है। पञ्चशील, अष्टशील एवं दसशील का, सभी प्रातिमोक्ष नियमों का, सैंतीस बोधिपाक्षिक धर्मों का, चार सत्यों का, समस्त प्रकार की समाधि एवं समापत्तियों का, चार अप्रमेय भावनाओं का, चार संग्रहवस्तुओं का, और तेरह धूतगुणों का-संक्षेप में सद्धर्म के समस्त तत्त्वों का सार्थक्य और औचित्य इस संसार में और संसार के लिए ही है। भगवान बुद्ध को इन तत्त्वों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, निर्वाण में इनकी कोई सत्ता अथवा उपयोगिता नहीं रह जाती है । परन्तु इन तत्त्वों के बिना कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकता है। बुद्धत्व वही प्राप्त करना चाहता है जो संसार में रहता है। अतएव इन सभी तत्त्वों का महत्त्व संसार में रहते हुए ही हैं, संसार के बाहर नहीं। दूसरे शब्दों में संसार ही बुद्धक्षेत्र हैं, धर्मक्षेत्र है और संघक्षेत्र भी है। जो तत्त्वदर्शी है वह इस तथ्य को जानता है, उसके लिए व्यष्टि एवं समष्टि का भेद असम्भव है। उसके लिये संसार और निर्वाण दोनों में कोई भेद नहीं हो सकता है। ऐसे तत्त्वदर्शी के लिए यमकव्यत्यस्तता समाप्त हो जाती है। समस्त प्रपञ्चों का उपशमन हो जाता है । उसको सर्वत्र नैरात्म्य का दर्शन होता है। यह दृष्टिकोण केवल विमलकीर्ति निर्देश की विशेषता नहीं है। आचार्य नागार्जुन ने मध्यमा प्रतिपत्ति की, और अन्य तान्त्रिक सिद्धों ने सहजावस्था की सम्यक् व्याख्या में यही दृष्टिकोण अपनाया है। क्योंकि यही वस्तुतः विशुद्धि का अथवा शान्ति का मार्ग है। प्राचीन परम्परा के स्थविरों ने भी बुद्धवचनों का यह अंश पालि में सुरक्षित रखा है
सब्बे धम्मा अनत्ता ति यदा पञ्जाय पस्सति ।
अथ निधिबन्दति दुक्खे एस भग्गो विसुद्धिया ॥ धम्मपद १७९ । आत्मदष्टि सभी भेदों व क्लेशों का मूल है। स्व एवं पर का भेद इसी आस्रव पर आधारित है। व्यक्तिवाद और समाजवाद के पारस्परिक भेद एवं संघर्ष आत्मदृष्टि अथवा सत्कायदृष्टि के कारण हैं। जिसका आत्मस्नेह समाप्त हो गया है ऐसे वीतराग बोधिसत्त्व के लिए न व्यष्टि है, न समष्टि हैं और न उन दोनों के बीच संघर्ष ही है। विमलकीतिनिर्देश के प्रथम परिवर्त में तथागत लिच्छविकुमार रत्नाकर से कहते हैं- "कुलपुत्र, बोधिसत्त्व को बुद्धक्षेत्र की परिशुद्धि पूर्ण करने के लिए अपने चित्त की परिशुद्धि करनी चाहिए । ज्यों-ज्यों बोधिसत्त्व का चित्त परिशुद्ध होता है, परिसंवाद -२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org