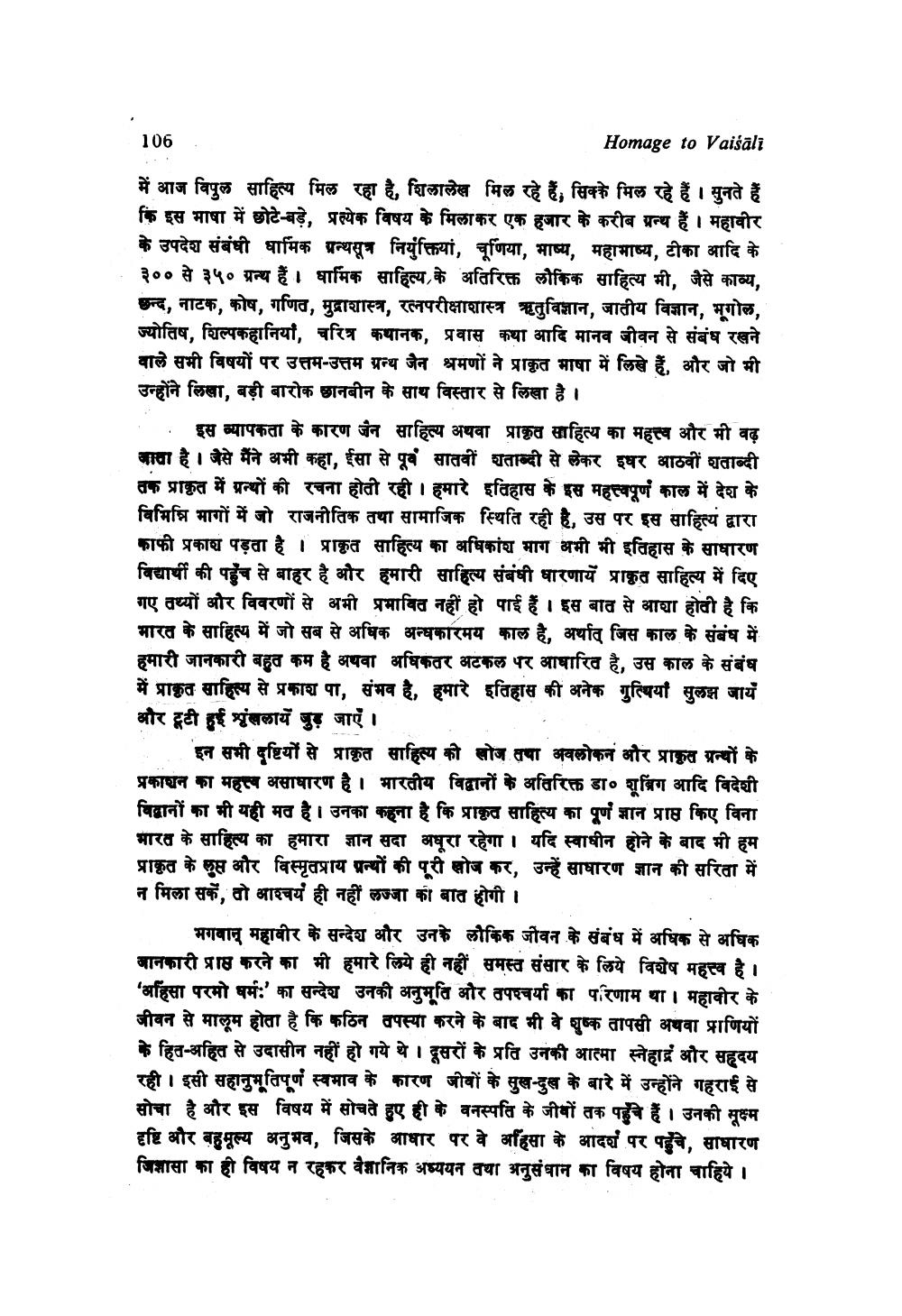________________ 106 Homage to Vaisali में आज विपुल साहित्य मिल रहा है, शिलालेख मिल रहे हैं, सिक्के मिल रहे हैं / सुनते हैं कि इस भाषा में छोटे-बड़े, प्रत्येक विषय के मिलाकर एक हजार के करीब ग्रन्थ हैं / महावीर के उपदेश संबंधी धार्मिक ग्रन्थसूत्र नियुक्तियां, चूणिया, भाष्य, महाभाष्य, टीका आदि के 300 से 350 ग्रन्थ हैं। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त लौकिक साहित्य भी, जैसे काव्य, छन्द, नाटक, कोष, गणित, मुद्राशास्त्र, रत्नपरीक्षाशास्त्र ऋतुविज्ञान, जातीय विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, शिल्पकहानियां, चरित्र कथानक, प्रवास कथा आदि मानव जीवन से संबंध रखने वाले सभी विषयों पर उत्तम-उत्तम ग्रन्थ जैन श्रमणों ने प्राकृत भाषा में लिखे हैं, और जो भी उन्होंने लिखा, बड़ी बारोक छानबीन के साथ विस्तार से लिखा है। .. इस व्यापकता के कारण जैन साहित्य अथवा प्राकृत साहित्य का महत्त्व और भी बढ़ जाता है / जैसे मैंने अभी कहा, ईसा से पूर्व सातवीं शताब्दी से लेकर इधर आठवीं शताब्दी तक प्राकृत में ग्रन्थों की रचना होती रही / हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण काल में देश के विभिन्नि भागों में जो राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति रही है, उस पर इस साहित्य द्वारा काफी प्रकाश पड़ता है / प्राकृत साहित्य का अधिकांश भाग अभी भी इतिहास के साधारण विद्यार्थी की पहुंच से बाहर है और हमारी साहित्य संबंधी धारणायें प्राकृत साहित्य में दिए गए तथ्यों और विवरणों से अभी प्रभावित नहीं हो पाई हैं / इस बात से आशा होती है कि भारत के साहित्य में जो सब से अधिक अन्धकारमय काल है, अर्थात् जिस काल के संबंध में हमारी जानकारी बहुत कम है अथवा अधिकतर अटकल पर आधारित है, उस काल के संबंध में प्राकृत साहित्य से प्रकाश पा, संभव है, हमारे इतिहास की अनेक गुत्थियां सुलझ जायें और टूटी हुई शृंखलायें जुड़ जाएं। इन सभी दृष्टियों से प्राकृत साहित्य को खोज तथा अवलोकन और प्राकृत ग्रन्थों के प्रकाशन का महत्त्व असाधारण है। भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त डा० शूबिंग आदि विदेशी विद्वानों का भी यही मत है। उनका कहना है कि प्राकृत साहित्य का पूर्ण मान प्राप्त किए विना भारत के साहित्य का हमारा ज्ञान सदा अधूरा रहेगा। यदि स्वाधीन होने के बाद भी हम प्राकृत के लुप्त और विस्मृतप्राय ग्रन्थों की पूरी खोज कर, उन्हें साधारण ज्ञान की सरिता में न मिला सके, तो आश्चर्य ही नहीं लज्जा की बात होगी। भगवान महावीर के सन्देश और उनके लौकिक जीवन के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का भी हमारे लिये ही नहीं समस्त संसार के लिये विशेष महत्त्व है। 'अहिंसा परमो धर्मः' का सन्देश उनकी अनुभूति और तपश्चर्या का परिणाम था। महावीर के जीवन से मालूम होता है कि कठिन तपस्या करने के बाद भी वे शुष्क तापसी अथवा प्राणियों के हित-अहित से उदासीन नहीं हो गये थे / दूसरों के प्रति उनकी आत्मा स्नेहाई और सहृदय रही। इसी सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के कारण जीवों के सुख-दुख के बारे में उन्होंने गहराई से सोचा है और इस विषय में सोचते हुए ही के वनस्पति के जीवों तक पहुंचे हैं। उनकी सूक्ष्म दृष्टि और बहुमूल्य अनुभव, जिसके आधार पर वे अहिंसा के आदर्श पर पहुंचे, साधारण जिज्ञासा का ही विषय न रहकर वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान का विषय होना चाहिये /