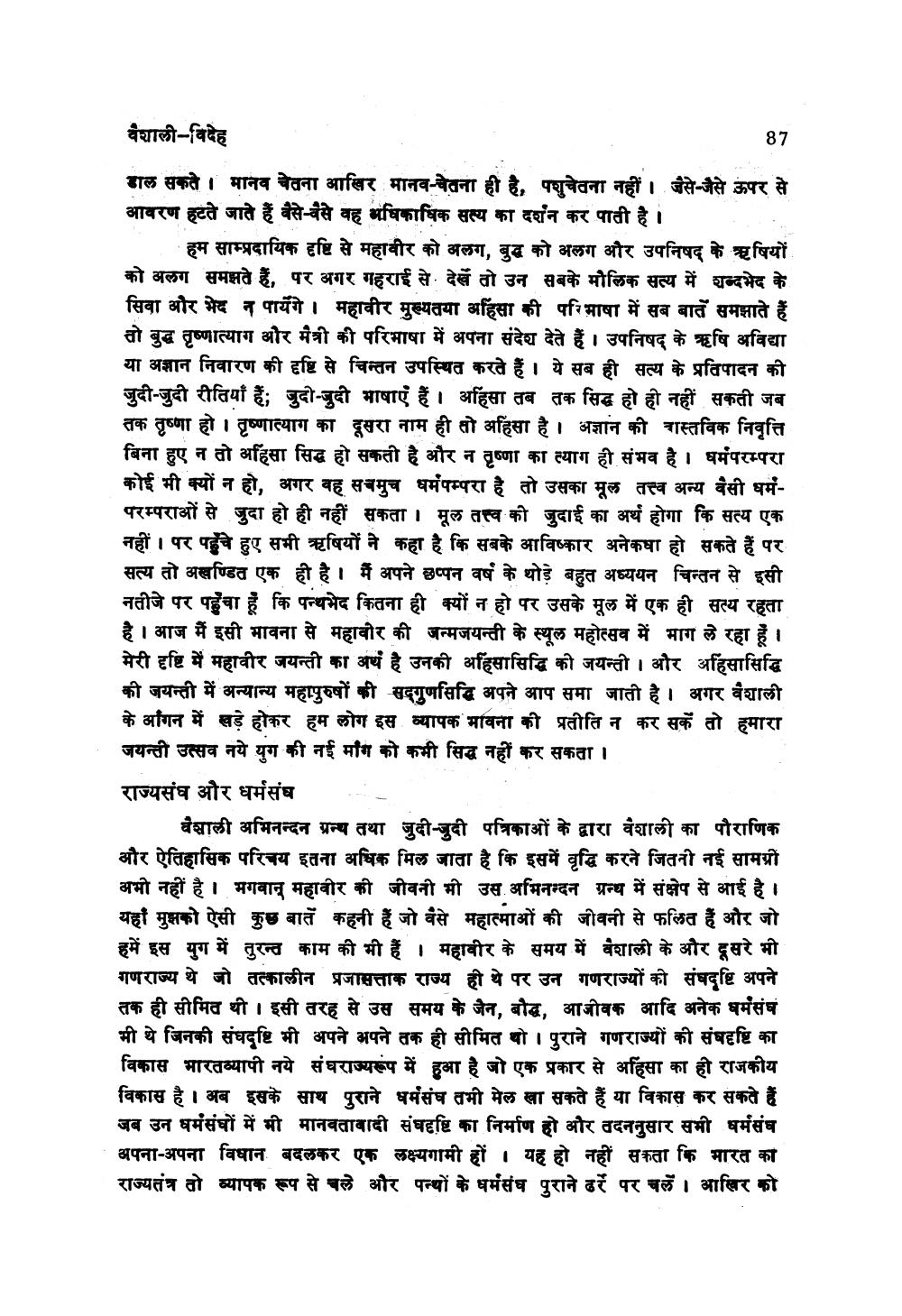________________ वैशाली-विदेह 87 डाल सकते / मानव चेतना आखिर मानव-चेतना ही है, पशुचेतना नहीं। जैसे-जैसे ऊपर से आवरण हटते जाते हैं वैसे-वैसे वह अधिकाधिक सत्य का दर्शन कर पाती है / हम साम्प्रदायिक दृष्टि से महावीर को अलग, बुद्ध को अलग और उपनिषद् के ऋषियों को अलग समझते हैं, पर अगर गहराई से देखें तो उन सबके मौलिक सत्य में शब्दभेद के सिवा और भेद न पायेंगे। महावीर मुख्यतया अहिंसा की परिभाषा में सब बातें समझाते हैं तो बुद्ध तृष्णात्याग और मैत्री की परिभाषा में अपना संदेश देते हैं / उपनिषद् के ऋषि अविद्या या अज्ञान निवारण की दृष्टि से चिन्तन उपस्थित करते हैं। ये सब ही सत्य के प्रतिपादन की जुदी-जुदी रीतियाँ हैं; जुदी-जुदी भाषाएं हैं। अहिंसा तब तक सिद्ध हो ही नहीं सकती जब तक तृष्णा हो / तृष्णात्याग का दूसरा नाम ही तो अहिंसा है। अज्ञान की वास्तविक निवृत्ति बिना हुए न तो अहिंसा सिद्ध हो सकती है और न तृष्णा का त्याग ही संभव है। धर्मपरम्परा कोई भी क्यों न हो, अगर वह सचमुच धर्मपम्परा है तो उसका मूल तत्व अन्य वैसी धर्मपरम्पराओं से जुदा हो ही नहीं सकता। मूल तत्त्व की जुदाई का अर्थ होगा कि सत्य एक नहीं / पर पहुंचे हुए सभी ऋषियों ने कहा है कि सबके आविष्कार अनेकधा हो सकते हैं पर सत्य तो अखण्डित एक ही है। मैं अपने छप्पन वर्ष के थोड़े बहुत अध्ययन चिन्तन से इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पन्थभेद कितना ही क्यों न हो पर उसके मूल में एक ही सत्य रहता है / आज मैं इसी भावना से महावीर की जन्मजयन्ती के स्थूल महोत्सव में भाग ले रहा हूँ। मेरी दृष्टि में महावीर जयन्ती का अर्थ है उनकी अहिंसासिद्धि की जयन्ती / और अहिंसासिद्धि की जयन्ती में अन्यान्य महापुरुषों की सद्गुणसिद्धि अपने आप समा जाती है। अगर वैशाली के आंगन में खड़े होकर हम लोग इस व्यापक भावना की प्रतीति न कर सकें तो हमारा जयन्ती उत्सव नये युग की नई मांग को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। राज्यसंघ और धर्मसंघ वैशाली अभिनन्दन ग्रन्थ तथा जुदी-जुदी पत्रिकाओं के द्वारा वैशाली का पौराणिक और ऐतिहासिक परिचय इतना अधिक मिल जाता है कि इसमें वृद्धि करने जितनी नई सामग्री अभी नहीं है। भगवान महावीर की जीवनी भी उस अभिनन्दन ग्रन्थ में संक्षेप से आई है। यहां मुझको ऐसी कुछ बातें कहनी हैं जो वैसे महात्माओं की जीवनी से फलित हैं और जो हमें इस युग में तुरन्त काम की भी हैं / महावीर के समय में वैशाली के और दूसरे भी गणराज्य थे जो तत्कालीन प्रजासत्ताक राज्य ही थे पर उन गणराज्यों को संघदृष्टि अपने तक ही सीमित थी। इसी तरह से उस समय के जैन, बौद्ध, आजीवक आदि अनेक धर्मसंघ भी थे जिनकी संघदृष्टि भी अपने अपने तक ही सीमित थो / पुराने गणराज्यों की संघदृष्टि का विकास भारतव्यापी नये संघराज्यरूप में हुआ है जो एक प्रकार से अहिंसा का ही राजकीय विकास है / अब इसके साथ पुराने धर्मसंघ तमी मेल खा सकते हैं या विकास कर सकते हैं जब उन धर्मसंघों में भी मानवतावादी संघदृष्टि का निर्माण हो और तदननुसार सभी धर्मसंघ अपना-अपना विधान बदलकर एक लक्ष्यगामी हों / यह हो नहीं सकता कि भारत का राज्यतंत्र तो व्यापक रूप से चले और पन्थों के धर्मसंघ पुराने ढर्रे पर चलें। आखिर को