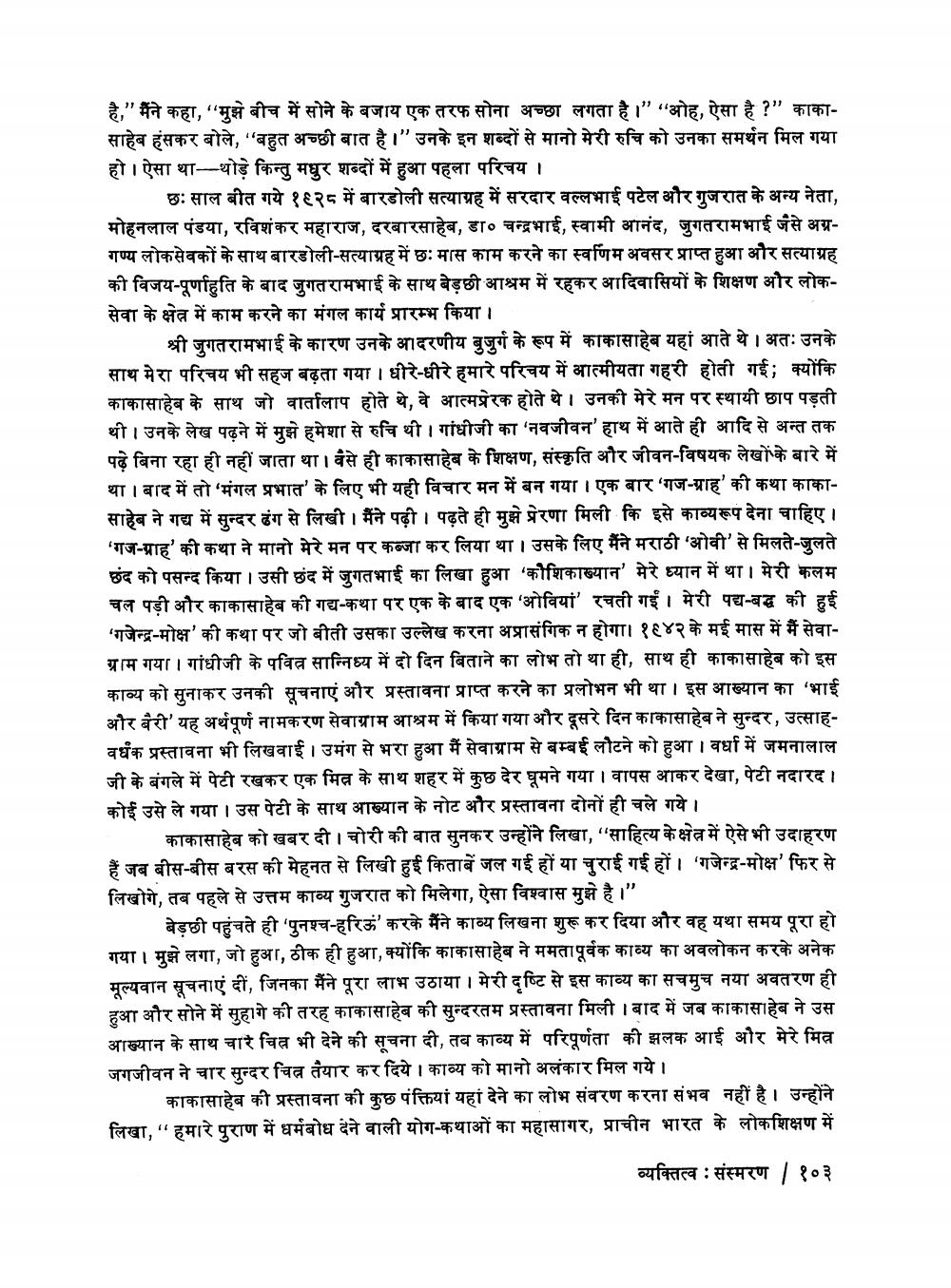________________
है," मैंने कहा, "मुझे बीच में सोने के बजाय एक तरफ सोना अच्छा लगता है।" "ओह, ऐसा है ?" काकासाहेब हंसकर बोले, "बहुत अच्छी बात है।" उनके इन शब्दों से मानो मेरी रुचि को उनका समर्थन मिल गया हो । ऐसा था-थोड़े किन्तु मधुर शब्दों में हुआ पहला परिचय ।
छः साल बीत गये १६२८ में बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभाई पटेल और गुजरात के अन्य नेता, मोहनलाल पंडया, रविशंकर महाराज, दरबारसाहेब, डा० चन्द्रभाई, स्वामी आनंद, जुगतरामभाई जैसे अग्रगण्य लोकसेवकों के साथ बारडोली-सत्याग्रह में छः मास काम करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ और सत्याग्रह की विजय-पूर्णाहुति के बाद जुगतरामभाई के साथ बेड़छी आश्रम में रहकर आदिवासियों के शिक्षण और लोकसेवा के क्षेत्र में काम करने का मंगल कार्य प्रारम्भ किया।
श्री जुगतरामभाई के कारण उनके आदरणीय बुजुर्ग के रूप में काकासाहेब यहां आते थे। अतः उनके साथ मेरा परिचय भी सहज बढ़ता गया। धीरे-धीरे हमारे परिचय में आत्मीयता गहरी होती गई; क्योंकि काकासाहेब के साथ जो वार्तालाप होते थे, वे आत्मप्रेरक होते थे। उनकी मेरे मन पर स्थायी छाप पड़ती थी। उनके लेख पढ़ने में मुझे हमेशा से रुचि थी। गांधीजी का 'नवजीवन' हाथ में आते ही आदि से अन्त तक पढ़े बिना रहा ही नहीं जाता था। वैसे ही काकासाहेब के शिक्षण, संस्कृति और जीवन-विषयक लेखों के बारे में था । बाद में तो 'मंगल प्रभात' के लिए भी यही विचार मन में बन गया। एक बार 'गज-ग्राह' की कथा काकासाहेब ने गद्य में सुन्दर ढंग से लिखी। मैंने पढ़ी। पढ़ते ही मुझे प्रेरणा मिली कि इसे काव्यरूप देना चाहिए। 'गज-ग्राह' की कथा ने मानो मेरे मन पर कब्जा कर लिया था। उसके लिए मैंने मराठी 'ओवी' से मिलते-जुलते छंद को पसन्द किया। उसी छंद में जुगतभाई का लिखा हुआ 'कौशिकाख्यान' मेरे ध्यान में था। मेरी कलम चल पड़ी और काकासाहेब की गद्य-कथा पर एक के बाद एक 'ओवियां' रचती गई। मेरी पद्य-बद्ध की हुई 'गजेन्द्र-मोक्ष' की कथा पर जो बीती उसका उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। १९४२ के मई मास में मैं सेवाग्राम गया। गांधीजी के पवित्र सान्निध्य में दो दिन बिताने का लोभ तो था ही, साथ ही काकासाहेब को इस काव्य को सुनाकर उनकी सूचनाएं और प्रस्तावना प्राप्त करने का प्रलोभन भी था। इस आख्यान का 'भाई और बैरी' यह अर्थपूर्ण नामकरण सेवाग्राम आश्रम में किया गया और दूसरे दिन काकासाहेब ने सुन्दर, उत्साहवर्धक प्रस्तावना भी लिखवाई। उमंग से भरा हुआ मैं सेवाग्राम से बम्बई लौटने को हुआ। वर्धा में जमनालाल जी के बंगले में पेटी रखकर एक मित्र के साथ शहर में कुछ देर घूमने गया। वापस आकर देखा, पेटी नदारद । कोई उसे ले गया। उस पेटी के साथ आख्यान के नोट और प्रस्तावना दोनों ही चले गये।
काकासाहेब को खबर दी। चोरी की बात सुनकर उन्होंने लिखा, "साहित्य के क्षेत्र में ऐसे भी उदाहरण हैं जब बीस-बीस बरस की मेहनत से लिखी हुई किताबें जल गई हों या चुराई गई हों। 'गजेन्द्र-मोक्ष' फिर से लिखोगे, तब पहले से उत्तम काव्य गुजरात को मिलेगा, ऐसा विश्वास मुझे है।"
बेड़छी पहुंचते ही 'पुनश्च-हरिऊं' करके मैंने काव्य लिखना शुरू कर दिया और वह यथा समय पूरा हो गया। मुझे लगा, जो हुआ, ठीक ही हुआ, क्योंकि काकासाहेब ने ममतापूर्वक काव्य का अवलोकन करके अनेक मूल्यवान सूचनाएं दीं, जिनका मैंने पूरा लाभ उठाया। मेरी दृष्टि से इस काव्य का सचमुच नया अवतरण ही हुआ और सोने में सूहागे की तरह काकासाहेब की सुन्दरतम प्रस्तावना मिली। बाद में जब काकासाहेब ने उस आख्यान के साथ चारे चित्र भी देने की सूचना दी, तब काव्य में परिपूर्णता की झलक आई और मेरे मित्र जगजीवन ने चार सुन्दर चित्र तैयार कर दिये । काव्य को मानो अलंकार मिल गये।
काकासाहेब की प्रस्तावना की कुछ पंक्तियां यहां देने का लोभ संवरण करना संभव नहीं है। उन्होंने लिखा, "हमारे पुराण में धर्मबोध देने वाली योग-कथाओं का महासागर, प्राचीन भारत के लोकशिक्षण में
व्यक्तित्व : संस्मरण | १०३