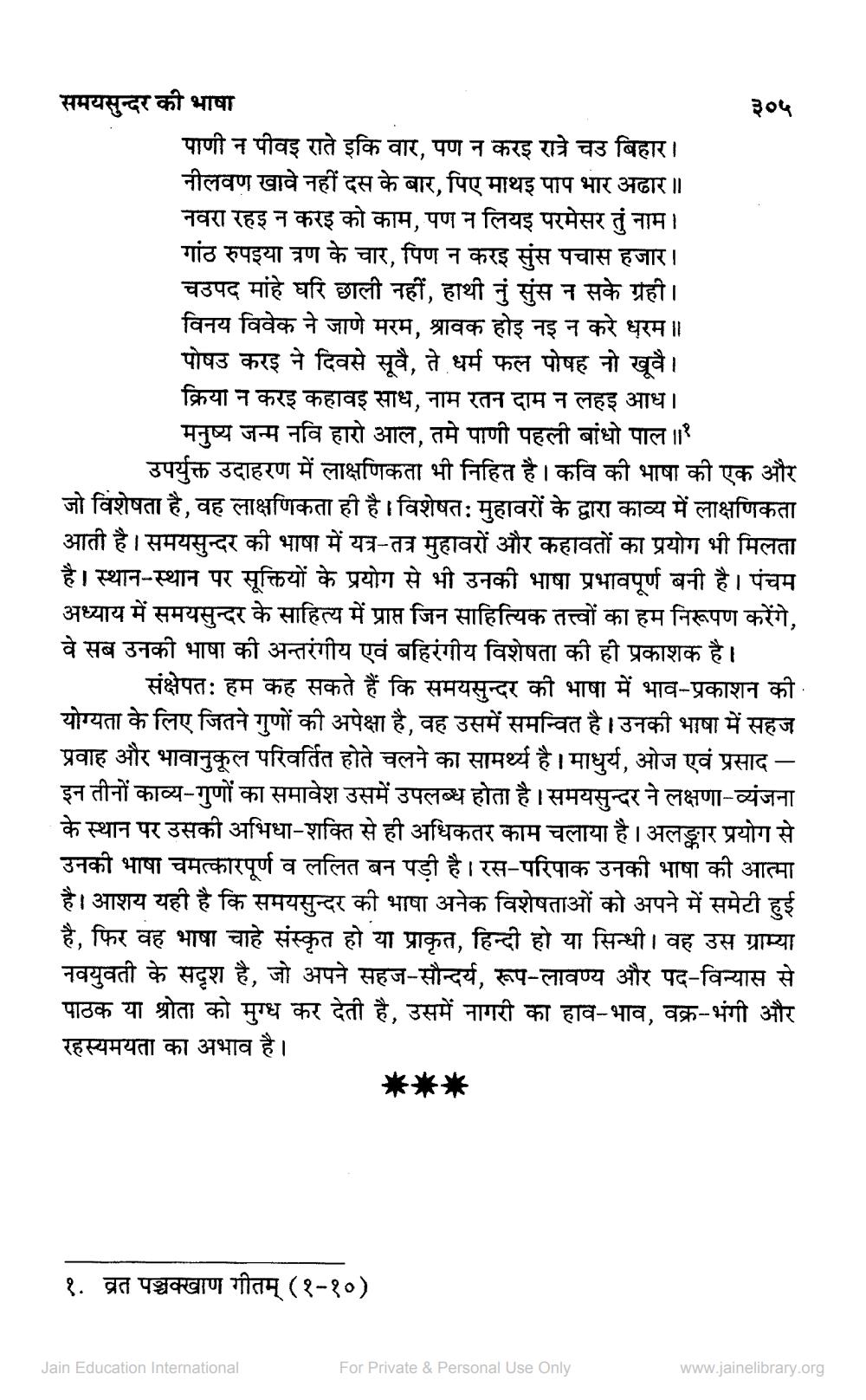________________
समयसुन्दर की भाषा
३०५ पाणी न पीवइ राते इकि वार, पण न करइ रात्रे चउ बिहार। नीलवण खावे नहीं दस के बार, पिए माथइ पाप भार अढार॥ नवरा रहइ न करइ को काम, पण न लियइ परमेसर तुं नाम। गांठ रुपइया त्रण के चार, पिण न करइ सुंस पचास हजार। चउपद मांहे घरि छाली नहीं, हाथी नुं सुंस न सके ग्रही। विनय विवेक ने जाणे मरम, श्रावक होइ नइ न करे धरम ॥ पोषउ करइ ने दिवसे सूवै, ते धर्म फल पोषह नो खूवै। क्रिया न करइ कहावइ साध, नाम रतन दाम न लहइ आध।
मनुष्य जन्म नवि हारो आल, तमे पाणी पहली बांधो पाल ॥
उपर्युक्त उदाहरण में लाक्षणिकता भी निहित है। कवि की भाषा की एक और जो विशेषता है, वह लाक्षणिकता ही है। विशेषत: मुहावरों के द्वारा काव्य में लाक्षणिकता आती है। समयसुन्दर की भाषा में यत्र-तत्र मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भी मिलता है। स्थान-स्थान पर सूक्तियों के प्रयोग से भी उनकी भाषा प्रभावपूर्ण बनी है। पंचम अध्याय में समयसुन्दर के साहित्य में प्राप्त जिन साहित्यिक तत्त्वों का हम निरूपण करेंगे, वे सब उनकी भाषा की अन्तरंगीय एवं बहिरंगीय विशेषता की ही प्रकाशक है।
संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि समयसुन्दर की भाषा में भाव-प्रकाशन की योग्यता के लिए जितने गुणों की अपेक्षा है, वह उसमें समन्वित है। उनकी भाषा में सहज प्रवाह और भावानुकूल परिवर्तित होते चलने का सामर्थ्य है। माधुर्य, ओज एवं प्रसाद - इन तीनों काव्य-गुणों का समावेश उसमें उपलब्ध होता है। समयसुन्दर ने लक्षणा-व्यंजना के स्थान पर उसकी अभिधा-शक्ति से ही अधिकतर काम चलाया है। अलङ्कार प्रयोग से उनकी भाषा चमत्कारपूर्ण व ललित बन पड़ी है। रस-परिपाक उनकी भाषा की आत्मा है। आशय यही है कि समयसुन्दर की भाषा अनेक विशेषताओं को अपने में समेटी हुई है, फिर वह भाषा चाहे संस्कृत हो या प्राकृत, हिन्दी हो या सिन्धी। वह उस ग्राम्या नवयुवती के सदृश है, जो अपने सहज-सौन्दर्य, रूप-लावण्य और पद-विन्यास से पाठक या श्रोता को मुग्ध कर देती है, उसमें नागरी का हाव-भाव, वक्र-भंगी और रहस्यमयता का अभाव है।
***
१. व्रत पञ्चक्खाण गीतम् (१-१०)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org