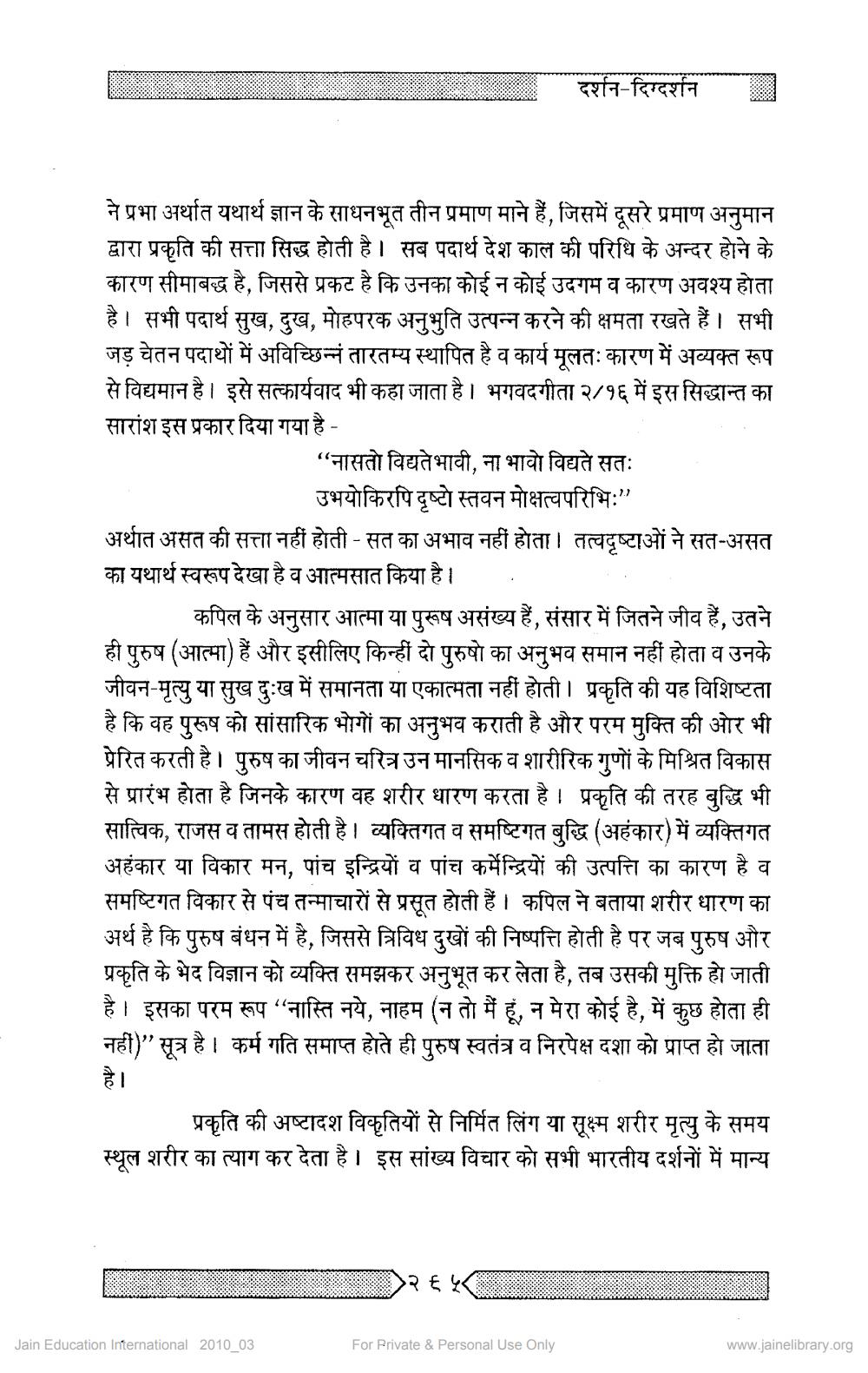________________
888888882
56989
दर्शन-दिग्दर्शन
3505000
ने प्रभा अर्थात यथार्थ ज्ञान के साधनभूत तीन प्रमाण माने हैं, जिसमें दूसरे प्रमाण अनुमान द्वारा प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। सब पदार्थ देश काल की परिधि के अन्दर होने के कारण सीमाबद्ध है, जिससे प्रकट है कि उनका कोई न कोई उदगम व कारण अवश्य होता है। सभी पदार्थ सुख, दुख, मोहपरक अनुभुति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। सभी जड़ चेतन पदाथों में अविच्छिन्नं तारतम्य स्थापित है व कार्य मूलतः कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान है। इसे सत्कार्यवाद भी कहा जाता है। भगवदगीता २/१६ में इस सिद्धान्त का सारांश इस प्रकार दिया गया है -
"नासतो विद्यतेभावी, ना भावो विद्यते सतः
उभयोकिरपि दृष्टो स्तवन मोक्षत्वपरिभिः" अर्थात असत की सत्ता नहीं होती - सत का अभाव नहीं होता। तत्वदृष्टाओं ने सत-असत का यथार्थ स्वरूप देखा है व आत्मसात किया है।
कपिल के अनुसार आत्मा या पुरुष असंख्य हैं, संसार में जितने जीव हैं, उतने ही पुरुष (आत्मा) हैं और इसीलिए किन्हीं दो पुरुषो का अनुभव समान नहीं होता व उनके जीवन-मृत्यु या सुख दुःख में समानता या एकात्मता नहीं होती। प्रकृति की यह विशिष्टता है कि वह पुरूष को सांसारिक भोगों का अनुभव कराती है और परम मुक्ति की ओर भी प्रेरित करती है। पुरुष का जीवन चरित्र उन मानसिक व शारीरिक गुणों के मिश्रित विकास से प्रारंभ होता है जिनके कारण वह शरीर धारण करता है। प्रकृति की तरह बुद्धि भी सात्विक, राजस व तामस होती है। व्यक्तिगत व समष्टिगत बुद्धि (अहंकार) में व्यक्तिगत अहंकार या विकार मन, पांच इन्द्रियों व पांच कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति का कारण है व समष्टिगत विकार से पंच तन्माचारों से प्रसूत होती हैं। कपिल ने बताया शरीर धारण का अर्थ है कि पुरुष बंधन में है, जिससे त्रिविध दुखों की निष्पत्ति होती है पर जब पुरुष और प्रकृति के भेद विज्ञान को व्यक्ति समझकर अनुभूत कर लेता है, तब उसकी मुक्ति हो जाती है। इसका परम रूप “नास्ति नये, नाहम (न तो मैं हूं, न मेरा कोई है, में कुछ होता ही नहीं)" सूत्र है। कर्म गति समाप्त होते ही पुरुष स्वतंत्र व निरपेक्ष दशा को प्राप्त हो जाता
है।
प्रकृति की अष्टादश विकृतियों से निर्मित लिंग या सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय स्थूल शरीर का त्याग कर देता है। इस सांख्य विचार को सभी भारतीय दर्शनों में मान्य
Jain Education International 2010_03
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org