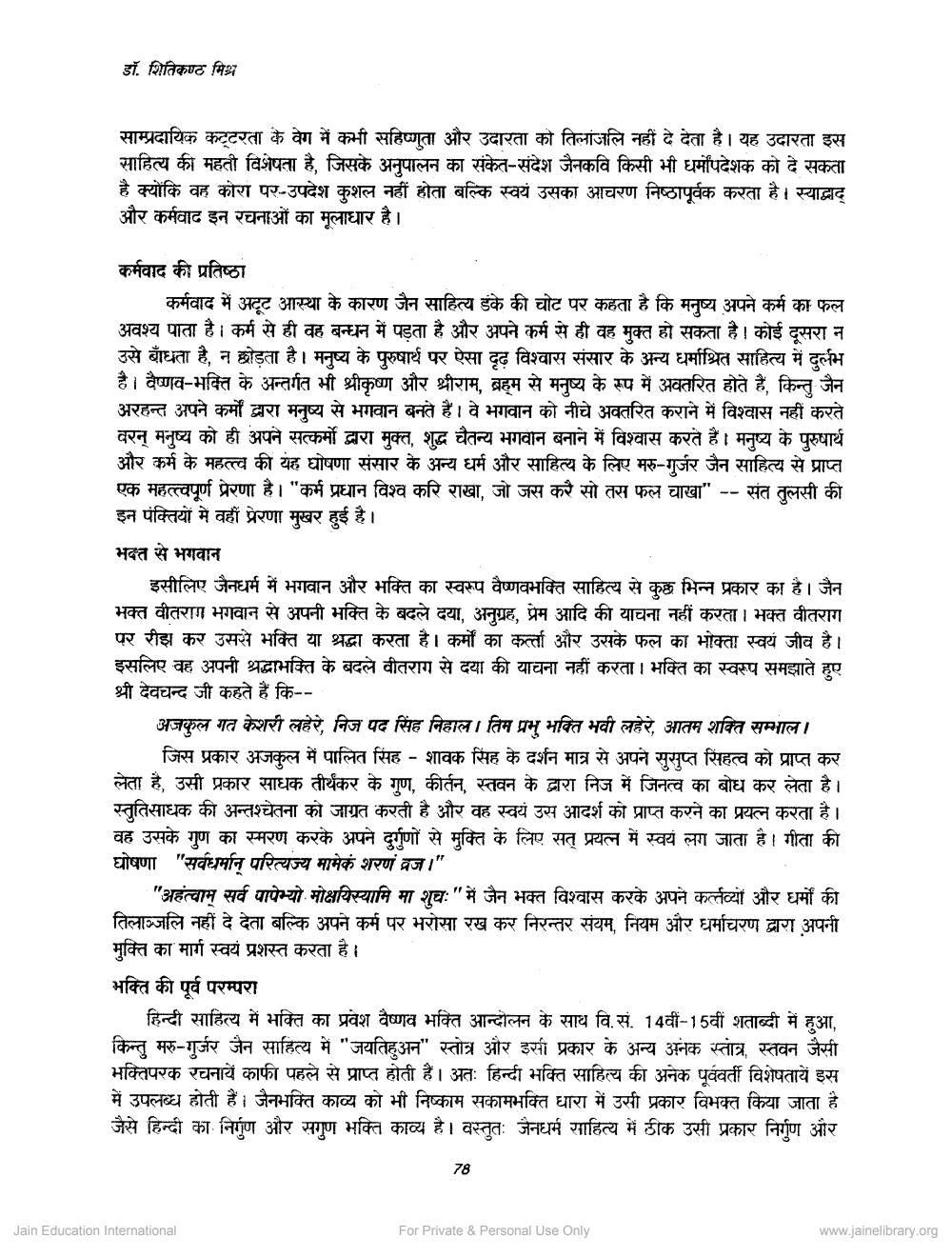________________
डॉ. शितिकण्ठ मिश्र
साम्प्रदायिक कट्टरता के वेग में कभी सहिष्णुता और उदारता को तिलांजलि नहीं दे देता है। यह उदारता इस साहित्य की महती विशेषता है, जिसके अनुपालन का संकेत-संदेश जैनकवि किसी भी धर्मोपदेशक को दे सकता है क्योंकि वह कोरा पर-उपदेश कुशल नहीं होता बल्कि स्वयं उसका आचरण निष्ठापूर्वक करता है। स्याद्वाद और कर्मवाद इन रचनाओं का मूलाधार है।
कर्मवाद की प्रतिष्ठा
कर्मवाद में अटूट आस्था के कारण जैन साहित्य डंके की चोट पर कहता है कि मनुष्य अपने कर्म का फल अवश्य पाता है। कर्म से ही वह बन्धन में पड़ता है और अपने कर्म से ही वह मुक्त हो सकता है। कोई दूसरा न उसे बाँधता है, न छोड़ता है। मनुष्य के पुरुषार्थ पर ऐसा दृढ़ विश्वास संसार के अन्य धर्माश्रित साहित्य में दुर्लभ है। वैष्णव-भक्ति के अन्तर्गत भी श्रीकृष्ण और श्रीराम, ब्रह्म से मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, किन्तु जैन अरहन्त अपने कर्मों द्वारा मनुष्य से भगवान बनते हैं। वे भगवान को नीचे अवतरित कराने में विश्वास नहीं करते वरन् मनुष्य को ही अपने सत्कर्मो द्वारा मुक्त, शुद्ध चैतन्य भगवान बनाने में विश्वास करते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ
और कर्म के महत्त्व की यह घोषणा संसार के अन्य धर्म और साहित्य के लिए मरु-गुर्जर जैन साहित्य से प्राप्त एक महत्त्वपूर्ण प्रेरणा है। "कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करै सो तस फल चाखा" -- संत तुलसी की इन पंक्तियों में वहीं प्रेरणा मुखर हुई है। भक्त से भगवान
इसीलिए जैनधर्म में भगवान और भक्ति का स्वरूप वैष्णवभक्ति साहित्य से कुछ भिन्न प्रकार का है। जैन भक्त वीतराग भगवान से अपनी भक्ति के बदले दया, अनुग्रह, प्रेम आदि की याचना नहीं करता। भक्त वीतराग पर रीझ कर उससे भक्ति या श्रद्धा करता है। कर्मों का कर्ता और उसके फल का भोक्ता स्वयं जीव है। इसलिए वह अपनी श्रद्धाभक्ति के बदले वीतराग से दया की याचना नहीं करता। भक्ति का स्वरूप समझाते हुए श्री देवचन्द जी कहते हैं कि--
अजकुल गत केशरी लहेरे, निज पद सिंह निहाल । तिम प्रभु भक्ति भवी लहेरे, आतम शक्ति सम्भाल।
जिस प्रकार अजकुल में पालित सिंह - शावक सिंह के दर्शन मात्र से अपने सुसुप्त सिंहत्व को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार साधक तीर्थंकर के गुण, कीर्तन, स्तवन के द्वारा निज में जिनत्व का बोध कर लेता है। स्तुतिसाधक की अन्तश्चेतना को जाग्रत करती है और वह स्वयं उस आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह उसके गुण का स्मरण करके अपने दुर्गुणों से मुक्ति के लिए सत् प्रयत्न में स्वयं लग जाता है। गीता की घोषणा "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।"
"अहंत्वाम् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिस्यामि मा शुचः" में जैन भक्त विश्वास करके अपने कर्तव्यों और धर्मों की तिलाञ्जलि नहीं दे देता बल्कि अपने कर्म पर भरोसा रख कर निरन्तर संयम, नियम और धर्माचरण द्वारा अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। भक्ति की पूर्व परम्परा
हिन्दी साहित्य में भक्ति का प्रवेश वैष्णव भक्ति आन्दोलन के साथ वि.सं. 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ, किन्तु मरु-गुर्जर जैन साहित्य में "जयतिहुअन" स्तोत्र और इसी प्रकार के अन्य अनेक स्तोत्र, स्तवन जैसी भक्तिपरक रचनायें काफी पहले से प्राप्त होती हैं। अतः हिन्दी भक्ति साहित्य की अनेक पूर्ववर्ती विशेषतायें इस में उपलब्ध होती हैं। जैनभक्ति काव्य को भी निष्काम सकामभक्ति धारा में उसी प्रकार विभक्त किया जाता है जैसे हिन्दी का निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य है। वस्तुतः जैनधर्म साहित्य में ठीक उसी प्रकार निर्गुण और
78
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org