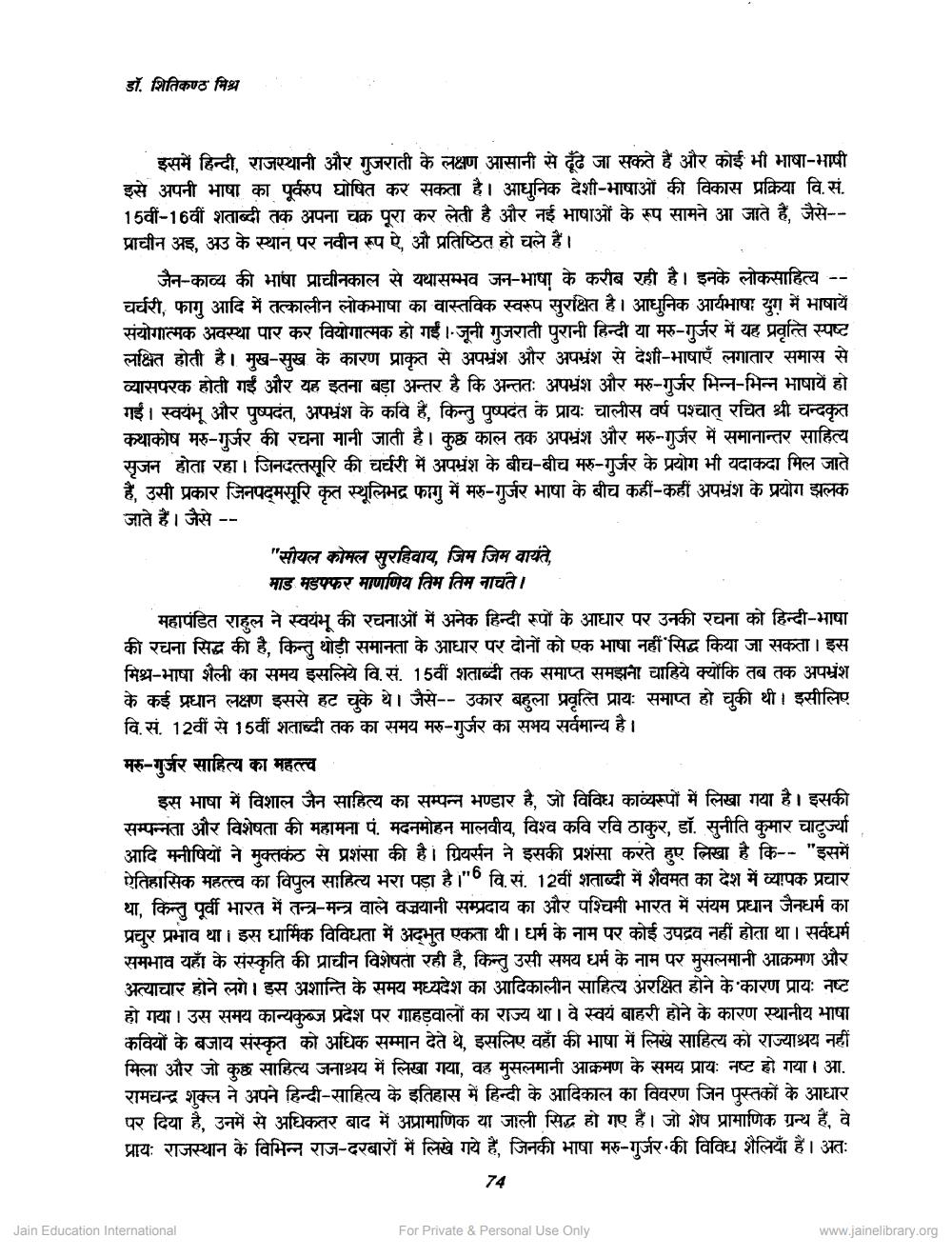________________
डॉ. शितिकण्ठ मिश्र
इसमें हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती के लक्षण आसानी से ढूँढे जा सकते है और कोई भी भाषा-भाषी इसे अपनी भाषा का पूर्वरुप घोषित कर सकता है। आधुनिक देशी-भाषाओं की विकास प्रक्रिया वि.सं. 15वीं-16वीं शताब्दी तक अपना चक्र पूरा कर लेती है और नई भाषाओं के रूप सामने आ जाते हैं, जैसे-- प्राचीन अइ, अउ के स्थान पर नवीन रूप ऐ, औ प्रतिष्ठित हो चले हैं।
जैन-काव्य की भाषा प्राचीनकाल से यथासम्भव जन-भाषा के करीब रही है। इनके लोकसाहित्य -- चर्चरी, फागु आदि में तत्कालीन लोकभाषा का वास्तविक स्वरूप सुरक्षित है। आधुनिक आर्यभाषा युग में भाषायें संयोगात्मक अवस्था पार कर वियोगात्मक हो गईं। जूनी गुजराती पुरानी हिन्दी या मरु-गुर्जर में यह प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है। मुख-सुख के कारण प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से देशी-भाषाएँ लगातार समास से व्यासपरक होती गईं और यह इतना बड़ा अन्तर है कि अन्ततः अपभ्रंश और मरु-गुर्जर भिन्न-भिन्न भाषायें हो गई। स्वयंभू और पुष्पदंत, अपभ्रंश के कवि है, किन्तु पुष्पदंत के प्रायः चालीस वर्ष पश्चात् रचित श्री चन्दकृत कथाकोष मरु-गुर्जर की रचना मानी जाती है। कुछ काल तक अपभ्रंश और मरु-गुर्जर में समानान्तर साहित्य सृजन होता रहा। जिनदत्तसूरि की चर्चरी में अपभ्रंश के बीच-बीच मरु-गुर्जर के प्रयोग भी यदाकदा मिल जाते हैं, उसी प्रकार जिनपद्मसूरि कृत स्थूलिभद्र फागु में मरु-गुर्जर भाषा के बीच कहीं-कहीं अपभ्रंश के प्रयोग झलक जाते हैं। जैसे --
"सीयल कोमल सुरहिवाय, जिम जिम वायंते,
माड मडफ्फर माणणिय तिम तिम नाचते। महापंडित राहुल ने स्वयंभू की रचनाओं में अनेक हिन्दी रूपों के आधार पर उनकी रचना को हिन्दी-भाषा की रचना सिद्ध की है, किन्तु थोड़ी समानता के आधार पर दोनों को एक भाषा नहीं सिद्ध किया जा सकता। इस मिथ्र-भाषा शैली का समय इसलिये वि.सं. 15वीं शताब्दी तक समाप्त समझना चाहिये क्योंकि तब तक अपभ्रंश के कई प्रधान लक्षण इससे हट चुके थे। जैसे-- उकार बहुला प्रवृत्ति प्रायः समाप्त हो चुकी थी। इसीलिए वि.सं. 12वीं से 15वीं शताब्दी तक का समय मरु-गुर्जर का सभय सर्वमान्य है। मरु-गुर्जर साहित्य का महत्त्व
इस भाषा में विशाल जैन साहित्य का सम्पन्न भण्डार है, जो विविध काव्यरूपों में लिखा गया है। इसकी सम्पन्नता और विशेषता की महामना पं. मदनमोहन मालवीय, विश्व कवि रवि ठाकुर, डॉ. सुनीति कुमार चाटुा आदि मनीषियों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। ग्रियर्सन ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि-- "इसमें ऐतिहासिक महत्त्व का विपुल साहित्य भरा पड़ा है।" वि.सं. 12वीं शताब्दी में शैवमत का देश में व्यापक प्रचार था, किन्तु पूर्वी भारत में तन्त्र-मन्त्र वाले वज्रयानी सम्प्रदाय का और पश्चिमी भारत में संयम प्रधान जैनधा प्रचुर प्रभाव था। इस धार्मिक विविधता में अद्भुत एकता थी। धर्म के नाम पर कोई उपद्रव नहीं होता था। सर्वधर्म समभाव यहाँ के संस्कृति की प्राचीन विशेषता रही है, किन्तु उसी समय धर्म के नाम पर मुसलमानी आक्रमण और अत्याचार होने लगे। इस अशान्ति के समय मध्यदेश का आदिकालीन साहित्य अरक्षित होने के कारण प्रायः नष्ट हो गया। उस समय कान्यकुब्ज प्रदेश पर गाहड़वालों का राज्य था। वे स्वयं बाहरी होने के कारण स्थानीय भाषा कवियों के बजाय संस्कृत को अधिक सम्मान देते थे, इसलिए वहाँ की भाषा में लिखे साहित्य को राज्याश्रय नहीं मिला और जो कुछ साहित्य जनाथय में लिखा गया, वह मुसलमानी आक्रमण के समय प्रायः नष्ट हो गया। आ. रामचन्द्र शक्ल ने अपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में हिन्दी के आदिकाल का विवरण जिन पुस्तकों के आधार पर दिया है, उनमें से अधिकतर बाद में अप्रामाणिक या जाली सिद्ध हो गए हैं। जो शेष प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, वे प्रायः राजस्थान के विभिन्न राज-दरबारों में लिखे गये हैं, जिनकी भाषा मरु-गुर्जर की विविध शैलिया है। अतः
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org