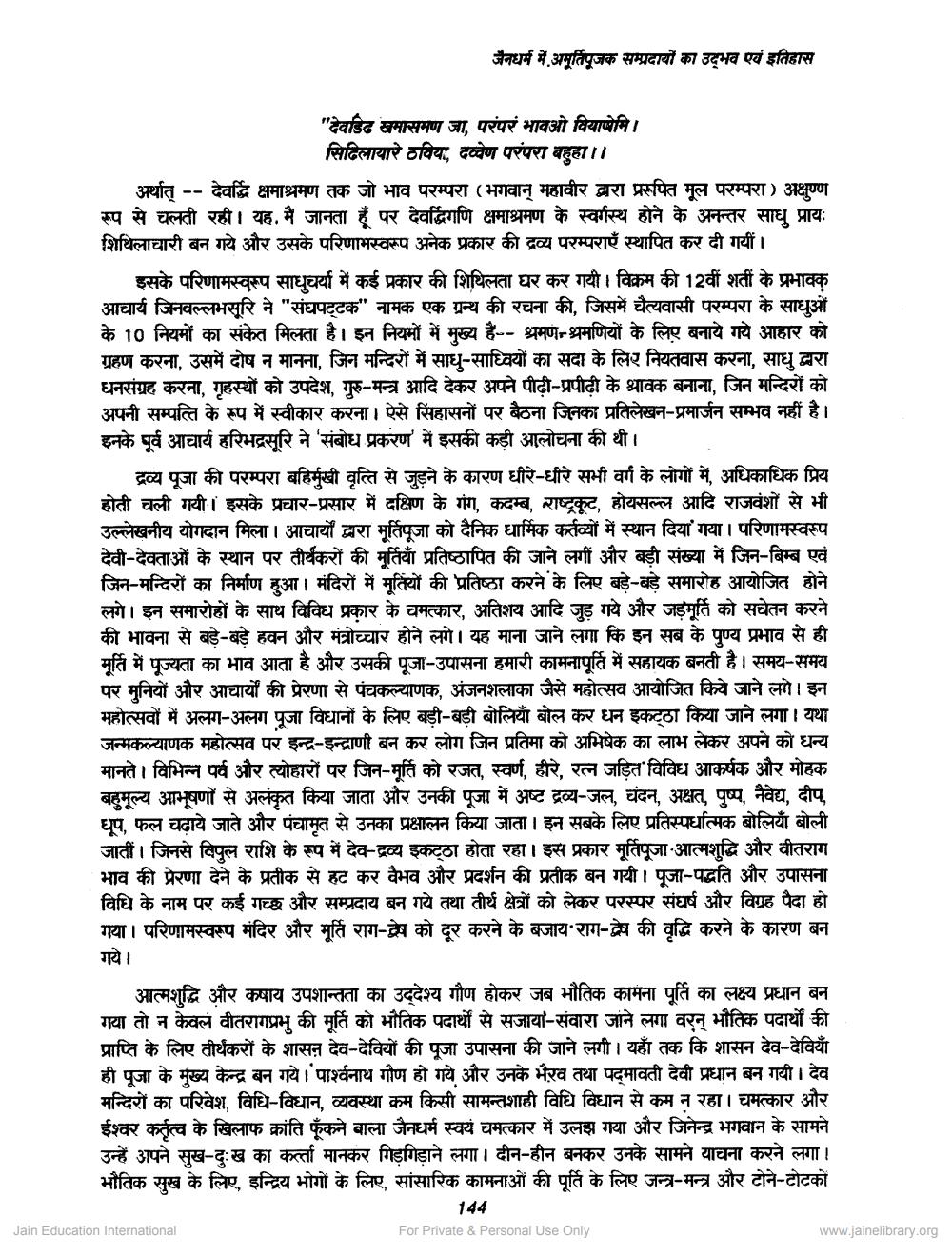________________
जैनधर्म में अमूर्तिपूजक सम्प्रदायों का उद्भव एवं इतिहास
"देवडिट खमासमण जा, परंपरं भावओ वियायोमि।
सिदिलायारे ठविया, दव्वेण परंपरा बहुहा।। अर्थात -- देवर्द्धि क्षमाश्रमण तक जो भाव परम्परा (भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित मूल परम्परा) अक्षुण्ण रूप से चलती रही। यह. मैं जानता हूँ पर देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर साधु प्रायः शिथिलाचारी बन गये और उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की द्रव्य परम्पराएँ स्थापित कर दी गयीं।
इसके परिणामस्वरूप साधुचर्या में कई प्रकार की शिथिलता घर कर गयी। विक्रम की 12वीं शती के प्रभावक आचार्य जिनवल्लभसूरि ने "संघपट्टक" नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें चैत्यवासी परम्परा के साधुओं के 10 नियमों का संकेत मिलता है। इन नियमों में मुख्य है-- श्रमण-श्रमणियों के लिए बनाये गये आहार को ग्रहण करना, उसमें दोष न मानना, जिन मन्दिरों में साधु-साध्वियों का सदा के लिए नियतवास करना, साधु दरा धनसंग्रह करना, गृहस्थों को उपदेश, गुरु-मन्त्र आदि देकर अपने पीढ़ी-प्रपीढ़ी के श्रावक बनाना, जिन मन्दिरों को अपनी सम्पत्ति के रूप में स्वीकार करना। ऐसे सिंहासनों पर बैठना जिनका प्रतिलेखन-प्रमार्जन सम्भव नहीं है। इनके पूर्व आचार्य हरिभद्रसूरि ने 'संबोध प्रकरण में इसकी कड़ी आलोचना की थी।
द्रव्य पूजा की परम्परा बहिर्मुखी वृत्ति से जुड़ने के कारण धीरे-धीरे सभी वर्ग के लोगों में, अधिकाधिक प्रिय होती चली गयी। इसके प्रचार-प्रसार में दक्षिण के गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट, होयसल्ल आदि राजवंशों से भी उल्लेखनीय योगदान मिला। आचार्यों द्वारा मूर्तिपूजा को दैनिक धार्मिक कर्तव्यों में स्थान दिया गया। परिणामस्वरूप देवी-देवताओं के स्थान पर तीर्थंकरों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की जाने लगी और बड़ी संख्या में जिन-बिम्ब एवं जिन-मन्दिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों में मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने के लिए बड़े-बड़े समारोह आयोजित होने लगे। इन समारोहों के साथ विविध प्रकार के चमत्कार, अतिशय आदि जुड़ गये और जड़मूर्ति को सचेतन करने की भावना से बड़े-बड़े हवन और मंत्रोच्चार होने लगे। यह माना जाने लगा कि इन सब के पुण्य प्रभाव से ही मूर्ति में पूज्यता का भाव आता है और उसकी पूजा-उपासना हमारी कामनापूर्ति में सहायक बनती है। समय-समय पर मुनियों और आचार्यों की प्रेरणा से पंचकल्याणक, अंजनशलाका जैसे महोत्सव आयोजित किये जाने लगे। इन महोत्सवों में अलग-अलग पूजा विधानों के लिए बड़ी-बड़ी बोलियाँ बोल कर धन इकट्ठा किया जाने लगा। यथा जन्मकल्याणक महोत्सव पर इन्द्र-इन्द्राणी बन कर लोग जिन प्रतिमा को अभिषेक का लाभ लेकर अपने को धन्य मानते। विभिन्न पर्व और त्योहारों पर जिन-मूर्ति को रजत, स्वर्ण, हीरे, रत्न जड़ित विविध आकर्षक और मोहक बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत किया जाता और उनकी पूजा में अष्ट द्रव्य-जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल चढ़ाये जाते और पंचामृत से उनका प्रक्षालन किया जाता । इन सबके लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियाँ बोली जातीं। जिनसे विपुल राशि के रूप में देव-द्रव्य इकट्ठा होता रहा। इस प्रकार मूर्तिपूजा-आत्मशुद्धि और वीतराग भाव की प्रेरणा देने के प्रतीक से हट कर वैभव और प्रदर्शन की प्रतीक बन गयी। पूजा-पद्धति और उपासना विधि के नाम पर कई गच्छ और सम्प्रदाय बन गये तथा तीर्थ क्षेत्रों को लेकर परस्पर संघर्ष और विग्रह पैदा हो गया। परिणामस्वस्प मंदिर और मूर्ति राग-द्रो को दूर करने के बजाय राग-द्वेय की वृद्धि करने के कारण बन गये। ___ आत्मशुद्धि और कषाय उपशान्तता का उद्देश्य गौण होकर जब भौतिक कामना पूर्ति का लक्ष्य प्रधान बन गया तो न केवल वीतरागप्रभु की मूर्ति को भौतिक पदार्थों से सजाया-संवारा जाने लगा वरन् भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए तीर्थंकरों के शासन देव-देवियों की पूजा उपासना की जाने लगी। यहाँ तक कि शासन देव-देवियाँ ही पूजा के मुख्य केन्द्र बन गये। पार्श्वनाथ गौण हो गये और उनके भैरव तथा पद्मावती देवी प्रधान बन गयी। देव मन्दिरों का परिवेश, विधि-विधान, व्यवस्था क्रम किसी सामन्तशाही विधि विधान से कम न रहा। चमत्कार और ईश्वर कर्तृत्व के खिलाफ क्रांति फॅकने बाला जैनधर्म स्वयं चमत्कार में उलझ गया और जिनेन्द्र भगवान के सामने उन्हें अपने सुख-दुःख का कर्ता मानकर गिड़गिड़ाने लगा। दीन-हीन बनकर उनके सामने याचना करने लगा। भौतिक सुख के लिए, इन्द्रिय भोगों के लिए, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए जन्त्र-मन्त्र और टोने-टोटको
144 Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org