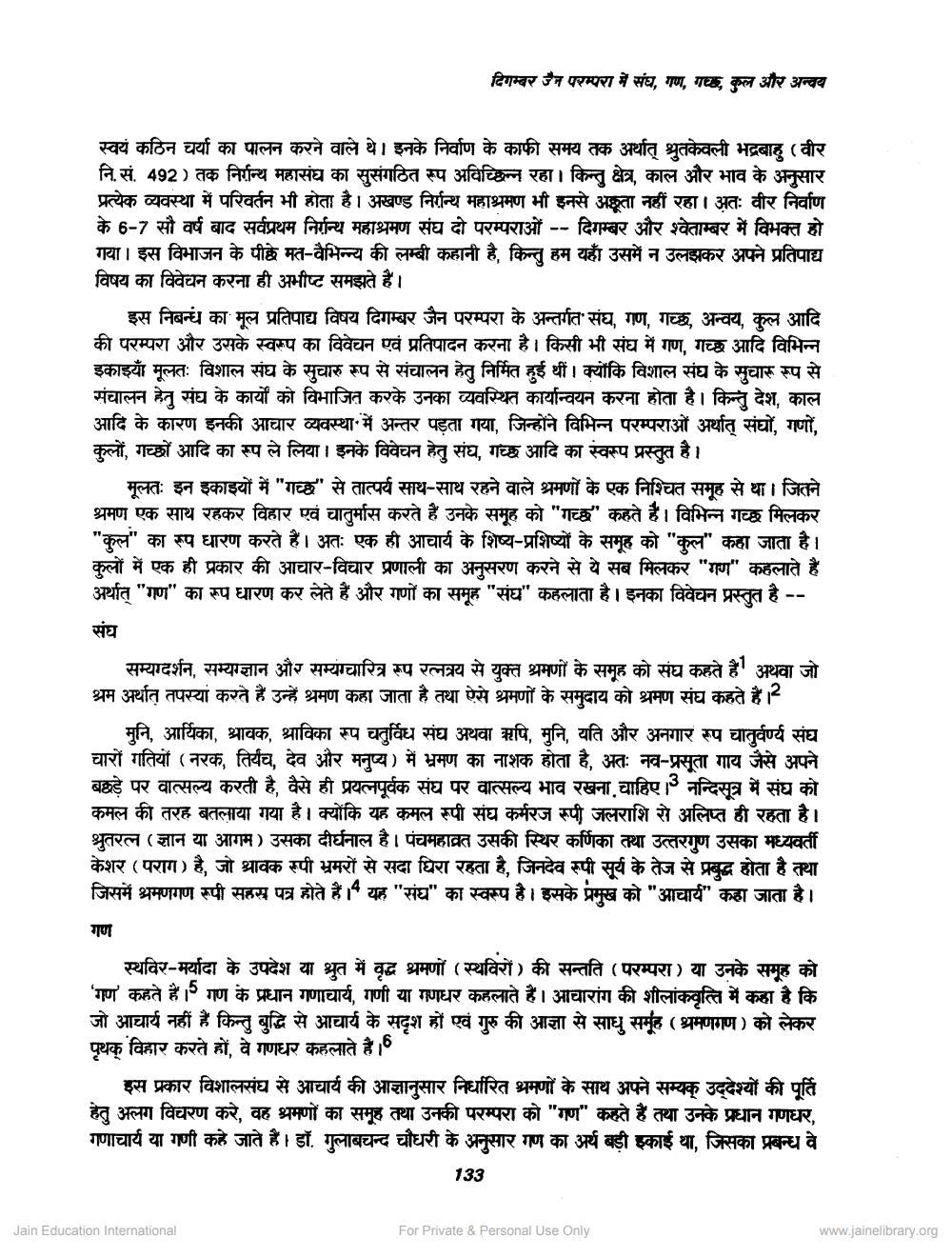________________
दिगम्बर जैन परम्परा में संघ, गण, गच्छ, कुल और अन्वय
स्वयं कठिन चर्या का पालन करने वाले थे। इनके निर्वाण के काफी समय तक अर्थात् श्रुतकेवली भद्रबाहु (वीर नि.सं. 492) तक निर्गन्थ महासंघ का सुसंगठित रूप अविच्छिन्न रहा। किन्तु क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन भी होता है। अखण्ड निर्गन्थ महाश्रमण भी इनसे अछूता नहीं रहा। अतः वीर निर्वाण के 6-7 सौ वर्ष बाद सर्वप्रथम निर्गन्थ महाश्रमण संघ दो परम्पराओं -- दिगम्बर और श्वेताम्बर में विभक्त हो गया। इस विभाजन के पीछे मत-वैभिन्न्य की लम्बी कहानी है, किन्तु हम यहाँ उसमें न उलझकर अपने प्रतिपाद्य विषय का विवेचन करना ही अभीष्ट समझते हैं।
इस निबन्ध का मूल प्रतिपाद्य विषय दिगम्बर जैन परम्परा के अन्तर्गत संघ, गण, गच्छ, अन्वय, कुल आदि की परम्परा और उसके स्वरूप का विवेचन एवं प्रतिपादन करना है। किसी भी संघ में गण, गच्छ आदि विभिन्न इकाइयाँ मूलतः विशाल संघ के सुचारु रूप से संचालन हेतु निर्मित हुई थीं। क्योंकि विशाल संघ के सुचारू रूप से संचालन हेतु संघ के कार्यों को विभाजित करके उनका व्यवस्थित कार्यान्वयन करना होता है। किन्तु देश, काल आदि के कारण इनकी आचार व्यवस्था में अन्तर पड़ता गया, जिन्होंने विभिन्न परम्पराओं अर्थात् संघों, गणों, कुलों, गच्छों आदि का रूप ले लिया। इनके विवेचन हेतु संघ, गच्छ आदि का स्वरूप प्रस्तुत है।
मूलतः इन इकाइयों में "गच्छ" से तात्पर्य साथ-साथ रहने वाले श्रमणों के एक निश्चित समह से था। जितने श्रमण एक साथ रहकर विहार एवं चातुर्मास करते हैं उनके समूह को "गच्छ" कहते है। विभिन्न गच्छ मिलकर "कुल" का रूप धारण करते हैं। अतः एक ही आचार्य के शिष्य-प्रशिष्यों के समूह को "कुल" कहा जाता है। कुलों में एक ही प्रकार की आचार-विचार प्रणाली का अनुसरण करने से ये सब मिलकर "गण" कहलाते हैं अर्थात् "गण" का रूप धारण कर लेते हैं और गणों का समूह "संघ" कहलाता है। इनका विवेचन प्रस्तुत है -- संघ
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र रूप रत्नत्रय से युक्त श्रमणों के समूह को संघ कहते हैं अथवा जो श्रम अर्थात तपस्या करते हैं उन्हें श्रमण कहा जाता है तथा ऐसे श्रमणों के समुदाय को श्रमण संघ कहते हैं।
मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ अथवा ऋषि, मुनि, यति और अनगार रूप चातुर्वर्ण्य संघ चारों गतियों (नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य ) में भ्रमण का नाशक होता है, अतः नव-प्रसूता गाय जैसे अपने बछड़े पर वात्सल्य करती है, वैसे ही प्रयत्नपूर्वक संघ पर वात्सल्य भाव रखना चाहिए। नन्दिसूत्र में संघ को कमल की तरह बतलाया गया है। क्योंकि यह कमल स्पी संघ कर्मरज स्पी जलराशि से अलिप्त ही रहता है। श्रुतरत्न (ज्ञान या आगम) उसका दीर्घनाल है। पंचमहाव्रत उसकी स्थिर कर्णिका तथा उत्तरगुण उसका मध्यवर्ती केशर (पराग) है, जो श्रावक रूपी भ्रमरों से सदा घिरा रहता है, जिनदेव रूपी सूर्य के तेज से प्रबद्ध होता है तथा जिसमें श्रमणगण रूपी सहस पत्र होते हैं। यह "संघ" का स्वरूप है। इसके को "आचार्य" कहा जाता है।
गण
स्थविर-मर्यादा के उपदेश या श्रुत में वृद्ध श्रमणों (स्थविरों) की सन्तति (परम्परा) या उनके समूह को 'गण कहते हैं। गण के प्रधान गणाचार्य, गणी या गणधर कहलाते हैं। आचारांग की शीलांकवृत्ति में कहा है कि जो आचार्य नहीं है किन्तु बुद्धि से आचार्य के सदृश हों एवं गुरु की आज्ञा से साधु समूह ( श्रमणगण) को लेकर पृथक विहार करते हों, वे गणधर कहलाते हैं।
इस प्रकार विशालसंघ से आचार्य की आज्ञानुसार निर्धारित श्रमणों के साथ अपने सम्यक् उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग विचरण करे, वह श्रमणों का समूह तथा उनकी परम्परा को "गण" कहते हैं तथा उनके प्रधान गणधर. गणाचार्य या गणी कहे जाते हैं। डॉ. गुलाबचन्द चौधरी के अनुसार गण का अर्थ बड़ी इकाई था, जिसका प्रबन्ध वे
133
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org