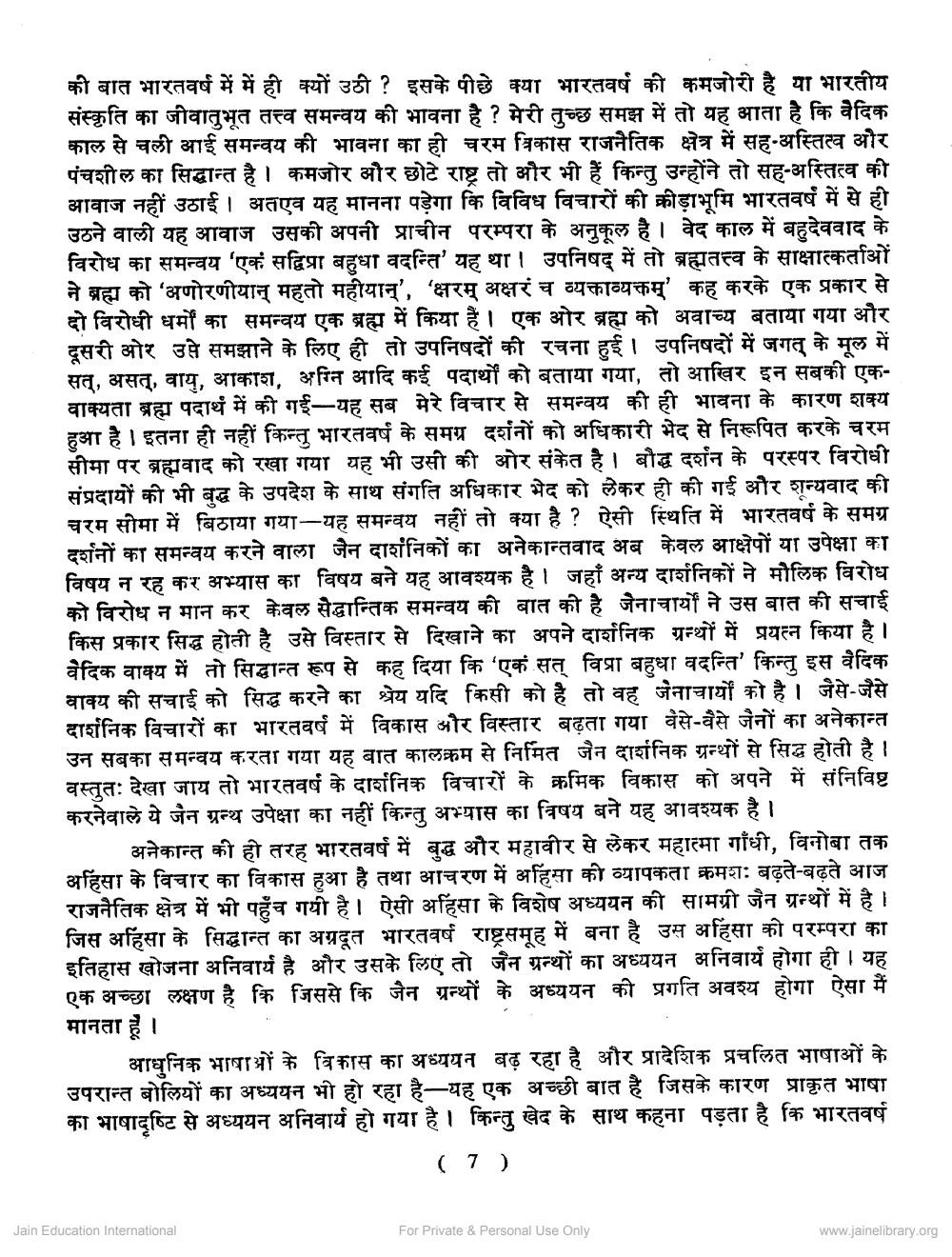________________
की बात भारतवर्ष में में ही क्यों उठी ? इसके पीछे क्या भारतवर्ष की कमजोरी है या भारतीय संस्कृति का जीवातुभूत तत्त्व समन्वय की भावना है ? मेरी तुच्छ समझ में तो यह आता है कि वैदिक काल से चली आई समन्वय की भावना का ही चरम विकास राजनैतिक क्षेत्र में सह-अस्तित्व और पंचशील का सिद्धान्त है। कमजोर और छोटे राष्ट्र तो और भी हैं किन्तु उन्होंने तो सह-अस्तित्व की आवाज नहीं उठाई। अतएव यह मानना पड़ेगा कि विविध विचारों की क्रीड़ाभूमि भारतवर्ष में से ही उठने वाली यह आवाज उसकी अपनी प्राचीन परम्परा के अनुकूल है। वेद काल में बहुदेववाद के विरोध का समन्वय ‘एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' यह था। उपनिषद् में तो ब्रह्मतत्त्व के साक्षात्कर्ताओं ने ब्रह्म को 'अणोरणीयान् महतो महीयान्', 'क्षरम् अक्षरं च व्यक्ताव्यक्तम्' कह करके एक प्रकार से दो विरोधी धर्मों का समन्वय एक ब्रह्म में किया हैं। एक ओर ब्रह्म को अवाच्य बताया गया और दूसरी ओर उसे समझाने के लिए ही तो उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों में जगत् के मूल में सत्, असत्, वायु, आकाश, अग्नि आदि कई पदार्थों को बताया गया, तो आखिर इन सबकी एकवाक्यता ब्रह्म पदार्थ में की गई—यह सब मेरे विचार से समन्वय की ही भावना के कारण शक्य हुआ है। इतना ही नहीं किन्तु भारतवर्ष के समग्र दर्शनों को अधिकारी भेद से निरूपित करके चरम सीमा पर ब्रह्मवाद को रखा गया यह भी उसी की ओर संकेत है। बौद्ध दर्शन के परस्पर विरोधी संप्रदायों की भी बुद्ध के उपदेश के साथ संगति अधिकार भेद को लेकर ही की गई और शन्यवाद की चरम सीमा में बिठाया गया-यह समन्वय नहीं तो क्या है ? ऐसी स्थिति में भारतवर्ष के समग्र दर्शनों का समन्वय करने वाला जैन दार्शनिकों का अनेकान्तवाद अब केवल आक्षेपों या उपेक्षा का विषय न रह कर अभ्यास का विषय बने यह आवश्यक है। जहाँ अन्य दार्शनिकों ने मौलिक विरोध को विरोध न मान कर केवल सैद्धान्तिक समन्वय की बात की है जैनाचार्यों ने उस बात की सचाई किस प्रकार सिद्ध होती है उसे विस्तार से दिखाने का अपने दार्शनिक ग्रन्थों में प्रयत्न किया है। वैदिक वाक्य में तो सिद्धान्त रूप से कह दिया कि 'एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' किन्तु इस वैदिक वाक्य की सचाई को सिद्ध करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह जैनाचार्यों को है। जैसे-जैसे दार्शनिक विचारों का भारतवर्ष में विकास और विस्तार बढ़ता गया वैसे-वैसे जैनों का अनेकान्त उन सबका समन्वय करता गया यह बात कालक्रम से निर्मित जैन दार्शनिक ग्रन्थों से सिद्ध होती है। वस्तुतः देखा जाय तो भारतवर्ष के दार्शनिक विचारों के क्रमिक विकास को अपने में संनिविष्ट करनेवाले ये जैन ग्रन्थ उपेक्षा का नहीं किन्तु अभ्यास का विषय बने यह आवश्यक है।
अनेकान्त की ही तरह भारतवर्ष में बुद्ध और महावीर से लेकर महात्मा गाँधी, विनोबा तक अहिंसा के विचार का विकास हआ है तथा आचरण में अहिंसा की व्यापकता क्रमशः बढते-बढते आज राजनैतिक क्षेत्र में भी पहुंच गयी है। ऐसी अहिंसा के विशेष अध्ययन की सामग्री जैन ग्रन्थों में है। जिस अहिंसा के सिद्धान्त का अग्रदूत भारतवर्ष राष्ट्रसमूह में बना है उस अहिंसा को परम्परा का इतिहास खोजना अनिवार्य है और उसके लिए तो जैन ग्रन्थों का अध्ययन अनिवार्य होगा ही। यह एक अच्छा लक्षण है कि जिससे कि जैन ग्रन्थों के अध्ययन की प्रगति अवश्य होगा ऐसा मैं मानता हूँ।
आधनिक भाषाओं के विकास का अध्ययन बढ़ रहा है और प्रादेशिक प्रचलित भाषाओं के उपरान्त बोलियों का अध्ययन भी हो रहा है-यह एक अच्छी बात है जिसके कारण प्राकृत भाषा का भाषादृष्टि से अध्ययन अनिवार्य हो गया है। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतवर्ष
( 7 )
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org