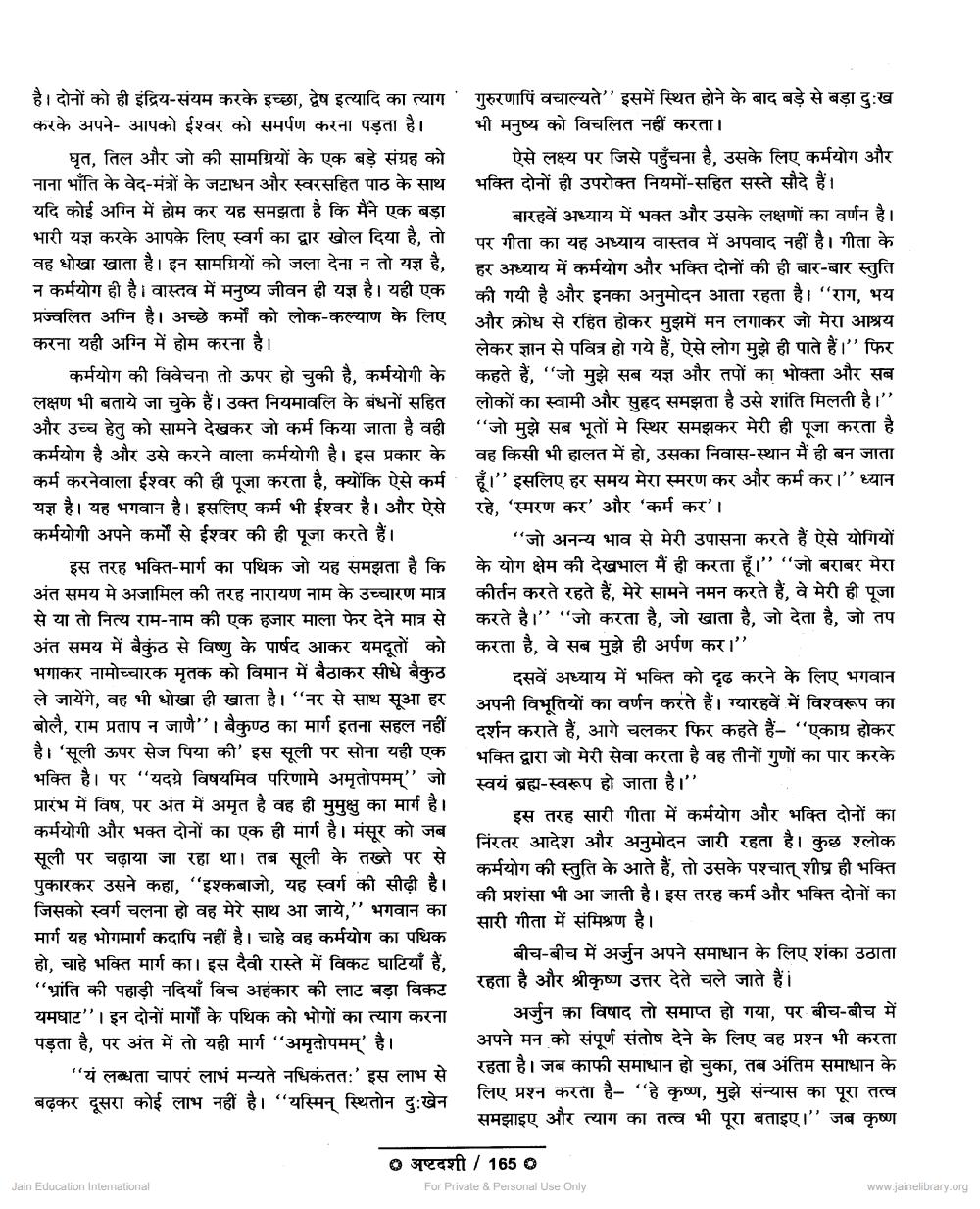________________
है। दोनों को ही इंद्रिय-संयम करके इच्छा, द्वेष इत्यादि का त्याग ' गुरुरणापिं वचाल्यते" इसमें स्थित होने के बाद बड़े से बड़ा दुःख करके अपने- आपको ईश्वर को समर्पण करना पड़ता है। भी मनुष्य को विचलित नहीं करता।
घृत, तिल और जो की सामग्रियों के एक बड़े संग्रह को ऐसे लक्ष्य पर जिसे पहुँचना है, उसके लिए कर्मयोग और नाना भाँति के वेद-मंत्रों के जटाधन और स्वरसहित पाठ के साथ भक्ति दोनों ही उपरोक्त नियमों-सहित सस्ते सौदे हैं। यदि कोई अग्नि में होम कर यह समझता है कि मैंने एक बड़ा बारहवें अध्याय में भक्त और उसके लक्षणों का वर्णन है। भारी यज्ञ करके आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, तो पर गीता का यह अध्याय वास्तव में अपवाद नहीं है। गीता के वह धोखा खाता है। इन सामग्रियों को जला देना न तो यज्ञ है,
हर अध्याय में कर्मयोग और भक्ति दोनों की ही बार-बार स्तुति न कर्मयोग ही है। वास्तव में मनुष्य जीवन ही यज्ञ है। यही एक
की गयी है और इनका अनुमोदन आता रहता है। "राग, भय प्रज्वलित अग्नि है। अच्छे कर्मों को लोक-कल्याण के लिए और क्रोध से रहित होकर मुझमें मन लगाकर जो मेरा आश्रय करना यही अग्नि में होम करना है।
लेकर ज्ञान से पवित्र हो गये हैं, ऐसे लोग मुझे ही पाते हैं।" फिर कर्मयोग की विवेचना तो ऊपर हो चुकी है, कर्मयोगी के कहते हैं, "जो मुझे सब यज्ञ और तपों का भोक्ता और सब लक्षण भी बताये जा चुके हैं। उक्त नियमावलि के बंधनों सहित लोकों का स्वामी और सुहृद समझता है उसे शांति मिलती है।" और उच्च हेतु को सामने देखकर जो कर्म किया जाता है वही "जो मुझे सब भूतों मे स्थिर समझकर मेरी ही पूजा करता है कर्मयोग है और उसे करने वाला कर्मयोगी है। इस प्रकार के वह किसी भी हालत में हो, उसका निवास-स्थान मैं ही बन जाता कर्म करनेवाला ईश्वर की ही पूजा करता है, क्योंकि ऐसे कर्म हूँ।" इसलिए हर समय मेरा स्मरण कर और कर्म कर।" ध्यान यज्ञ है। यह भगवान है। इसलिए कर्म भी ईश्वर है। और ऐसे रहे, ‘स्मरण कर' और 'कर्म कर'। कर्मयोगी अपने कर्मों से ईश्वर की ही पूजा करते हैं।
"जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं ऐसे योगियों इस तरह भक्ति-मार्ग का पथिक जो यह समझता है कि के योग क्षेम की देखभाल मैं ही करता हूँ।" "जो बराबर मेरा अंत समय मे अजामिल की तरह नारायण नाम के उच्चारण मात्र कीर्तन करते रहते हैं, मेरे सामने नमन करते हैं, वे मेरी ही पूजा से या तो नित्य राम-नाम की एक हजार माला फेर देने मात्र से करते है।" "जो करता है, जो खाता है, जो देता है, जो तप अंत समय में बैकुंठ से विष्णु के पार्षद आकर यमदूतों को करता है, वे सब मुझे ही अर्पण कर।" भगाकर नामोच्चारक मृतक को विमान में बैठाकर सीधे बैकुठ दसवें अध्याय में भक्ति को दृढ करने के लिए भगवान ले जायेंगे, वह भी धोखा ही खाता है। "नर से साथ सूआ हर अपनी विभतियों का वर्णन करते हैं। ग्यारहवें में विश्वरूप का बोलै, राम प्रताप न जाणै"। बैकुण्ठ का मार्ग इतना सहल नहीं दर्शन कराते हैं. आगे चलकर फिर कहते हैं- "एकाग्र होकर है। 'सूली ऊपर सेज पिया की' इस सूली पर सोना यही एक भक्ति द्वारा जो मेरी सेवा करता है वह तीनों गुणों का पार करके भक्ति है। पर "यदने विषयमिव परिणामे अमृतोपमम्' जो स्वयं ब्रह्म-स्वरूप हो जाता है।" प्रारंभ में विष, पर अंत में अमृत है वह ही मुमुक्षु का मार्ग है।
इस तरह सारी गीता में कर्मयोग और भक्ति दोनों का कर्मयोगी और भक्त दोनों का एक ही मार्ग है। मंसूर को जब
निंरतर आदेश और अनुमोदन जारी रहता है। कुछ श्लोक सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तब सूली के तख्ते पर से
कर्मयोग की स्तुति के आते हैं, तो उसके पश्चात् शीघ्र ही भक्ति पुकारकर उसने कहा, "इश्कबाजो, यह स्वर्ग की सीढ़ी है।
की प्रशंसा भी आ जाती है। इस तरह कर्म और भक्ति दोनों का जिसको स्वर्ग चलना हो वह मेरे साथ आ जाये," भगवान का
सारी गीता में संमिश्रण है। मार्ग यह भोगमार्ग कदापि नहीं है। चाहे वह कर्मयोग का पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग का। इस दैवी रास्ते में विकट घाटियाँ हैं,
बीच-बीच में अर्जुन अपने समाधान के लिए शंका उठाता "भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ विच अहंकार की लाट बडा विकट रहता है और श्रीकृष्ण उत्तर देते चले जाते हैं। यमघाट"। इन दोनों मार्गों के पथिक को भोगों का त्याग करना अर्जुन का विषाद तो समाप्त हो गया, पर बीच-बीच में पड़ता है, पर अंत में तो यही मार्ग "अमृतोपमम्' है। अपने मन को संपूर्ण संतोष देने के लिए वह प्रश्न भी करता __ "यं लब्धता चापरं लाभं मन्यते नधिकंततः' इस लाभ से
रहता है। जब काफी समाधान हो चुका, तब अंतिम समाधान के बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। "यस्मिन् स्थितोन दुःखेन ।
लिए प्रश्न करता है- "हे कृष्ण, मुझे संन्यास का पूरा तत्व समझाइए और त्याग का तत्व भी पूरा बताइए।" जब कृष्ण
० अष्टदशी /1650
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org