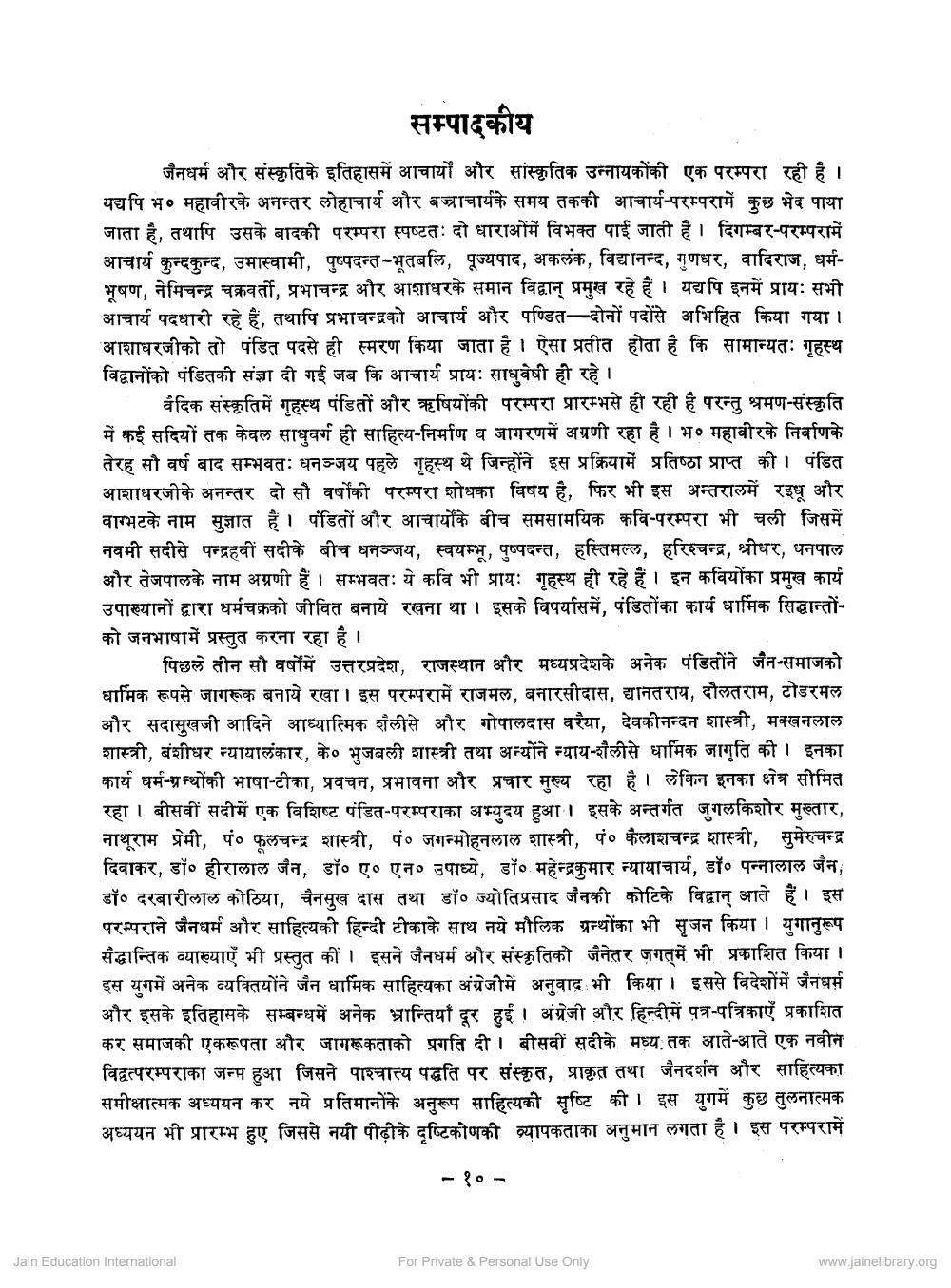________________
सम्पादकीय
जैनधर्म और संस्कृतिके इतिहासमें आचार्यों और सांस्कृतिक उन्नायकोंकी एक परम्परा रही है । यद्यपि भ. महावीरके अनन्तर लोहाचार्य और बज्राचार्यके समय तककी आचार्य-परम्परामें कुछ भेद पाया जाता है, तथापि उसके बादकी परम्परा स्पष्टतः दो धाराओंमें विभक्त पाई जाती है। दिगम्बर-परम्परामें आचार्य कुन्दकुन्द, उमास्वामी, पुष्पदन्त-भूतबलि, पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द, गुणधर, वादिराज, धर्मभूषण, नेमिचन्द्र चक्रवर्ती, प्रभाचन्द्र और आशाधरके समान विद्वान् प्रमुख रहे हैं। यद्यपि इनमें प्रायः सभी आचार्य पदधारी रहे हैं, तथापि प्रभाचन्द्रको आचार्य और पण्डित-दोनों पदोंसे अभिहित किया गया। आशाधरजीको तो पंडित पदसे ही स्मरण किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्यतः गहस्थ विद्वानोंको पंडितकी संज्ञा दी गई जब कि आचार्य प्रायः साधुवेषी ही रहे।
वैदिक संस्कृतिमें गृहस्थ पंडितों और ऋषियोंकी परम्परा प्रारम्भसे ही रही है परन्तु श्रमण-संस्कृति में कई सदियों तक केवल साधुवर्ग ही साहित्य-निर्माण व जागरणमें अग्रणी रहा है । भ० महावीरके निर्वाणके तेरह सौ वर्ष बाद सम्भवतः धनञ्जय पहले गृहस्थ थे जिन्होंने इस प्रक्रियामें प्रतिष्ठा प्राप्त की। पंडित आशाधरजीके अनन्तर दो सौ वर्षोंकी परम्परा शोधका विषय है, फिर भी इस अन्तरालमें रइधू और वाग्भटके नाम सुज्ञात है। पंडितों और आचार्योंके बीच समसामयिक कवि-परम्परा भी चली जिसमें नवमी सदीसे पन्द्रहवीं सदीके बीच धनञ्जय, स्वयम्भू, पुष्पदन्त, हस्तिमल्ल, हरिश्चन्द्र, श्रीधर, धनपाल और तेजपालके नाम अग्रणी हैं। सम्भवतः ये कवि भी प्रायः गृहस्थ ही रहे हैं। इन कवियोंका प्रमुख कार्य उपाख्यानों द्वारा धर्मचक्रको जीवित बनाये रखना था। इसके विपर्यासमें, पंडितोंका कार्य धार्मिक सिद्धान्तोंको जनभाषामें प्रस्तुत करना रहा है।
पिछले तीन सौ वर्षों में उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेशके अनेक पंडितोंने जैन समाजको धार्मिक रूपसे जागरूक बनाये रखा। इस परम्परामें राजमल, बनारसीदास, द्यानतराय, दौलतराम, टोडरमल और सदासुखजी आदिने आध्यात्मिक शैलीसे और गोपालदास वरैया, देवकीनन्दन शास्त्री, मक्खनलाल शास्त्री, बंशीधर न्यायालंकार, के० भुजबली शास्त्री तथा अन्योंने न्याय-शैलीसे धार्मिक जागृति की। इनका कार्य धर्म-ग्रन्थोंकी भाषा-टीका, प्रवचन, प्रभावना और प्रचार मुख्य रहा है। लेकिन इनका क्षेत्र सीमित रहा । बीसवीं सदीमें एक विशिष्ट पंडित-परम्पराका अभ्युदय हुआ। इसके अन्तर्गत जुगलकिशोर मुख्तार, नाथूराम प्रेमी, पं० फूलचन्द्र शास्त्री, पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री, पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, सुमेरुचन्द्र दिवाकर, डॉ० हीरालाल जैन, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, डॉ०. महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, डॉ० पन्नालाल जैन, डॉ० दरबारीलाल कोठिया, चैनसुख दास तथा डॉ० ज्योतिप्रसाद जैनकी कोटिके विद्वान् आते हैं। इस परम्पराने जैनधर्म और साहित्यकी हिन्दी टीकाके साथ नये मौलिक ग्रन्थोंका भी सूजन किया। युगानुरूप सैद्धान्तिक व्याख्याएँ भी प्रस्तुत की। इसने जैनधर्म और संस्कृतिको जैनेतर जगत्में भी प्रकाशित किया। इस युगमें अनेक व्यक्तियोंने जैन धार्मिक साहित्यका अंग्रेजीमें अनुवाद भी किया। इससे विदेशोंमें जैनधर्म
और इसके इतिहासके सम्बन्धमें अनेक भ्रान्तियाँ दूर हई। अंग्रेजी और हिन्दीमें पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित कर समाजकी एकरूपता और जागरूकताको प्रगति दी। बीसवीं सदीके मध्य तक आते-आते एक नवीन विद्वत्परम्पराका जन्म हआ जिसने पाश्चात्त्य पद्धति पर संस्कृत, प्राकृत तथा जैनदर्शन और साहित्यका समीक्षात्मक अध्ययन कर नये प्रतिमानोंके अनुरूप साहित्यकी सृष्टि की। इस युगमें कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी प्रारम्भ हुए जिससे नयी पीढ़ीके दृष्टिकोणकी व्यापकताका अनुमान लगता है । इस परम्परामें
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org