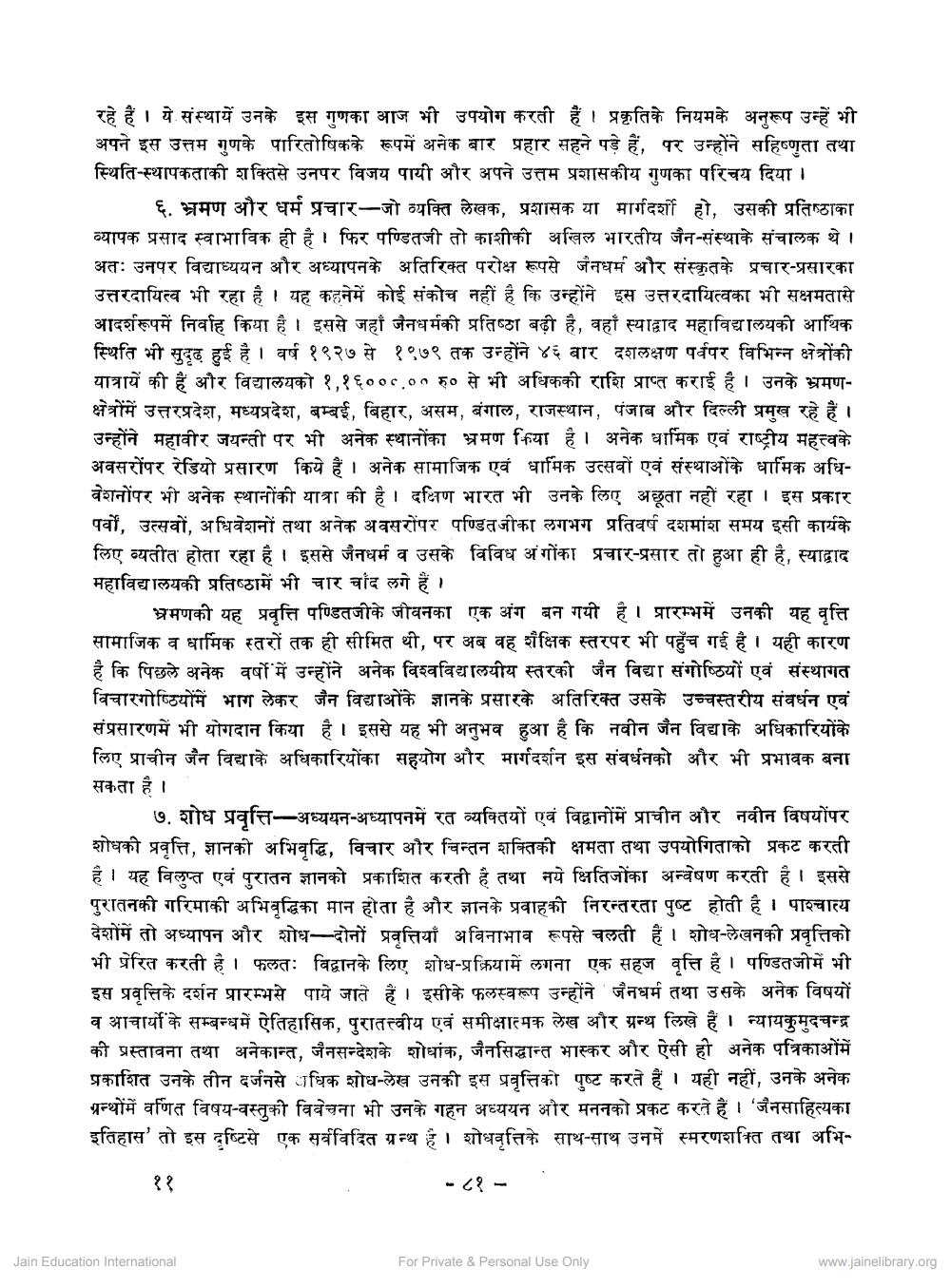________________
रहे हैं । ये संस्थायें उनके इस गुणका आज भी उपयोग करती हैं । प्रकृतिके नियमके अनुरूप उन्हें भी अपने इस उत्तम गुणके पारितोषिक के रूपमें अनेक बार प्रहार सहने पड़े हैं, पर उन्होंने सहिष्णुता तथा स्थिति-स्थापकताकी शक्तिसे उनपर विजय पायी और अपने उत्तम प्रशासकीय गुणका परिचय दिया ।
६. भ्रमण और धर्म प्रचार - जो व्यक्ति लेखक, प्रशासक या मार्गदर्शी हो, उसकी प्रतिष्ठाका व्यापक प्रसाद स्वाभाविक ही है । फिर पण्डितजी तो काशीकी अखिल भारतीय जैन संस्थाके संचालक थे । अतः उनपर विद्याध्ययन और अध्यापनके अतिरिक्त परोक्ष रूपसे जैनधर्म और संस्कृतके प्रचार- प्रसारका उत्तरदायित्व भी रहा है । यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने इस उत्तरदायित्वका भी सक्षमता से आदर्शरूपमें निर्वाह किया है । इससे जहाँ जैनधर्मकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, वहाँ स्याद्वाद महाविद्यालयको आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है । वर्ष १९२७ से १९७९ तक उन्होंने ४६ बार दशलक्षण पर्वपर विभिन्न क्षेत्रोंकी यात्रायें की हैं और विद्यालयको १,१६०००.०० रु० से भी अधिककी राशि प्राप्त कराई है । उनके भ्रमणक्षेत्रों में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बम्बई, बिहार, असम, बंगाल, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली प्रमुख रहे हैं । उन्होंने महावीर जयन्ती पर भी अनेक स्थानोंका भ्रमण किया है । अनेक धार्मिक एवं राष्ट्रीय महत्त्वके अवसरोंपर रेडियो प्रसारण किये हैं । अनेक सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों एवं संस्थाओंके धार्मिक अधिवेशनों पर भी अनेक स्थानोंकी यात्रा की है । दक्षिण भारत भी उनके लिए अछूता नहीं रहा । इस प्रकार पर्वों, उत्सवों, अधिवेशनों तथा अनेक अवसरोंपर पण्डितजीका लगभग प्रतिवर्ष दशमांश समय इसी कार्यके लिए व्यतीत होता रहा है । इससे जैनधर्म व उसके विविध अंगोंका प्रचार-प्रसार तो हुआ ही है, स्याद्वाद महाविद्यालयकी प्रतिष्ठामें भी चार चांद लगे हैं ।
भ्रमणकी यह प्रवृत्ति पण्डितजीके जीवनका एक अंग बन गयी है । प्रारम्भ में उनकी यह वृत्ति सामाजिक व धार्मिक स्तरों तक ही सीमित थी, पर अब वह शैक्षिक स्तरपर भी पहुँच गई हैं । यही कारण है कि पिछले अनेक वर्षों में उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयीय स्तरको जैन विद्या संगोष्ठियों एवं संस्थागत विचारगोष्ठियों में भाग लेकर जैन विद्याओंके ज्ञानके प्रसारके अतिरिक्त उसके उच्चस्तरीय संवर्धन एवं संप्रसारणमें भी योगदान किया है। इससे यह भी अनुभव हुआ है कि नवीन जैन विद्याके अधिकारियोंके लिए प्राचीन जैन विद्या के अधिकारियोंका सहयोग और मार्गदर्शन इस संवर्धनको और भी प्रभावक बना सकता है ।
७. शोध प्रवृत्ति - अध्ययन-अध्यापनमें रत व्यक्तियों एवं विद्वानोंमें प्राचीन और नवीन विषयों पर शोधकी प्रवृत्ति, ज्ञानको अभिवृद्धि, विचार और चिन्तन शक्तिकी क्षमता तथा उपयोगिताको प्रकट करती है । यह विलुप्त एवं पुरातन ज्ञानको प्रकाशित करती है तथा नये क्षितिजोंका अन्वेषण करती है । इससे पुरातनकी गरिमाकी अभिवृद्धिका मान होता है और ज्ञान के प्रवाहकी निरन्तरता पुष्ट होती है । पाश्चात्य देशोंमें तो अध्यापन और शोध - दोनों प्रवृत्तियाँ अविनाभाव रूपसे चलती हैं। शोध लेखनकी प्रवृत्तिको भी प्रेरित करती है । फलतः विद्वानके लिए शोध प्रक्रियामें लगना एक सहज वृत्ति है । पण्डितजी में भी इस प्रवृत्तिके दर्शन प्रारम्भसे पाये जाते हैं । इसीके फलस्वरूप उन्होंने जैनधर्म तथा उसके अनेक विषयों व आचार्यो के सम्बन्धमें ऐतिहासिक, पुरातत्त्वीय एवं समीक्षात्मक लेख और ग्रन्थ लिखे हैं । न्यायकुमुदचन्द्र की प्रस्तावना तथा अनेकान्त, जैनसन्देशके शोधांक, जैनसिद्धान्त भास्कर और ऐसी ही अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके तीन दर्जन से अधिक शोध लेख उनकी इस प्रवृत्तिको पुष्ट करते हैं । यही नहीं, उनके अनेक ग्रन्थोंमें वर्णित विषय-वस्तुको विवेचना भी उनके गहन अध्ययन और मननको प्रकट करते हैं । 'जैनसाहित्यका इतिहास' तो इस दृष्टिसे एक सर्वविदित ग्रन्थ है । शोधवृत्तिके साथ-साथ उनमें स्मरणशक्ति तथा अभि
११
- ८१ -
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org