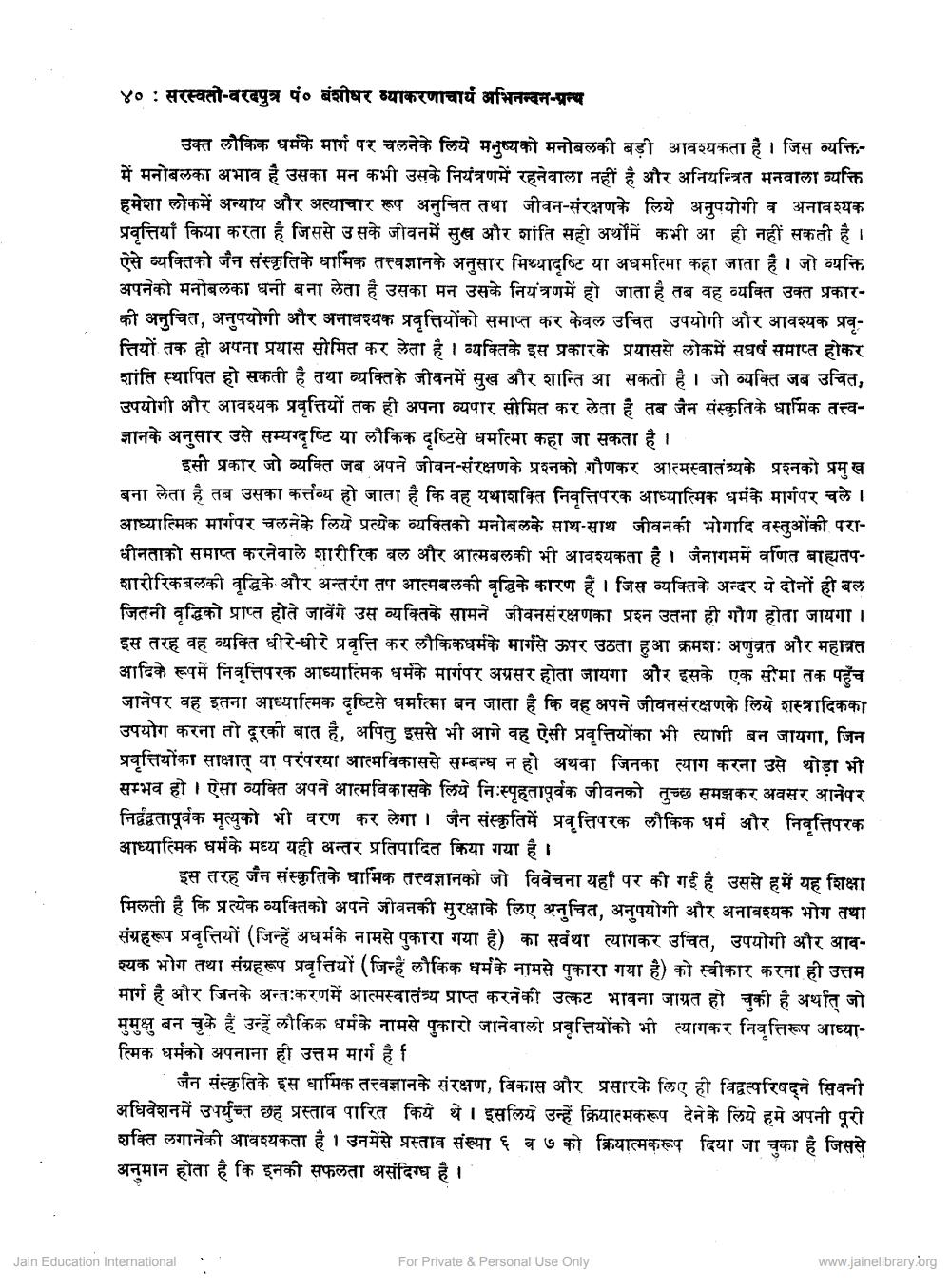________________
४० : सरस्वती-वरदपुत्र पं. बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-प्रन्य
उक्त लौकिक धर्मके मार्ग पर चलनेके लिये मनुष्यको मनोबलकी बड़ी आवश्यकता है। जिस व्यक्तिमें मनोबलका अभाव है उसका मन कभी उसके नियंत्रणमें रहनेवाला नहीं है और अनियन्त्रित मनवाला व्यक्ति हमेशा लोकमें अन्याय और अत्याचार रूप अनुचित तथा जीवन-संरक्षणके लिये अनुपयोगी व अनावश्यक प्रवृत्तियाँ किया करता है जिससे उसके जीवनमें सुख और शांति सही अर्थों में कभी आ ही नहीं सकती है । ऐसे व्यक्तिको जैन संस्कृतिके धार्मिक तत्त्वज्ञानके अनुसार मिथ्यादृष्टि या अधर्मात्मा कहा जाता है । जो व्यक्ति अपनेको मनोबलका धनी बना लेता है उसका मन उसके नियंत्रणमें हो जाता है तब वह व्यक्ति उक्त प्रकारकी अनुचित, अनुपयोगी और अनावश्यक प्रवृत्तियोंको समाप्त कर केवल उचित उपयोगी और आवश्यक प्रवृतियों तक हो अपना प्रयास सीमित कर लेता है । व्यक्तिके इस प्रकारके प्रयाससे लोकमें सघर्ष समाप्त होकर शांति स्थापित हो सकती है तथा व्यक्तिके जीवनमें सुख और शान्ति आ सकती है। जो व्यक्ति जब उचित, उपयोगी और आवश्यक प्रवृत्तियों तक ही अपना व्यपार सीमित कर लेता है तब जैन संस्कृतिके धार्मिक तत्त्वज्ञानके अनुसार उसे सम्यग्दृष्टि या लौकिक दृष्टिसे धर्मात्मा कहा जा सकता है।
इसी प्रकार जो व्यक्ति जब अपने जीवन-संरक्षणके प्रश्नको गौणकर आत्मस्वातंत्र्यके प्रश्नको प्रमुख बना लेता है तब उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह यथाशक्ति निवृत्तिपरक आध्यात्मिक धर्मके मार्गपर चले । आध्यात्मिक मार्गपर चलने के लिये प्रत्येक व्यक्तिको मनोबलके साथ-साथ जीवनकी भोगादि वस्तुओंकी पराधीनताको समाप्त करनेवाले शारीरिक बल और आत्मबलकी भी आवश्यकता है। जैनागममें वणित बाह्यतपशारीरिकबलकी वृद्धिके और अन्तरंग तप आत्मबलकी वृद्धिके कारण हैं। जिस व्यक्तिके अन्दर ये दोनों ही बल जितनी वृद्धिको प्राप्त होते जावेंगे उस व्यक्तिके सामने जीवनसंरक्षणका प्रश्न उतना ही गौण होता जायगा । इस तरह वह व्यक्ति धीरे-धीरे प्रवृत्ति कर लौकिकधर्मके मार्गसे ऊपर उठता हआ क्रमशः अणव्रत और महाव्रत आदिके रूपमें निवृत्तिपरक आध्यात्मिक धर्मके मार्गपर अग्रसर होता जायगा और इसके एक सीमा तक पहुँच जानेपर वह इतना आध्यात्मिक दृष्टिसे धर्मात्मा बन जाता है कि वह अपने जीवनसंरक्षणके लिये शस्त्रादिकका उपयोग करना तो दूरकी बात है, अपितु इससे भी आगे वह ऐसी प्रवृत्तियोंका भी त्यागी बन जायगा, जिन प्रवृत्तियोंका साक्षात् या परंपरया आत्मविकाससे सम्बन्ध न हो अथवा जिनका त्याग करना उसे थोड़ा भी सम्भव हो । ऐसा व्यक्ति अपने आत्मविकासके लिये निःस्पृहतापूर्वक जीवनको तुच्छ समझकर अवसर आनेपर निद्वतापूर्वक मृत्युको भी वरण कर लेगा। जैन संस्कृतिमें प्रवृत्तिपरक लौकिक धर्म और निवृत्तिपरक आध्यात्मिक धर्मके मध्य यही अन्तर प्रतिपादित किया गया है।
इस तरह जैन संस्कृतिके धार्मिक तत्वज्ञानको जो विवेचना यहाँ पर की गई है उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने जीवनकी सुरक्षाके लिए अनुचित, अनुपयोगी और अनावश्यक भोग तथा संग्रहरूप प्रवृत्तियों (जिन्हें अधर्मके नामसे पुकारा गया है) का सर्वथा त्यागकर उचित, उपयोगी और आवश्यक भोग तथा संग्रहरूप प्रवृत्तियों (जिन्हें लौकिक धर्म के नामसे पुकारा गया है) को स्वीकार करना ही उत्तम मार्ग है और जिनके अन्तःकरणमें आत्मस्वातंत्र्य प्राप्त करने की उत्कट भावना जाग्रत हो चुकी है अर्थात् जो मुमुक्षु बन चुके हैं उन्हें लौकिक धर्म के नामसे पुकारो जानेवालो प्रवृत्तियोंको भी त्यागकर निवृत्तिरूप आध्यात्मिक धर्मको अपनाना ही उत्तम मार्ग है ।
जैन संस्कृतिके इस धार्मिक तत्त्वज्ञानके संरक्षण, विकास और प्रसारके लिए ही विद्वत्परिषद्ने सिवनी अधिवेशनमें उपर्युक्त छह प्रस्ताव पारित किये थे । इसलिये उन्हें क्रियात्मकरूप देने के लिये हमे अपनी पूरी शक्ति लगानेकी आवश्यकता है। उनमेंसे प्रस्ताव संख्या ६ व ७ को क्रियात्मकरूप दिया जा चुका है जिससे अनुमान होता है कि इनकी सफलता असंदिग्ध है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org