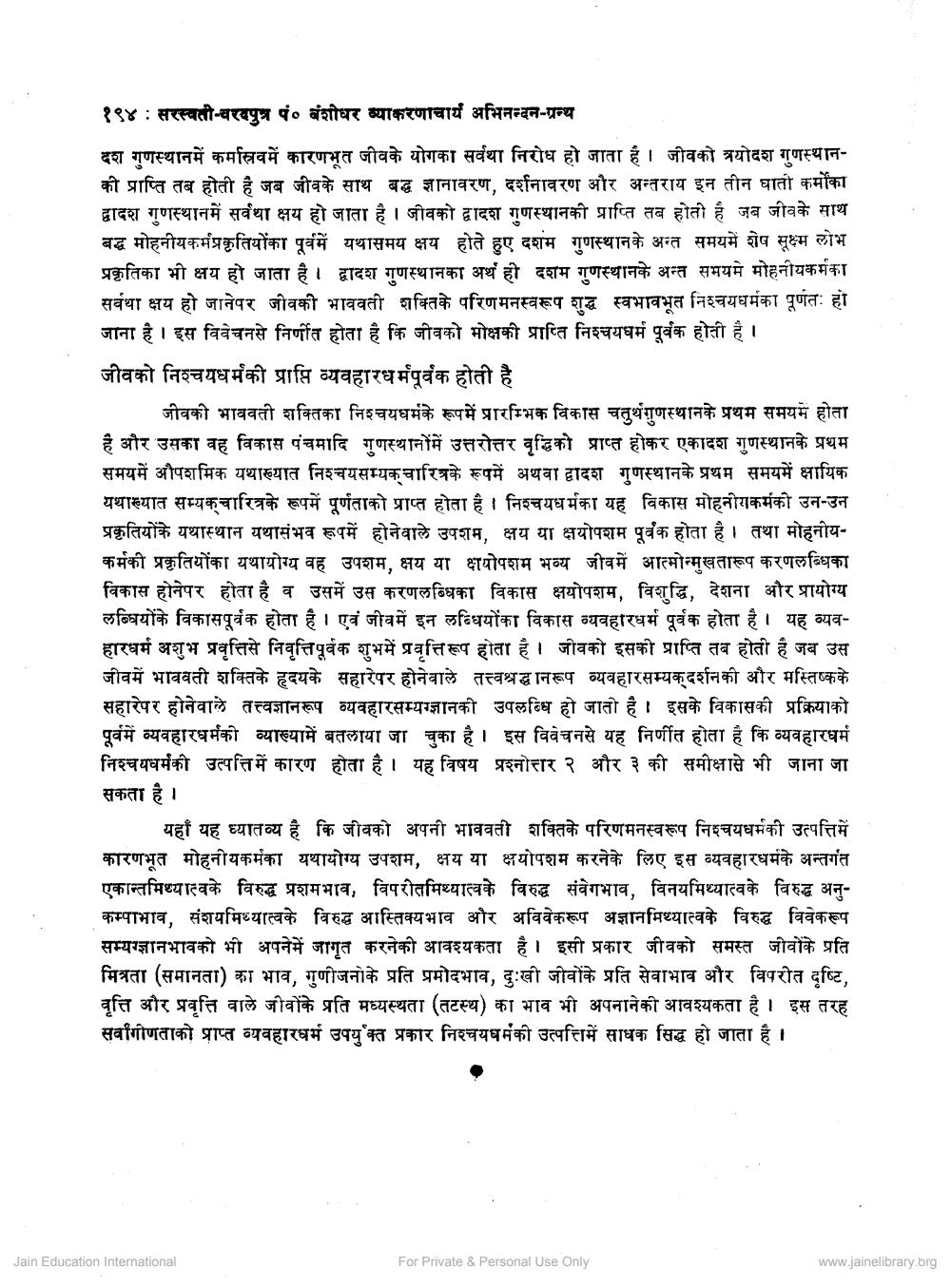________________
१९४ : सरस्वती-वरवपुत्र पं०बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ
दश गुणस्थानमें कर्मास्रवमें कारणभूत जीवके योगका सर्वथा निरोध हो जाता है। जीवको त्रयोदश गुणस्थानकी प्राप्ति तब होती है जब जीवके साथ बद्ध ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घाती कर्मोका द्वादश गुणस्थानमें सर्वथा क्षय हो जाता है। जीवको द्वादश गणस्थानकी प्राप्ति तब होती है जब जीवके साथ बद्ध मोहनीयकर्मप्रकृतियोंका पूर्व में यथासमय क्षय होते हुए दशम गुणस्थान के अन्त समयमें शेष सूक्ष्म लोभ प्रकृतिका भी क्षय हो जाता है। द्वादश गुणस्थानका अर्थ ही दशम गुणस्थानके अन्त समयमे मोहनीयकर्मका सर्वथा क्षय हो जानेपर जीवकी भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मका पूर्णतः हो जाना है। इस विवेचनसे निर्णीत होता है कि जीवको मोक्षकी प्राप्ति निश्चयधर्म पूर्वक होती है ।
जीवको निश्चयधर्मकी प्राप्ति व्यवहारधर्मपूर्वक होती है
जीवकी भाववती शक्तिका निश्चयधर्मके रूप में प्रारम्भिक विकास चतुर्थगुणस्थानके प्रथम समयमें होता है और उसका वह विकास पंचमादि गुणस्थानोंमें उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होकर एकादश गुणस्थानके प्रथम समयमें औपशमिक यथाख्यात निश्चयसम्यक चारित्रके रूपमें अथवा द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें क्षायिक यथाख्यात सम्यक्चारित्रके रूपमें पूर्णताको प्राप्त होता है। निश्चयधर्मका यह विकास मोहनीयकर्मको उन-उन प्रकृतियोंके यथास्थान यथासंभव रूपमें होनेवाले उपशम. क्षय या क्षयोपशम पूर्वक होता है। तथा मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंका यथायोग्य वह उपशम, क्षय या क्षयोपशम भव्य जीवमें आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धिका विकास होनेपर होता है व उसमें उस करणलब्धिका विकास क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियोंके विकासपूर्वक होता है। एवं जीवमें इन लब्धियोंका विकास व्यवहारधर्म पूर्वक होता है। यह हारधर्म अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक शुभमें प्रवृत्तिरूप होता है। जीवको इसकी प्राप्ति तब होती है जब उस जीवमें भाववती शक्तिके हृदयके सहारेपर होनेवाले तत्त्वश्रद्धानरूप व्यवहारसम्यक् दर्शन की और मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाले तत्त्वज्ञानरूप व्यवहारसम्यग्ज्ञानकी उपलब्धि हो जाती है। इसके विकास पूर्वमें व्यवहारधर्मको व्याख्यामें बतलाया जा चुका है। इस विवेचनसे यह निर्णीत होता है कि व्यवहारधर्म निश्चयधर्मकी उत्पत्तिमें कारण होता है। यह विषय प्रश्नोत्तर २ और ३ की समीक्षासे भी जाना जा सकता है।
यहाँ यह ध्यातव्य है कि जीवको अपनी भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप निश्चयधर्मकी उत्पत्तिमें। कारणभूत मोहनीयकर्मका यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम करनेके लिए इस व्यवहारधर्मके अन्तर्गत एकान्तमिथ्यात्वके विरुद्ध प्रशमभाव, विपरीतमिथ्यात्वके विरुद्ध संवेगभाव, विनयमिथ्यात्वके विरुद्ध अनुकम्पाभाव, संशयमिथ्यात्वके विरुद्ध आस्तिक्यभाव और अविवेकरूप अज्ञानमिथ्यात्वके विरुद्ध विवेकरूप सम्यग्ज्ञानभावको भी अपनेमें जागृत करनेकी आवश्यकता है। इसी प्रकार जीवको समस्त जीवोंके प्रति मित्रता (समानता) का भाव, गुणीजनोके प्रति प्रमोदभाव, दुःखी जीवोंके प्रति सेवाभाव और विपरीत दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति वाले जीवोंके प्रति मध्यस्थता (तटस्थ) का भाव भी अपनाने की आवश्यकता है। इस तरह सर्वांगीणताको प्राप्त व्यवहारधर्म उपयुक्त प्रकार निश्चयधर्मकी उत्पत्तिमें साधक सिद्ध हो जाता है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org