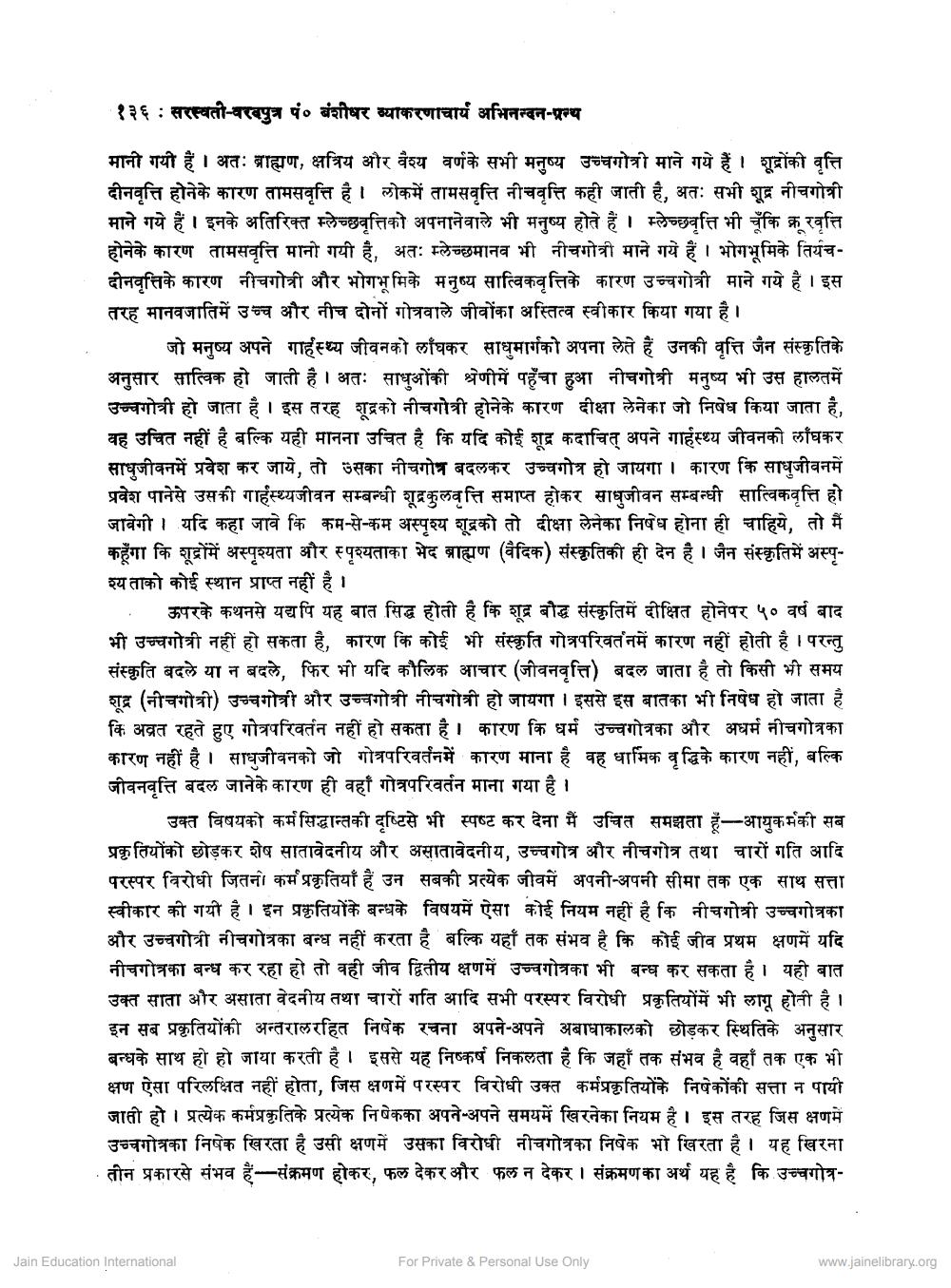________________
१३६ : सरस्वती - वरवपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन - प्रन्थ
गयी हैं । अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णके सभी मनुष्य उच्चगोत्री माने गये हैं । शूद्रोंकी वृत्ति दीनवृत्ति होनेके कारण तामसवृत्ति है । लोकमें तामसवृत्ति नीचवृत्ति कही जाती है, अतः सभी शूद्र नीचगोत्री ये हैं । इनके अतिरिक्त म्लेच्छवृत्तिको अपनानेवाले भी मनुष्य होते हैं । म्लेच्छवृत्ति भी चूँकि क्रूरवृत्ति होनेके कारण तामसवृत्ति मानो गयी है, अतः म्लेच्छमानव भी नीचगोत्री माने गये हैं । भोगभूमिके तियंचदोनवृत्ति के कारण नीचगोत्री और भोगभूमिके मनुष्य सात्विकवृत्तिके कारण उच्चगोत्री माने गये है । इस तरह मानवजाति में उच्च और नीच दोनों गोत्रवाले जीवोंका अस्तित्व स्वीकार किया गया है ।
जो मनुष्य 'अपने गार्हस्थ्य जीवनको लाँघकर साधुमार्गको अपना लेते हैं उनकी वृत्ति जैन संस्कृतिके अनुसार सात्विक हो जाती है । अतः साधुओंकी श्रेणीमें पहुँचा हुआ नीचगोत्री मनुष्य भी उस हालत में उच्चगोत्री हो जाता है । इस तरह शूद्रको नीचगोत्री होनेके कारण दीक्षा लेनेका जो निषेध किया जाता है, वह उचित नहीं है बल्कि यही मानना उचित है कि यदि कोई शूद्र कदाचित् अपने गार्हस्थ्य जीवनको लाँघकर साधुजीवनमें प्रवेश कर जाये, तो उसका नीचगोत्र बदलकर उच्चगोत्र हो जायगा । कारण कि साधुजीवनमें प्रवेश पानेसे उसकी गार्हस्थ्यजीवन सम्बन्धी शूद्रकुलवृत्ति समाप्त होकर साधुजीवन सम्बन्धी सात्विकवृत्ति हो जावेगी । यदि कहा जावे कि कम-से-कम अस्पृश्य शूद्रको तो दीक्षा लेनेका निषेध होना ही चाहिये, तो मैं कहूँगा कि शूद्रोंमें अस्पृश्यता और स्पृश्यताका भेद ब्राह्मण (वैदिक) संस्कृतिकी ही देन है । जैन संस्कृतिमें अस्पृश्यताको कोई स्थान प्राप्त नहीं है ।
ऊपर के कथनसे यद्यपि यह बात सिद्ध होती है कि शूद्र बौद्ध संस्कृतिमें दीक्षित होनेपर ५० वर्ष बाद भी उच्चगोत्री नहीं हो सकता है, कारण कि कोई भी संस्कृति गोत्रपरिवर्तनमें कारण नहीं होती है । परन्तु संस्कृति बदले या न बदले, फिर भी यदि कौलिक आचार ( जीवनवृत्ति) बदल जाता है तो किसी भी समय शूद्र (नीचगोत्री) उच्चगोत्री और उच्चगोत्री नीचगोत्री हो जायगा । इससे इस बातका भी निषेध हो जाता है कि अव्रत रहते हुए गोत्रपरिवर्तन नहीं हो सकता है। कारण कि धर्म उच्चगोत्रका और अधर्म नीचगोत्रका कारण नहीं है । साधुजीवनको जो गोत्रपरिवर्तनमें कारण माना है वह धार्मिक वृद्धिके कारण नहीं, बल्कि जीवनवृत्ति बदल जानेके कारण ही वहाँ गोत्रपरिवर्तन माना गया है ।
उक्त विषयको कर्म सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी स्पष्ट कर देना मैं उचित समझता हूँ - आयुकर्मकी सब प्रकृतियोंको छोड़कर शेष सातावेदनीय और असातावेदनीय, उच्चगोत्र और नीचगोत्र तथा चारों गति आदि परस्पर विरोधी जितनी कर्म प्रकृतियाँ हैं उन सबकी प्रत्येक जीवमें अपनी-अपनी सीमा तक एक साथ सत्ता स्वीकार की गयी है । इन प्रकृतियोंके बन्धके विषयमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि नीचगोत्री उच्चगोत्रका और उच्चगोत्री नीचगोत्रका बन्ध नहीं करता है बल्कि यहाँ तक संभव है कि कोई जीव प्रथम क्षणमें यदि नीचगोत्रका बन्ध कर रहा हो तो वही जीव द्वितीय क्षण में उच्चगोत्रका भी बन्ध कर सकता है । यही बात उक्त साता और असाता वेदनीय तथा चारों गति आदि सभी परस्पर विरोधी प्रकृतियोंमें भी लागू होती है । इन सब प्रकृतियोंकी अन्तरालरहित निषेक रचना अपने-अपने अबाघाकालको छोड़कर स्थितिके अनुसार बन्धके साथ हो हो जाया करती है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक एक भी क्षण ऐसा परिलक्षित नहीं होता, जिस क्षण में परस्पर विरोधी उक्त कर्मप्रकृतियोंके निषेकोंकी सत्ता न पायी जाती हो । प्रत्येक कर्मप्रकृतिके प्रत्येक निषेकका अपने-अपने समयमें खिरनेका नियम है। इस तरह जिस क्षण में उच्चगोत्रका निषेक खिरता है उसी क्षणमें उसका विरोधी नीचगोत्रका निषेक भो खिरता है । यह खिरना तीन प्रकारसे संभव हैं - संक्रमण होकर, फल देकर और फल न देकर । संक्रमणका अर्थ यह है कि उच्चगोत्र
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org