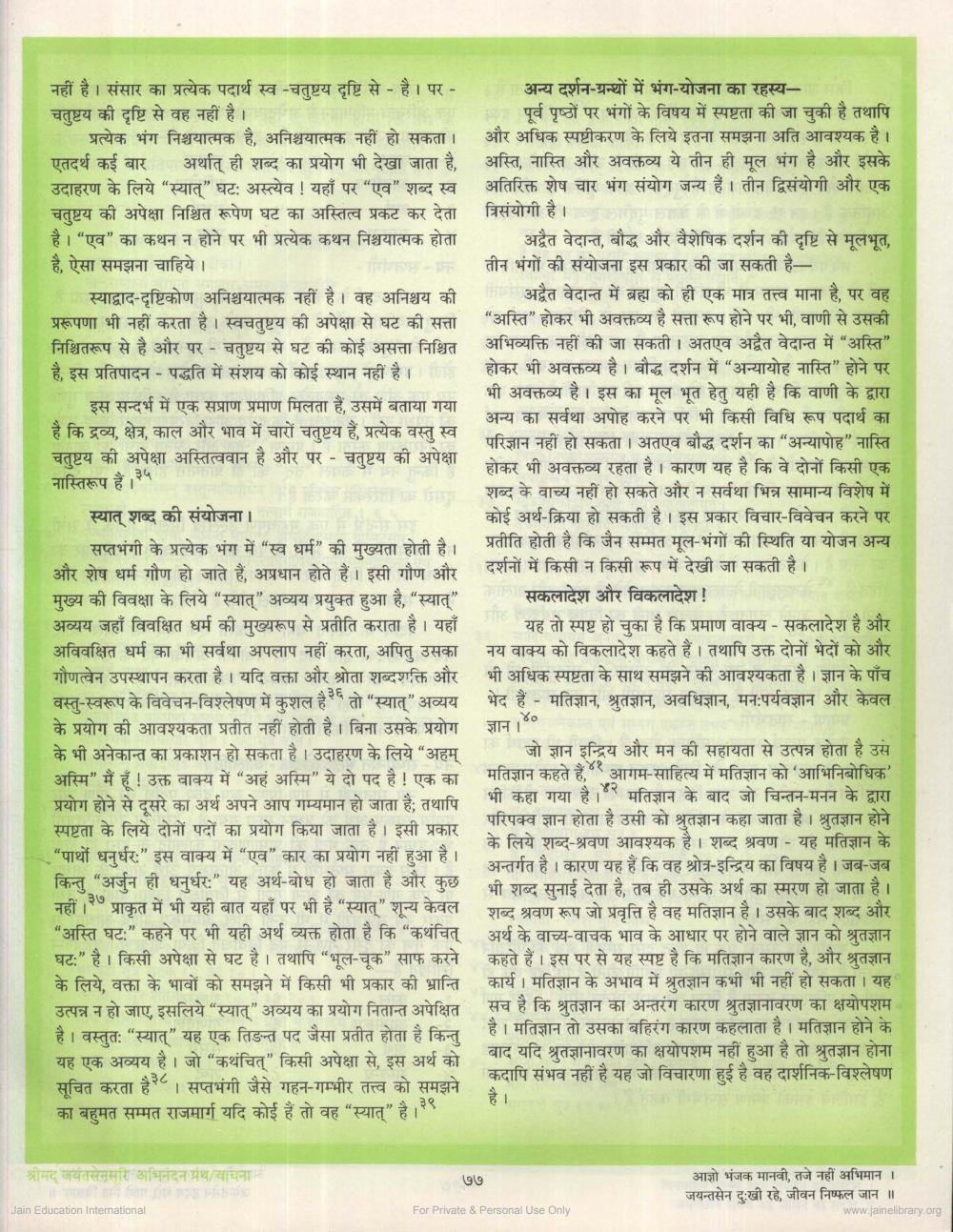________________
नहीं है। संसार का प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय दृष्टि से है पर चतुष्टय की दृष्टि से वह नहीं है।
प्रत्येक भंग निश्चयात्मक है, अनिशयात्मक नहीं हो सकता। एतदर्थ कई बार अर्थात् ही शब्द का प्रयोग भी देखा जाता है उदाहरण के लिये "स्यात्" घटः अस्त्येव यहाँ पर "एव" शब्द स्व चतुष्टय की अपेक्षा निश्चित रूपेण घट का अस्तित्व प्रकट कर देता है "एव" का कथन न होने पर भी प्रत्येक कथन निक्षयात्मक होता है, ऐसा समझना चाहिये।
स्वाद्वाद दृष्टिकोण अनिश्चयात्मक नहीं है वह अनिश्चय की प्ररूपणा भी नहीं करता है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से घट की निश्चितरूप से है और पर चतुष्टय से घट की कोई असता निश्चित है. इस प्रतिपादन पद्धति में संशय को कोई स्थान नहीं है।
इस सन्दर्भ में एक सप्राण प्रमाण मिलता हैं, उसमें बताया गया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में चारों चतुष्टय हैं, प्रत्येक वस्तु स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्ववान है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है। ३५ sap
स्यात् शब्द की संयोजना।
३६
सप्तभंगी के प्रत्येक भंग में "स्व धर्म" की मुख्यता होती है। और शेष धर्म गौण हो जाते हैं, अप्रधान होते हैं। इसी गौण और मुख्य की विवक्षा के लिये "स्यात्” अव्यय प्रयुक्त हुआ है, “स्यात् " अव्यय जहाँ विवक्षित धर्म की मुख्यरूप से प्रतीति कराता है। यहाँ अविवक्षित धर्म का भी सर्वथा अपलाप नहीं करता, अपितु उसका गौणत्वेन उपस्थापन करता है। यदि वक्ता और श्रोता शब्दशक्ति और वस्तु-स्वरूप के विवेचन-विश्लेषण में कुशल है तो " स्यात् ” अव्यय के प्रयोग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बिना उसके प्रयोग के भी अनेकान्त का प्रकाशन हो सकता है। उदाहरण के लिये “अहम् अस्मि" मैं हूँ! उक्त वाक्य में "अहं अस्मि" ये दो पद है! एक का प्रयोग होने से दूसरे का अर्थ अपने आप गम्यमान हो जाता है, तथापि स्पष्टता के लिये दोनों पदों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार “पार्थो धनुर्धरः " इस वाक्य में “एव" कार का प्रयोग नहीं हुआ है। किन्तु " अर्जुन ही धनुर्धरः " यह अर्थ-बोध हो जाता है और कुछ नहीं । प्राकृत में भी यही बात यहाँ पर भी है " स्यात् " शून्य केवल “अस्ति घटः " कहने पर भी यही अर्थ व्यक्त होता है कि “कथंचित् घटः " है। किसी अपेक्षा से घट है तथापि "भूल-चूक" साफ करने के लिये, वक्ता के भावों को समझने में किसी भी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न न हो जाए, इसलिये "स्यात्" अव्यय का प्रयोग नितान्त अपेक्षित है । वस्तुतः "स्यात्" यह एक तिङन्त पद जैसा प्रतीत होता है किन्तु यह एक अव्यय है । जो “कथंचित्" किसी अपेक्षा से, इस अर्थ को सूचित करता है३८। सप्तभंगी जैसे गहन-गम्भीर तत्त्व को समझने का बहुमत सम्मत राजमार्ग यदि कोई हैं तो वह " स्यात्" है।
३७
३९
श्रीमद् जयंतसेनरि अभिनंदन ग्रंथ वाचना
Seni
Fable
Jain Education International
अन्य दर्शन-ग्रन्थों में भंग-योजना का रहस्य
पूर्व पृष्ठों पर भंगों के विषय में स्पष्टता की जा चुकी है तथापि और अधिक स्पष्टीकरण के लिये इतना समझना अति आवश्यक है। अस्ति नास्ति और अवक्तव्य ये तीन ही मूल भंग है और इसके अतिरिक्त शेष चार भंग संयोग जन्य हैं। तीन द्विसंयोगी और एक त्रिसंयोगी है।
अद्वैत वेदान्त, बौद्ध और वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से मूलभूत, तीन भंगों की संयोजना इस प्रकार की जा सकती है
अद्वैत वेदान्त में ब्रा को ही एक मात्र तत्त्व माना है, पर वह "अस्ति" होकर भी अवक्तव्य है सत्ता रूप होने पर भी वाणी से उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। अतएव अद्वैत वेदान्त में " अस्ति” होकर भी अवतव्य है। बौद्ध दर्शन में 'अन्यायोह नास्ति" होने पर भी अवक्तव्य है। इस का मूल भूत हेतु यही है कि वाणी के द्वारा अन्य का सर्वथा अपोह करने पर भी किसी विधि रूप पदार्थ का परिज्ञान नहीं हो सकता। अतएव बौद्ध दर्शन का "अन्यापोह" नास्ति होकर भी अवक्तव्य रहता है। कारण यह है कि वे दोनों किसी एक शब्द के वाच्य नहीं हो सकते और न सर्वथा भिन्न सामान्य विशेष में कोई अर्थ-क्रिया हो सकती है। इस प्रकार विचार-विवेचन करने पर प्रतीति होती है कि जैन सम्मत मूल-भंगों की स्थिति या योजन अन्य दर्शनों में किसी न किसी रूप में देखी जा सकती है। सकलादेश और विकलादेश !
गाँठ
यह तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रमाण वाक्य सकलादेश है और नय वाक्य को विकलादेश कहते हैं। तथापि उक्त दोनों भेदों को और भी अधिक स्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है। ज्ञान के पाँच भेद हैं मतिज्ञान् श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्यवज्ञान और केवल
४०
ज्ञान ।
जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं, आगम-साहित्य में मतिज्ञान को 'आभिनिबोधिक' भी कहा गया है। ४२ मतिज्ञान के बाद जो चिन्तन-मनन के द्वारा परिपक्व ज्ञान होता है उसी को श्रुतज्ञान कहा जाता है। श्रुतज्ञान होने के लिये शब्द-श्रवण आवश्यक है। शब्द श्रवण यह मतिज्ञान के अन्तर्गत है । कारण यह हैं कि वह श्रोत्र- इन्द्रिय का विषय है। जब-जब भी शब्द सुनाई देता है, तब ही उसके अर्थ का स्मरण हो जाता है। शब्द श्रवण रूप जो प्रवृत्ति है वह मतिज्ञान है। उसके बाद शब्द और अर्थ के वाच्य वाचक भाव के आधार पर होने वाले ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। इस पर से यह स्पष्ट है कि मतिज्ञान कारण है, और श्रुतज्ञान कार्य। मतिज्ञान के अभाव में श्रुतज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। यह सच है कि श्रुतज्ञान का अन्तरंग कारण श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम है मतिज्ञान तो उसका बहिरंग कारण कहलाता है। मतिज्ञान होने के बाद यदि श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं हुआ है तो श्रुतज्ञान होना कदापि संभव नहीं है यह जो विचारणा हुई है वह दार्शनिक विश्लेषण है ।
७७
For Private & Personal Use Only
आज्ञो भंजक मानवी, तजे नहीं अभिमान | जयन्तसेन दुःखी रहे, जीवन निष्फल जान ॥ www.jainelibrary.org.