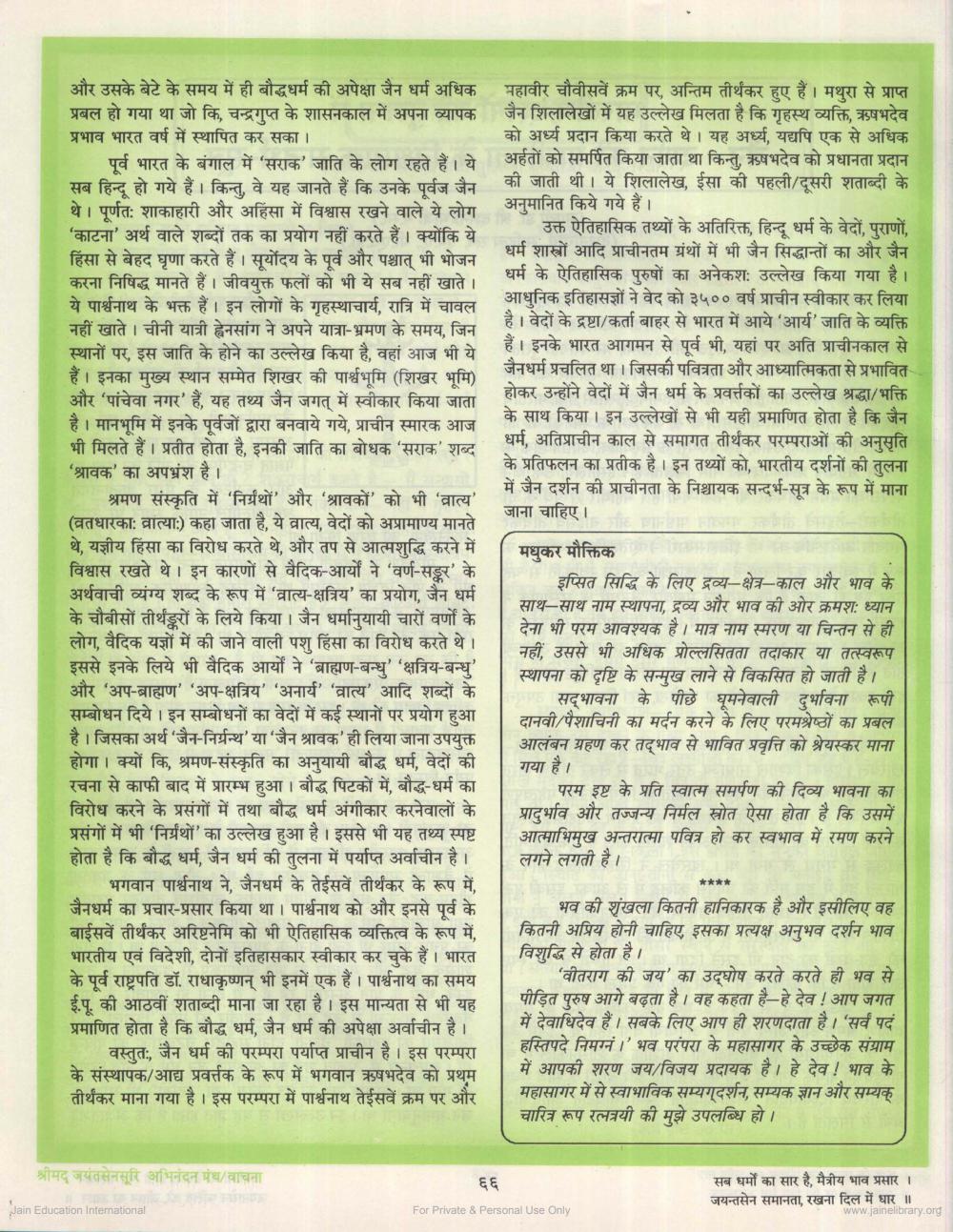________________
और उसके बेटे के समय में ही बौद्धधर्म की अपेक्षा जैन धर्म अधिक प्रबल हो गया था जो कि, चन्द्रगुप्त के शासनकाल में अपना व्यापक प्रभाव भारत वर्ष में स्थापित कर सका ।
पूर्व भारत के बंगाल में 'सराक' जाति के लोग रहते हैं। ये सब हिन्दू हो गये हैं । किन्तु वे यह जानते हैं कि उनके पूर्वज जैन थे । पूर्णत: शाकाहारी और अहिंसा में विश्वास रखने वाले ये लोग 'काटना' अर्थ वाले शब्दों तक का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि ये हिंसा से बेहद घृणा करते हैं। सूर्योदय के पूर्व और पश्चात् भी भोजन करना निषिद्ध मानते हैं । जीवयुक्त फलों को भी ये सब नहीं खाते। ये पार्श्वनाथ के भक्त हैं। इन लोगों के गृहस्थाचार्य, रात्रि में चावल नहीं खाते। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा - भ्रमण के समय, जिन स्थानों पर, इस जाति के होने का उल्लेख किया है, वहां आज भी ये हैं। इनका मुख्य स्थान सम्मेत शिखर की पार्श्वभूमि (शिखर भूमि) और 'पांचेवा नगर' हैं, यह तथ्य जैन जगत् में स्वीकार किया जाता है। मानभूमि में इनके पूर्वजों द्वारा बनवाये गये, प्राचीन स्मारक आज भी मिलते हैं प्रतीत होता है, इनकी जाति का बोधक 'सराक' शब्द 'श्रावक' का अपभ्रंश है।
श्रमण संस्कृति में 'निग्रंथों' और 'श्रावकों' को भी 'वात्य' (व्रतधारका: व्रात्याः) कहा जाता है, ये व्रात्य, वेदों को अप्रामाण्य मानते थे, यज्ञीय हिंसा का विरोध करते थे, और तप से आत्मशुद्धि करने में विश्वास रखते थे। इन कारणों से वैदिक आर्यों ने 'वर्ण-सङ्कर' के अर्थवाची व्यंग्य शब्द के रूप में 'व्रात्य क्षत्रिय' का प्रयोग, जैन धर्म के चौबीसों तीर्थङ्करों के लिये किया। जैन धर्मानुयायी चारों वर्णों के लोग, वैदिक यज्ञों में की जाने वाली पशु हिंसा का विरोध करते थे। इससे इनके लिये भी वैदिक आर्यों ने 'ब्राह्मण-बन्धु' 'क्षत्रिय-बन्धु' और 'अप-ब्राह्मण' 'अप-क्षत्रिय' 'अनार्य' 'व्रात्य' आदि शब्दों के सम्बोधन दिये। इन सम्बोधनों का वेदों में कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है। जिसका अर्थ 'जैन-निर्ग्रन्थ' या 'जैन श्रावक' ही लिया जाना उपयुक्त होगा। क्यों कि, श्रमण-संस्कृति का अनुयायी बौद्ध धर्म, वेदों की रचना से काफी बाद में प्रारम्भ हुआ। बौद्ध पिटकों में, बौद्ध-धर्म का विरोध करने के प्रसंगों में तथा बौद्ध धर्म अंगीकार करनेवालों के प्रसंगों में भी 'निग्रंथों' का उल्लेख हुआ है। इससे भी यह तथ्य स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म की तुलना में पर्याप्त अर्वाचीन है। भगवान पार्श्वनाथ ने जैनधर्म के तेईसवें तीर्थंकर के रूप में, जैनधर्म का प्रचार-प्रसार किया था पार्श्वनाथ को और इनसे पूर्व के बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में, भारतीय एवं विदेशी, दोनों इतिहासकार स्वीकार कर चुके हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन् भी इनमें एक हैं। पार्श्वनाथ का समय ई.पू. की आठवीं शताब्दी माना जा रहा है। इस मान्यता से भी यह प्रमाणित होता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म की अपेक्षा अर्वाचीन है। जैन धर्म की परम्परा पर्याप्त प्राचीन है। इस परम्परा वस्तुतः, के संस्थापक/ आद्य प्रवर्तक के रूप में भगवान ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना गया है। इस परम्परा में पार्श्वनाथ तेईसवें क्रम पर और
श्रीमद जयंवर अभिनंदन पंचा
Jain Education International
महावीर चौवीसवें क्रम पर, अन्तिम तीर्थंकर हुए हैं। मथुरा से प्राप्त जैन शिलालेखों में यह उल्लेख मिलता है कि गृहस्थ व्यक्ति, ऋषभदेव को अर्ध्य प्रदान किया करते थे। यह अर्ध्य, यद्यपि एक से अधिक अर्हतों को समर्पित किया जाता था किन्तु भदेव को प्रधानता प्रदान की जाती थी ये शिलालेख ईसा की पहली / दूसरी शताब्दी के अनुमानित किये गये हैं।
1
उक्त ऐतिहासिक तथ्यों के अतिरिक्त हिन्दू धर्म के वेदों, पुराणों, धर्म शास्त्रों आदि प्राचीनतम ग्रंथों में भी जैन सिद्धान्तों का और जैन धर्म के ऐतिहासिक पुरुषों का अनेकशः उल्लेख किया गया है। आधुनिक इतिहासज्ञों ने वेद को ३५०० वर्ष प्राचीन स्वीकार कर लिया है। वेदों के द्रष्टा / कर्ता बाहर से भारत में आये 'आर्य' जाति के व्यक्ति हैं। इनके भारत आगमन से पूर्व भी यहां पर अति प्राचीनकाल से जैनधर्म प्रचलित था। जिसकी पवित्रता और आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों में जैन धर्म के प्रवर्त्तकों का उल्लेख श्रद्धा भक्ति के साथ किया। इन उल्लेखों से भी यही प्रमाणित होता है कि जैन धर्म, अतिप्राचीन काल से समागत तीर्थंकर परम्पराओं की अनुसृति के प्रतिफलन का प्रतीक है। इन तथ्यों को, भारतीय दर्शनों की तुलना में जैन दर्शन की प्राचीनता के निश्चायक सन्दर्भ-सूत्र के रूप में माना जाना चाहिए।
मधुकर मौक्तिक
इप्सित सिद्धि के लिए द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव के साथ-साथ नाम स्थापना, द्रव्य और भाव की ओर क्रमश: ध्यान देना भी परम आवश्यक है। मात्र नाम स्मरण या चिन्तन से ही नहीं, उससे भी अधिक प्रोल्लसितता तदाकार या तत्स्वरूप स्थापना को दृष्टि के सन्मुख लाने से विकसित हो जाती है।
सद्भावना के पीछे घूमनेवाली दुर्भावना रूपी दानवी/ पैशाचिनी का मर्दन करने के लिए परमश्रेष्ठों का प्रबल आलंबन ग्रहण कर तद्द्भाव से भावित प्रवृत्ति को श्रेयस्कर माना गया है ।
परम इष्ट के प्रति स्वात्म समर्पण की दिव्य भावना का प्रादुर्भाव और तज्जन्य निर्मल स्रोत ऐसा होता है कि उसमें आत्माभिमुख अन्तरात्मा पवित्र हो कर स्वभाव में रमण करने लगने लगती है।
****
भव की शृंखला कितनी हानिकारक है और इसीलिए वह कितनी अप्रिय होनी चाहिए, इसका प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन भाव विशुद्धि से होता है।
'वीतराग की जय' का उद्घोष करते करते ही भव से पीड़ित पुरुष आगे बढ़ता है। वह कहता है-हे देव ! आप जगत में देवाधिदेव हैं। सबके लिए आप ही शरणदाता है। 'सर्वं पदं हस्तिपदे निमग्नं भव परंपरा के महासागर के उच्छेक संग्राम में आपकी शरण जय/विजय प्रदायक है। हे देव ! भाव के महासागर में से स्वाभाविक सम्यग्दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रयी की मुझे उपलब्धि हो ।
६६
For Private & Personal Use Only
सब धर्मों का सार है, मैत्रीय भाव प्रसार । जयन्तसेन समानता, रखना दिल में धार ॥ www.jainelibrary.org