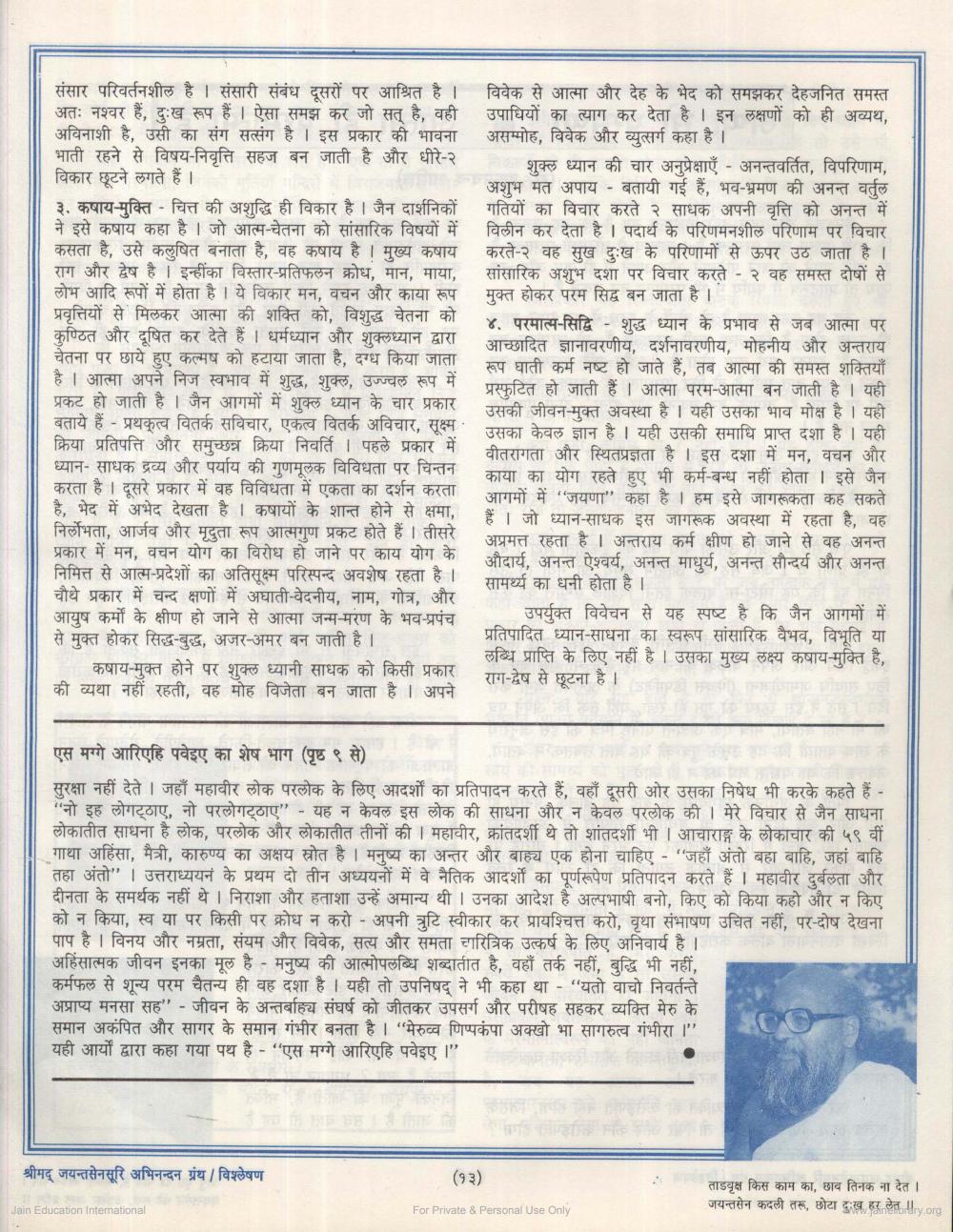________________
संसार परिवर्तनशील है । संसारी संबंध दूसरों पर आश्रित है। विवेक से आत्मा और देह के भेद को समझकर देहजनित समस्त अतः नश्वर हैं, दुःख रूप हैं । ऐसा समझ कर जो सत् है, वही उपाधियों का त्याग कर देता है । इन लक्षणों को ही अव्यथ, अविनाशी है, उसी का संग सत्संग है । इस प्रकार की भावना असम्मोह, विवेक और व्युत्सर्ग कहा है। भाती रहने से विषय-निवृत्ति सहज बन जाती है और धीरे-२
शुक्ल ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ - अनन्तवर्तित, विपरिणाम, विकार छूटने लगते हैं।
अशुभ मत अपाय - बतायी गई हैं, भव-भ्रमण की अनन्त वर्तुल ३. कषाय-मुक्ति - चित्त की अशुद्धि ही विकार है । जैन दार्शनिकों गतियों का विचार करते २ साधक अपनी वृत्ति को अनन्त में ने इसे कषाय कहा है । जो आत्म-चेतना को सांसारिक विषयों में विलीन कर देता है । पदार्थ के परिणमनशील परिणाम पर विचार कसता है, उसे कलुषित बनाता है, वह कषाय है । मुख्य कषाय करते-२ वह सुख दुःख के परिणामों से ऊपर उठ जाता है । राग और द्वेष है । इन्हींका विस्तार-प्रतिफलन क्रोध, मान, माया, सांसारिक अशुभ दशा पर विचार करते - २ वह समस्त दोषों से लोभ आदि रूपों में होता है । ये विकार मन, वचन और काया रूप मुक्त होकर परम सिद्व बन जाता है। प्रवृत्तियों से मिलकर आत्मा की शक्ति को, विशुद्ध चेतना को
४. परमात्म-सिद्वि - शुद्ध ध्यान के प्रभाव से जब आत्मा पर कुण्ठित और दूषित कर देते हैं | धर्मध्यान और शुक्लध्यान द्वारा
आच्छादित ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय चेतना पर छाये हुए कल्मष को हटाया जाता है, दग्ध किया जाता
रूप घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा की समस्त शक्तियाँ है । आत्मा अपने निज स्वभाव में शुद्ध, शुक्ल, उज्ज्वल रूप में
प्रस्फुटित हो जाती हैं | आत्मा परम-आत्मा बन जाती है । यही प्रकट हो जाती है । जैन आगमों में शुक्ल ध्यान के चार प्रकार
उसकी जीवन-मुक्त अवस्था है । यही उसका भाव मोक्ष है । यही बताये हैं - प्रथक्त्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म -
उसका केवल ज्ञान है । यही उसकी समाधि प्राप्त दशा है । यही क्रिया प्रतिपत्ति और समुच्छन्न क्रिया निवर्ति । पहले प्रकार में
वीतरागता और स्थितप्रज्ञता है । इस दशा में मन, वचन और ध्यान-साधक द्रव्य और पर्याय की गुणमूलक विविधता पर चिन्तन
काया का योग रहते हुए भी कर्म-बन्ध नहीं होता | इसे जैन करता है । दूसरे प्रकार में वह विविधता में एकता का दर्शन करता
आगमों में "जयणा" कहा है । हम इसे जागरूकता कह सकते है, भेद में अभेद देखता है । कषायों के शान्त होने से क्षमा,
हैं । जो ध्यान-साधक इस जागरूक अवस्था में रहता है, वह निर्लोभता, आर्जव और मृदुता रूप आत्मगुण प्रकट होते हैं । तीसरे
अप्रमत्त रहता है । अन्तराय कर्म क्षीण हो जाने से वह अनन्त प्रकार में मन, वचन योग का विरोध हो जाने पर काय योग के
औदार्य, अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त माधुर्य, अनन्त सौन्दर्य और अनन्त निमित्त से आत्म-प्रदेशों का अतिसूक्ष्म परिस्पन्द अवशेष रहता है ।
सामर्थ्य का धनी होता है । चौथे प्रकार में चन्द क्षणों में अघाती-वेदनीय, नाम, गोत्र, और आयुष कर्मों के क्षीण हो जाने से आत्मा जन्म-मरण के भव-प्रपंच
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन आगमों में से मुक्त होकर सिद्ध-बुद्ध, अजर-अमर बन जाती है।
प्रतिपादित ध्यान-साधना का स्वरूप सांसारिक वैभव, विभूति या
लब्धि प्राप्ति के लिए नहीं है । उसका मुख्य लक्ष्य कषाय-मुक्ति है, कषाय-मुक्त होने पर शुक्ल ध्यानी साधक को किसी प्रकार
राग-द्वेष से छूटना है। की व्यथा नहीं रहती, वह मोह विजेता बन जाता है । अपने
एस मग्गे आरिएहि पवेइए का शेष भाग (पृष्ठ ९ से) सुरक्षा नहीं देते । जहाँ महावीर लोक परलोक के लिए आदर्शों का प्रतिपादन करते हैं, वहाँ दूसरी ओर उसका निषेध भी करके कहते हैं - "नो इह लोगट्ठाए, नो परलोगट्ठाए" - यह न केवल इस लोक की साधना और न केवल परलोक की । मेरे विचार से जैन साधना लोकातीत साधना है लोक, परलोक और लोकातीत तीनों की । महावीर, क्रांतदर्शी थे तो शांतदर्शी भी । आचाराङ्ग के लोकाचार की ५९ वीं गाथा अहिंसा, मैत्री, कारुण्य का अक्षय स्रोत है। मनुष्य का अन्तर और बाय एक होना चाहिए - "जहाँ अंतो बहा बाहि, जहां बाहि तहा अंतो" | उत्तराध्ययनं के प्रथम दो तीन अध्ययनों में वे नैतिक आदर्शों का पूर्णरूपेण प्रतिपादन करते हैं । महावीर दुर्बलता और दीनता के समर्थक नहीं थे। निराशा और हताशा उन्हें अमान्य थी । उनका आदेश है अल्पभाषी बनो, किए को किया कहो और न किए को न किया, स्व या पर किसी पर क्रोध न करो - अपनी त्रुटि स्वीकार कर प्रायश्चित्त करो, वृथा संभाषण उचित नहीं, पर-दोष देखना पाप है | विनय और नम्रता, संयम और विवेक, सत्य और समता चारित्रिक उत्कर्ष के लिए अनिवार्य है। अहिंसात्मक जीवन इनका मूल है - मनुष्य की आत्मोपलब्धि शब्दातीत है, वहाँ तर्क नहीं, बुद्धि भी नहीं, कर्मफल से शून्य परम चैतन्य ही वह दशा है । यही तो उपनिषद् ने भी कहा था - "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" - जीवन के अन्तर्बाह्य संघर्ष को जीतकर उपसर्ग और परीषह सहकर व्यक्ति मेरु के समान अकंपित और सागर के समान गंभीर बनता है। "मेरुव्व णिप्पकंपा अक्खो भा सागरुत्व गंभीरा ।" यही आर्यों द्वारा कहा गया पथ है - "एस मग्गे आरिएहि पवेइए।"
श्रीमद् जयन्तसेनसूरि अभिनन्दन ग्रंथ / विश्लेषण
(१३)
ताडवृक्ष किस काम का, छाव तिनक ना देत । जयन्तसेन कदली तरू, छोटा दुःख हर लेत.ly.org
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only