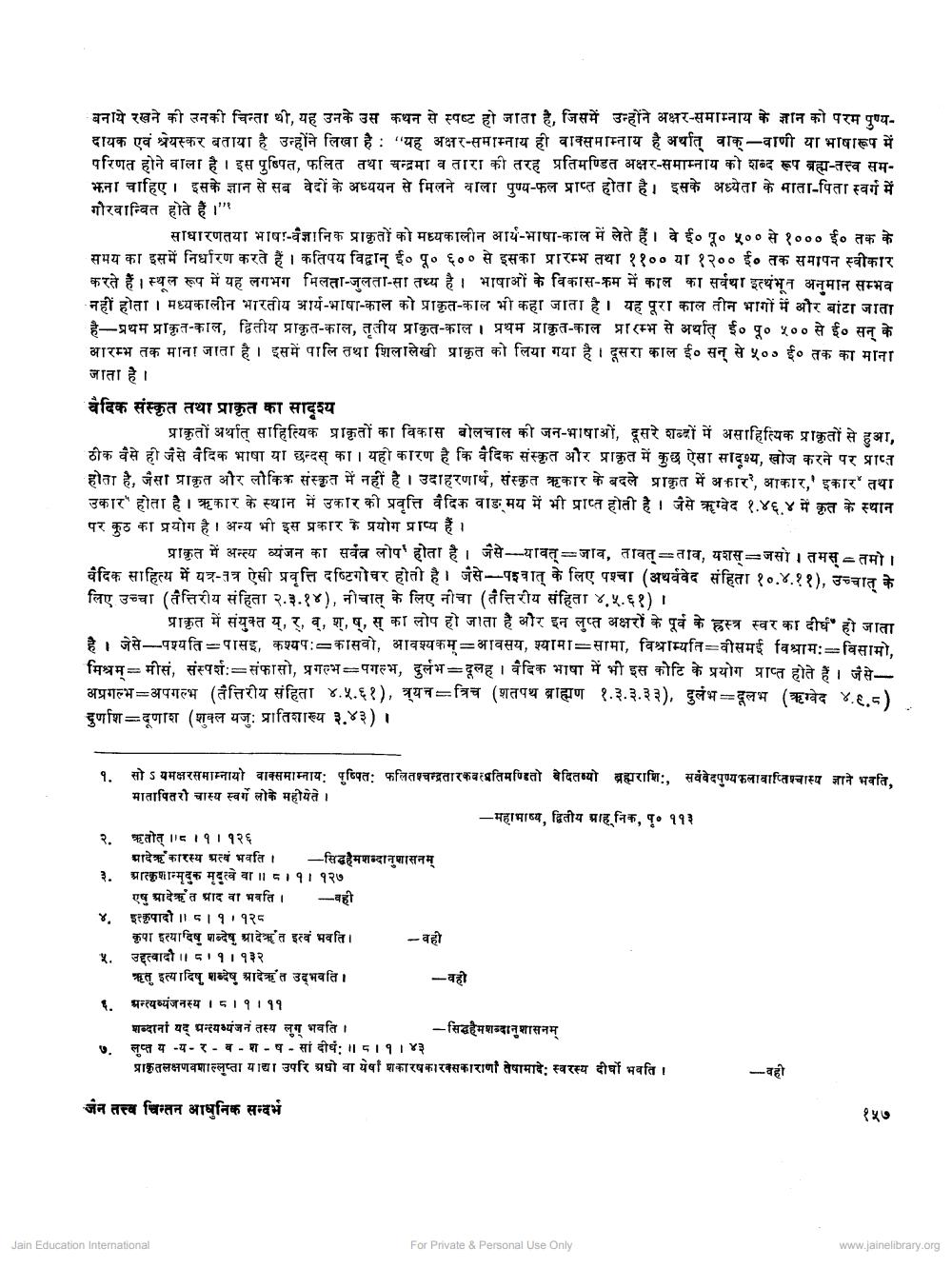________________
बनाये रखने की उनकी चिन्ता थी, यह उनके उस कथन से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें उन्होंने अक्षर-समाम्नाय के ज्ञान को परम पूण्यदायक एवं श्रेयस्कर बताया है उन्होंने लिखा है : “यह अक्षर-समाम्नाय ही वाक्समाम्नाय है अर्थात् वाक्-वाणी या भाषारूप में परिणत होने वाला है । इस पुष्पित, फलित तथा चन्द्रमा व तारा की तरह प्रतिमण्डित अक्षर-समाम्नाय को शब्द रूप ब्रह्म-तत्त्व समभना चाहिए। इसके ज्ञान से सब वेदों के अध्ययन से मिलने वाला पुण्य-फल प्राप्त होता है। इसके अध्येता के माता-पिता स्वर्ग में गौरवान्वित होते हैं।"
साधारणतया भाषा-वैज्ञानिक प्राकृतों को मध्यकालीन आर्य-भाषा-काल में लेते हैं। वे ई० पू० ५०० से १००० ई० तक के समय का इसमें निर्धारण करते हैं । कतिपय विद्वान् ई० पू० ६०० से इसका प्रारम्भ तथा ११०० या १२०० ई. तक समापन स्वीकार करते हैं । स्थूल रूप में यह लगभग मिलता-जुलता-सा तथ्य है। भाषाओं के विकास-क्रम में काल का सर्वथा इत्थंभूत अनुमान सम्भव नहीं होता । मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषा-काल को प्राकृत-काल भी कहा जाता है। यह पूरा काल तीन भागों में और बांटा जाता है-प्रथम प्राकृत-काल, द्वितीय प्राकृत-काल, तृतीय प्राकृत-काल । प्रथम प्राकृत-काल प्रारम्भ से अर्थात् ई० पू० ५०० से ई० सन के आरम्भ तक माना जाता है। इसमें पालि तथा शिलालेखी प्राकृत को लिया गया है। दूसरा काल ई० सन् से ५०० ई० तक का माना जाता है। वैदिक संस्कृत तथा प्राकृत का सादृश्य
प्राकृतों अर्थात साहित्यिक प्राकृतों का विकास बोलचाल की जन-भाषाओं, दूसरे शब्दों में असाहित्यिक प्राकृतों से हआ, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक भाषा या छन्दस् का । यही कारण है कि वैदिक संस्कृत और प्राकृत में कुछ ऐसा सादृश्य, खोज करने पर प्राप्त होता है, जैसा प्राकृत और लौकिक संस्कृत में नहीं है। उदाहरणार्थ, संस्कृत ऋकार के बदले प्राकृत में अकार, आकार, इकार तथा उकार" होता है। ऋकार के स्थान में उकार की प्रवृत्ति वैदिक वाङमय में भी प्राप्त होती है। जैसे ऋग्वेद १.४६.४ में कृत के स्थान पर कुठ का प्रयोग है। अन्य भी इस प्रकार के प्रयोग प्राप्य हैं।
प्राकृत में अन्त्य व्यंजन का सर्वत्र लोप होता है। जैसे-यावत् =जाव, तावत्=ताव, यशस्जसो । तमस् - तमो। वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र ऐसी प्रवृत्ति दष्टिगोचर होती है। जैसे--पश्चात् के लिए पश्चा (अथर्ववेद संहिता १०.४.११), उच्चात के लिए उच्चा (तैत्तिरीय संहिता २.३.१४), नीचात् के लिए नीचा (तैत्तिरीय संहिता ४.५.६१) ।
प्राकृत में संयुक्त य, र, व्, श, ष, स् का लोप हो जाता है और इन लुप्त अक्षरों के पूर्व के ह्रस्त्र स्वर का दीर्घ हो जाता है। जेसे-पश्यति =पासइ, कश्यपः= कासवो, आवश्यकम् = आवसय, श्यामा=सामा, विश्राम्यति वीसमई विश्रामः-विसामो, मिश्रम- मीसं, संस्पर्श:=संफासो, प्रगल्भ-पगल्भ, दुर्लभ = दूलह । वैदिक भाषा में भी इस कोटि के प्रयोग प्राप्त होते हैं। जैसेअप्रगल्भ अपगल्भ (तैत्तिरीय संहिता ४.५.६१), त्र्यच=त्रिच (शतपथ ब्राह्मण १.३.३.३३), दुर्लभ == दूलभ (ऋग्वेद ४.६.) . दुर्णाश= दूणाश (शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य ३.४३)।
१. सो 5 यमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशि:, सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिाचास्य ज्ञाने भवति, मातापितरो चास्य स्वर्ग लोके महीयते।
-महाभाष्य, द्वितीय प्राह निक, पृ० ११३ ऋतोत् ।।८।१ । १२६
मादेऋकारस्य प्रत्वं भवति । -सिद्धहमशम्दानुशासनम् ३. अात्कृशान्मृदुक मुदत्वे वा ॥८॥१।१२७
एषु आदेऋत पाद वा भवति। -वही ४. इत्कृपादो।। ८।१।१२८ ।।
कृपा इत्यादिषु शाब्देषु प्रादेत इत्वं भवति । -वही उद्दत्वादौ।। ८।१।१३२ ऋतु इत्यादिषु शब्देष आदेत उद्भवति।
-वही अन्त्यव्यंजनस्य । ८।१ । ११ शब्दानां यद् अन्त्यव्यंजनं तस्य लुग भवति ।
-सिद्धहैमशब्दानुशासनम् ७. लप्त य -य- र - व-श-ष- सां दीर्घः ।।८।१ । ४३
प्राकृतलक्षणवशाल्लुप्ता याद्या उपरि अधो वा येषां शकारषकारक्सकाराणां तेषामादे: स्वरस्य दीर्घो भवति ।
जैन तत्त्व चिन्तन आधुनिक सन्दर्भ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org