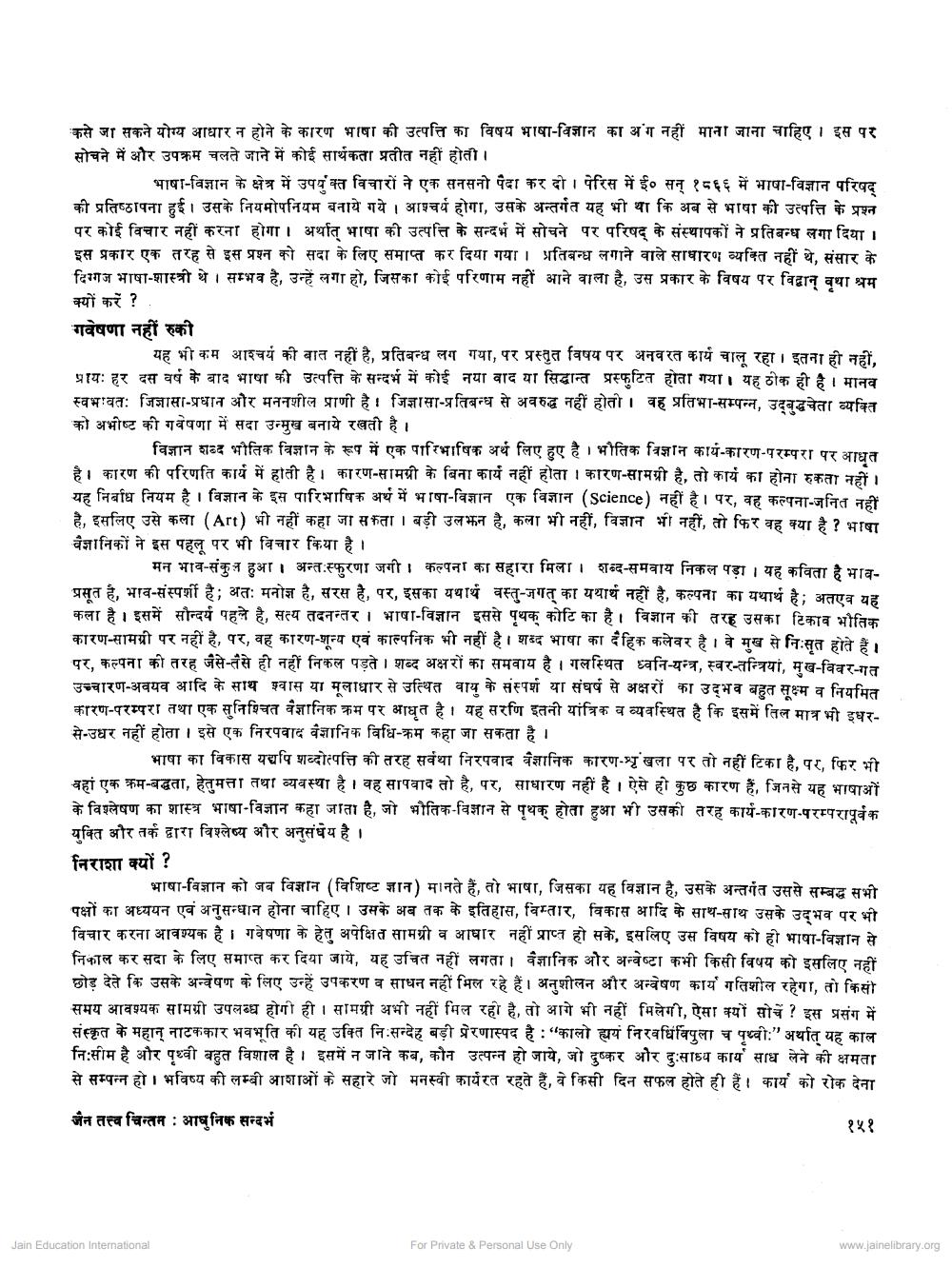________________
कसे जा सकने योग्य आधार न होने के कारण भाषा की उत्पत्ति का विषय भाषा-विज्ञान का अंग नहीं माना जाना चाहिए। इस पर सोचने में और उपक्रम चलते जाने में कोई सार्थकता प्रतीत नहीं होती।
भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में उपर्युक्त विचारों ने एक सनसनो पैदा कर दो। पेरिस में ई० सन् १८६६ में भाषा-विज्ञान परिषद की प्रतिष्ठापना हुई। उसके नियमोपनियम बनाये गये । आश्चर्य होगा, उसके अन्तर्गत यह भी था कि अब से भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न पर कोई विचार नहीं करना होगा। अर्थात् भाषा की उत्पत्ति के सन्दर्भ में सोचने पर परिषद् के संस्थापकों ने प्रतिबन्ध लगा दिया। इस प्रकार एक तरह से इस प्रश्न को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। प्रतिबन्ध लगाने वाले साधारण व्यक्ति नहीं थे, संसार के दिग्गज भाषा-शास्त्री थे। सम्भव है, उन्हें लगा हो, जिसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है, उस प्रकार के विषय पर विद्वान वृथा श्रम क्यों करें ? . गवेषणा नहीं रुकी
यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है, प्रतिबन्ध लग गया, पर प्रस्तुत विषय पर अनवरत कार्य चाल रहा। इतना ही नहीं, प्रायः हर दस वर्ष के बाद भाषा की उत्पत्ति के सन्दर्भ में कोई नया वाद या सिद्धान्त प्रस्फुटित होता गया। यह ठीक ही है। मानव स्वभावत: जिज्ञासा-प्रधान और मननशील प्राणी है। जिज्ञासा-प्रतिबन्ध से अवरुद्ध नहीं होती। वह प्रतिभा सम्पन्न, उदबद्धता व्यक्ति को अभीष्ट की गवेषणा में सदा उन्मुख बनाये रखती है।
विज्ञान शब्द भौतिक विज्ञान के रूप में एक पारिभाषिक अर्थ लिए हुए है । भौतिक विज्ञान कार्य-कारण-परम्परा पर आधत है। कारण की परिणति कार्य में होती है। कारण-सामग्री के बिना कार्य नहीं होता । कारण-सामग्री है, तो कार्य का होना रुकता नहीं। यह निर्बाध नियम है । विज्ञान के इस पारिभाषिक अर्थ में भाषा-विज्ञान एक विज्ञान (Science) नहीं है। पर, वह कल्पना-जनित नहीं है, इसलिए उसे कला (Art) भी नहीं कहा जा सकता । बड़ी उलझन है, कला भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, तो फिर वह क्या है ? भाषा वैज्ञानिकों ने इस पहलू पर भी विचार किया है।
मन भाव-संकुल हुआ। अन्तःस्फुरणा जगी। कल्पना का सहारा मिला। शब्द-समवाय निकल पड़ा। यह कविता है भावप्रस्त है, भाव-संस्पर्शी है; अत: मनोज्ञ है, सरस है, पर, इसका यथार्थ वस्तु-जगत् का यथार्थ नहीं है, कल्पना का यथार्थ है। अतएव यह कला है। इसमें सौन्दर्य पहले है, सत्य तदनन्तर । भाषा-विज्ञान इससे पृथक् कोटि का है। विज्ञान की तरह उसका टिकाव भौतिक कारण-सामग्री पर नहीं है, पर, वह कारण-शून्य एवं काल्पनिक भी नहीं है। शब्द भाषा का दैहिक कलेवर है। वे मुख से निःसत होते हैं। पर. कल्पना की तरह जैसे-तैसे ही नहीं निकल पड़ते । शब्द अक्षरों का समवाय है । गलस्थित ध्वनि-यन्त्र, स्वर-तन्त्रियां, मुख-विवर-गत उच्चारण-अवयव आदि के साथ श्वास या मूलाधार से उत्थित वायु के संस्पर्श या संघर्ष से अक्षरों का उद्भव बहुत सुक्ष्म व नियमित कारण-परम्परा तथा एक सुनिश्चित वैज्ञानिक क्रम पर आधृत है। यह सरणि इतनी यांत्रिक व व्यवस्थित है कि इसमें तिल मात्र भी इधरसे-उधर नहीं होता । इसे एक निरपवाद वैज्ञानिक विधि-क्रम कहा जा सकता है ।
भाषा का विकास यद्यपि शब्दोत्पत्ति की तरह सर्वथा निरपवाद वैज्ञानिक कारण-शृखला पर तो नहीं टिका है, पर, फिर भी वहां एक क्रम-बद्धता, हेतुमत्ता तथा व्यवस्था है। वह सापवाद तो है, पर, साधारण नहीं है। ऐसे ही कुछ कारण हैं, जिनसे यह भाषाओं के विश्लेषण का शास्त्र भाषा-विज्ञान कहा जाता है, जो भौतिक-विज्ञान से पृथक् होता हुआ भी उसकी तरह कार्य-कारण-परम्परापूर्वक युक्ति और तर्क द्वारा विश्लेष्य और अनुसंधय है । निराशा क्यों ?
भाषा-विज्ञान को जब विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) मानते हैं, तो भाषा, जिसका यह विज्ञान है, उसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध सभी पक्षों का अध्ययन एवं अनुसन्धान होना चाहिए। उसके अब तक के इतिहास, विस्तार, विकास आदि के साथ-साथ उसके उद्भव पर भी विचार करना आवश्यक है। गवेषणा के हेतु अपेक्षित सामग्री व आधार नहीं प्राप्त हो सके, इसलिए उस विषय को ही भाषा-विज्ञान से निकाल कर सदा के लिए समाप्त कर दिया जाये, यह उचित नहीं लगता। वैज्ञानिक और अन्वेष्टा कभी किसी विषय को इसलिए नहीं छोड़ देते कि उसके अन्वेषण के लिए उन्हें उपकरण व साधन नहीं मिल रहे हैं। अनुशीलन और अन्वेषण कार्य गतिशील रहेगा, तो किसी समय आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी ही। सामग्री अभी नहीं मिल रही है, तो आगे भी नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों सोचें ? इस प्रसंग में संस्कृत के महान् नाटककार भवभूति की यह उक्ति निःसन्देह बड़ी प्रेरणास्पद है : "कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी:" अर्थात् यह काल निःसीम है और पृथ्वी बहुत विशाल है। इसमें न जाने कब, कौन उत्पन्न हो जाये, जो दुष्कर और दुःसाध्य कार्य साध लेने की क्षमता से सम्पन्न हो। भविष्य की लम्बी आशाओं के सहारे जो मनस्वी कार्यरत रहते हैं, वे किसी दिन सफल होते ही हैं। कार्य को रोक देना
जैन तत्त्व चिन्तन : आधुनिक सन्दर्भ
१५१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org