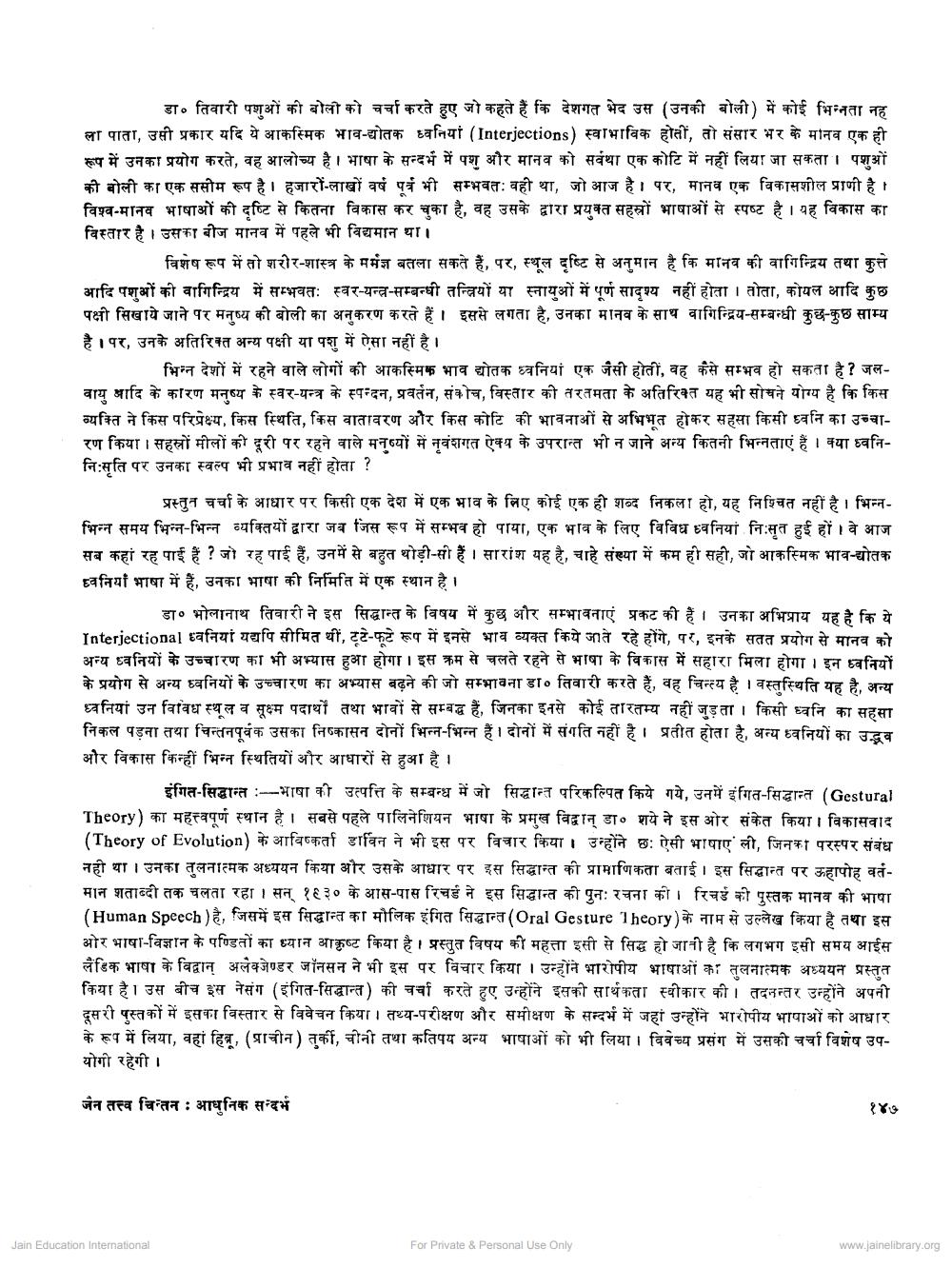________________
डा. तिवारी पशुओं की बोली को चर्चा करते हुए जो कहते हैं कि देशगत भेद उस (उनकी बोली) में कोई भिन्नता नह ला पाता, उसी प्रकार यदि ये आकस्मिक भाव-द्योतक ध्वनियां (Interjections) स्वाभाविक होतीं, तो संसार भर के मानव एक ही रूप में उनका प्रयोग करते, वह आलोच्य है। भाषा के सन्दर्भ में पशु और मानव को सर्वथा एक कोटि में नहीं लिया जा सकता। पशुओं की बोली का एक ससीम रूप है। हजारों-लाखों वर्ष पूर्व भी सम्भवतः वही था, जो आज है। पर, मानव एक विकासशील प्राणी है । विश्व-मानव भाषाओं की दृष्टि से कितना विकास कर चुका है, वह उसके द्वारा प्रयुक्त सहस्रों भाषाओं से स्पष्ट है । यह विकास का विस्तार है । उसका बीज मानव में पहले भी विद्यमान था।
विशेष रूप में तो शरीर-शास्त्र के मर्मज्ञ बतला सकते हैं, पर, स्थूल दृष्टि से अनुमान है कि मानव की वागिन्द्रिय तथा कुत्ते आदि पशुओं की वागिन्द्रिय में सम्भवतः स्वर-यन्त्र-सम्बन्धी तन्त्रियों या स्नायुओं में पूर्ण सादृश्य नहीं होता । तोता, कोयल आदि कुछ पक्षी सिखाये जाने पर मनुष्य की बोली का अनुकरण करते हैं। इससे लगता है, उनका मानव के साथ वागिन्द्रिय-सम्बन्धी कुछ-कुछ साम्य है। पर, उनके अतिरिक्त अन्य पक्षी या पशु में ऐसा नहीं है।
_ भिन्न देशों में रहने वाले लोगों की आकस्मिक भाव द्योतक ध्वनियां एक जैसी होती, वह कैसे सम्भव हो सकता है ? जलवायु आदि के कारण मनुष्य के स्वर-यन्त्र के स्पन्दन, प्रवर्तन, संकोच, विस्तार की तरतमता के अतिरिक्त यह भी सोचने योग्य है कि किस व्यक्ति ने किस परिप्रेक्ष्य, किस स्थिति, किस वातावरण और किस कोटि की भावनाओं से अभिभूत होकर सहसा किसी ध्वनि का उच्चारण किया। सहस्रों मीलों की दूरी पर रहने वाले मनुष्यों में नृवंशगत ऐक्य के उपरान्त भी न जाने अन्य कितनी भिन्नताएं हैं । क्या ध्वनिनि:सृति पर उनका स्वल्प भी प्रभाव नहीं होता ?
प्रस्तुत चर्चा के आधार पर किसी एक देश में एक भाव के लिए कोई एक ही शब्द निकला हो, यह निश्चित नहीं है । भिन्नभिन्न समय भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा जब जिस रूप में सम्भव हो पाया, एक भाव के लिए विविध ध्वनियां निःसृत हुई हों । वे आज सब कहां रह पाई हैं ? जो रह पाई हैं, उनमें से बहुत थोड़ी-सी हैं । सारांश यह है, चाहे संख्या में कम ही सही, जो आकस्मिक भाव-द्योतक ध्वनियाँ भाषा में हैं, उनका भाषा की निर्मिति में एक स्थान है।
डा० भोलानाथ तिवारी ने इस सिद्धान्त के विषय में कुछ और सम्भावनाएं प्रकट की हैं। उनका अभिप्राय यह है कि ये Interiectional ध्वनियां यद्यपि सीमित थीं, टूटे-फूटे रूप में इनसे भाव व्यक्त किये जाते रहे होंगे, पर, इनके सतत प्रयोग से मानव को अन्य ध्वनियों के उच्चारण का भी अभ्यास हुआ होगा। इस क्रम से चलते रहने से भाषा के विकास में सहारा मिला होगा। इन ध्वनियों के प्रयोग से अन्य ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास बढ़ने की जो सम्भावना डा० तिवारी करते हैं, वह चिन्त्य है । वस्तुस्थिति यह है, अन्य ध्वनियां उन विविध स्थल व सूक्ष्म पदार्थों तथा भावों से सम्बद्ध हैं, जिनका इनसे कोई तारतम्य नहीं जुड़ता। किसी ध्वनि का सहसा निकल पड़ना तथा चिन्तनपूर्वक उसका निष्कासन दोनों भिन्न-भिन्न हैं। दोनों में संगति नहीं है। प्रतीत होता है, अन्य ध्वनियों का उद्धव और विकास किन्हीं भिन्न स्थितियों और आधारों से हुआ है ।
इंगित-सिद्धान्त :-भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त परिकल्पित किये गये, उनमें इंगित-सिद्धान्त (Gestural Theory) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले पालिनेशियन भाषा के प्रमुख विद्वान् डा० शये ने इस ओर संकेत किया। विकासवाद (Theory of Evolution) के आविष्कर्ता डार्विन ने भी इस पर विचार किया। उन्होंने छ: ऐसी भाषाए ली, जिनका परस्पर संबंध नही था। उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके आधार पर इस सिद्धान्त की प्रामाणिकता बताई। इस सिद्धान्त पर ऊहापोह वर्तमान शताब्दी तक चलता रहा । सन् १९३० के आस-पास रिचर्ड ने इस सिद्धान्त की पुन: रचना की। रिचर्ड की पुस्तक मानव की भाषा (Human Speech)है, जिसमें इस सिद्धान्त का मौलिक इंगित सिद्धान्त (Oral Gesture Theory) के नाम से उल्लेख किया है तथा इस ओर भाषा-विज्ञान के पण्डितों का ध्यान आकृष्ट किया है। प्रस्तुत विषय की महत्ता इसी से सिद्ध हो जाती है कि लगभग इसी समय आईस लैंडिक भाषा के विद्वान् अलेक्जेण्डर जॉनसन ने भी इस पर विचार किया । उन्होंने भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उस बीच इस नेसंग (इंगित-सिद्धान्त) की चर्चा करते हुए उन्होंने इसकी सार्थकता स्वीकार की। तदनन्तर उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तकों में इसका विस्तार से विवेचन किया। तथ्य-परीक्षण और समीक्षण के सन्दर्भ में जहां उन्होंने भारोपीय भाषाओं को आधार के रूप में लिया, वहां हिब्रू, (प्राचीन ) तुर्की, चीनी तथा कतिपय अन्य भाषाओं को भी लिया। विवेच्य प्रसंग में उसकी चर्चा विशेष उपयोगी रहेगी।
जैन तत्त्व चिन्तन : आधुनिक सन्दर्भ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org